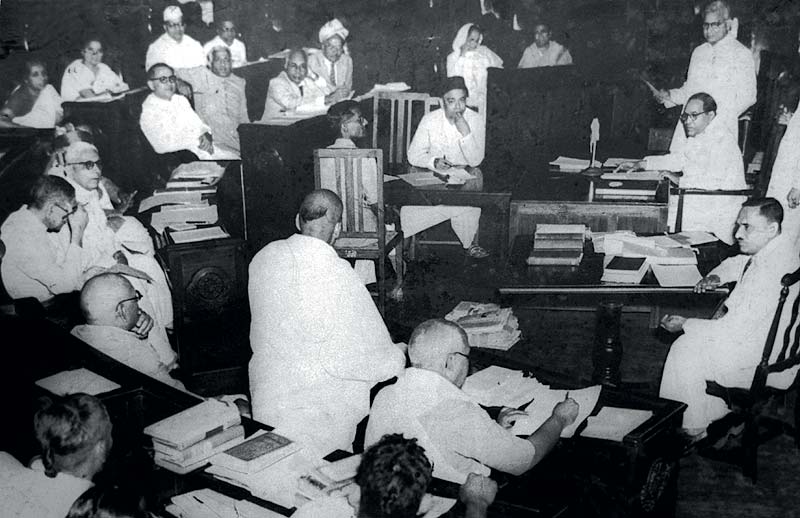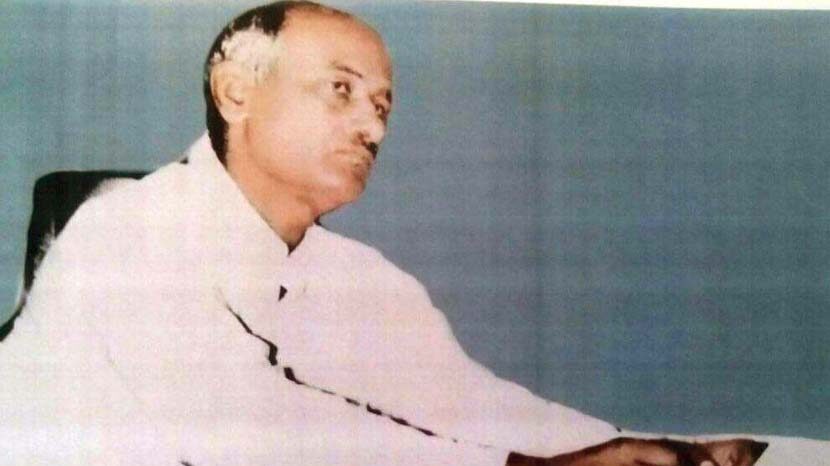“शैतान को गाली दी जा सकती है,
वह है ही बुरा,
उस पर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं,
और उसे अकारण दोषी ठहराया जा सकता है
जब इंसान स्वयं को दोषी ठहराना नहीं चाहता
तब वह अपने अपराधों को शैतान के सर मढ़ देता है”
–डेनियल डिफो की किताब ‘द हिस्ट्री ऑफ डेविल’ से
“जुहार दादा! देखिये आपको पहले बिशुनपुर [1] पहुंचना होगा। और इस वक्त आपको बिशुनपुर के लिए कोई सीधी बस नहीं मिलेगी क्योंकि वहां के लिए जो एकमात्र सीधी बस चलती है, वह छूट गई होगी। वही एक बस है जो रोजाना (बंदी अर्थात आर्थिक नाकाबंदी के दिनों को छोड़कर) लोहरदगा रेलवे स्टेशन से महुआडांड़ [2] के लिए चलती है। लेकिन बाक्साइट के ट्रक हमेशा चलते रहते हैं। इनमें से कोई भी ट्रक, जो गुरदारी या कुजाम खदानों की तरफ जा रहा हो, पकड़ लीजिए और बिशुनपुर प्रखंड विकास कार्यालय के पास उतर जाइये। मैं आपको वहीं मिल जाउंगा।”

यह बात जनवरी 2015 की एक ठंडी सुबह टेलीफोन पर अमर असुर ने मुझसे कही। मैंने ट्रक पर सवार होने से पहले हिंदी दैनिक प्रभात खबर की एक प्रति खरीदी। अखबार का पहला पन्ना हाल में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों से भरा था और इसमें कहा गया था कि भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को झारखंड में सरकार बनाने का ‘बहुमत’ मिला है। ट्रक के केबिन में ड्राइवर और खलासी के अलावा दो लोग और थे। केबिन की छत पर लगे स्पीकर से कानफोड़ू नागपुरिया गीत बज रहा था। आवाज इतनी तेज थी कि बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सब चुपचाप टकटकी लगाए सामने सड़क को देख रहे थे। मैंने अखबार पर सरसरी निगाह डालने का निर्णय लिया। ढाई घंटे की यात्रा के बाद मैं बिशुनपुर पहुंचा। मैंने खलासी को 50 रुपये का नोट दिया और उसने मुझे 30 रूपये वापस किये। मैं प्रखंड विकास कार्यालय के ठीक सामने ट्रक से उतरा।
मेरे उतरते ही फोटोकॉपी की एक दुकान के सामने इकट्ठा लोगों के बीच से चमकते काले बालों वाले एक 40-50 साल के व्यक्ति निकल कर बाहर आये। उन्होंने खादी की नीली सदरी (बिना बांह वाली जैकेट) पहन रखी थी। वे अमर असुर थे। हम लोगों ने आपस में अभिवादन किया। वे मुझे पास के ही एक छोटे से होटल में ले गए, जहां हम दोनों ने दो घंटे बिताए। इस दौरान चाय के कई दौर चले। यह असुर समुदाय के किसी व्यक्ति से मेरी पहली भेंट थी और वह भी काफी लंबी। विकास, आदिवासी समुदाय, टकराव और प्रतिरोध आदि के बारे में मेरे बहुत सारे पूर्वाग्रहों और मान्यताओं पर अमर असुर ने जोरदार तरीके से प्रश्न उठाए और उन्हें चुनौती दी। उनकी दो टूक और सहज भाषा उनके अनुभवों और आक्रोश को प्रतिबिंबित कर रही थी। इस बातचीत के दरमियान अमर असुर ने बिशुनपुर की धरती और यहां के निवासियों से मेरा एक बिल्कुल अलग अन्दाज में परिचय कराया। उन्होंने कहा, “यहां आपको दूर-दूर तक जमीन दिखेगी, लेकिन पूरा इलाका बंजर है। यहां जंगल ही जंगल हैं, लेकिन उनमें कोई फल नहीं ऊगता। यहां इंसानों की भरमार है लेकिन उनके पास कोई कौशल नहीं है”। अमर का यह जटिल और अन्तर्विरोधों से भरा विवरण, झारखण्ड के आदिवासी समूहों में से एक(असुर) के मेरे मानवविज्ञानी अध्ययन का प्रारंभिक बिन्दु बना।

इस आलेख का मुख्य उद्देश्य उदारीकरण के युग में असुर समुदाय की दुर्दशा से पाठकों को रुबरु कराना है। और इसमें दिए गए विस्तृत मानववैज्ञानिक विवरण का लक्ष्य राज्य और वंचितों के परस्पर संबंधों का बयान करना और यह बताना है कि कैसे हाशिए पर धकेल दिए गये तबके हिंसा का प्रतिरोध करते हैं और अंततः उससे हार जाते हैं। मैं “होमो सेकर” (लातिनी भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है पवित्र या शापित व्यक्ति, जिसकी जान कोई भी ले सकता है परन्तु जिसकी किसी धार्मिक अनुष्ठान में बलि नहीं दी जा सकती) की सैद्धांतिक अवधारणा के संदर्भ में कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। जैसे – असुरों को जीने और जीवनयापन करने के उनके अधिकार से क्यों वंचित किया जा रहा है? राज्य द्वारा उनके कल्याण के लिए उठाये गए क़दमों के बावजूद, असुरों का अस्तित्व संकट में क्यों पड़ गया है? उनके विरुद्ध हिंसा और उनकी असहायता के लिए कौन जिम्मेदार है?
असुर कौन हैं?
असुर भारत के उन 75 आदिवासी समूहों में से एक है, जिन्हें विशेष विलुप्तप्राय जनजाति(पीवीटीजी) घोषित किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजातियों की पहचान के लिए निम्न मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं: (1) आजीविका के लिए वनों पर निर्भरता (2) कृषि-पूर्व समाज (3) स्थिर या गिरती जनसंख्या (4) साक्षरता का निम्न स्तर व (5) निर्वाह अर्थव्यवस्था[3]। झारखण्ड में ऐसे आठ आदिवासी समूह हैं जो इन मानदण्डों को पूरा करते हैं और असुर उनमें से एक हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य में उनकी कुल जनसंख्या 22,000 है[4]। असुर मुख्य रूप से दक्षिणी छोटानागपुर की जंगलों से घिरी पहाड़ियों में रहते हैं। दक्षिणी छोटानागपुर पठार झारखण्ड के तीन जिलों – गुमला, लोहारदगा और लातेहार – में फैला हैं परन्तु इनमें से गुमला में विशेष पिछड़ी जनजातियों और विशेषकर असुर समुदाय की सबसे बड़ी आबादी है। यूनेस्को ने असुर भाषा को ‘निश्चित रूप से लुप्तप्राय’ भाषा बतौर सूचीबद्ध किया है। यह भाषा बोलने वाले अब केवल सात हजार लोग बचे हैं[5]। इन आदिवासियों के जीवन जीने के आदिम तरीके और उनके सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के चलते सन 2006 तक इन्हें ‘आदिम जनजाति समूह’ कहा जाता था। उसके बाद इस शब्द को अपमानजनक मानते हुए उसकी जगह “विशेष विलुप्तप्राय जनजाति” शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। विमर्श को परिवर्तित करने के इस सचेत प्रयास के बावजूद ‘आदिम जनजाति’ शब्द का इस्तेमाल सरकारी अधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा निरंतर किया जाता रहा है। सन 2014 में एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और अन्य विकास सूचकांकों के संबंध में प्रस्तुत एक रपट, विशेष पिछड़ी जनजातियों की कमज़ोर स्थिति की चर्चा भी करती है। उनके क्षेत्रों में राज्य और बाज़ार की क्रमिक शोषक घुसपैठ के कारण इन समूहों द्वारा जीवनयापन के उनके परंपरागत साधनों, निवास स्थान और प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकार को खो बैठने की रूपरेखा प्रस्तुत करते रपट कहती है। यह घुसपैठ असुर जैसे समुदायों की दुर्दशा के लिए ज़िम्मेदार कारकों में से एक महत्वपूर्ण करक है।

असुर आदिवासियों की तीन शाखायें हैं – बीर असुर, अगरिया और बिरजिया[6]। झारखण्ड में बिरजिया को असुरों से पृथक एक अति पिछड़ी जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है जबकि आगरिया को मध्यप्रदेश और छतीसगढ़ में अनसूचित जनजाति के तहत वर्गीकृत किया गया है। मेरे अध्ययन का केंद्र बीर असुर हैं –वे शक्तिशाली लोग हैं[7]। जो असुर के नाम से भी जाने जाते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के अलावा, वैदिक और उत्तर-वैदिक साहित्य में भी लोहे को गलाने की कला को असुर विद्या कहा गया है। इसके इस तथ्य की पुष्टि होती है कि लोहे को गलाना असुरों का परंपरागत पेशा रहा है। इसके अलावा, गैर-इमारती वन उत्पाद भी उनकी आजीविका के स्रोत थे। सन् 1868 में ब्रिटिश सरकार ने वन संबंधी कानून लागू किये, जिनके चलने असुरों की जंगलों तक पहुंच सीमित हो गयी और उनके परंपरागत पेशे पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। वे अब जंगल से लकड़ी नहीं ला सकते थे। इसी लकड़ी को जला कर वे कोयला बनाते थे जो लोहा गलाने के लिए ईंधन का काम करता था. नतीजे में उनके पूर्वजों को अपने भरण-पोषण के लिए वैकल्पिक साधनों की खोज करनी पड़ी। दक्षिणी छोटानागपुर के पठार में बाक्साइट प्रचुर मात्र में उपलब्ध है, परन्तु यहां की जलवायु और मिट्टी ऐसी है कि उसमें केवल कुछ फसलें ही उपजायी जा सकती हैं। सन 1980 के दशक से इस पठार में एक बहुराष्ट्रीय खनन कंपनी और अनेक निजी छोटी कम्पनियां बाक्साइट का खनन कर रही हैं। पिछले 30 वर्षों में असुरों ने अपनी जमीन के बहुत बड़े हिस्से को खनन कंपनियों को पट्टे पर दे दिया है। इसके बदले इन कंपनियों ने उन्हें उनकी ही ज़मीन पर मजदूर बना दिया और वह भी केवल इतने वेतन पर कि वे जिंदा भर रह सकें।

के.के. लेउवा ने असुरों पर अपने एक प्रामाणिक ग्रंथ में इस आदिवासी समूह की वंशावली का सूक्ष्म अध्ययन किया है। असुरों के उद्भव के विभिन्न सिद्धांतों और लिखित प्रमाणों की पड़ताल कर लेउवा इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि असुर, आर्यों से भिन्न थे और सिंधु घाटी में बसने वाले सबसे शुरुआती समूहों में से एक थे। चूंकि असुरों ने नवागत आर्यों की राजनीतिक संरचना को अपनाने से इंकार कर दिया, इसलिए पहले उन्हें राक्षस या दैत्य करार दिया गया और बाद में उत्तर (बिहार और झारखण्ड) की ओर खदेड़ दिया गया। लेउवा कुछ पुरातत्वविदों के इस तर्क से असहमति प्रकट करते हैं कि “असुर, रांची के मुण्डा आदिवासियों की एक शाखा हैं”। कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि खूंटी उपसंभाग में असुरों और मुण्डाओं के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें असुरों को खदेड़ दिया गया और वे इस पठार (नेतरहाट की पहाड़ियों) पर बस गए[8]। मुंडाओं के विपरीत, असुर हिंदू धर्म या ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में नहीं आये और उन सामाजिक और धार्मिक विश्वासों पर कायम रहे, जो उन्हें उनके पूर्वजों से मिले थे। कुछ अन्य नृवंशविज्ञानियों की तरह, लेउवा का तर्क है कि असुरों और मुण्डाओं की भाषा, उनकी शारीरिक व सामाजिक संरचना और राजनीति में अत्यधिक समानताओं के बावजूद दोनों पृथक समूह हैं। असुर, मुण्डाओं की शाखा नहीं हैं। जो भी हो, मेरे मानव-वैज्ञानिक अध्ययन का विषय न तो आर्यों और असुरों के परस्पर रिश्तों की तलाश है और ना ही यह पता लगाना है कि असुर, मुण्डा लोगों से पृथक हैं या नहीं। मेरे अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि किस कारण असुरों को 21वीं सदी में एक नई वैधानिक पहचान मिली और वे विशेष पिछड़ी जनजाति बन गए।
खनन मजदूर बनने को बाध्य असुर
मैं अपने अध्ययन के मैदानी कार्य के लिए असुरों के एक गांव साखुआपाथ[9] में रहा। यह इस पठारी (पाथ) क्षेत्र में स्थित उन कुछ छोटे गांवों में से एक है, जहाँ मुख्य रूप से केवल असुर ही रहते हैं। इस छोटे-से गांव में 110 से अधिक परिवार रहते हैं और यह इस समय यह, यहां के सबसे बड़े गांवों में से एक है। साखुआपाथ के लोगों की भोर बाक्साइट की खदानों में विस्फोटों की आवाज़ के साथ होती है और शाम ढले, खनन श्रमिक थके कदमों से हाथों में सब्बल लिए अपने गांव लौटते हैं। उनके साथ आतीं हैं धूल से ढकीं भीमकाय अर्थमूवर मशीनें। ये दोनों दृश्य मानो इस गांव को परिभाषित करते हैं। यह एक “औद्योगिक गांव” है। रहन-सहन देहाती है परन्तु भाषा शहरी। इन सबके बीच एक समुदाय अपने अस्तित्व पर मँडरा रहे खतरे को टालने के प्रयास में लगा है।

पंद्रह नवम्बर 2015 की शाम इस गांव के सभी 28 खनन मजदूरों को सुरेन्द्र असुर ने सूचित कि कल से खनन का काम नहीं होगा। दिन का दूसरा और आखिरी खाना खाने के बाद, लगभग सभी खनन मजदूर अखाड़े (बैठक स्थल) पर इकट्ठा हुए। उनमें कुछ ने खूब पी रखी थी। लकड़ियों के एक ढेर को सुलगाया गया और लोग आग के इर्द-गिर्द बैठ गए। बैठक शुरू हो गई। इस बैठक में कोई महिला नहीं थी। जल्दी में बुलाई गयी इस सभा का मुख्य एजेंडा यह था कि ठेकेदार मिश्राजी ने सुरेन्द्र को यह निर्देश क्यों दिया कि कल से खनन नहीं होगा। सुरेन्द्र असुर इस गांव के उन चंद नौजवानों में से हैं, जिन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की है। इस समय वे खनन ठेकादार के मुंशी के रूप में काम करते हैं।
सुरेन्द्र के वहां आने से पहले ही अखाड़े में उपस्थित लोगों में विचार-विमर्श शुरू हो गया। अधेड़ जोगेश्वर असुर ने बातचीत शुरू करते हुए कहा कि, “पिछले साल खनन का काम जनवरी के अंत तक चला था और किसी तरह हम लोगों ने दो-तीन महीने काट लिये। लेकिन इस साल क्या करेगें?” जोगेश्वर की चिंता से सहमति व्यक्त करते हुए परमेश्वर असुर ने निर्णायक स्वर में कहा, “हम ठेकेदार से कहेंगे कि भले ही खनन का काम न हो लेकिन हमें पैसे मिलने चाहिए”। तभी सुरेन्द्र अखाड़े में आया और आग के पास बैठ गया। उसने अपने हाथ फैला कर आग तापी। बिना देरी के जोगेश्वर असुर ने सुरेन्द्र से पूछा, “ठेकेदार ने तुमसे क्या कहा? कल से खंता (खान) में कोई काम क्यों नहीं होगा?” आग में कुछ और लकड़ियां डालने के बाद सुरेन्द्र ने धीमे स्वर में कहा, “कंपनी ने कोटा 22 ट्रकों से घटा कर 8 ट्रक कर दिया है और मिश्राजी ने कहा है कि इससे उन्हें घाटा होगा। एक आदमी, जो सुरेन्द्र के बगल में बैठा था, आगबबूला हो बोला, “हमारे बच्चों का पेट कौन भरेगा?” थोड़ी देर के लिए सभा शांत हो गई। फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए सुरेन्द्र ने कहा, “ऐसा केवल मिश्राजी के साथ नहीं हुआ है दूसरे ठेकेदारों का कोटा भी कम कर दिया गया है।” जोगेश्वर असुर ने सुरेन्द्र को टोकते हुए कहा, “मैं सब कुछ समझता हूं। यह और कुछ नहीं बल्कि कंपनी और ठेकेदार की चाल है ताकि उन्हें हमारी मजदूरी न देनी पड़े। इन दिनों बाक्साइट जंगलों से ज्यादा निकाला जा रहा है, खदानों से कम। ठेकेदार को गांव में बुलाओ, हम उससे बात करेंगे”। अब कहने-सुनने लिए कुछ बचा नहीं था। कुछ लोग अपने घर की ओर चले गए, जबकि कुछ अन्य छोटे-छोटे घेरे बना कर बातें करते रहे। इस मुद्दे पर मजदूरों से बात करने ठेकेदार एक सप्ताह बाद भी गांव नहीं आया। ठेकेदार के निर्देश पर जमीन की खुदाई करने वाली भारी-भरकम मशीनें, ड्रिलें और मिट्टी फेंकने वाले वाहन, खनन बंद होने के दो दिन के भीतर ही गांव से कहीं और भेज दिए गए।
मानववैज्ञानिक अध्ययन के लिए उस पूरे मसले के संदर्भों को समझना ज़रूरी हैं जिसके चलते ऐसे हालात पैदा हुए। इस पठार की तीन पंचायतों की 1500 एकड़ से अधिक जमीन हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को खनन के लिए पट्टे पर दी गयी है। कंपनी ने इस क्षेत्र में स्थित विभिन्न खदानों से बाक्साइट निकालने के लिए 12 छोटी कंपनियों से समझौते किये हैं। वर्तमान में बाक्साइट खनन की दो पद्धतियां हैं – कंपनी द्वारा सीधे और ठेकेदार द्वारा। खनन का जो काम सीधे कंपनी द्वारा किया जाता है, उसकी देखरेख कंपनी करती है जबकि ठेकेदारों को उनके द्वारा निकाले गए बाक्साइट की मात्रा के अनुसार भुगतान किया जाता है। कंपनी की तुलना में ठेकेदारों द्वारा ज्यादा बाक्साइट निकाला जाता है[10]। इस पठार का खनन-क्षेत्र तीन परिचालन इकाइयों में बंटा हुआ है[11]। साखुआपाथ गांव की खदानें, गुरदारी खनन प्रभाग के अंतर्गत आती हैं। गुरदारी प्रभाग को प्रति वर्ष 3.20 लाख टन बाक्साइट निकालने की पर्यावरणीय स्वीकृति मिली है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ (1 अप्रैल) से खनन शुरू होता है परन्तु इस तरह की परियोजनों में अनिश्चितता बनी रहती है। एक ओर खनन के लिए बड़ी-बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है तो दूसरी तरफ बहुत सारे छोटे ठेकेदार अवैध खनन के माध्य्म से पैसा बनाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, हर बड़े ठेकेदार के साथ कम से कम पांच छोटे ठेकेदार जुड़े हुए हैं और ये एक दिन में जितना संभव होता है, उतने ट्रक बाक्साइट निकालते हैं।

खनन में भारी मशीनों और ठेकेदारों के साथ छोटे ठेकेदारों की भूमिका का विश्लेषण करने से हमें यह पता चलता है कि एक वर्ग के ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का प्रयास दूसरे वर्ग को किस प्रकार संकट में डाल देता है। भारी मशीनों का इस्तेमाल कर कंपनी और ठेकेदार की कोशिश यह रहती है कि वे कम से कम समय में अधिक से अधिक बाक्साइट निकालें, जिससे उनकी उत्पादन लागत कम हो। परन्तु बड़े ठेकेदार यह नहीं चाहते कि उन्हें जो खदान आवंटित की गई है वह खाली हो जाये इसलिए वे इस बात की कोशिश करते हैं वे उन क्षेत्रों से निकाला गया बाक्साइट अधिक से अधिक मात्रा में खरीद लें जो या तो वन विभाग के अधीन है या जो पट्टे वाले क्षेत्र से बाहर हैं। इन छोटे ठेकेदारों में कुछ स्थानीय शिक्षित आदिवासी नौजवान भी शामिल हैं जो अन्य आदिवासी नौजवानों की तरह, गांव छोड़कर किसी दूसरे राज्य में रोटी कमाने जाने की जगह यहीं गांव में रहकर पैसा कमा रहे हैं। यहां से बाहर भेजे जाने वाले बाक्साइट का 40 प्रतिशत से अधिक छोटे और बड़े ठेकेदार निकलते हैं[12]। त्योहारों के मौसम में इन छोटे ठेकेदारों का बाक्साइट उत्पादन में योगदान अचानक बढ़ जाता है। इस सब से बाक्साइट उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया जाता है।
रोजगार दिलाने वाली अथवा उजाड़ने वाली एजेंसियां?
पर्यावरण पर खनन का विध्वंसक दुष्प्रभाव, हमेशा से कार्यकर्ताओं और अकादमिक जगत में चर्चा का विषय रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि खनन का पारिस्थितिकी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है लेकिन स्थानीय समुदायों के जीवन और आजीविका पर पड़ने वाला तात्कालिक प्रभाव भी उतनी ही गंभीर चिन्ता का विषय है। यह पता लगाने के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि 1991 के बाद से खनन के कारण यहां से कितने लोग विस्थापित हुए[13] परन्तु यहां यह याद दिलाना समीचीन होगा कि 1991 ही वह वर्ष था जब व्यापक आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, जिसने भारत के द्वार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोल दिए। यहां की विशाल जनसँख्या के जीवन जीने के तरीके और आजीविका के पारंपरिक साधनों की कीमत पर इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जमीनों और प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण सौंप दिया गया। वर्तमान विकास मॉडल के समर्थन में यह तर्क दिया जाता है कि दूरदराज के खनिज-बहुल इलाकों में खनन से स्थानीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा और पलायन पर नियंत्रण लगेगा। परन्तु यह मानववैज्ञानिक अध्ययन इस धारणा का खंडन करता है।
नवंबर 2015 की एक दोपहर जब मैं साखुआपाथ के नजदीक के एक खनन स्थल से लौट रहा था तब मेरी भेंट एक महिला से हुई। इस आदिवासी महिला को देख कर उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था क्योंकि यहां बहुत कम आयु में महिलाओं की शादी हो जाती है। मैंने यह अंदाजा लगाया कि रंगीन साड़ी पहने वह महिला अपने जीवन के चौथे दशक में रही होगी। वह अखबार के खोखे में मूंगफली बेच रही थी। मैंने सुबह खाना खाया था फिर भी मुझे भूख लग आयी थी। मैने एक खोखा, जिसका दाम पांच रुपया था, खरीदने के बाद उस महिला से पूछा, “क्या आप यहां रोज आती हैं?” उसने कहा, “यदि मैं यहां न आऊँ तो क्या करूं? इस पाथ में हमारे (महिला) लिए कोई काम ही नहीं है”। वह कैरीपाथ की थी, जो साखुआपाथ के बगल का गांव और जहां मुख्यतः असुर रहते हैं। उस महिला से बातचीत के बाद मेरा ध्यान खदानों में काम करने वाली श्रमशक्ति के लैंगिक संयोजन की ओर गया। यह जान कर किसी को भी आश्चर्य होगा कि खदानों में काम करने वालों में एक भी महिला नहीं थी – न तो खदान स्थलों में और न ही कार्यालयों में। इस प्रकार, पठार की ये खदानें विशुद्ध मरदाना कार्यस्थल हैं। खदानों के संदर्भ में प्राप्त इस नई अन्तर्दृष्टि ने मेरे सामने प्रश्नों का अंबार लगा दिया और मेरे भीतर एक नई जिज्ञासा ने जन्म लिया।
इन पठारों से महानगरों में लड़कियों की तस्करी आम है। हर वर्ष सैकड़ों लड़कियाँ यहां से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसे शहरी क्षेत्रों में ले जाई जाती हैं। पिछले कुछ समय में कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं और कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और मीडिया के एक तबके ने इसे तवज्जो दी। झारखण्ड में लड़कियों की तस्करी पर मीड़िया के फोकस और नागरिक समाज संगठनों के बढ़ते दबाव के चलते झारखण्ड सरकार ने इस समस्या के समाधान और लड़कियों की सुरक्षा के लिए कुछ नीतियां बनायी। इनमें शामिल हैं मानव तस्करों के गिरोहों पर नियंत्रण के लिए एक विशेष दल का गठन, लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रम इत्यादि। ये नीतियां मानव तस्करी को रोकने में कितनी कारगार हुईं हैं, यह कहना मुश्किल है। परन्तु नीचे वर्णित एक घटना से राज्य के पिछड़े इलाकों से लड़कियों की तस्करी रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए क़दमों के काफी हद तक निष्प्रभावी होने का पता चलता है।
दिसंबर 2015 की एक ठिठुरती रात को, हमेशा की तरह, गांव के कुछ लोग भाडवा असुर के घर के सामने जुटे। कुछ लोगों ने पतले कम्बल ओढ़ रखे थे तो अन्यों ने रंगीन चादरें लपेटी हुईं थीं। ये लोग तरह-तरह के विषयों, जिनमें रोजी-रोटी, गांव और कभी-कभी सरकार शामिल थे, पर चर्चा कर रहे थे। मैं रात का खाना खाने से पहले, इस गपशप में भाग लेना पसंद करता था। यह नियमित चर्चा, अखबार के विकल्प का काम करती थी क्योंकि इस इलाके में न तो मीडिया की पहुंच है और ना ही यहां के लोगों की ‘आधुनिक मीडिया’ (रेडियो को छोड़कर) तक। इस तरह की गपशप में शामिल होकर आसपास के इलाकों के घटनाक्रम से परिचित हुआ जा सकता है। तिपुन असुर ने बताया कि कल सुमन, स्कूल जाने वाली तीन लड़कियों के साथ भाग गई। वे तीनों ही अवस्यक थीं। भाडवा असुर ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, “सुषमा दिल्ली में रहती है और हर साल एक-दो महीने के लिए यहां आती है। वापस जाते समय वो दो या तीन लड़कियों को अपने साथ ले जाती है। यह उसका धंधा है। वह इन लड़कियों को कोठियों(बड़े घर) में बेच कर हर लड़की पर 25 से 30 हजार रुपया कमा लेती है”। भाडवा असुर के बेटे विल्सन भड़क उठते हैं और कहते हैं कि “इसमें केवल माता-पिता का दोष है। वे गैर-जिम्मेदार हैं। हमेशा पी कर टुन्न रहते हैं और अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते”। तिपुन कहते हैं कि माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे दिल्ली जायें और वहां से उनके लिए पैसा भेजें। महावीर असुर, जो बैठक में बाद में आए, की इस मामले में राय भिन्न थी। उन्होंने कहा कि “ये बच्चे गांवों में रहना नहीं चाहते। वे खेतों में मेहनत करने की जगह शहरी जीवन का मजा लेना चाहते हैं। मोबाइल फोन रखना चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं।’’ महावीर असुर की चार बेटियां और एक बेटा है। लड़कियों की तस्करी के सवाल पर सबकी राय सुनने का बाद मैं बैचैन हो उठा क्योंकि कोई भी इन लड़कियों को वापस लाने की बात नहीं कर रहा था। एक घंटे की बैठक जब संपन्न होने जा रही थी तब मैंने तिपुन असुर से पूछा, “क्या हम गायब हो गयी लड़कियों के बारे में पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करायेंगे या वे कहां हैं, यह पता लगाने की कोशिश नहीं करेंगे?” भाडवा असुर ने गंभीर आवाज में इसका जवाब दिया। “उन्हें खोजने की कोशिश करना बेकार है। अब तक वे झारखण्ड की सीमा पार कर चुकी होंगी और उनके माता-पिता सहित, कोई भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर परेशानी मोल नहीं लेना चाहेगा। वैसे भी, एक या दो वर्ष बाद ये लड़कियां अपने गांव वापस आ जायेंगी।” महावीर असुर का यह कथन इस बैठक का निष्कर्षात्मक वक्तव्य था। उसके बाद सब लोग अपने-अपने घर चले गए। मेरे लिए यह घटना पठार में महिलायें और लड़कियों की हालत बताने के लिए पर्याप्त थी।
इसके बाद मैंने यह महसूस किया कि यहां पर कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो पांचवी या छठी कक्षा में पढ़ती हो। हालांकि मैंने यह पता नहीं लगाया कि गांव में स्थित मिडिल स्कूल में कितनी लड़कियों का नाम इन दो कक्षाओं में दर्ज है। हैरानी की बात यह है कि इस स्कूल में केवल एक अस्थायी अध्यापक (अप्रशिक्षित, स्थाई अध्यापक के सहयोग के लिए रखा गया) है, जिसे कक्षा एक से लेकर छह तक के 90 विद्यार्थियों को पढ़ाना होता है और जिनमें 0-3 वर्ष आयु-वर्ग के बच्चे शामिल हैं। लगभग 40-45 वर्षीय विधवा सुमित्रा असुर, शिशुओं की देखभाल में तिपुन असुर का सहयोग करती है। तिपुन असुर ही उस स्कूल के अस्थाई अध्यापक हैं। सुमित्रा की नियुक्ति 600 रुपये प्रति माह वेतन पर हिंडाल्को ने की है। उन्हें प्रतिदिन चार घंटे स्कूल में देने होते हैं। यहां सरकारी सहायता प्राप्त एक हाईस्कूल है, जिसका प्रबंधन और संचालन रोमन कैथोलिक चर्च करता है। इस पाथ में केवल यही लड़कों और लड़कियों का एकमात्र हाईस्कूल है।

यह केवल साखुआपाथ की स्थिति नहीं है। इस पूरे पठार में बहुत सारी लड़कियां और लड़के ऐसे हैं जिन्होंने या स्कूल छोड़ दिया (ज्यादातर मामलों में) या हाईस्कूल तक ही पढ़ाई कर पाए (कुछ ही इंटरमीडिएट के स्तर तक पहुंचे)। ये बेरोजगार नौजवान ही मानव तस्करों और पूरे झारखण्ड में सक्रिय नौकरी दिलाने वाली एजेंसियों (प्लेसमेंट एजेंसियां) के पहले शिकार होते हैं। हम यह बता चुके हैं कि कैसे इस क्षेत्र में आजीविका के साधन तेजी से सिकुड़ते जा रहे हैं, खास कर खनन क्षेत्र में। खेती योग्य जमीन की उर्वरता के क्षरण और जल संसाधनों पर खनन के दुष्प्रभाव के चलते कृषि उत्पादन में गिरावट आई है। इस क्षेत्र में गहराते आर्थिक संकट के चलते यहां के नौजवानों के पास आजीविका की खोज में शहरों की ओर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में ईंट के भट्ठों और खेतों में मजदूरी करते हैं। इसके अलावा, तेजी से फलते-फूलते भवन निर्माण क्षेत्र में ये सस्ते मजदूर के रूप में खटते हैं। शहरों में तेजी से उभरते मध्यम वर्ग ने भी घरेलू काम के लिए नौकरानियों और नौकरों की भरी मांग उत्पन्न की है।
एक असुर लड़की का मानवता को शर्मसार कर देने वाला अन्त
राजमुनी असुर उन महिलाओं में से एक हैं जो सात वर्षों से अधिक समय तक दिल्ली में काम कती थीं। अब वे गांव में बस गई हैं। उनकी शादी हो गई है और उनके तीन बच्चे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वे फिर से दिल्ली जायेंगी तो उन्होंने तपाक से कहा, “नहीं, कभी नहीं। मैं अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए गांव में कुछ भी कर सकती हूं लेकिन अब मैं फिर कभी दिल्ली नहीं जाउंगी”। शहरी जीवन के प्रति वितृष्णा, उनकी भाव-भंगिमा में साफ झलक रही थी। कई मुलाकातों में उन्होंने दिल्ली में करीब सात वर्षों तक घरेलू नौकरानी के तौर पर काम करने के अपने दर्दनाक अनुभवों को मुझसे सांझा किया। उन्होंने बताया कि उनके गांव के पास की सरदारिन (तस्कर एजेंट) 1998 में उन्हें दिल्ली ले गई और वहां उन्हें एक छोटे से कमरे में एक महीने से अधिक समय तक रखा। यह वह जगह थी जहां से बच्चे खरीदे-बेचे जाते थे। वह सूअर के बाड़े जैसी थी जहां एक दर्जन से ज्यादा बच्चे एक ही कमरे में थे और उन्हें कमरे से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। रात को इन बच्चों को उनकी काम की जगह पर “बंद-गाड़ी” (टैक्सी) में भेजा जाता था, ताकि वे उस जगह को न पहचान सकें जहां उन्हें रखा गया था। जब राजमुनि को एक कोठी में काम पर लगाया गया, तब वे मात्र 15 वर्ष की थीं। पहले साल उन्हें काम के बदले खाना और कुछ कपड़ों के अलावा कुछ नहीं मिला, अलबत्ता सरदारिन ने ‘मैडम जी’, जिनके घर वे काम करती थीं, से 15 हजार रूपया लिए। वे खाना बनाने से लेकर घर के सारे काम करती थीं। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच के समय को छोड़कर उन्हें आराम नसीब नहीं था। वे इस बात पर जोर देती हैं कि उनके साथ ‘मैडम जी’ का बर्ताव बहुत बुरा, जानवरों जैसा, था। इसका कारण यह था कि वे उनके जीने के तरीके से परिचित नहीं थीं। तीन वर्ष से अधिक समय तक उनका अपने परिवार या झारखण्ड के किसी भी व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं था। कई बार विनती करने पर उन्हें अपने परिवार के पास झारखण्ड जाने की इजाजत इस शर्त पर दी गई कि वे दिल्ली वापस लौट आयेंगी। फिर, भर्राती हुयी आवाज़ में उन्होंने अपने ही गांव की एक अन्य असुर लड़की सुनीता की दुख भरी कहानी बयान की। “मैं तो फिर भी भाग्यशाली थी कि मुझे कोठी में काम करने को मिला। सुनीता को किसी के हाथों बेच दिया गया। उसे यौन शोषण के लिए खरीदा गया। दो साल तक उसे एक कमरे में रखा गया। उसे पहनने के लिए इतने छोटे कपड़े दिए जाते थे जिसे पहनकर आप लोगों के सामने नहीं जा सकते। जिस आदमी ने उसे खरीदा था, वह रोज उसका शारीरिक शोषण करता था। एक घर में दो वर्ष तक बंद रहने के बाद, वह वहां से किसी तरह भागने में सफल हुई और उसने पुलिस को अपनी कहानी सुनायी। पुलिस की मदद से सुनीता अपने गाव वापस आई। लेकिन दो सालों की बेइंतहा प्रताड़ना और शारीरिक शोषण के चलते वह अपना दिमागी सन्तुलन खो बैठी और अर्द्धविक्षिप्त हो गई। गांव लौटने के दो महीने बाद उसने अपने ऊपर एक गैलन मिट्टी का तेल उड़ेल लिया और खुद को आग के हवाले कर दिया। सुनीता मर गई!”
शहर आने वाले असुर नौजवानों की हालत
राजमुनि और सुनीता जैसी लड़कियों की तरह, पाथ छोड़कर आजीविका की तलाश में दूसरी जगहों पर जाने वाले यहां के लड़कों के अनुभव भी उतने ही कटु हैं। खदानों में रोज़गार के अवसर सिकुड़ने से मजबूर होकर यहां से पलायन करने वाले नौजवानों में से एक हैं 23 वर्षीय सुधीर असुर। सुधीर के पिता की 2011 में तपेदिक से मृत्यु हो गई थी। उनके पिता हिंडाल्को में खनन श्रमिक थे और वे ही परिवार का पेट पालते थे। पिता की मृत्यु के बाद परिवार के सात सदस्यों का जीवन चलाना अब सुधीर की जिम्मेदारी थी। उसने भी वही रास्ता चुना, जो उसके अन्य साथियों ने चुना था। यह अपने आप में भारी विडंबना है कि एक ओर लगातार कारपोरेट घरानों से एमओयू हो रहे हैं तो दूसरी ओर झारखण्ड से पलायन की दर नई ऊँचाइयां छू रही है[14]।
सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, साखुआपाथ के 18 वर्ष से अधिक आयु के बहुत सारे लड़के गुरूकुल नामक एक कौशल विकास संस्थान में भर्ती है[15]। इस संस्थान में राजमिस्त्रीरी(गृह निर्माण संबंधी कार्य) का 6 महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण लेने के बाद सुधीर को पुणे के एक निर्माणस्थल पर काम पर लगाया गया। वहा उसने झारखण्ड के अपने अन्य आदिवासी साथियों के साथ करीब डेढ़ वर्ष तक काम किया। बातचीत में उसने बताया उसे “बहुत दिक्कत में रहकर, बहुत मेहनत वाला काम करना पड़ता था। ज़रुरत पड़ने पर, उन्हें 12 से लेकर 18 घंटे तक काम करना पड़ता था। कार्यस्थल पर गंदगी, लगातार काम और कम खुराक के चलते सुधीर का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। वह ज्यादा दिनों तक वहां काम नहीं कर सका। उसके बहुत सारे मित्र इन निर्माणस्थलों की दिल दहला देने वाले हालातों में काम करना जारी रखे हुए हैं। अब सुधीर असुर अपने परिवार के साथ गांव में रहता है। वह और उसके दो भाई ट्रकों पर बाक्साइट लादने का काम करके अपना और अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैंने सुधीर से पूछा कि “तुम अपना जीवन कैसे चलाते हो जबकि तुम्हारे पास ज्यादा कृषि भूमि नहीं है।” गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, “सरकार हमें 35 किलोग्राम राशन देती है[16] और कुछ पैसा हम लोग ट्रकों पर बाक्साइट लाद कर कमा लेते है। इस तरह गुजर-बसर चल रहा है[17]। लेकिन जब आने वाले 4 से 5 वर्षों में इस पाथ का सारा बाक्साइट खत्म हो जायेगा, तब लोगों का जीवन खतरे में पड़ जायेगा। असुर तभी तक बचे रहेंगे, जब तक इस पाथ में बाक्साइट है। कुछ समय बाद यहां कोई असुर नहीं होगा। वे देश के अलग-अलग हिस्सों में बिखर जायेंगे”।
शापग्रस्त पवित्र मानव के रूप में असुर
अपनी किताब ‘होमो सैकरः सावरेन पावर एण्ड बेयर लाइफ’ की प्रस्तावना में जिआरगिया एगामबेन लिखते हैं कि उनकी किताब का नायक सिर्फ एक जैविक प्राणी है। उसका जीवन शापग्रस्त मानव का जीवन है। शापग्रस्त मानव को परिभाषित करते हुए वे कहते हैं कि वह एक ऐसा मानव है जिसकी हत्या की जा सकती है लेकिन जिसकी बलि नहीं दी जा सकती। यहां एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है कि एगामबेन के लिए पवित्र मानव, आदर के अर्थों में पवित्र नहीं है, बल्कि, इसके विपरीत, अवमानना के अर्थ में पवित्र है। एगामबेन द्वारा प्रतिपादित शापग्रस्त पवित्र मानव की अवधारणा, जैव-राजनीति और जैव-शक्ति की समाजशास्त्रीय समझ में एक बुनियादी परिवर्तन लाई। जैव-शक्ति की मिशेल फूको की व्याख्या ‘मारे जाने’ के विचार पर जोर देती है जबकि एगामबेन इसे परिष्कृत कर ‘मरने के लिए छोड़ दिए गए’ के अर्थ में प्रस्तुत करते हैं। एगामबेन ने शापग्रस्त मानव शब्द प्राचीन रोमन कानून से लिया है। शापग्रस्त मानव (होमो सैकर) एक ऐसा पुरुष या स्त्री है, जिसे जघन्य अपराध करने के कारण शहर से बहिष्कृत कर दिया जाता था[18]। जब किसी व्यक्ति को शापग्रस्त घोषित कर दिया जाता था तो उसकी हत्या, बलि देने के लिए आवश्यक अनुष्ठान किये बगैर की जा सकती थी। जो सामाजिक समूह इन्हें बहिष्कृत करता था, उसके लिए वे “विशिष्ट जीवन” के अधिकारी नहीं होते थे। इस तरह के बहिष्कृत लोगों से उनके अधिकार छीन लिए जाने के बाद उनके पास क्या बचता था? सिर्फ और सिर्फ जीव के रूप में अस्तित्व।

कानून जीवन को कैसे देखता है, इसकी व्याख्या करने के लिए एगामबेन नाजी यातना शिविरों का उदाहरण देते हैं। वे नाजी यातना शिविरों को एक ऐसे स्थान के रूप में परिभाषित करते हैं जहां “अपवाद की स्थिति” है। सामान्य शब्दों में, “अपवाद की स्थिति” ऐसी “आपातकालीन स्थिति” हैं जिसमें “व्यापक जनहित” के नाम पर सत्ता को कानून के राज का उल्लंघन करने का अधिकार मिल जाता है। एगामबेन की किताब में यातना शिविर को विरोधाभासी लक्षणों के साथ चित्रित किया गया है – जहां ‘देखभाल’ भी होती है और दमन भी। एगामबेन की दृष्टि उधार लेकर मैं यह परिकल्पना प्रस्तुत कर रहा हूं कि असुर समुदाय के परंपरागत निवासस्थान “यातना शिविर” हैं। विशेष विलुप्तप्राय जनजाति (पीवीजीटी) का तमगा इस तबके को उनके लिए घोषित सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का अधिकारी बना देता है। यानी सरकार इनकी सुरक्षा की विशेष तौर पर चिंता कर रही है। जबकि यह मानवशास्त्रीय अध्ययन बताता है कि इस समुदाय का लगातार घोर दमन किया जा रहा है। मेरा यह भी तर्क है कि ये लोग जब अपने इस यातना शिविर को छोड़कर अन्य जगहों – राजमुनी असुर के मामले में कोठी और सुधीर असुर के मामले में निर्माणस्थल पर जाते हैं – तब वे, दरअसल, अपने जैव-अस्तित्व को विशिष्ट अस्तित्व में तब्दील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। परन्तु वहां भी वे अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं होते। ये दूसरे स्थान – कोठी और निर्माणस्थल – यातना शिविर से अलग नहीं हैं – जहाँ, एगामबेन के अनुसार, लोगों से उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं और उन्हें मात्र जीवित प्राणी बना दिया जाता है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि स्वयंसेवी संस्थाओं और गैर-सरकारी सहायता एजेंसियों द्वारा शरणार्थियों और आन्तरिक तौर पर विस्थापित लोगों के लिए चलाए जा रहे शिविर, उनके नागरिक अधिकारों को बहाल करते हैं। लेकिन जिन मामलों की चर्चा मैंने इस आलेख में की है, उनसे यह साफ़ है कि अपने अस्तित्व के खात्मे के कगार पर खड़े इन समुदायों को पुनर्जीवन प्रदान करने में ये संगठन कुछ खास कारगर नहीं सिद्ध हुए हैं या शायद वे ” परदे के पीछे से उन्हीं शक्तियों से गठबंधन कर रहे हैं, जिनसे उन्हें लड़ना चाहिए”. इस क्षेत्र में अधिकांश स्वंयसेवी संस्थाएं सरकारी परियोजनाओं और कार्यक्रमों को ही क्रियान्वित करने में लगी हुई हैं। इसी के चलते मैं इन संस्थाओं को ‘नए सरकारी संगठन’ कहना पसंद करता हूं। अपने को गैर-राजनीतिक संगठन कहना इन स्वंयसेवी संस्थाएं की एक चाल है ताकि वे कोई भी राजनीतिक कदम उठाने से बच सकें। उनका हित इसी में है कि वे आदिवासियों को केवल जीवित प्राणी के रूप में बनाये रखें। विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए इन स्वंयसेवी संस्थाओं द्वारा आजीविका संवर्धन प्रशिक्षण अभियान और कार्यक्रम चलाये जाते हैं। मेरा मानना है कि इस तरह के कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इन लोगों को यह बताना होता है कि वे कितने ‘आदिम’ और ‘पिछड़े’ हैं। ऐसा शायद ही कोई मानवतावादी संगठन हो जो उन प्रक्रियाओं और संरचनाओं पर प्रश्न उठाता हो जो इन समूहों के पिछड़ेपन के लिए ज़िम्मेदार हैं। इससे यह साफ़ है कि ये संगठन, सत्ता के साथ मिलीभगत से काम करते हैं।
21वीं सदी में असुर आदिवसियों की हालात का बयान करने के लिए मैं अखिल गुप्ता के तर्कों का सहारा लेना चाहता हूं। वे कहते हैं कि गरीबी, संरचनात्मक हिस्सा का सबसे बदतर स्वरूप है क्योंकि वह किसी समुदाय को काम और गुजर-बसर करने के अधिकार और प्राकृतिक संसाधनों पर उसके स्वामित्व से,उसे वंचित करता है। उनके रहवास के परंपरागत स्थानों से समुदायों की बेदखली संरचनात्मक हिंसा की अभिव्यक्ति है। मेरा यह कहना है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों को लूटना और उनकी धरती का विध्वंस, असुरों को केवल मरने के लिए छोड़ना नहीं है बल्कि यह इस पूरे समुदाय और उसकी भावी पीढ़ियों की निर्लज्जतापूर्ण हत्या है। और असुरों की यह हत्या, राज्य द्वारा स्थापित किसी कानून या नियम का उल्लंघन नहीं है क्योंकि असुरों की मौत, केवल मौत है और उसे कभी हत्या के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। इस अघोषित और अप्रत्यक्ष नरसंहार की ओर से राज्य का मुंह मोड़ लेना, राज्य के असली चरित्र को उजागर करता है और इस राज्य को लोकतांत्रिक कहा जाये या एकाधिकारवादी, इस सम्बन्ध में किसी भ्रम की गुंजाईश नहीं छोड़ता। इस आलेख से राज्य की इस राजनीति की पोल खुलती है जिसके तहत वह एक ओर लोगों के कल्याण और सुरक्षा के लिए उपाय कर और दूसरी और जन-विरोधी हितों की संरक्षा कर लोगों पर नियंत्रण रखता है।
समय से पहले खदान के बंद हो जाने के बाद असुर आदिवासियों द्वारा कुछ न करना और कुछ कर पाने में अक्षम होना और तीन लड़कियों की तस्करी के बाद उन्हें बचाने के लिए या वापस लाने के लिए कुछ करने की अनिच्छा यह बताती है कि इस समुदाय के लिए दमन और हिंसा एक सामान्य बात बन गई है। यहां एक बात ध्यान देने लायक है कि यह समुदाय कभी-कभार हिंसा का शिकार नहीं होता; उसके साथ सतत हिंसा होती रहती है। इसी का नतीजा है कि हिंसा और दमन उसके जीवन का हिस्सा बन गया है। एक ओर यह हिंसा सामाजिक तालमेल और सामाजिक व्यवस्था को छिन-भिन्न करती है तो दूसरी ओर भविष्य को लेकर गहन अनिश्चितता और निराशा उत्पन्न करती है जिसकी अभिव्यक्ति सुधीर असुर की अंतिम पंक्तियों में दिखाई देती है। हिंसा की उत्पत्ति और उसके कारणों को समझने के लिए उसके जनक की पहचान करना जरूरी है। जहां तक असुरों का मामला है, किसी एक शक्ति, एजेंसी अथवा व्यक्तियों के समूह इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए असमानता और अन्याय पर आधारित एक ऐसी सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक प्रक्रियाएं ज़िम्मेदार हैं जो निरंतर इस समुदाय को हाशिए की ओर ढकेल रही है और उनके जीवन को और असुरक्षित बना रहीं हैं। इस स्थिति में हिंसा के उस जनक की पहचान करना, जो असुरों को केवल जीवित प्राणी बनाने पर आमादा है, बहुत कठिन है। यह एक ऐसा अपराध है, जिसका अपराधी कहीं नहीं दिखता। इसके चलते, यदि कल को असुर समुदाय (यहां शापग्रस्त मानव) पूरी तरह से लुप्त हो जाये तो उसके लिए किसी को सजा नहीं दी जा सकेगी।
[1] झारखण्ड के गुमला जिले का एक प्रशासनिक प्रखण्ड
[2] छतीसगढ़ की सीमा से जुड़े लातेहार जिले का प्रशासनिक प्रखण्ड
[3] भारत सरकार के आदिवसी मामलों का मंत्रालय, “भारत के आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थति के संदर्भ में एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट, मई 2014,पृ. 59
[4] अभिषेक साहा, “झारखण्ड असुर ट्राइब लूजिंग ट्रेडिशनल स्किल इन मार्डन टाइम्स”, हिंदुस्तान टाइम्स, 2 जनवरी 2015
[5] अभिषेक साहा, “झारखण्ड असुर ट्राइब लूजिंग ट्रेडिशनल स्किल इन मार्डन टाइम्स”, हिंदुस्तान टाइम्स, 2 जनवरी 2015
[6] के. के. लेउवा, “ दी असुर : स्टड़ी ऑफ प्रीमीटिव आयरन-स्मेलटिंग (नई दिल्ली : भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, 1963),पृ. 2
[7] के. के. लेउवा, “ दी असुर : स्टड़ी ऑफ प्रीमीटिव आयरन-स्मेलटिंग (नई दिल्ली : भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, 1963),पृ. 4
[8] के. के. लेउवा, “ दी असुर : स्टड़ी ऑफ प्रीमीटिव आयरन-स्मेलटिंग (नई दिल्ली : भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, 1963), पृ.18
[9] ये छद्मम नाम रणेन्द्र के उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता से लिए गए हैं।
[10] यह आंकड़ा गुरदारी खदान के तौल घर से लिया गया है, 16 दिसंबर 2015
[11] प्रत्येक पट्टे के क्षेत्र के नियमों के अनुसार, जो विभिन्न ग्राम पंचायतों की पृथक खदान इकाई के तहत आते हैं। वहां पृथक खदान इकाई स्थापित करने की आवश्कता होती है।
[12] यह आंकड़ा गुरदारी खदान के तौल घर से लिया गया है, 16 दिसंबर 2015
[13] सेंटर फार साइंस और इनवार्नमेंट, रीच लैंड पूअर पीपुलः इज ‘सस्टेनेबल’ माइनिंग पासिबल? (न्यू देलही : सेंटर फार साइंस एण्ड इनवार्मेंटल, 2008), पृ. 67
[14] भारत सरकार के आदिवसी मामलों का मंत्रालय, “भारत के आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थति के संदर्भ में एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट, मई 2014, 255
[15] गुरूकुल एक निजी कौशल विकास और प्रशिक्षण संस्थान है, जो गुमला जिले में है। इस संस्थान को कुछ मुट्ठीभर व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है, जिन्हें झारखण्ड सरकार का सहयोग मिलता है।
[16] यदि ट्रंक में बाक्साइट भरने वाले 10 टन बाक्साइट भर देते है, तो उन्हें 600 रूपया मिलता है।
[17] विलुप्तप्राय आदिवासी समूहों के प्रत्येक परिवार को अन्त्योदय कार्ड मिलता है, उनको छोड़कर जो सरकारी सेवा में हैं।
[18] लेलांड डे ला दुरानतेय, जिओरगियो एगामबेन : एक क्रिटिकल इंट्रोडक्शन (कैर्लिफोर्नियाः स्टैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस-स्टैंडफोर्ड, 2009),पृ. 206
संदर्भ ग्रंथ
- एगामबेन जिआरजिओ, होमोसैकर : सावरेन पावर एण्ड बेयर लाइफ, कैर्लिफोर्निया : स्टैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1998
- सेंटर फार साइंस और इनवार्नमेंट, रीच लैंड पूअर पीपुल : इज ‘सस्टेनेबल’ माइनिंग पासिबल?( न्यू देलही : सेंटर फार साइंस एण्ड इनवार्मेंटल, 2008),
- लेलांड डे ला दुरानतेय, जिओरगियो एगामबेन : एक क्रिटिकल इंट्रोडक्शन (कैर्लिफोर्निया : स्टैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस-स्टैंडफोर्ड, 2009),
- गुप्ता, अखिल, रेड टेप : ब्यूरोक्रेसी, स्ट्रक्चरल वायलेंस, एण्ड पावर्टी इन इंडिया, न्यू देलही : ओरिएन्ट ब्लैक स्वान प्राइवेट लिमिटेड 2012
- के. के. लेउवा, “ दी असुर : स्टड़ी ऑफ प्रीमीटिव आयरन-स्मेलटिंग (नई दिल्ली : भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, 1963),
- भारत सरकार के आदिवसी मामलों का मंत्रालय, “भारत के आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थति के संदर्भ में एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट, मई 2014,
- आक्सफाम, दी पोलिटिकल इकोनामी ऑफ कैपिटेलिज्म, ‘डवलपमेंट’ एण्ड रेजिस्टेंस : दी स्टेट एण्ड आदिवासी ऑफ इंडिया (न्यू देलहीः आक्सफाम इंडिया, 2015)
- रणेन्द्र, ग्लोबल गांव के देवता, नई दिल्ली : भारतीय ज्ञानपीठ, 2013
- अभिषेक साहा, “झारखण्ड असुर ट्राइब लूजिंग ट्रेडिशनल स्किल इन मार्डन टाइम्स”, हिंदुस्तान टाइम्स, 2 जनवरी 2015
- सासा, विरगिनियस, “ट्राइब्स इन इंडिया” इन दी आक्सफोर्ड इंडिया कंपेनियन टू सोशियालोजी एण्ड सोशल एंथ्रोपोलोजी, न्यू देलही : आक्सफोर्ड इंडिया प्रेस, 2013
(विकास दुबे का यह लेख शीध्र प्रकाश्य किताब ‘पस्पेक्टिव ऑफ ट्राइबल स्टडीज : थियरेटिकल,कॉनसेप्चुअल एण्ड इम्पीरिकल इनवेस्टिगेशन ‘में संकलित है। इस किताब का संपादन मागुनी चरन बेहरा ने किया है।)
महिषासुर से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए ‘महिषासुर: एक जननायक’ शीर्षक किताब देखें। ‘द मार्जिनलाइज्ड प्रकाशन, वर्धा/दिल्ली। मोबाइल : 9968527911. ऑनलाइन आर्डर करने के लिए यहाँ जाएँ: अमेजन, और फ्लिपकार्ट। इस किताब के अंग्रेजी संस्करण भी Amazon,और Flipkart पर उपलब्ध हैं।