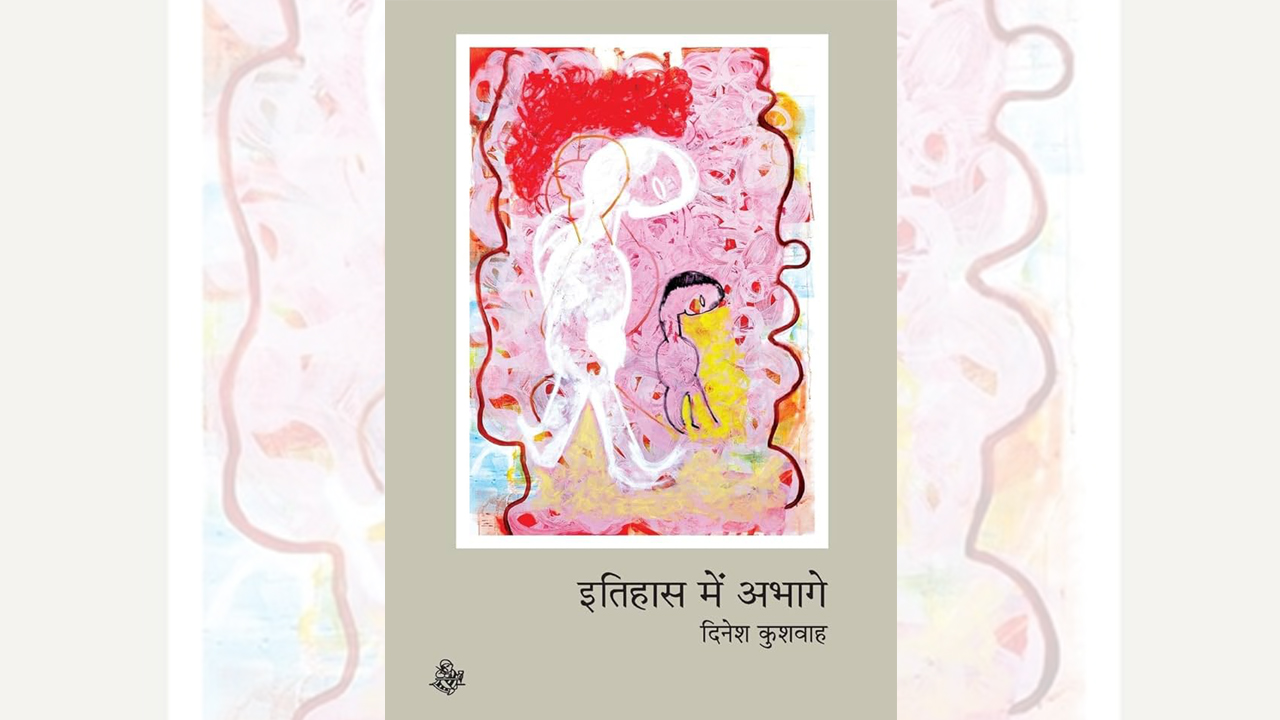जन विकल्प
प्रेमचंद और बहुजन -चिंतन
हिंदी लेखक प्रेमचंद (31 जुलाई 1880 – 8 अक्टूबर 1936) बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध के लेखक थे ,और उन्हें गुजरे हुए जमाना हो गया ,फिर भी कई मायनों में वह आज भी आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक हैं। उनकी प्रासंगिकता कम से कम मुझे उत्साहित नहीं करती; कुछ अर्थों में वह तकलीफदेह ही कही जानी चाहिए। यह इसलिए कि वह इस बात का परिचायक है कि प्रेमचंद-कालीन समाज और आज के समाज में कोई बड़ा अंतर नहीं आया है। यह एक ठहरे हुए गतिहीन अथवा सुस्त समाज के लक्षण हैं। इस गतिहीनता पर केवल अफ़सोस ही व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए ही मैंने बतलाया कि उनकी प्रासंगिकता मेरे अंतरमन में अपने किस्म की एक उदासी सृजित करती है।
प्रेमचंद का जन्म उन्नीसवीं सदी में हुआ और उनका लिखना बीसवीं सदी के आरम्भ में शुरू हो गया। विषय के आकलन के लिए हमें उस दौर की सामाजिक-राजनैतिक स्थिति का स्मरण करना चाहिए। उनके जन्म के पांचवें वर्ष में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हो गया था और कमोबेश एक राष्ट्रीय चेतना का स्फुरण देश अनुभव करने लगा था। लेकिन ये तमाम स्फुरण बंगाल और महाराष्ट्र तक ही सीमित थे। प्रेमचंद का हिंदी इलाका इस चेतना से तनिक दूर था। पुरोहिती-कर्मकांडी नगर काशी-बनारस से कुछ ही किलोमीटर दूर उनका गांव लमही था। बनारसी साड़ियों के लिए मशहूर बनारस में कभी कबीर जैसा बौद्धिक हुआ था, और बगल के सारनाथ में ढाई हज़ार वर्ष पूर्व बुद्ध ने अपने क्रान्तिकारी धर्म-दर्शन का पहला उद्घोष किया था; लेकिन प्रेमचंद के समय का बनारस पण्डे-पुरोहितों का नगर था – सुस्त, काहिल और विचारशून्य। प्रेमचंद इस विचारशून्यता को गहराई से समझ रहे थे। उनकी यही समझ उनके साहित्य का आधार है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसकी वाजिब समीक्षा अब तक हिंदी साहित्य में नहीं हुई है।

किसी भी लेखक का एक विचार पक्ष होता है। यदि लेखक साधारण स्तर का हुआ था, तब उसके युग की प्रतिनिधि विचारधारा उसकी विचारधारा बन जाती है और अपनी लेखनी द्वारा वह उस विचारधारा का प्रचारक बन जाता है। यदि लेखक स्वयं में एक विचारक है, तब उसका साहित्य उसके विचारों का पाठ बन जाता है और एक प्रस्ताव के रूप में वह अपने ज़माने के समक्ष प्रस्तुत होता है। कबीर और तुलसी स्वयं में एक विचार थे। उनका साहित्य उनकी विचारधारा की प्रस्तावना करता है। आधुनिक ज़माने में रवींद्रनाथ टैगोर की अपनी विचारधारा है; टॉलस्टॉय, चेखब की अपनी विचारधारा है। हाँ, गोर्की की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, वह अपने ज़माने की एक खास विचारधारा के उन्नायक बनते हैं। चूंकि वह विचारधारा उत्पीड़ित जनता के पक्ष की विचारधारा थी, इसलिए गोर्की जनता के लेखक बन जाते हैं।
प्रेमचंद अपने समय की किसी प्रचलित विचारधारा के प्रचारक नहीं बने दीखते। हालांकि उन पर कई बार गांधीवादी और राष्ट्रवादी होने की बात कही गयी है। लेकिन उन्हें तय वैचारिक खांचों में रखना मुश्किल प्रतीत होता है। उन पर गांधी और राष्ट्र सवार नहीं दीखते। हाँ, मनुष्य की चिंता उनके साहित्य में अवश्य है। लेकिन वह मनुष्य कौन -सा और कैसा है? क्या प्रेमचंद के यहां भारत-व्याकुल पात्र प्रमुखता लिए हुए दीखते हैं? शायद नहीं। किसान -मजदूर , उत्पीड़ित स्त्रियां और दलित-अछूत उनकी कहानियों और उपन्यासों में आगे-आगे रहते हैं। सामंत-पुरोहित ,जमींदार और जनता को अनेक प्रकार से ठगने वाले सरकारी कारिंदे उनके साहित्य में चिन्हित किये जाते हैं। पाठकों को समझते देर नहीं लगती कि लेखक किनके पक्ष में खड़ा है।
प्रेमचंद के ज़माने में उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रीय संघर्ष चरम पर था। देश एक राष्ट्र के रूप में विकसित होने के लिए उत्सुक और सक्रिय था। राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर गांधी के हाथों में जरूर आ गयी थी, किन्तु अनेक विचारधाराएं उभरना चाहती थीं। वह जब उम्र के सैंतीसवें साल में थे, तब रूस में बोल्शेविक क्रांति (1917) हुई और दुनिया में पहली दफा मिहनतकश वर्ग राजसत्ता में आया। 1922 में उनके बाजू में चौरी-चौरा की घटना हुई, जिसमे किसानों ने पुलिस चौकी पर हमला कर कई सिपाहियों की हत्या कर दी और और पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद गाँधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को स्थगित किये जाने की घोषणा कर दी। बोल्शेविक क्रांति और चौरी-चौरा की घटना में बस पांच साल का अंतराल था। प्रेमचंद के दिल-दिमाग को ये घटनाएं निश्चय ही प्रभावित कर रही थीं।
लेकिन उनके समय में राजनैतिक आंदोलनों के साथ-साथ एक सामाजिक विचारधारा व आंदोलन भी हिंदी इलाके में उठ रहा था, जिसका केंद्र जाने-अनजाने बनारस बन रहा था। महाराष्ट्र से ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद का जो गुबार बाल गंगाधर तिलक की अगुआई में उठा था, वह महाराष्ट्र से अधिक हिंदी इलाकों में फैला। महाराष्ट्र में तो फुले और आंबेडकर के नेतृत्व में उस विचारधारा को चुनौती मिली, किन्तु हिंदी क्षेत्र इनके लिए बिलकुल खाली था। तिलक की वैचारिकता को महाराष्ट्र से अधिक इसी इलाके में अनुकूलता मिली। विशिष्ट स्थिति यह बनी कि यहां का साहित्य इसका वाहक बन गया। हिंदी साहित्य राष्ट्रवाद के कोलाहल से भर गया और ऐसा लगा मानों साहित्य ने ही राजनैतिक स्वतंत्रता का पूरा जिम्मा ले लिया हो। इसकी परिणति हुई कि सामाजिक परिवर्तन के सवाल पीछे छूटने, अथवा कमजोर पड़ने लगे। हिंदुत्व से आप्लावित प्रचंड राष्ट्रवाद हिंदी साहित्य की आत्मा बनती चली गयी। छायावादी काव्य आंदोलन से सार्थक हस्तक्षेप की अपेक्षा बनती थी, लेकिन यह भी संभव नहीं हुआ। प्रेमचंद ने इस स्थिति को भांप लिया था। अपने प्रथम कथा-संकलन ‘सोजे वतन’ की एक कहानी ‘संसार का सब से अनमोल रतन’ का जब हम अध्ययन करेंगे, तब पाएंगे कि देश के लिए वह व्याकुलता प्रेमचंद की बाद की कहानियों में नहीं मिलती। इस व्याकुलता का परित्याग कम से कम उन्होंने अपने लेखन के दूसरे दौर में तो कर ही दिया था। ‘अनमोल रतन’ मार्का कहानियां फिर नहीं मिलतीं। उनके वर्ण्य और पात्र किसान-मजदूर, दलित, स्त्रियां और समाज के उपेक्षित लोग होने लगते हैं। यह सब उनके वैचारिक परिवर्तन का ही साक्ष्य देता है।
प्रेमचंद आधुनिक हिंदी के पहले लेखक थे, जिन्होंने स्पष्टतया ब्राह्मणवादी पाखंड को बार-बार अपनी रचनाओं में चिन्हित करने की कोशिश की है। हिन्दुओं की वर्ण-व्यवस्था पर प्रश्न उठाने का साहस किसी अन्य हिंदी लेखक ने नहीं किया था। उन्होंने यह किया। उनपर मुकदमे दर्ज़ किये किये गए और कई तरह से उनकी अवमानना की गयी, लेकिन वह रुके नहीं। ‘ठाकुर का कुआँ’ कहानी उन्होंने उसी वर्ष लिखी, जिस वर्ष आंबेडकर के नेतृत्व में चौहद का जल सत्याग्रह चला। ‘सद्गति’ और ‘सवा सेर गेहूं’ जैसी कहानियों में ब्राह्मणवादी प्रपंचों का अपने तरीके से पर्दाफाश करने की कोशिश की। इन सब को लेकर उन पर लेखक समाज में टिप्पणियां भी हुईं। ऐसे ही किसी हमले से आहत हो, उन्होंने 12 जनवरी 1934 को बाबू बनारसीदास जी को लिखा – “उसने (किसी निर्मल ने) मुझ पर यह दोष लगाया है कि मैं ब्राह्मण वर्ग का द्रोही हूँ। सिर्फ इसलिए कि मैंने इन पुजारियों और धार्मिक लुच्चे-लफंगों के कुछ पाखंडों का मज़ाक उड़ाया है। उनको वह ब्राह्मण कहता है और जरा भी नहीं सोचता कि उनको ब्राह्मण कहकर वह अच्छे-भले ब्राह्मणों का कितना अपमान करता है। ब्राह्मण का मेरा आदर्श सेवा और त्याग है, वह कोई भी हो। पाखण्ड और कट्टरता और सीधे-सादे हिन्दू समाज के अन्धविश्वास का फायदा उठाना, इन पुजारियों और पंडों का धंधा है और इसीलिए मैं उन्हें हिन्दू समाज का एक अभिशाप समझता हूँ और उन्हें अपने अधःपतन के लिए उत्तरदायी समझता हूँ। वे इसी काबिल हैं कि उनका मखौल उड़ाया जाय और यही मैंने किया है। यह निर्मल और उसी थैली के चट्टे-बट्टे दूसरे लोग ऊपर से बहुत राष्ट्रीयतावादी बनते हैं, मगर उनके दिल में पुजारी वर्ग की सारी कमजोरियां भरी पड़ी हैं और इसीलिए वे हम लोगों को गालियां देते हैं जो स्थिति में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं . … मैं कुछ नहीं समझ सका कि आप किस चीज में पंच बनने जा रहे हैं और मेरे खिलाफ फर्द-ए-जुर्म क्या है, क्या वे कहानियां जिनमें मैंने इन पाखंडियों का मखौल उड़ाया है ? बराय मेहरबानी उन्हें पढ़ जाइये। बहुत नहीं हैं . …वह द्वेष और विष से पूरी तरह मुक्त हैं।”
प्रेमचंद सामाजिक सवालों पर किसी ओह-पोह में नहीं रहते थे। भारतीय संस्कृति के प्रसंग में कवि जयशंकर प्रसाद को लिखे एक पत्र में उन्होंने लिखा – “किस बात पर गर्व करें ,वर्णाश्रम धर्म पर ! जिसने हमारी जड़ खोद डाली … “
तुलसीदास और उनके रामचरित मानस का उस दौर में साहित्यिक समाज में बड़ा मान था, लेकिन प्रेमचंद ने उसे पढ़ने लायक कभी नहीं समझा। कोलकाता के उनके मित्र बनारसीदास चतुर्वेदी प्रेमचंद को वहां तुलसी जयंती पर बोलने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। टैगोर ने मिलना चाहा था। लेकिन तुलसी जयंती के नाम पर उन्होंने जाने से इंकार कर दिया। चतुर्वेदी जी को लिखा – “अगर तुलसी जयंती की कैद मेरे ऊपर न लगायी होती तो मैं आ जाता। लेकिन तुलसी जयंती का सभापतित्व एक ऐसा व्यक्ति करे जिसने कभी तुलसी का अध्ययन नहीं किया और जो उनके नाम के साथ जुडी हुई अतिमानव बातों में विश्वास नहीं करता, यह बात ही मुझे हास्यास्पद जान पड़ती है।” (‘कलम का सिपाही’, पृष्ठ 605 )
वैचारिक मामलों में वह ढुल-मुल बिलकुल नहीं थे। दिन-रात जाति-तंत्र के जाल बुन रहे कुछ व्याकुल तत्वों ने इधर के वर्षों में उनकी प्रतिबद्धता पर प्रश्न उठाये हैं। वे यह भूल जाते हैं कि जिस वातावरण और स्थान से प्रेमचंद ने ब्राह्मणवादी विचारधारा पर हल्ला बोला था, वह चुनौती भरा और मुश्किल कार्य था। वह अपने समय से बहुत आगे थे। हंस की सम्पादकीय टिप्पणियों से उनकी वैचारिकता के पक्ष स्पष्ट होते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए गांधी का महत्व स्वीकारते हुए भी वह गांधीवाद से प्रभावित नहीं थे। उनकी स्थिति कुछ हद तक नेहरू जैसी थी। नेहरू के विचारों से वह प्रभावित भी दीखते हैं। हंस की कम से कम तीन सम्पादकीय टिप्पणियां नेहरू पर केंद्रित हैं, जिसमें प्रेमचंद उनके विचारों की प्रशंसा करते हैं, ख़ास कर समाजवादी आर्थिक विचारों की। आंबेडकर के पूना पैक्ट मामले पर उन्होंने दलित प्रसंग को राष्ट्रीयता से जोड़ कर देखा है। किसानों-मजदूरों और अन्य मिहनतक़श तबकों के पक्ष में वह बराबर खड़े दीखते हैं।
(कॉपी संपादन : सिद्धार्थ)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in