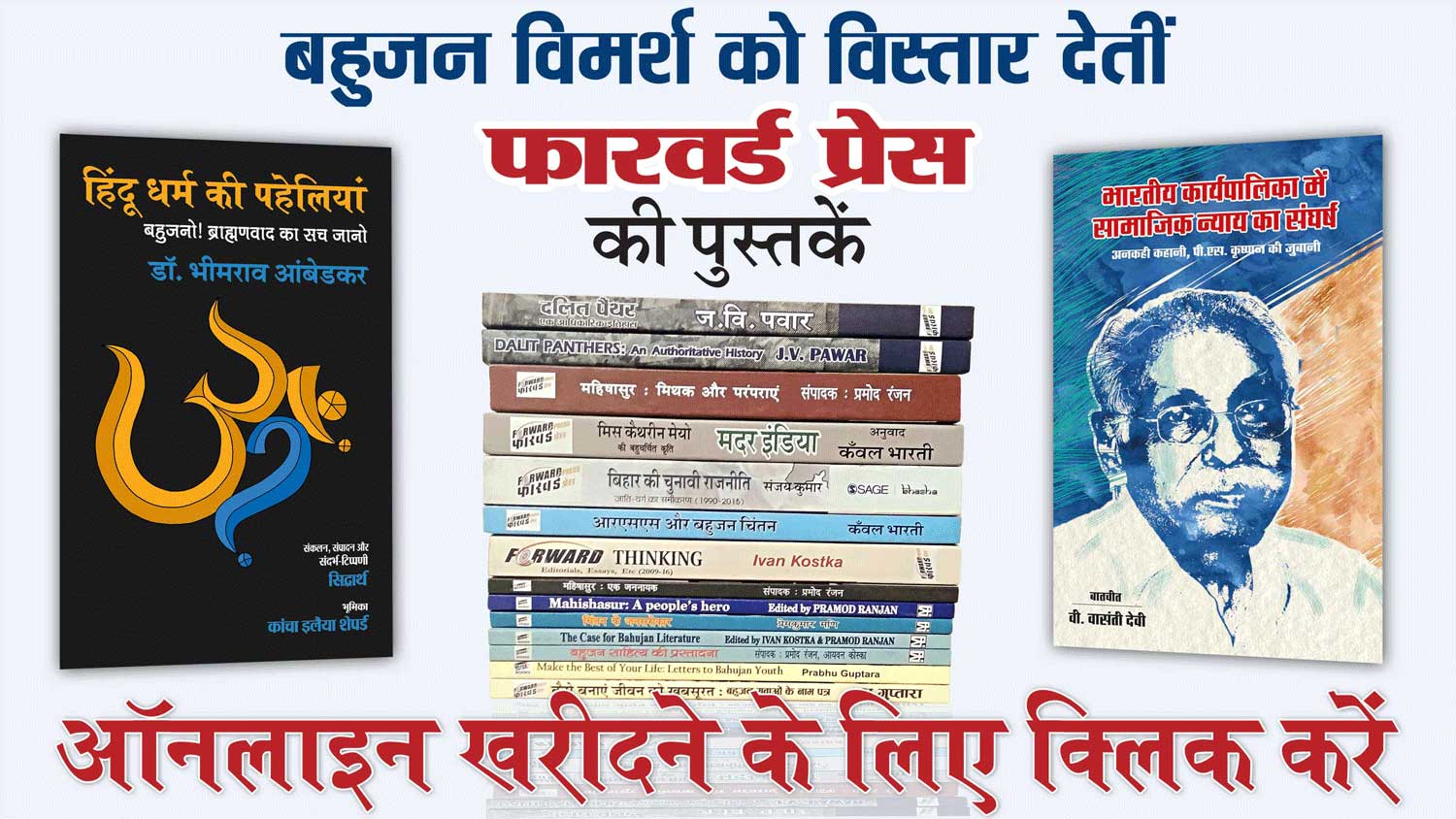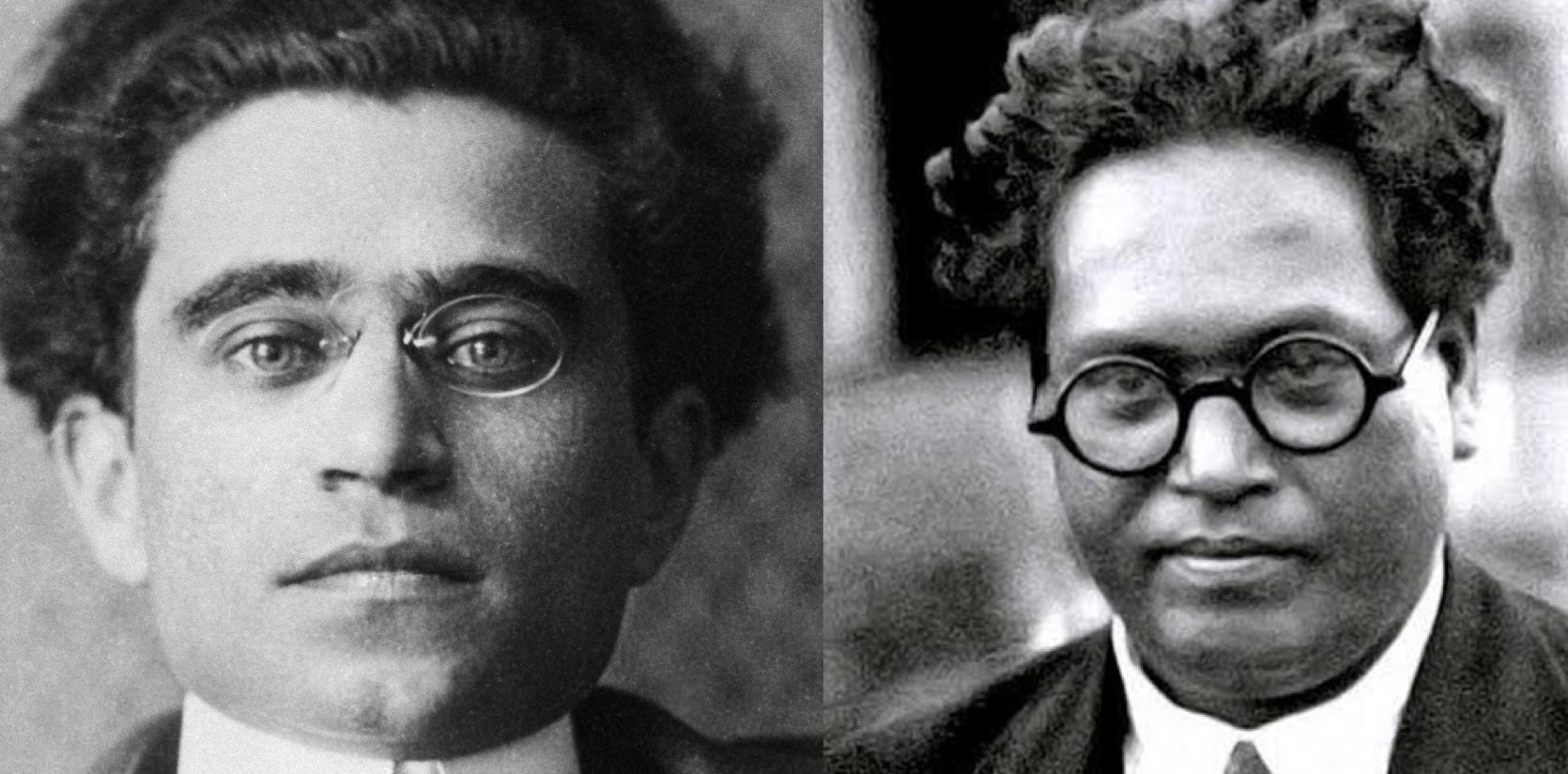मैं आत्मकथा लेखन को सृजनात्मक लेखन नहीं मानता, हालांकि संस्मरण-विधा भी इसी के अंतर्गत आती है, जो दूसरों के बारे में होने के बावजूद लेखक के अपने जीवन से ही जुड़ी होती है, मगर उसमें लेखक का अपना मूल्यांकन साथ रहता है, इसलिए कुछ हद तक उसमें सृजनात्मकता होती है। किन्तु आत्मकथा में ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें भोगे हुए जीवन की सपाट कहानी होती है। जैसा जिया या जैसा घटा, वैसा लिखा। एक बार शुरू हुई, तो वर्तमान परिणिति पर ही समाप्त होती है। यही कारण है कि आत्मकथा लिखने के लिए साहित्यकार होना जरूरी नहीं है। उसे कोई भी लिख सकता है, राजनेता, अभिनेता, अभिनेत्री, क्रिकेटर, वैज्ञानिक, वगैरा-वगैरा। लेकिन एक साहित्यकार की आत्मकथा से यह अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल भाषा और शिल्प में बेजोड़ होगी, बल्कि पठनीयता की दृष्टि से भी एक अच्छी कृति होगी। इस कसौटी पर दलित साहित्य में अब तक ओमप्रकाश वाल्मीकि की ‘जूठन’, मोहनदास नैमिशराय की ‘अपने-अपने पिंजरे’, तुलसी राम की ‘मुर्दहिया’ व ‘मणिकर्णिका’ और श्योराजसिंह बेचैन की ‘अपना बचपन अपने कंधों पर’ बेहतरीन कृतियां साबित हुई हैं।
लेकिन, कौशल पंवार की आत्मकथा ‘बवंडरों के बीच’ को पढ़कर ऐसा प्रतीत हुआ कि सीधी-सादी आत्मकथा भाषा और शिल्प की मोहताज नहीं होती, वह भावनाओं और दिल की भाषा से लिखी जाती है। उन्होंने अपनी कथा का आरंभ अपने जन्म और जन्म की परिस्थितियों के वर्णन से नहीं किया है, जैसा कि अधिकांश आत्मकथाएं शुरू होती हैं। उनकी आत्मकथा उनकी मां की मृत्यु की खबर से शुरू होती है, जो उन्हें तब मिली थी, जब वह बार्सिलोना यूनिवर्सिटी में धर्मशास्त्रों में जातिप्रथा की भूमिका पर व्याख्यान देने के लिए स्पेन गईं हुईं थीं। वह अपनी आत्मकथा अपने जन्म से शुरू कर सकती थीं, पर वहां क्या था? गरीबी, अस्पृश्यता, गंदगी, सूअर, बदबू, सीलन और अभाव। उससे प्रेरणा की लहरें नहीं उठतीं, जुगुप्सा के बवंडर उठते। स्पेन से शुरू करके उन्होंने यह बताया कि उस बवंडर से जूझकर निकली एक लड़की ने वह महानता अर्जित की कि उसे सात समंदर पार विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए सम्मान से बुलाया गया। उन्होंने लिखा है, “कहां तो गांव की गलियों में गोबर बटोरती लड़की और कहाँ आज यहाँ इतने विदेशी बड़े-बड़े विद्वानों के बीच। ऐसे ही ये शब्द कागज पर लिख दिए थे। मेरा माथा झुक गया था, माँ और चाचा को याद करके। भीगी हुई आँखों से मैंने उस समय अनायास ही कुछ पंक्तियाँ लिखीं– फख्र क्यों न करूं खुद पर, थाली में परोसकर नहीं दिया किसी ने।”

‘बवंडरों के बीच’ का पहला अध्याय खुद पर गर्व करने का अध्याय है। भारत में हरियाणा के राजौंद गांव में मां का निष्प्राण शरीर अंतिम संस्कार के लिए बेटी की प्रतीक्षा कर रहा है, और बेटी अपना दौरा छोड़कर स्पेन से तुरंत वापस आ रही है। गांव जाकर मां को अंतिम विदाई देती है। पिता पहले ही चले गए थे, जिन्हें वह चाचा कहती थी। मां और चाचा ये ही दोनों पूरी आत्मकथा के केन्द्र में उत्प्रेरक के रूप में आए हैं। तीसरा अध्याय चाचा पर है। ‘चाचा जो मेरे लिए बाबासाहेब थे।’ किन्तु वह किस तरह बाबासाहेब थे, इसका कोई विवरण इस अध्याय में नहीं है। उन्होंने अकादमिक ढंग से विश्लेषण करते हुए आत्मकथा नहीं लिखी है, बल्कि भावनाओं के प्रवाह में, जो याद आता गया, उसे वह लिखती गई हैं। आत्मकथा के इस तरह के लेखन में तारतम्यता नहीं रहती, जो अखरता है। लेकिन पाठक जैसे-जैसे आगे पढ़ता जाता है, उसे ज्ञात होता जाता है कि भावनाओं ने उन जानकारियों को आगे उछाल दिया है, जो शुरू में आनी चाहिए थीं। यही भावनाओं का आवेग ही है कि वह ‘स्कूल पढ़ाई और चाचा का साथ’ में यह तो बताती हैं कि वह आठवीं में संस्कृत पढ़ना चाहती थी, लेकिन मास्टर सुरेन्द्र शास्त्री ने यह कहकर अपमानित करके क्लास से निकाल दिया कि संस्कृत तुम्हारे बस की नहीं, तुम पढकर क्या करोगी? लेकिन उन्होंने फिर किस तरह संस्कृत पढ़ी और किस तरह एमए, एमफिल और पीएचडी तक संस्कृत में किया, इसका विवरण वह नहीं देतीं। इसके बाद वह प्राइमरी क्लास की बातें करने लगती हैं कि कैसे मास्टर ने अपने से ही उनकी जन्मतिथि लिख दी और कैसे चाचा उनको गिनती सिखाते थे।
पाठकों को यह बेतरतीब आत्मकथा लग सकती है, क्योंकि तथ्य और जानकारियां इसमें टुकड़ों में बिखरी हुई हैं, उन तमाम कड़ियों को जोड़कर ही कौशल पंवार के जीवन-संघर्ष को समझा जा सकता है।
तुलनात्मक दृष्टि से प्राय: सभी दलित जातियों का जीवन अमानवीय अस्पृश्यता, घृणित गरीबी और धार्मिक अंधविश्वासों का दंश झेलने का रहा है। इसलिए सभी दलित लेखकों की आत्मकथाओं में ये चीजें समान रूप से मिलती हैं। कौशल पंवार का जीवन-संघर्ष भी इससे भिन्न नहीं रहा है। दलित जातियों में जो थोड़ी बहुत जागरूकता पैदा हुई, वह भारत में दलित अस्मिता और मानवीय अधिकार के आंदोलनों की वजह से हुई। इसी जागरूकता से उन्होंने गंदे पेशे छोड़े और शिक्षित होने के लिए संघर्ष किए। यह संघर्ष आसान नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण-ठाकुरों की जमात नहीं चाहती थी कि दलित जातियां गंदे पेशे छोड़ें और पढ़-लिखकर उनकी बराबरी करें। इसलिए उन्होंने समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए दलित जातियों पर बर्बर अत्याचार किये और उनके विकास के खिलाफ हर प्रकार की घेरेबन्दी की। जिन दलितों ने उनके अत्याचारों और उनकी घेरेबंदी को तोड़ने के लिए संघर्ष किये, वे ही आगे बढ़े। भारत के संविधान ने उन्हें समान अवसर दिए, पर उन्होंने बड़ी कीमत चुकाकर उन अवसरों को प्राप्त किया। इसलिए कौशल ठीक कहती हैं कि सफलता उन्होंने अर्जित की है, किसी ने थाल में परोसकर नहीं दी है।
अस्पृश्यता और गरीबी पर काफी चर्चा हुई है, पर अगर नहीं हुई है, तो दलित जातियों के बीच मौजूद अंधविश्वासों पर। भूत-प्रेत, झाड़-फूंक और टोना-टोटका में विश्वास दलित जातियों के जीवन का अनिवार्य हिस्सा रहा है। यह उनमें शिक्षा के आ जाने के बाद भी मौजूद है। डॉ. आंबेडकर ने एक जगह लिखा है कि निम्न जातियों में अंधविश्वास उनकी जिजीविषा का प्रतीक हैं। वे जीना चाहते हैं। कल्पना कीजिए, जिनकी सारी आर्थिक, सामाजिक और परिवेशीय परिस्थितियां उनके जीवन पर संकट की तरह हों – न पौष्टिक भोजन, न स्वच्छ वातावरण, न स्वच्छ पेशे, न ढंग के बिस्तर-कपड़े, न सर पर ठीक से छत, न सुविधाएँ, ऊपर से उच्च जातियों का डाँटना-फटकारना, अपमानित करना, गालियाँ देना, ऐसे परिवेश में रहने वाले बच्चे बच गए, तो जी गए, वरना मर गए। ज्यादातर बच्चे कुपोषण से मरते हैं। माता-पिता उनके जीवन के लिए ही टोने-टोटके करते हैं और गंडे-ताबीज बंधवाते हैं। इन सारे गंडे-ताबीज, टोने-टोटके, झाड़-फूंक के अंधविश्वासों के पीछे हमारे लोगों की जीने की इच्छा काम करती है। कौशल पंवार ने लिखा है कि उनसे पहले उनकी पांच बहनें नहीं जी सकीं थीं। जब वह पैदा हुई, तो उनके चाचा ने एक बाबा की भभूत को ताबीज में रखकर उसके गले में डाल दिया था, ताकि वह जिंदा रहे। यह ताबीज काफी बड़ी उमर तक उसके गले में पड़ा रहा था, और फिर एक दिन उसी ने उसे नई बनती दीवार की मोरी में रखकर उससे मुक्ति पाई थी।
कौशल पंवार ने अपने चाचा के एक और अंधविश्वास की चर्चा की है, जिसके कारण पंचायत बुलानी पड़ गई थी। यह अन्धविश्वास भी जिजीविषा से जुड़ा है। उन्होंने लिखा है कि वह माँ के पेट में थी, तभी चाचा को विश्वास हो गया था कि बेटी ही होगी। वह बच्ची के जिन्दा रहने का उपाय जानने के लिए किसी पंडित के पास गए। उसने बच्ची को किसी को दान करने का उपाय बताया। चाचा के एक दोस्त सूबेदार थे, उसकी पत्नी के भी बच्चा होने वाला था। चाचा ने पंडित की बात मानकर अपने दोस्त के होने वाले बच्चे को अपनी होने वाली बच्ची को दान कर दिया। उससे कहा, बच्चों को पढ़ाना है। अगर नहीं पढ़ाया, तो रिश्ता टूट जायेगा। संयोग से इधर लड़की ही हुई, और उधर भी लड़का ही हुआ। सूबेदार के लड़के ने कुछ क्लास पढ़कर पढ़ाई छोड़ दी, पर कौशल पढ़ती रही। शर्त के हिसाब से रिश्ता टूट गया था, पर सूबेदार शर्त भूल गया, और उसने चाचा के इनकार पर बाईस गांवों की पंचायत बुला ली। पंचायत में कौशल के चाचा ने शर्त की याद दिलाई, और इस तरह पंचायत का फैसला सूबेदार के खिलाफ गया।
कौशल पंवार अपनी आत्मकथा के कुछ प्रसंगों पर कहानियां लिख चुकी हैं, जो उनके ‘जोहड़ी’ कहानी-संग्रह में संकलित हैं। जैसे ‘दिहाड़ी’, ‘जोहड़ी’, ‘वर्दी’ और ‘लच्छो’। सच यह है कि उनके आत्म-संघर्ष में कथा के रूप में यही चीजें हैं। ‘दिहाड़ी’ में उन्होंने अपने पिता के बीमार होने पर उनकी एवज में पीडब्लूडी के लेबर के रूप में काम किया है। और यह तब की बात है, जब वह कालेज में बीए की छात्रा थीं। ‘वर्दी’ का प्रसंग भी मार्मिक है। स्कूल की ड्रेस सफ़ेद रंग की है, पर कौशल्या (स्कूल में यही नाम है) हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनकर स्कूल जाती है, जिसे देखकर उसे सब ‘चूहड़े की’ कहकर अपमानित करते हैं। इस पर वह घर में जाकर रोती है। तब उसके चाचा कहीं से उसे सफेद रंग का कपड़ा लाकर देते हैं, जिसे पाकर वह खुश हो जाती है। माँ चाचा को अलग ले जाकर पूछती है, घर में तो पैसा है नहीं, तुम यह कपड़ा कहाँ से लाए हो? तब चाचा बताते हैं कि जलती हुई चिता के पास से। आत्मकथा में ‘लच्छो’ का प्रसंग वीभत्स है, और जुगुप्सा पैदा करता है। यह उसके घर में पलने वाली एक सुअरी का नाम है। वह गांव के प्रेम राजपूत के गुआड में जाकर, जिसमें घास और पराली रखी जाती है, ब्या जाती है। प्रेम को जब पता चलता है तो वह कौशल्या के चाचा के घर जाकर गंदी-गंदी गालियाँ बकता है और उसे तुरंत ले जाने को कहता है। घर में कोई है नहीं, तब कौशल्या स्वयं ही उसे लेकर आती है। सुअरी को ले जाते हुए एक दृश्य को कौशल ने इस तरह व्यक्त किया है– “मैं और लच्छो एक गली से होते हुए दूसरी गली, फिर तीसरी गली, ऐसे ही घूमते हुए राजपूतों के मोहल्ले से गुजर रहे थे। मेरे कपड़ों पर चाट (सूअरों को खिलाने वाली) के छींटों के कारण मक्खियाँ भिनभिना रही थीं और बदबू भी आ रही थी। गली से मुड़ते हुए मुझे मेरी क्लास में पढ़ने वाला सतबीर दिखाई दे गया। मैंने उससे आंख बचाकर निकलना चाहा कि कहीं वह मुझे देख न ले, पर वह देख चुका था। मुझे लच्छो को अपने साथ-साथ रखने के लिए आवाज निकालनी पड़ती थी, जिससे न चाहते हुए भी अनायास ही सबका ध्यान मेरी ओर जाता था, पर मुझे इसकी परवाह भी नहीं थी, क्योंकि चाचा ने यही समझाया था कि कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता।”
बेशक काम छोटा-बड़ा नहीं होता। दलित जातियों के लोग इन्हीं छोटे-बड़े कामों को करके आगे बढ़े हैं और उन्होंने आसमान छुआ है। कौशल पंवार ने भी आसमान छुआ है। लेकिन उनकी आत्मकथा व्यवस्थित नहीं है। वह उनके जीवन पर कोई खास प्रकाश नहीं डालती है। व्यक्तित्व का निर्माण और विकास किस तरह होता है, उसकी एक उत्तरोत्तर स्थिति होती है, जिसका इस आत्मकथा में कुछ पता नहीं चलता। उनकी आत्मकथा एक जल्दबाजी का उपक्रम है, जिसमें भावनाएं तो हैं, पर जीवन का इतिहास नहीं है। अगर वह इसे फिर से लिखना चाहें, तो मेरी सलाह है कि उन्हें कुछ अच्छी आत्मकथाएँ पढ़ने की आवश्यकता होगी।
समीक्षित पुस्तक : बवंडरों के बीच
लेखिका : कौशल पंवार
प्रकाशक : द मार्जिनलाइज्ड, नई दिल्ली
मूल्य : 350 रुपए
(संपादन : नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें
मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया