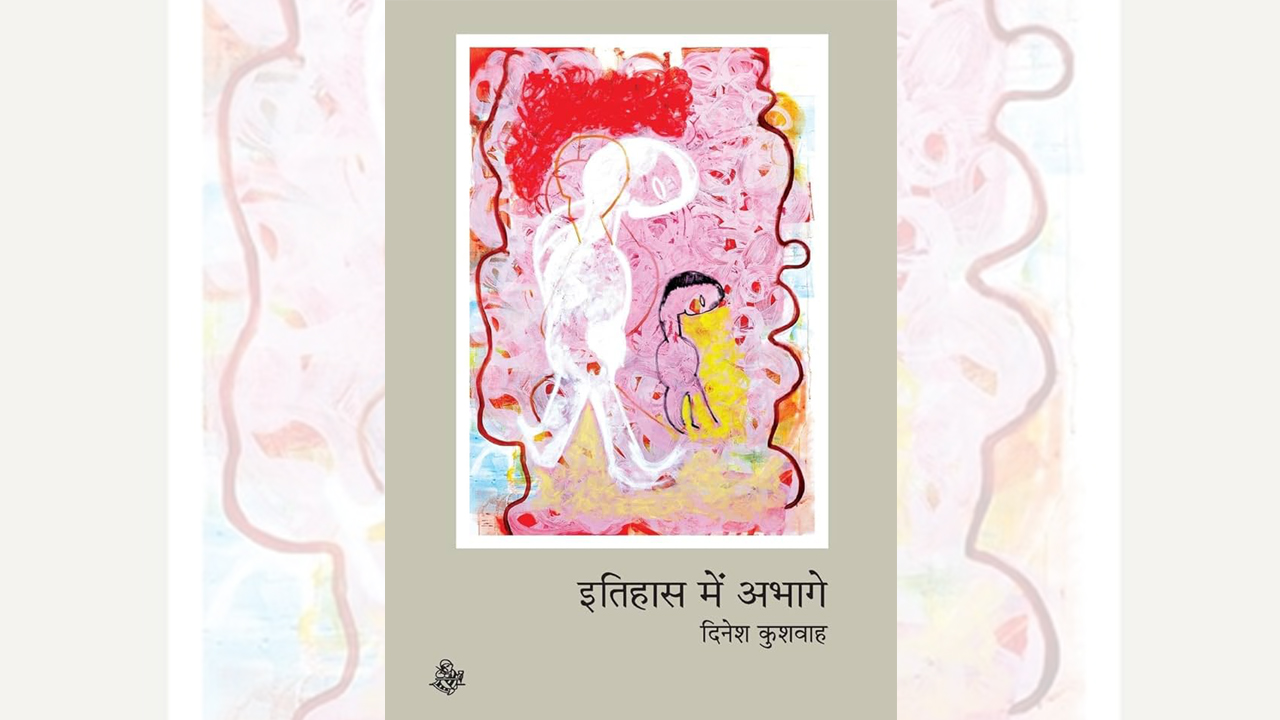पुस्तक समीक्षा
गणेश शंकर विद्यार्थी की वैचारिकी पर काम करने के दौरान पहाड़ों के बारे में मैंने उनका एक लेख उनकी रचनावली में पढ़ा था, जिसका शीर्षक है– ‘ऊंचे पहाड़ों के अंचल में’। यह 1927 के दौर का लेख है, जब उन्होंने उत्तराखंड के अल्मोड़ा-नैनीताल आदि अंचलों की स्वतंत्रता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में एक राजनीतिक यात्रा की थी। इस लेख में उन्होंने एक स्थान पर डोम जाति के बारे में बहुत ही गौरतलब टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है–
“डोम पहाड़ों में बहुत व्यापक शब्द है। उनमें अनेक छोटी-छोटी जातियां शामिल हैं। ये सब अछूत समझी जाती हैं । पहाड़ों के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य उन्हें पास नहीं फटकने देते। एक बार पूछने पर मालूम हुआ कि जितने शिल्पकार हैं, जैसे बढ़ई, ठठेरा आदि, वे भी अछूत ही माने जाते हैं। हाथ से परिश्रम करके अपना पेट भरने, किंतु बड़े आदमियों के लिए सत-खंडों को खड़ा करने वाले लोगों की यह दुर्गति, हिंदुओं के इस भयंकर पतन का एक बहुत बड़ा कारण है।”[1]
लेकिन हिंदुओं का तो कोई पतन हुआ नहीं, पतन हुआ पहाड़ के अछूतों का ही, और वर्तमान में भी हो रहा है। उन्होंने आगे लिखा, “लालकुआं से लेकर काशीपुर तक एक पहाड़ी क्षत्रिय से बातें होती रहीं, जहां उसने यह खुशी की बात सुनाई कि पहाड़ों में क्षत्रिय और वैश्यों में विवाह संबंध हो जाया करता है। उसने कई उदाहरण भी दिए। वहीं वह छोटी जातियों और विशेषतया डोमों को ‘साले’ के शुभ नाम से बार-बार याद करता रहा। ‘भई, वे भी तो अपने ही भाई हैं।’ यह वाक्य उसे नहीं रुचा। उसकी कुलीनता इन ‘सालों’ के साथ बराबरी के लिए तैयार न थी। वे साले उसके मजदूर ही बनकर रह सकते थे।”[2]
यह पहाड़ का वह रामराज्य है, जिस पर सारे पहाड़ी ब्राह्मण-ठाकुर गर्व करते हैं। देश के मैदानों में हो, या न हो, पर पहाड़ों में औकात से बाहर निकलते ही दलित की गर्दन पर तलवार चल जाती है। यही कारण है कि पहाड़ के सारे ब्राह्मणन-ठाकुरों का अहंकार बोलता है– मेरा पहाड़! मेरा पहाड़! देव भूमि!
इस अवधारणा का पहाड़ों की माटी से निकले सशक्त दलित विमर्शकार व कवि मोहन मुक्त ने अपने कविता-संग्रह ‘हिमालय दलित है’[3] में, अकाट्य खंडन किया है। ‘मेरा पहाड़’ उनके संग्रह की एक महत्वपूर्ण कविता है, जो पहाड़ी अस्मिता का इतिहास बताती है। यह कविता आरंभ में ही कहती है–
मुंडा कोल
गोंड नाग
या हड़प्पन बाद के
जो कोई भी थे मेरे पुरखे
उन्होंने कभी नहीं कहा, ‘मेरा पहाड़’
फिर किन लोगों ने कहा, ‘मेरा पहाड़’–
खसों ने बनाया खस देश
उन्होंने जरूर कहा, ‘मेरा पहाड़’।
गुप्तों के अधीन कत्यूरियों ने कहा, ‘मेरा पहाड़’।
आर्यों ने कहा, ‘गंगा मेरी तो मेरा पहाड़’।
नीलगिरी पर कब्जा छोड़े बिना
विंध्य को लांघकर
सारी बुद्ध प्रतिमाओं को
शिव बनाकर शंकराचार्य ने कहा, ‘मेरा पहाड़’।
मैदानी चंदों ने कत्यूरियों को कहा खदेड़ कर,
अब मेरा पहाड़।
नेपाली गोरखाओं ने चंदों से छीनकर
कहा गरजते हुए, मेरा पहाड़।
मल्ल पंवार कहते रहे मेरा पहाड़।
गंगोली मड़कोटी राजा ने भी कहा, मेरा पहाड़।
राजा का राजपुरोहित उप्रेती भी कहता रहा मेरा पहाड़।
गुमानी के मराठी पुरखे भी बोले मेरा पहाड़।
नेपाल के ज्योतिष
जिन्हें राजा ने दी
पोखरी की जागीर
वो भी कहने लगे, मेरा पहाड़।
महाराष्ट्र से आए डबराल ने तो
अपना नाम ही रखा
हिमाल के डाबर गांव पर
और कहा मेरा पहाड़।
लेकिन कवि रेखंकित करता है–
जो भी कहता है मेरा पहाड़।
वो प्यार नहीं करता/ वो जताता है दावा
जीती गई/ लूटी गई/ छीनी गई/ कब्जाई गई
और बांटी गई/ जमीनों पर/ जागीरों पर।
इन सारे दावेदारों को कवि झूठा और बेईमान घोषित करता है। उसके मुताबिक इन झूठे और बेईमान लोगों ने पहाड़ नहीं बनाया, बल्कि उस पर कब्जा किया। कवि कहता है कि जो असली दावेदार हैं, उन्हें पहाड़ के ब्राह्मणन-ठाकुरों ने अछूत कहा। पर, वे “मेरा पहाड़” नहीं कहते, बल्कि “मैं ही पहाड़ हूं”, यह कहते हैं। यथा–
और सबके सब कवि एक साथ भी कहें अगर …
मेरा पहाड़,
तो भी मैं नहीं कहूंगा मेरा पहाड़
मैं कह ही नहीं सकता कभी मेरा पहाड़
दो वजहों के चलते
एक तो ‘मेरा पहाड़’ यह मेरी भाषा नहीं,
और ज्यादा मजबूत वजह
मैं ही पहाड़ हूं।[4]
‘मैं ही पहाड़ हूं’ का मतलब है ‘पहाड़ दलित है’, लेकिन पहाड़ को देव-भूमि कहने वाले इस अभिव्यंजना को नहीं समझ सकते। देव-भूमि दलित कैसे हो सकती है? लेकिन कवि मोहन मुक्त ने इसका बेहतरीन विश्लेषण अपनी भूमिका में किया है। उन्होंने लिखा है, “हिमालय के इर्द-गिर्द जो एक खास किस्म का आभामंडल बना दिया गया है, वह एक विशिष्ट सांप्रदायिक और ब्राह्मणीवादी नॅरेटिव की पैदाइश है, जो हिमालय को दलित कहने पर आहत होता है।” और वह इसलिए आहत होता है, क्योंकि ब्राह्मणों ने ‘गीता’ में कृष्ण के मुख से कहलवा दिया है– “मैं स्थावरों में हिमालय हूं।” इस पर मोहन मुक्त की सटीक टिप्पणी है– “हिंदुओं का ईश्वर खुद को अचलों में हिमालय सदृश बताता है, और भले ही आप नास्तिक हों, लेकिन एक खास सांस्कृतिक प्रभाव में हिमालय को लेकर आपका मंतव्य साफ तौर पर हिंदुओं के ईश्वर के इस वक्तव्य से ख़ासा प्रभावित है। सांस्कृतिक प्रभाव हमेशा ही धार्मिक प्रभाव से ज्यादा गहरा और बुनियादी होता है, इसलिए इस कविता संग्रह की कविताओं का एक प्रमुख स्वर सांस्कृतिक प्रतिरोध भी है।”[5]
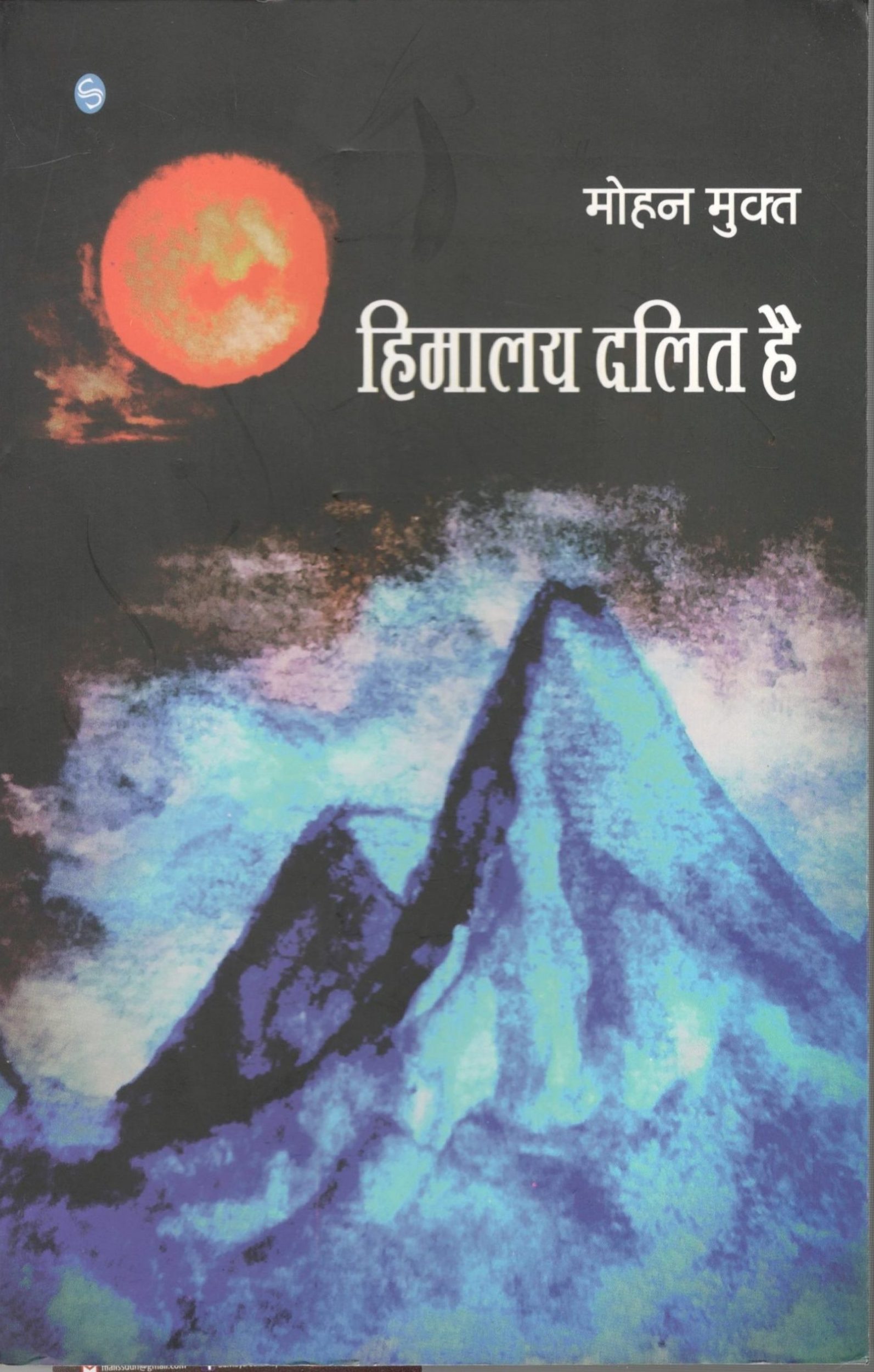
निस्संदेह, मोहन मुक्त की कविताओं में एक गहरा सांस्कृतिक प्रतिरोध है, जो हर कविता में न सिर्फ प्रभावित करता है, बल्कि एक नए दलित विमर्श को भी जन्म देता है। उदाहरण के तौर पर पहाड़ के कवि वीरेन डंगवाल की कविता ‘विद्वेष’ को लें, जो उनके कविता संग्रह ‘दुष्चक्र में सृष्टा’ में संकलित है। इस कविता में वीरेन कहते हैं–
यह बूचड़खाने की नाली है,
इसी से होकर आते हैं नदी के जल में
खून, चर्बी, रोयें और लोथड़े।
प्रेम की सुंदरता का निषेध करने वाले
इसी तट पर आते हैं हाथ-पैर धोने।
इस कविता में डंगवाल कहना चाहते हैं कि प्रेम के शत्रु, प्रेमियों की हत्या करने के बाद उस नदी के जल में हाथ-पैर धोने आते हैं, जिसमें बूचड़खाने से खून, चर्बी और लोथड़े बहकर आते हैं। यहां वीरेन डंगवाल ने प्रेम के हिंसक शत्रुओं की तुलना कसाई से की है, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है। कसाई, मांस खाने वालों के लिए मांस उपलब्ध कराने का पेशा करता है, किसी नफ़रत के अधीन होकर पशुओं की हत्या नहीं करता है, जबकि प्रेम के विरुद्ध हिंसा से भरे हुए लोग इसलिए हत्या करते हैं, क्योंकि वे अंतरधर्मीय या अंतरवर्णीय प्रेम के शत्रु हैं। मोहन मुक्त ने इसके प्रतिरोध में ‘प्रेम’[6] कविता लिखी, जिसने वीरेन डंगवाल धारणा को पूरी तरह उलट दिया है–
प्रेम का निषेध करने वाले
न तो बूचड़खाने की नाली देखते हैं
ना ही देखते हैं बूचड़ का चेहरा
वो देखते हैं
बूचड़ की दुकान खुली तो नहीं है
मंगलवार के दिन।
वे आते हैं
बूचड़ के टपरे टीन के दरवाजे पर लात मारते हैं
कटे बकरे को देखकर दहाड़ते हैं नफ़रत से
भो…ड़ी के मुल्ले
बहन…द कटुवे
यहीं काट देंगे तुझे मादर…द
कसाई के हाथ में बड़ा सा चाकू
उस वक्त
दुनिया की सबसे निरीह बेड़ी
दुनिया का सबसे बेकार औजार
कांपने लगता है…
आर्तनाद करता है कसाई का सबसे छोटा बच्चा
कसाई की बीवी दुआ बड़बड़ाती है
माहौल में भय के साथ तैरता है प्रेम भी।
मुख्यधारा की पहाड़ी कविता में जुल्म की यह तहरीर नहीं मिलती। सुनते हैं कि पहाड़ी लेखक शैलेश मटियानी ने कसाई की दुकान पर काम किया था। पर उनके साहित्य में वह अनुभव नहीं मिलता।
एक और ब्राह्मण कवि गिरीश तिवारी ‘गिर्दा’ को संबोधित कविता ‘गिर्दा से बात’[7] उत्तराखंड के एक ऐसे सामंती यथार्थ से अवगत कराती है, जिसका चेहरा मनुष्य-विरोधी है। मोहन मुक्त ने इस कविता की पृष्ठभूमि बताते हुए लिखा है कि “गिर्दा को मंगलेश डबराल ने पहाड़ का नागार्जुन कहा था, लेकिन … नागार्जुन ने बिहार के दलित नरसंहार पर एक बिल्कुल सटीक न सही, पर उम्दा कविता लिखी थी[8], जबकि तमाम सक्रियताओं में दिखने वाला गिर्दा अपने खुद के जिले में कफल्टा में हुए दलित नरसंहार पर चुप हो जाता है।” मोहन कहते हैं कि पहाड़ के तमाम कथित अपर कास्ट बौद्धिक और एक्टिविस्ट एक तंगनजरी के शिकार हैं। वे अपने ही गांव और परिवेश में दलितों के शोषण को न केवल अनदेखा करते हैं, बल्कि लोकसंस्कृति के नाम पर उसका महिमामंडन भी करते हैं। ‘गिर्दा से बात’ कविता उस दौर की है, जब उत्तराखंड में 1994 में शिक्षण संस्थाओं में पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के उत्तरप्रदेश सरकार के आदेश के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं का उग्र आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन के लगभग सभी नेता ब्राह्मण-ठाकुर थे, जिसे भाजपा और आरएसएस का ब्राह्मण-तंत्र चला रहा था। मोहन मुक्त ने सही लिखा है कि वे आरक्षण की आड़ में अलग राज्य की मांग दलित-आदिवासियों के लिए उत्तराखंड को यातना-गृह बनाने के लिए कर रहे थे। इस आंदोलन के ब्राह्मण-कार्यकर्त्ता गिरीश तिवारी ‘गिर्दा’ को संबोधित यह कविता बेहद विचारोत्तेजक है। यथा–
गिर्दा …
मैं भी कहना चाहता हूं एक बात
यह जानते हुए भी
कि आज ये सुनी भी नहीं जाएगी
लेकिन एक दिन
मान ली जाएगी जरूर …
पिरामिड की तरह पसरे
इन हरे पहाड़ों का भार
इनकी गर्त के अछूत पत्थर उठाते हैं गिर्दा,
पानी इन नदियों के अलावा भी है कई जगह मौजूद
कि जिनके लिए युद्ध लड़ा था तुमने
सुनो नदी के घोषित नायक
तुम्हारे गांव में
पानी आज भी कसमसाता हुआ कैद है
पवित्र नौलों के भीतर
वो पानी किसने बंधवा बनाया गिर्दा
और जमीन का यह टुकड़ा
जो तुमने बनाया है स्वायत्त
ये किसका है गिर्दा?
यह कविता यहीं नहीं रूकती है, आगे और भी गिर्दा से सवाल करती हैवह पूछती है, वह कफल्टा कांड पर मौन क्यों था? उस दिन उसका हुड़का[9] कहां था? हुड़का बजाने वाला उच्च और उसे बनाने वाला अछूत क्यों माना गया? इस विडंबना पर कवि कहता है–
हुड़का बनाया जाता है गिर्दा
नमक लगी खाल में
सुरों की मिठास नहीं होती
बदबू आती है
कितनी अजीब बात है न गिर्दा,
तुम हुड़का बजाकर भी हुड़क्या[10] नहीं हुए
मैंने हुड़का छुआ नहीं …
मैं हुड़क्या हो गया।
लोक-संस्कृति की एक अन्य कविता में कवि कहता है– मोहन उप्रेती, गिरीश तिवारी और नारायणदत्त तिवारी भी बजाते थे गजब का हुड़का, लेकिन उन्हें कोई भी हुड़क्या नहीं कहता। कवि कहता है–
जिस दिन आप कह दोगे कि
मोहन उप्रेती, गिरीश तिवारी भी
तीनों बेमिसाल हुड़क्या थे,
उस दिन से मैं भी लोकसंस्कृति का संरक्षण करूंगा
आपसे ज्यादा करूंगा।[11]
लेकिन कवि हुड़का बनाने में नहीं, बल्कि हुड़का को जलाने में दलित-मुक्ति देखता है। वह कहता है, उसकी यह बात एक दिन जरूर मानी जाएगी–
हुड़का बजाना बड़ी बात है गिर्दा,
लेकिन ज्यादा बड़ी बात है/हुड़का बनाना
और सबसे बड़ी बात है/हुड़का जलाना …
उसे जला डालना यही वो बात है गिर्दा
जो आज सुनी भी नहीं जाएगी
लेकिन एक दिन मान ली जाएगी जरूर।
कवि ने लोक-संस्कृति के तत्वों का बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। लोक-संस्कृति, जिसका जुआ दलितों के कंधों पर रखा हुआ है, सवर्णों के सामंती जीवन का एक बड़ा आधार है। इसके अंतर्गत कवि ने छोटी-छोटी बाइस कविताएं लिखी हैं, जिनके बिंब लघु खंड-काव्य जैसे प्रभावशाली हैं। एक तरह से कवि ने लोक-संस्कृति के शोषक चरित्र पर ये 22 लघु खंडकाव्य ही लिखे हैं। इन कविताओं को पढ़ते हुए, जिस लोक और संस्कृति के गूढ़ अर्थों के अमूर्त अनुभवों से गुजरना पड़ा, वैसे अनुभव दलित कविता में इससे पहले मुझे कभी नहीं हुए। मैं समझता हूं कि दलित कवियों ने हमेशा ही समाज और संस्कृति का पुनर्पाठ किया है, परंतु मोहन मुक्त ने पुनर्पाठ में भी नए समाज का निर्माण किया है। वह जिस तरह कविता में लोक और संस्कृति को परिभाषित करते हैं, वैसी परिभाषा अन्यत्र नहीं मिलती। कवि की लोक-संस्कृति की अवधारणा में ब्राह्मण-ठाकुरों के खेतों में दलितों का काम करना, फसल उगाना, काटना, उनके घर पहुंचाना, उनका मनोरंजन करना, यही लोक है, और उन्हीं की अधीनता में रहना ही संस्कृति है। यह संस्कृति ब्राह्मण-ठाकुरों को मुफ्त की सेवक-श्रेणी देती है, इसलिए वे हमेशा इस संस्कृति के संरक्षण पर जोर देते हैं। इस ब्राह्मणी संरक्षणवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का स्वर कवि की एक अन्य कविता ‘सुनो गुमानी’[12] में मिलता है, जो पहले पहाड़ी लोककवि गुमानी पंत[13] को संबोधित है। इस कविता में कवि का आक्रोश एक मशाल बनकर उभरता है। वह गुमानी की लोक-चेतना को कटघरे में खड़ा करते हुए कहता है–
पौराणिक सब पात्र तुम्हारे
आत्मनिष्ठ अब मात्र तुम्हारे
दिशाभ्रमित सब छात्र तुम्हारे
सुनो गुमानी!
बामण बनिए कब थे कंगले
कब बन गए चमार के बंगले
तू जैसे चाहे वैसे रंग ले
चित्र नहीं ये आम गुमानी।
औरत सर पर नहीं चढ़ाओ
बगल में डुमड़ा नहीं बिठाओ
लेसिंगटन[14] सलाम गुलामी।
सुनो गुमानी!
तुम जो चाहे वही हो गया
अंग्रेज गया, सब सही हो गया
दूध सड़कर, दही हो गया.
छलकाओ अब जाम गुमानी।
18वीं-19वीं शताब्दी के सभी ब्राह्मण नेता और बुद्धिजीवी गुमानी पंत जैसे ही थे, जो एक तरफ अंग्रेजों की चापलूसी करके सारे लाभ ले रहे थे, और दूसरी ओर अपनी संस्कृति पर खतरा बताकर ब्राह्मणवाद का पुनर्जागरण कर रहे थे।
लोक-संस्कृति की ऐसी ही एक महत्वपूर्ण कविता ‘छलिया चला जाएगा’[15] है, जो उत्तराखंड में शादियों के अवसर पर तलवार लेकर नाचने वाले ‘छलिया’ कहलाने वाले दलित के बारे में है। इस लंबी कविता का अर्थ इसकी नौवीं कविता में खुलता है, जिसमें कवि जोतीराव फुलेले की ‘गुलामगिरी’ की शैली में कहता है–
तलवार सबसे पहले किसके हाथों में आई?
–लोहार के।
तलवार सबसे आखिर में किसके हाथों में बची रही?
–छलिया के।
लोहार ने तलवार से क्या काम किया?
कुछ काटा?
नहीं।
वह लोहा काटना जानता था
लोहे से कुछ काटना नहीं।
छलिया ने तलवार से क्या काम लिया?
कुछ काटा?
नहीं।
वो लोहे के साथ नाचना जानता था
लोहे से कुछ काटना नहीं।
लेकिन इस कविता की दलित-चेतना यहां है–
जिनकी जिंदगी लोहे के साथ बीती
वो सैनिक नहीं थे
जिनकी पत्नियों ने चुम्बनों से लोहे का स्वाद जाना था
वो भी सैनिक नहीं थे
वो विद्रोही भी नहीं थे।
वो क्या थे?
वो खुद लोहा थे
खदानों से निकले
पिघले जले पिटे ढले
औजार बने तो इस्तेमाल हुए लोहे के खिलाफ ही।
बस आखिरी सवाल–
वो हाथ किसके हैं
जो लोहे को लोहे की जिंदगी से
इतनी दूर ले आए हैं?
‘वे हाथ किसके हैं?’ जिस दिन पहाड़ के ही नहीं, भारत भर के शिल्पकार यह जान जाएंगे, उसी दिन वे अपने शोषक, अपने शत्रु के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे। लोक-संस्कृति की सत्रहवीं कविता[16] में कवि ने बहुत शिद्दत से दलितों की उस गुलाम लोक-संस्कृति को रेखांकित किया है, जिसमें वे शासकों के प्रशस्तियां गाते हैं। कवि कहता है– ‘इन्हें कैसे कह दूं लोक?’ नम्बूदरी, शंकराचार्य, कत्यूरियों, आर्यों, खसों के आने के बाद, और मुंडा और कौलों के डोम बन जाने के बाद–
क्या रहा होगा कोई गीत मुक्त?
जो मुक्त नहीं, वो लोक नहीं।
जब राज्य आता है
जब धर्म छा जाता है,
फिर लोक नहीं बचता,
बस गुलाम बचते हैं।
ब्राह्मणों की लोक-संस्कृति में महिलाओं का क्या स्थान है? इस पर कवि ने दो चित्र प्रस्तुत किए हैं।[17] पहला चित्र है–
वो ना तो खस थी, ना आर्य …
उसने कभी नहीं किया आक्रमण, घुसपैठ या कब्जा,
उसने नहीं बनाए साम्राज्य
वो है शाश्वत मूल निवासी
लेकिन उससे पूछना तो कभी
तुम्हारा घर कहां है? कहां है?
दूसरा चित्र गाली है, जो लोक-संस्कृति में औरत को में दी जाती है–
उसने अपनी मज्जा को खाद की तरह
खेतों में बिखेर दिया
लेकिन उसने जब भी यह कहना चाहा
जो महसूस किया
उसे एक ही गाली दी गई
उसे कहा गया पातर
जो एक नीच जाति की नाचने वाली औरत का नाम है।
लोकसंस्कृति से ही जुड़ी एक कविता ‘जड़ों की ओर’[18] है। गांधी भी चाहते थे लोग जड़ों की ओर लौटें। जयशंकर प्रसाद का स्वर्ण युग भी अतीत ही था। दयानंद और विवेकानंद ही नहीं, सारे ब्राह्मण कवि इसी अतीत के अनुरागी हैं, क्योंकि जड़ों की ओर लौटने का मतलब है ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान, जिसमें मनुष्य मनुष्य से प्रेम करने योग्य नहीं रहता। यथा–
लौटो जड़ों की ओर
जब वे कहते हैं
तो आप लौट पड़ते हैं
घर की ओर, रहवास की ओर, जमीन की ओर,
गांवों की ओर, कबीलों की ओर
और आखिरकार आप सिमटकर रह जाते हैं
इंसानद्रोही, जीवद्रोही, चैतन्यद्रोही, पदार्थद्रोही।
लेकिन कवि के जड़ों की ओर लौटने का अर्थ है पदार्थ की ओर लौटना, वैज्ञानिक सोच का बनना। यथा–
जब मैं कहता हूं लौटो जड़ों की ओर
तो मैं उस जगह की बात करता हूं
जहां विज्ञान और दर्शन में कोई विरोध नहीं।
जब मैं कहता हूं लौटो जड़ों की ओर
तो मैं इसी जड़ की बात करता हूं
मैं पदार्थ की बात करता हूं।
लोक-संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा है ढोल। बिना ढोल के मनोरंजन और नाच-गाना कैसा? लेकिन यह ढोल कौन बजाता है? क्या सवर्ण? नहीं। ये ढोल दलित बजाते हैं, जो अपने गले में डाले रहते हैं। पहाड़ी कवि मंगलेश डबराल ने ढोल बजाने वाले केशव अनुरागी पर इसी नाम से एक कविता लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था– “ढोल एक समुद्र है साहब/केशव अनुरागी कहता था/इसके बीसियों टाल हैं सैकड़ों सबद/और कई तो मर खप गए/हमारे पुरखों की ही तरह।” महेश चन्द्र पुनेठा ने इस कविता को दलित विमर्श की महत्त्वपूर्ण रचना माना है, जबकि मोहन मुक्त इस कविता में सामंतवाद का समर्थन देखते हैं। इसलिए उन्होंने इसके जवाब में ‘अनुरागी और डबराल’[19] नाम से एक विचारोत्तेजक कविता लिखी। यह कविता, जो इस संकलन की सबसे श्रेष्ठ रचना है, उस ब्राह्मण-सोच पर गंभीर सवाल खड़े करती है, जो लोक-संस्कृति के नाम पर दलित को मुक्त नहीं होने देती। वह कहते हैं–
डबराल नहीं जान पाया है अब तक
कि ढोल का समुद्र खारा होता है
जिनके हिस्से समुद्र-मंथन का सारा अमृत आया है
इसलिए हो सकता है कि ये लोग तुम्हें महान कलाकर बताएंगे
अफ़सोस जताएंगे तुम्हारे अछूतपन पर
धिक्कारेंगे उस समाज को, जिसने तुम्हें अछूत बनाया
लेकिन ये लोग कभी हाथ बढ़ाकर नहीं कहेंगे
कि यार अनुरागी बहुत हो गया
सदियां गुजर गई हैं तुम्हें इस समुद्र के भीतर
थक गए होगे यार, अब बाहर आ जाओ।
सामंती कवि कभी नहीं चाहेगा कि दलित अपनी गुलामी की कला से मुक्त हो। लेकिन मुक्ति तो गुलामी से मुक्त होने में ही है। कवि कहता है–
नहीं अनुरागी ढोल समुद्र नहीं होता
और तुम ढोल के भीतर नहीं रहते
कोई ढोल के भीतर नहीं रहता
यह दुनिया जिसमें तुम रहते हो
और डबराल रहता है
यह दुनिया ही रहती है दरअसल एक खोल के भीतर
तुम ढोल के भीतर नहीं रहते
दुनिया खोल के भीतर रहती है।
जिस दिन तुम इस ढोल को कांधे से खींचकर
इसमें आग लगा दोगे
उस दिन यह खोल अपने आप जल जाएगा अनुरागी
उस दिन दुनिया मुक्त होगी
उस दिन तुम मुक्त होगे
और मुक्त हो जाएगा डबराल भी।
इस सामंतवाद को ‘गांव में’[20] कविता और भी शिद्दत से रेखांकित करती है। गांव पर लगभग सभी दलित कवियों और लेखकों ने लिखा है, क्योंकि दलितों के लिए गांव के अनुभव सवर्णों के अनुभवों से एकदम अलग हैं। डॉ. आंबेडकर ने लिखा है कि सवर्णों के लिए गांव उनके स्वर्ग हैं, जबकि दलितों के लिए वे साक्षात घेटो (यातना-गृह) हैं। उन्होंने लिखा है कि हिंदू गांव वर्णव्यवस्था के ‘वर्किंग प्लांट’ हैं। इन गांवों में हिंदू और अछूत इस तरह रहते हैं, जैसे दो अलग-अलग दुश्मन राष्ट्रों के नागरिक हों।[21] मोहन मुक्त की ‘गांव में’ कविता डॉ. आंबेडकर के ही विचार का प्रतिनिधित्व करती है। वह लिखते हैं–
गांव में कोई चीज नहीं होती अकेली
वहां हमेशा दो होते हैं
दो रास्ते
दो नौले
दो थान
दो पुजारी
दो देवता।
गांव में गुरू होता है
गांव में घुरू होता है
गांव अकेला दीखता है जो
उसके भीतर होते हैं दो
दोनों के बीच रहती सीमा
दुश्मन देशों जैसी सीमा
क्या एक गांव के भीतर रहते हैं दो देश
गांव में साथ रहते हैं साम्राज्य उपनिवेश।
इस कविता और दलित कवि मलखान सिंह की कविता ‘हमारे गांव में’ अद्भुत समानता है, जो अब्दुल बिस्मिल्लाह की कविता ‘हमारे गांव में’ के जवाब में लिखी गई थी। यह कविता इन पंक्तियों से आरंभ होती है– “हमारे गांव में भी/ कुछ हरि होते हैं/कुछ जन होते हैं/जो हरि होते हैं/ वह जन के साथ न उठते हैं/न बैठते हैं/ न खाते हैं/न पीते हैं/यहां तक कि जन की परछाई से भी परहेज करते हैं।”[22]
दलित विमर्श की एक महत्वपूर्ण कविता ‘भू-कानून’[23] है, जो उत्तराखंड में बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर रोक लगाने के लिए एक संभावित कानून के विरोध में लिखी गई है। मोहन मुक्त इस कविता में उन सवर्ण घुसपैठियों को बेदखल करने पर जोर देते हैं, जो बाहर से आकर पहाड़ों में मूल निवासियों के जल-जंगल-जमीन पर कब्जा करके डेरे बनाए बैठे हैं। इन्हीं सब कब्जाधारी बाहरी लोगों के हाथों में शासन-सत्ता है, जो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए एक रात दलित के घर में रहने और खाने का राजनीतिक ड्रामा करते हैं। इस राजनीतिक नौटंकी को कवि ने एक लंबी कविता ‘सामंत तुम फिर आ गए’[24] लिखी है, जो कवि के अनुसार 2010 में शुरू होकर 2019 में पूरी हुई थी। सवर्ण नेताओं के सामंती चरित्र को बेपर्दा करती इस कविता में कवि कहता है–
नहीं जान सकते हो एक रात में तुम
कि जब मेरी मां तुम्हारी ड्योढ़ी के बाहर
गाती है चैत की ऋतु
तो जिस फासले से तुम्हारी मां
उसकी धोती में डाला करती है
महुआ, भांग के बीज और बीड़ी का बंडल
वो फासला बहुत बड़ा होता है
एक रात से बड़ा/एक प्रकाशवर्ष से बड़ा
तुम क्या एक रात में आकाशगंगा को पार कर सकते हो?
कवि में इन सामंतों के लिए सहानुभूति नहीं, आक्रोश है, जो दलित-चिंतन की ताकत है–
कि जब तुम मेरी बीवी को भाभी
और मेरे बाप को दाज्यू कहते हो
तो तुम्हारी आत्मीयता पोस्टमार्टम के मुर्दे से ज्यादा बास मारती है
तुम्हारी आत्मीयता बदबूदार है
मैं दुनिया की सभी बदबुओं को जानता हूं
तुम इस रात आए हो एक नई दुर्गंध के साथ।
इस कविता के दूसरे भाग में, कवि ने दलितों के घर आने वाले सामंतों के असली मंसूबे का पर्दाफाश किया है। यथा–
तुम वोट के लिए नहीं आते
कोई डर है
जो बार-बार तुम्हें मेरे पास ले आता है
तुम दरअसल आते हो
अनंत की ओर इशारा करती मेरी उंगली को देखने
कि स्याही लगी मेरी उंगली
अभी भी सीधी-सीधी ही खड़ी है
या वो कहीं मुड़कर
तैनात तो नहीं हो गई है
बंदूक के घोड़े पर।
ब्राह्मणों द्वारा रचे गए एकलव्य के मिथक पर भी कवि ने ‘अंगूठा’[25] कविता लिखी है। इसमें कवि एकलव्य को अंगूठा काटकर देने के लिए धिक्कारता है, और कहता है कि अच्छा अगर वह अपना सर ही काटकर दे देता, क्योंकि झुका हुआ सर कटे हुए सर से ज्यादा उपयोगी नहीं होता है। यहां कवि ब्राह्मण मिथक का विश्लेषण नहीं कर सका है। उसने ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित कहानी पर विश्वास किया, जो सही नहीं है। एकलव्य जैसा वीर कभी भी अंगूठा काटकर नहीं दे सकता था। सच यह है कि ब्राह्मण द्रोण ने राज्य-शक्ति के बल से एकलव्य का बलपूर्वक अंगूठा काटा था। यह एकलव्य की गुरू-दक्षिणा नहीं थी, क्योंकि एकलव्य ने कभी द्रोण से धनुर्विद्या नहीं सीखी थी, बल्कि यह द्रोण की वैसी ही खुली हिंसा थी, जैसी ब्राह्मणों ने शंबूक के लिए रची थी। अफ़सोस कि कवि ने मिथक का पुनर्पाठ नहीं किया, जबकि पुनर्पाठ के बिना दलित विमर्श संभव ही नहीं।
इसी तरह ‘मेरे पुरखे’[26] कविता में भी इतिहास की ठीक से गवेषणा नहीं हुई। यह सच है कि हमारे पुरखे इतिहास में दर्ज नहीं हैं, लेकिन वे आर्यों की विजयगाथाओं – वेदों और पौराणिक मिथकों में – अपने पूरे शौर्य के साथ दर्ज हैं। उनके भी पुनर्पाठ की जरूरत है। हालांकि नास्तिक जननेता पेरियार के जन्मदिन पर लिखी गई कविता ‘ईश्वर’[27] में कवि ने ईश्वर की अच्छी व्याख्या की है– “मेरा ईश्वर मेरे पुरखों से लूट लिया गया था/ हालांकि लुटेरों ने बेकार चीज लूटी थी/ लेकिन अब उनका डुप्लीकेट ईश्वर मुझे नहीं चाहिए।” हमारे पुरखों के धर्म और कौशल की हर चीज ब्राह्मणों ने डुप्लीकेट ही तैयार की है।
मोहन मुक्त की एक बेहद विचारणीय कविता ‘काला ब्राह्मण’[28] है। काला ब्राह्मण वह पुरोहित वर्ग है, जो दलित वर्गों में उभरे मध्यवर्ग में पैदा हुआ है। वह दलितों के घरों में जाकर धार्मिक संस्कार-अनुष्ठान कराता है। कवि के अनुसार, वह विवाह, नामकरण, उपनयन सबमें पारंगत है। लेकिन दलितों का उपनयन आश्चर्य में डालने वाली बात है। ब्राह्मणों ने दलितों का उपनयन कब स्वीकार कर लिया? पर कवि ने यह रेखांकित किया है कि काला ब्राह्मण भी जातिवाद को मानता है। यथा, “गोरे बामण को देखते ही वह बदल लेता है रास्ता/ मेहतर के सामने/ वो कुछ गोरा सा हो जाता है।” यह काला ब्राह्मण दिखने में कृशकाय है, मगर उसकी ताकत बड़ी है। कवि कहता है–
ब्राह्मणत्व-रहित काला बामण
लगता है बड़ा अकिंचन
दुर्बल सा दिखता है छवि है कृशकाय
असल में काला बामण है बहुत ताकतवर
अकेले ही रोक रखा है उसने करोड़ों की तादाद को
हाशिए के पार।
हाशिए के पार या हाशिए पर? ये दोनों एक नहीं हैं। इसलिए भ्रम पैदा करता है। दलित वर्ग हाशिए पर हैं, इसमें संदेह नहीं। किंतु, उनके हाशिए के पार जाने का मतलब है हाशिए की स्थिति से मुक्ति। क्या सचमुच दलित पुरोहित वर्ग के कारण करोड़ों दलितों की मुक्ति हुई है? शायद नहीं। कवि भी वास्तव में यही कहना चाहता है कि सामाजिक यथास्थिति बनाए रखने के लिए काला ब्राह्मण भी वही भूमिका निभा रहा है, जो गोरा ब्राह्मण निभाता है।
अंत में ‘हिमालय दलित है’[29] कविता को लेते हैं, जिस पर मोहन मुक्त ने अपने कविता संग्रह का नामकरण किया है। इस कविता की ये पंक्तियां विचारोत्तेजक हैं–
कहते हैं ईश्वर का घर है पवित्र है
मैं कहता हूं दलित है
गुस्से में कांपते हैं पूछते हैं कैसे?
मेरा जवाब–
अगर इंसान दलित हो सकते हैं तो पहाड़ क्या चीज हैं।
इस संबंध में संग्रह के आरंभ में कवि का ‘हिमालय दलित है’ शीर्षक निबंध पढ़ा जाना चाहिए, जो अकाट्य तर्कों से हिमालय के ब्राह्मणी आभामंडल का खंडन करके उसे दलित साबित करता है। जिन कवियों और बुद्धिजीवियों ने हिमालय को प्रहरी, संतरी और रक्षक कहा है, कवि उनका भी अकाट्य खंडन करता है। वह जोर देकर कहता है कि “हिमालय कभी भी स्थाई और बंद बार्डर नहीं रहा। इसके आर-पार लोगों और संस्कृतियों का आवागमन होता रहा है।” कवि का कथन है कि हिमालय में वर्तमान में निवास करने वाली दलित जातियां इस भू-भाग में बसने वाली सबसे पहली इंसानी कौमें हैं। लेकिन इस आधार पर कवि का दावा हिमालय को दलित कहने का नहीं है, बल्कि उसका आधार इससे भी महत्वपूर्ण है, जिसमें कवि कहता है– “मेरे लिए केवल इंसान ही प्राथमिक है और रहेगा और दुनिया ऐसी हो कि सभी के लिए इंसान प्राथमिक हो जाए। इसके लिए लड़ता हुआ, प्रतिरोध करता हुआ इंसान चाहिए, लड़ता हुआ, प्रतिरोध करता हुआ दलित चाहिए, लड़ता हुआ, प्रतिरोध करता हुआ हिमालय भी चाहिए और हमारे पास तीनों मौजूद हैं, इसलिए मैं पूर्ण रूप से सचेत और मुतमईन होकर यह घोषणा करता हूं कि हिमालय दलित है।”
समीक्षित पुस्तक : हिमालय दलित है
कवि : मोहन मुक्त
प्रकाशक : समय साक्ष्य, देहरादून
मूल्य : 295 रुपए
[1] गणेशशंकर विद्यार्थी रचनावली, संपादक : सुरेश सलिल, अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2004, खंड 1, पृष्ठ 257
[2] वही
[3] हिमालय दलित है, मोहन मुक्त, समय साक्ष्य, देहरादून, 2022
[4] वही, पृष्ठ 63-65
[5] वही, पृष्ठ 23
[6] वही, पृष्ठ 259
[7] वही, पृष्ठ 235-238
[8] हरिजन गाथा, नागार्जुन की चर्चित कविता है, जो बिहार में दलित नरसंहार पर आधारित है।
[9] कवि के अनुसार कुमाऊं हिमालय के हिस्सों में बजाया जाने वाला एक प्रसिद्ध वाद्य, जो बैल की खाल से तैयार किया जाता है।
[10] हुड़का बनाने और बजाने वाली एक अछूत जाति
[11] हिमालय दलित है, पृष्ठ 214
[12] वही, पृष्ठ 204-207
[13] कवि के अनुसार 18वीं सदी का एक ब्राह्मणवादी लोककवि, जिसे वर्तमान में उत्तराखंड के उच्च जातीय बुद्धिजीवी लोकचेतना का वाहक बताते हैं।
[14] कवि के अनुसार, गुमानी के समय में अल्मोड़ा का अंग्रेज कमिश्नर, जिसकी चापलूसी में गुमानी ने ‘लेसिग्टन की सलामी’ कविता लिखी थी।
[15] हिमालय दलित है, पृष्ठ 208
[16] वही, पृष्ठ 220-230
[17] देखिए, वही, अठारहवीं कविता, लोक्संकृति और औरतें – 1 और 2, पृष्ठ 221-222
[18] वही, पृष्ठ 70
[19] वही, पृष्ठ 186
[20] वही, पृष्ठ 72
[21] देखिए, डा. बाबासाहेब आंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वाल्यूम 5 में चैप्टर : अनटचेबुल्स ऑर द चिल्ड्रेन ऑफ इंडियाज घेट्टो
[22] सुनो ब्राह्मण, मलखान सिंह, परिवेश, चंदौसी, मुरादाबाद, पहला संस्करण 1996, पृष्ठ 26
[23] हिमालय दलित है, पृष्ठ 83
[24] वही, पृष्ठ 89
[25] वही, पृष्ठ 103
[26] वही, पृष्ठ 111
[27] वही, पृष्ठ 114
[28] वही, पृष्ठ 127
[29] वही, पृष्ठ 120
(संपादन : नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें
मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया