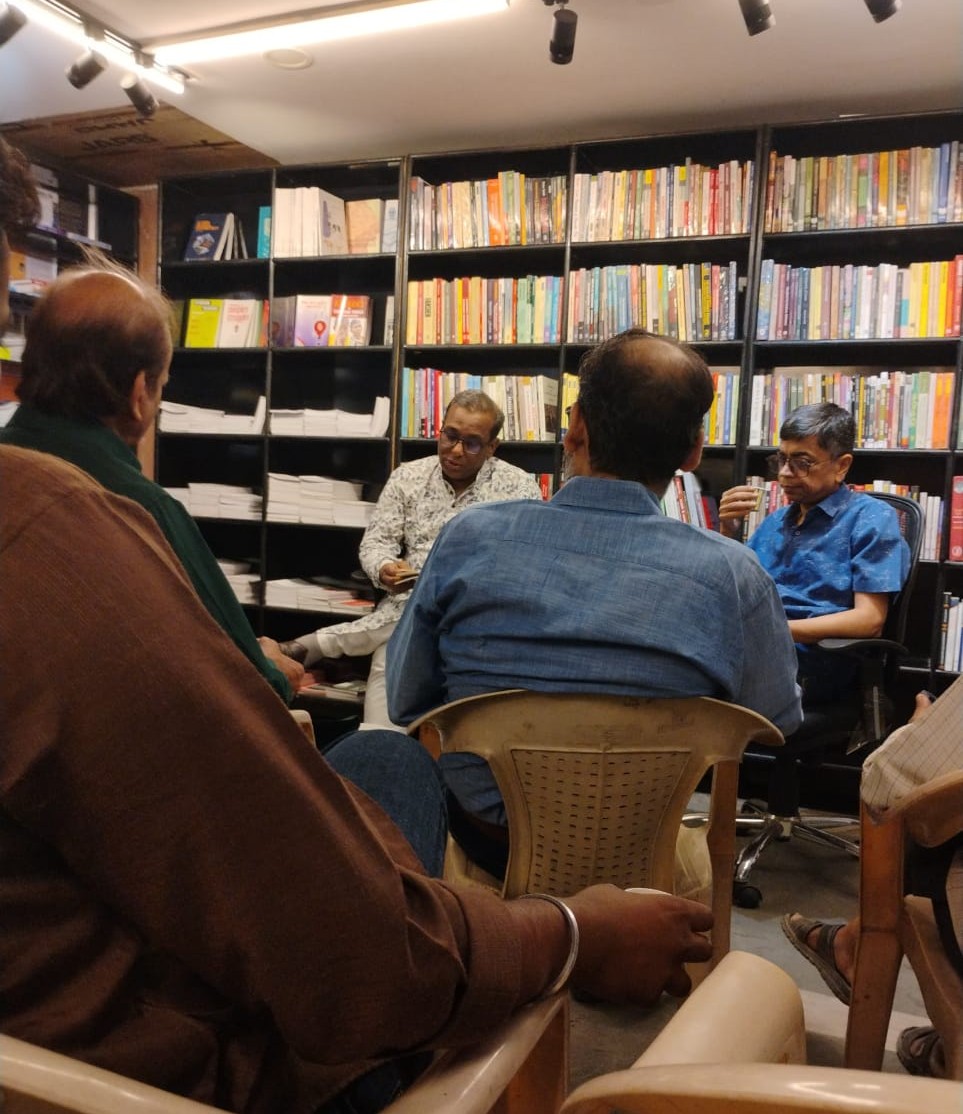लक्ष्मण उटकर द्वारा लिखित और निर्देशित तथा रोहन शंकर द्वारा सह-लिखित ‘मिमी’ एक हिंदी व्यंग्य फिल्म है। इसमें कृति सेनन, साई थमनकर, एवलिन एडवर्ड्स और पंकज त्रिपाठी मुख्य भूमिकाओं में हैं। हालांकि यह फिल्म वर्ष 2011 में आयी समृद्धि पोरे द्वारा निर्देशित मराठी फिल्म ‘मला आई व्हायचय’ की रीमेक है। फिल्म में रूहानी संगीत ए.आर. रहमान का है। यह फिल्म दर्शकों को भारतीय सरोगेट मां के जीवन से गुजारती है, जिसे बच्चे के जैविक माता-पिता द्वारा गर्भावस्था के ऐसी अवस्था में छोड़ दिया जाता है, जब न तो वो गर्भपात करा पाती है ना ही बच्चे को जन्म देकर पालने की स्थिति में रहती है। पूरी कहानी मिमी के जीवन में आये सामजिक एवं शारीरिक उथल-पुथल को दिखाती है।
फिल्म की पृष्ठभूमि राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में फिल्माई गयी है। क्षेत्र का यथार्थ और सरोगेसी पर दिखाई गयी कहानी में कोई जुडाव नजर नहीं आता है।
सरोगेसी की कीमत
कहानी की शुरूआत एक अमेरिकी जोड़े के द्वारा अपना बच्चा पैदा करने के लिए एक किराये की गोद की तलाश में राजस्थान आने से होती है। वहां उन्हें एक टैक्सी ड्राइवर भानू से मुलाक़ात होती है, जो उन्हें सरोगेट मां तलाशने में मदद करता है। अंततः वह एक कार्यक्रम में एक नर्तकी से प्रभावित हो जाते हैं, जिसका नाम मिमी होता है। वह दिखने में सुंदर और शारीरिक रूप से तंदरूस्त नज़र आती है। इसी के साथ अमेरिकी जोड़े की तलाश ख़त्म होती है। दूसरी ओर मिमी एक महत्वकांक्षी लड़की है, जिसकी उम्र 25 साल है। वह बॉलीवुड में हीरोइन बनने के ख्वाब संजोती है। मुंबई फिल्म उद्योग से जुड़े जॉली नामक एक शख्स से लगातार फ़ोन पर उसकी बातचीत होती रहती है। वह उसे मुंबई आने के लिए प्रेरित करता रहता है। लेकिन पैसों के अभाव में मिमी जा पाने में असफल होती नज़र आती है।
भानू जब उसे सरोगेट मदर बनने के संपर्क करता है तो वह चौंक जाती है। पहले तो उसे विश्वास नहीं होता है कि बिना शारीरिक संबंध बनाये भी बच्चा पैदा किया जा सकता है। हालांकि वह मना करती है। इसके पीछे फ़िल्म जगत में अभिनेत्री बनने की उसकी तमन्ना और शारीरिक सुंदरता के खो जाने का डर उसके मन में होता है। लेकिन जैसे ही भानू उसे कहता है कि इस काम के बदले उसे बीस लाख रुपए मिलेंगे तो वह अपने ख्वाबों को पूरा करने के इरादे से हां कर देती है।

कहानी रफ्ता-रफ्ता आगे बढ़ती है। अमेरिकी जोड़ा बहुत खुश नज़र आता है। संतानहीन से संतानवान बनने का उनका सपना पूरा होने जा रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डाक्टर द्वारा यह बताया जाता है कि मिमी के गर्भ में पल रहा उनका बच्चा मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है। वह अमेरिकी जोड़ा अंदर से टूट जाता है। उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है जिसके लिए वे भारत में एक साल से भटक रहें थे ताकि उन्हें स्वस्थ मां मिल सके और उनका होने वाला बच्चा पूरी तरह से हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त हो। वे बच्चे को स्वीकारने से भानू को मना कर देते हैं।
भारतीयता के परिप्रेक्ष्य में सरोगेसी
भारतीय सिनेमा जगत में सरोगेसी का विषय नया है। ‘मिमी’ फिल्म में कहानी नयापन और समसया की गंभीरता नजर आती है। जो समस्या सरोगेट मां इस फ़िल्म में झेलती है, वास्तविकता से दूर नहीं लगती। अव्वल तो यह कि कोई इस बात को स्वीकारने को ही तैयार नहीं होता है कि बिना शारीरिक संबंध के बच्चे पैदा किये जा सकते हैं। असल में यह आइडिया संतानहीन महिलाओं के घर में खुशहाली लाने के लिए लाया गया जो कभी मां नहीं बन सकती हैं। मगर इसका चलन उन अमीर परिवारों में ज़्यादा फैला, जो मां तो बन सकती हैं, मगर इस चलते कि कौन नौ महीने बच्चें को पेट में पाले और असहनीय दर्द झेले, सरोगेसी का विकल्प चुन लेती है। मगर इसकी पहुंच सीमित है क्योंकि यह बहुत खर्चीला है।
दरअसल, सरोगेसी एक ऐसा मुद्दा है, जिसके भारत जैसे तीसरी दुनिया के देश में जटिल कानूनी, सामाजिक, वित्तीय और नैतिक अर्थ हैं। हाशिए पर रहनेवाले, कम आय वाले समूहों की कई महिलाएं अक्सर इसे खुद को और अपने परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए एक व्यवहार्य तरीके के रूप में देखती हैं। मगर इस बीच वे तमाम समस्याओं का सामना भी करती हैं, जैसा कि ‘मिमी’ फिल्म में दिखाया भी गया है।
मगर यह फिल्म कहीं न कहीं वास्तविकता से कम नजदीक ही लगती है, क्योंकि भारत जैसे देश में एक मध्यवर्गीय परिवार द्वारा अपनी बेटी के बिना शादी के पैदा हुए बच्चे को स्वीकारना अपवाद ही संभव है। कहानी में बहुत सारी परतें हैं, मगर निर्देशक ने अपनी सुविधानुसार उन्हें खोला है।
कहानी का मध्यांतर
सरोगेट मां को अनेक तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अगर वह परिवार से छुपा कर करती है तो उसे नौ महीने तक कहीं दूर झूठ बोलकर रहना पड़ता है और अगर जिनके लिए वो सरोगेट मदर बनी है, वे ही भाग जाएं तो फ़िर उसके पास दो ही विकल्प बचते हैं। या तो गर्भपात करा ले या फिर पैदा करके समाज के ताने सुनती रहे, परिवार वालों की मारपीट सहे और फ़िर आजीवन कुंवारी रहकर बच्चे का लालन-पालन करे। साथ ही जो पहले से ही शादीशुदा होती हैं, जिनके अपने बच्चे होते है हैं तो उनके लिए समस्याएं भी तब बहुत बढ़ जाती हैं जब आखरी अवस्था में बच्चे के जैविक माता-पिता पीछे हट जाते हैंतो उसके ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ आन पड़ता है। गरीबी से छुटकारा पाने के लिए जिस चीज़ का वे सहारा लेती हैं, वही उनके लिए समस्या बन जाती है। हालांकि भारत में इस संबंध में क़ानूनी प्रावधान तो हैं, मगर लचर व्यवस्था के चलते अडचनें भी अनेक हैं।
वैसे तो फ़िल्म पूरी सरोगेसी के मुद्दे को केंद्र में रखकर बनायी गयी है, मगर कहानी के भीतर न जाने कितने ही और मुद्दे बारीकी से ही सही अलग-अलग मौकों पर दिखायी पड़ते हैं। खासतौर पर धार्मिक, रंगभेद, जाति, आर्थिक असम्पनता, स्त्रीविमर्श, महत्वकांक्षा, करियर इत्यादि।
जाति-धर्म का दंश
फिल्म में मिमी को होनेवाली प्रसव पीड़ा को बहुत ही भयावहता से फिल्माया गया है, जिसे देखकर मां बननेवाली हर स्त्री अपने दर्द को महसूस कर सकती हैं। साथ ही स्तनपान की महत्ता पर भी जोर दिया गया है। फिल्म के एक दृश्य में मिमी की मां कहती है कि दिन में 10 बार बच्चे को दूध पिलाना है। फिल्म में रंगभेद का मुद्दा भी उभरकर सामने तब आता है जब बच्चा पैदा हो जाता है और मिमी की मां कहती है कि “ऐसा नाती देने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ़ करती हूं।” साथ ही, मिमी के पिताजी एवं उसकी दोस्त शमा द्वारा भी गोरेपन पर टिप्पणी करना कि ऐसा गोरा बच्चा पूरे शहर में नहीं होगा और फ़िर पूरे शहर में उस गोरे बच्चे की चर्चा, आश्चर्य एवं कोलाहल कहीं न कहीं रंगभेद को बढ़ावा देता है। यह जाहिर तौर पर काले रंग की अवमानना है।
फिल्म के एक दृश्य में भानू द्वारा यह टिप्पणी कि “गोरेपन को लेकर इतना पागलपन है, ऐसे कैसे देश रंगभेद से उभरेगा?” के जरिए प्रगतिशीलता का परिचय भी दिया गया है। फिल्म में राजस्थान में बाल-विवाह पर भी कटाक्ष किया गया है। इसके अलावा मुस्लिम समाज में कुरीतियों पर भी ध्यान दिलाया गया है। जैसे मस्जिद में महिलाओं का प्रवेश वर्जित होना, तीन तलाक और इससे कारण होनेवाली परेशानियां। हिन्दू समाज में मुसलमानों के प्रति सोच का प्रतिबिंब भी इस फिल्म में नजर आती है। दरअसल फिल्म के एक हिस्से में सवर्ण परिवार द्वारा मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार करता दिखाया गया है। जैसे कि वे कैसे एक दूसरे के दुःख-सुख में शरीक होते हैं। मगर एक जगह जब मिमी के पति को लेकर मुद्दा छिड़ता है तब अफवाह के मार्फ़त घर में जब यह बात पहुंचती है कि पति मुस्लिम है तो सारे परिवार वाले अपना सर पकड़ लेते है और मिमी को भला बुरा कहने लगते हैं। सवर्ण समुदाय का यह दोहरा मापदंड बहुत कुछ कह जाता है। बाद में जब भानू (जो कि संयोगवश परिस्थिति को संभालने के लिए मिमी का पति बनाया जाता है ) का पहचान पत्र देखा जाता है और उसमें नाम मुस्लिम न होकर भानू प्रताप पांडे होता है, तब मिमी की दादी आगे बढ़कर उसे सवीकार लेती है और घर के अन्य सदस्यों को भी गर्भवती मिमी की देखभाल करने के लिए कहती है। मिमी के माता-पिता चैन की सांस लेते हैं कि अच्छा हुआ कि लड़का मुस्लिम नहीं है।
अगर देखा जाय तो राजस्थान जैसे प्रदेश में अंतरजातीय विवाह एक अभिशाप है। इस फिल्म में तो लड़का सवर्ण है, भले ही दूसरी जाति से है तो परिवार वालों द्वारा आसानी से स्वीकार लिया जाता है। लेकिन यदि वह दलित समुदाय से आता तो क्या मिमी की दादी की स्वीकार्यता समान रहती? परिवार वालो की प्रतिक्रिया दोनों स्थितियों में एक समान रहती? इससे मालूम चलता है कि जातिगत बंधन तोड़ने की आज़ादी किसको है और कौन इस तरह के कदम उठा पाने के लिए स्वतंत्र हैं!
स्त्री चेतना की दुर्गति
फिल्म का अंत मातृत्व पर आकर सिमट जाता है, जहां मिमी जैसी नारियों को यह संदेश दिया जाता है कि बच्चे पालना, उनकी ख़ुशी में अपनी ख़ुशी खोजना, मां के लिए इन सबसे बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं। इसके लिए चाहे उन्हें अपने सपनों की बलि क्यों न चढ़ानी पड़े। भारतीय समाज समझता है कि इसमें सबकी भलाई है। यह समाज और परिवार सभी महिलाओं से यही अपेक्षा रखते हैं।
(संपादन : नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें
मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया