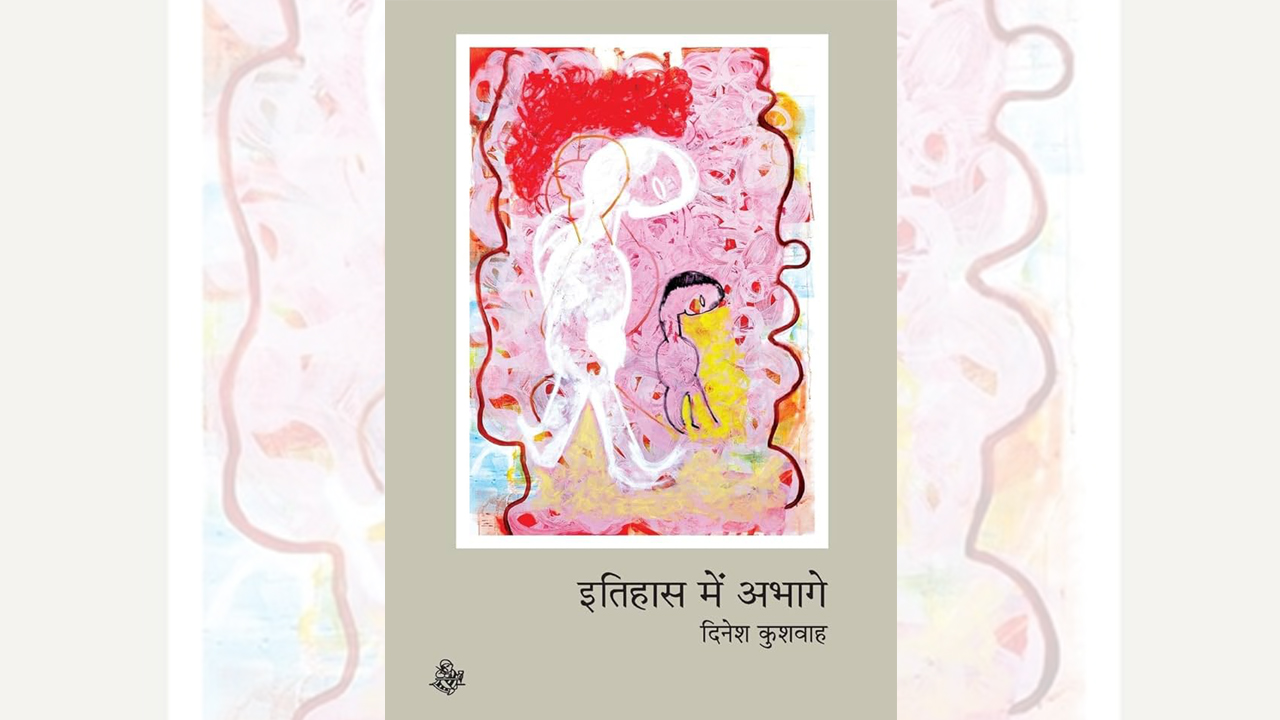दलित कविता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य (छठा भाग – पहली कड़ी)
बीसवीं सदी के नवें दशक के अंत तक दलित कविता डॉ. आंबेडकर के दैवीकरण से होती हुई, विद्रोह और प्रतिरोध के रास्तों पर चलकर जाति और वर्गविहीन समाज की परिकल्पना को मूर्त रूप देने की ओर अग्रसर हो चुकी थी। इस दशक के अंत में डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर का दूसरा कविता संग्रह ‘सिंधु घाटी बोल उठी’ (1990) प्रकाशित हुआ। इसमें 53 कविताएं संकलित हैं। इन कविताओं की विशेषता है उनकी भाषा। यह भाषा विद्रोह की है और दलितों की अपनी जन-भाषा है। कला और बिंब के स्तर पर भी इस संकलन ने अपनी नयी पहचान बनायी। उदाहरण के लिये इस संग्रह में दो कविताएं ‘अरे ओ चंदा’ और ‘अरे ओ सूरज’ कला और भाव दोनों की दृष्टि से अद्भुत कविताएं हैं। उनमें चंदा और सूरज के बिंबों में कवि की कल्पना की उड़ान जितनी मोहक है, उतनी ही मार्मिक भी है। ‘अरे ओ चंदा’ कविता की ये पंक्तियां देखिए–
अरे ओ चंदा
चमकते रहना, मेरी अटरिया पर
सारी रात।
हम दलितों का तू ही रखवारा है
तू ही एक सहारा है
चूंकि इन भेड़ियों की
न कोई मर्यादा है, न कोई जात।
मेरे इस गांव के हैं सभी बड़े लोग
सिर्फ नाम के।
अंधेरा पड़ते ही वे
दलितों के घरों में लगाते हैं घात।[1]
‘अरे ओ सूरज’ कविता में गांव की एक दलित स्त्री सूरज से अनुरोध करती है कि–
अरे ओ सूरज
आज मत उगना मेरे आंगन में
वरना दिन निकलते ही तेरे उजाले के साथ
जमींदार कहर ढायेगा।
मेरे आदमी को पकड़ ले जायेगा
दिन भर बेगार में हल चलवायेगा
सायं तेरे ढलने पर, मजदूरी मांगने पर
वह एवज में लट्ठ बरसायेगा।[2]
नवें दशक की दलित कविता के मुक्ति-संघर्ष ने अगले दशक में कई नये ऊर्जावान कवि पैदा किये। सन् 1991 से सन् 2000 तक इन दस वर्षों में दलित कविताओं के सबसे ज्यादा संकलन प्रकाशित हुए। इसी दशक में प्रतिष्ठित दलित कवि ओमप्रकाश वाल्मीकि और श्यौराज सिंह ‘बेचैन’ के नये कविता-संग्रह भी प्रकाशित हुए और मोहनदास नैमिशराय, जयप्रकाश कर्दम, ईश कुमार गंगानिया, सुदेश तनवर, असंग घोष, सी.बी. भारती और सूरजपाल चौहान जैसे कई नये कवि भी अस्तित्व में आये। इसी दशक ने हमें मलखान सिंह जैसा सशक्त दलित कवि भी दिया और इसी दशक में दलित कविता का स्त्रीवादी स्वर भी आया, जो एक बड़ी उपलब्धि है।
यहां यह बताना आवश्यक प्रतीत होता है कि मोहनदास नैमिशराय का कविता-संग्रह ‘आग और आंदोलन’ काफी विलंब से इस दशक के अंतिम वर्ष में प्रकाशित हुआ, जबकि वे नवें दशक के कवि हैं, उनका कविता-कर्म इससे भी पहले का हो सकता है। उन्होंने अपनी पहली कविता के बारे में सूचना दी है कि वह 1966 के आस-पास लिखी गयी थी।[3] नवें दशक में भी उनकी कुछ कविताएं पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं। पर, चूंकि पत्रकारिता उनकी पहली प्राथमिकता रही, इसलिये उन्होंने अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित कराने में रुचि नहीं ली। वे स्वयं इस बात को स्वीकार करते हुए लिखते हैं, “जितनी कविताएं लिखीं, वे कागजों में दबती चली गयीं। जीवन के आरंभिक वर्षों में संघर्ष क्षेत्र में रहने के कारण अधिकांश को छपने के लिये भी नहीं भेज सका, हालांकि उनमें कुछ छपीं भी।”[4]
मोहनदास नैमिशराय ऐसे दलित कवि हैं, जिनके सरोकार आम आदमी से जुड़े हैं। अपनी पहली ही कविता ‘एक व्यक्ति सड़क पर’ में उनका कवि सड़क पर पड़ी लाश को भी आदमी के रूप में देखता है, जिसकी राह चलते लोग उपेक्षा करके निकल जाते हैं। दूसरी कविता ‘खून और शहद’ में कवि जूठी पत्तलों पर कुत्तों और इंसानों के भूख मिटाने के संघर्ष को चित्रित करता है, तो ‘कांच और लड़की’ कविता में कूड़े के ढेर से कांच के टुकड़े बीनने वाली लड़की के भीतर छिपे गीत को चित्रित करता है।[5] ‘मेरा गांव’ कविता में कवि गांव की हरियाली और गांव के पनघट, चौपाल और गाय-बकरियों को बचाना चाहता है, जिसे आधुनिकता निगल रही है। इस आधुनिकता में आदमी भी नष्ट हो रहा है, ऐसी कवि की मान्यता है।[6] आम आदमी के प्रति कवि का अनुराग इतना गहरा है कि वह मसीहा नहीं बनना चाहता, वरन् आम आदमी के साथ रहकर उसकी धड़कन सुन सकने के लिये आम आदमी ही बना रहना चाहता है।[7] लेकिन यह आम आदमी की अवधारणा अजीब है कि वह न जाति के सवाल से टकराता है और न धर्म के सवालों से। एक कविता ‘सफदर हाशमी की याद में’ है, जो कवि की जनवादी चेतना को दर्शाती है। इस कविता में कवि शब्दों का विरोध करने वाले माफिया के खिलाफ मजदूर-किसानों को एक होने को कहता है और साहित्य तथा कला को विलासिता के दायरे से निकाल कर चाकू जैसी धार देने के लिये कहता है। वह कहता है–
हमें शासक की जमात की
पशुता से सीधी लड़ाई
लड़नी है।[8]
निश्चित ही नैमिशराय की काव्य-चेतना जातिवाद से मुक्त है। वह संपूर्ण शासक वर्ग को शोषक वर्ग मानता है और उसके विरुद्ध सीधी लड़ाई का आह्वान करता है। यह शासक वर्ग सिर्फ सत्ता में बैठा वर्ग ही नहीं है, वरन् वह वर्ग भी है, जिसे सत्ता पालती है। ‘रात में डूबा लोकतंत्र और वे’ में ये ‘वे’ ऐसे ही लोग हैं, जो शासक वर्ग के लिये बस्तियों में जाकर अत्याचार और व्यभिचार का नंगा तांडव करके दहशत फैलाते हैं और यही लोग ‘एक शव का बयान’ में, जो मलियाना कांड (1990) पर लिखी गयी कविता है, जिसमें वे बस्ती के जिंदलोगों को लाशों में बदल देते हैं। इसलिये, कवि इस शासक जमात से लड़ने के लिये साझी लड़ाई की बात करता है।[9]
यह साझी लड़ाई राजनीति के क्षेत्र की नहीं है, वरन् शब्दों के क्षेत्र की है। कवि ‘आंदोलन’ कविता में इसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है–
तुम्हारे पास केवल शब्द हैं
उन्हीं को तुम्हें आंदोलन बनाना है
क्रांति हथियारों से नहीं
शब्दों से ही आती है।[10]
‘आंदोलन’ कविता 1991 की है। 1992 में नैमिशराय अपनी कविता ‘शब्द’ लिखते हैं, जिसमें हमें पहली बार दलित चेतना का दर्शन मिलता है। संभवतः वे इसी समय आंबेडकर आंदोलन के भी प्रभाव में आये। उन्होंने ‘शब्द’ को नया अर्थ दिया है, परिवर्तन का। वे लिखते हैं–
दलितों के सीने जब
छलनी होते हैं
शब्द उभरते हैं
शब्द बनते हैं धारदार
जहर बुझे चाकू की तरह।[11]
लेकिन यह चेतना कवि की मूल काव्य चेतना नहीं बन पाती। उन्हें आम आदमी ही सर्वाधिक आकर्षित करता है और वही उनकी मूल चेतना के केंद्र में भी रहता है। 46 कविताओं के इस संग्रह में दलित चेतना की सिर्फ चार कविताएं हैं। दूसरी कविता तीन साल बाद 1995 में ‘झाड़ू और कलम’ शीर्षक से उन्होंने लिखी और दो अन्य कविताएं ‘गांव में शन्ति है’ तथा ‘रक्त मांगती हैं मेरी कविताएं’ 1998 में लिखीं। ‘झाड़ू और कलम’ कविता में वे दलितों में आये वैचारिक परिवर्तन को रेखांकित करते हैं। यथा–
कल मेरे हाथ में झाड़ू था
आज कलम
कल झाड़ू से मैं तुम्हारी गंदगी हटाता था
आज कलम से।
तुमने गन्दगी फैलाने के लिये
वेद/ पुराण/ मनुस्मृति का सहारा लिया।
कल उन्हें जलाने का
मुझे अधिकार न था।
आज शब्दों की आंच से
मैं उन्हें जलाऊंगा।[12]
‘गांव में शांति है’ कविता एक ऐसे दलित गांव से रू-ब-रू कराती है, जिसमें आततायियों द्वारा दस लोगों को मारा जा चुका है और गांव में फिर भी शांति है, अलबत्ता ‘औरतों ने अपनी-अपनी चूड़ियां तोड़ दी हैं, उनकी ‘आंखों में आक्रोश तैरने लगा है और बच्चों ने अपने-अपने माथे पर खून के टीके लगा लिये हैं’।[13] गांव में फिर भी शांति है, जो किसी भावी विप्लव की या प्रतिशोध की भी सूचक लगती है। ‘रक्त मांगती हैं मेरी कविताएं’ कविता में, जो संग्रह की अंतिम कविता है, यह विप्लव या प्रतिशोध दिखायी भी देता है, जब कवि कहता है–
थानों में परशुराम बैठा है
सर काटने को दलितों का,
स्कूलों में सरस्वती वंदना की गूंज
रक्त मांगती हैं मेरी कविताएं
तुम्हारे पास अगर हो तो।[14]
लेकिन, उन कविताओं में दलित चेतना का संघर्ष तीव्र नहीं हो सका। इस संग्रह की जो कविता विचारोत्तेजक और प्रभावशाली है, वह ‘ईश्वर की मौत’ है। यह कविता सचमुच कालजयी है और हिंदी की अब तक की दलित कविता में एक नयी अभिव्यंजना भी है। यथा–
ईश्वर की मौत
उस दिन होती है
जब बनता है कोई मंदिर या मठ।[15]
उर्दू शाइरी में खुदा को लामकां कहा गया है, अर्थात् जिसका कहीं आवास नहीं है। मन्दिर हों या मठ सभी ‘मकां’ हैं, जिनका ‘लामकां’ से कोई वास्ता नहीं हो सकता। कबीर भी कहते हैं कि ईश्वर मन्दिर, काबा और कैलाश में नहीं, बल्कि आदमी के दिल में रहता है। इसलिये कवि ठीक कहता है कि ईश्वर को जब मंदिर और मठ में सीमित कर दिया जाता है, तो वह मर जाता है। अंत में कवि ईश्वर के अस्तित्व का खंडन करते हुए बहुत ही तार्किक सवाल उठाता है—
ईश्वर की मौत उस पल होती है
जब मेरे भीतर उभरता है सवाल-
ईश्वर का जन्म
किस मां की कोख से हुआ था?
ईश्वर का बाप कौन?[16]

कुछ अन्य कवियों का कविता–संघर्ष
बीसवीं सदी के अंतिम दशक के पहले वर्ष में हरकिशन संतोषी का कविता-संग्रह ‘वीणा के नूपुर’ (1991) प्रकाशित हुआ, यह उनका दूसरा कविता-संग्रह था। पहला कविता-संग्रह ‘कमलिनी’ 1990 में प्रकाशित हुआ था। ‘कमलिनी’ में दलित चेतना के अंकुर फूट गये थे, पर ‘वीणा के नूपुर’ में वे कुछ विकसित हो गये, पर अभी परिपक्व नहीं हुए थे। कवि की रूमानी प्रवृत्ति ने कविता को फूल, पत्तियों, जुगनू और चिड़ियों के बिंबों में उलझा दिया, जिसके कारण मार्मिक अभिव्यक्ति भी प्रभाव नहीं छोड़ती। यथा, गरीबी और भूख का यह चित्रण–
अभावों की थाली
एक मुरझाये फूल सी
मखमली आंखें चमकाती हैं
भूख को अपनी पहचान कराकरअंतड़ियों में सेंध लगाती है।[17]
इसी तरह उनकी एक लंबी कविता ‘मुट्ठी में बंद अंधेरा’ है, जिसमें गरीब की झोपड़ी के अंधेरे की समस्या जुगनू और किरणों के बीच उलझकर विचार से ही दूर हो गयी है। इस संग्रह में तीन खंड हैं और कुल मिलाकर 50 कविताएं संकलित हैं। राजनैतिक दृष्टि से यह वह समय था, जब देश में मंदिर और आरक्षण की लड़ाई चल रही थी, जिसे मंडल और कमंडल की लड़ाई का नाम दिया गया था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के नेताओं का अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का आंदोलन चल रहा था, जिसकी परिणति 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत में हुई, तो दूसरी तरफ दलित-पिछड़े वर्गों के नेता मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसके तहत पिछड़ी जातियों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना था। भाजपा और संघ परिवार के नेता मंडल के खिलाफ सवर्ण छात्रों को भड़का रहे थे और उनसे आत्मदाह करा रहे थे। सरकारी सम्पत्तियां जलवा रहे थे। वामपंथी नेता भी, जिनमें अधिकांश ब्राह्मण थे, योग्यता का सवाल उठाकर आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत कर रहे थे, जो सवर्णों के ही पक्ष में था। दलित-बहुजन चिंतकों और साहित्यकारों के लिये यह अत्यंत संकट का समय था। लगभग सभी दलित-बहुजन लेखक इस हिंदू सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद का अपने-अपने स्तर से विरोध कर रहे थे। किंतु, दुखद यह कि से इस काल की हिंदी पत्रकारिता भी दलित-बहुजन विरोधी हो गयी थी और वह मंडल के विरोध में द्विज पत्रकारों और नेताओं को छाप रही थी। ऐसी स्थिति में दलित-बहुजन लेखकों का विचार अखबारों में नहीं आ सका। दलित-बहुजन कवियों ने भी इस समय आरक्षण के समर्थन में खूब कविताएं लिखीं, जो उनके संकलनों में तो आयीं, पर राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में नहीं आ सकीं।
हरकिशन संतोषी के काव्य में भी यह कालखंड प्रतिबिंबित होता है। आरक्षण-विरोध को लेकर उनकी कई कविताएं इस संकलन में मौजूद हैं। ‘मानव-श्रृंखला बनाने वालों’ शीर्षक कविता में उनका कवि अपनी प्रतिक्रिया इन शब्दों में प्रकट करता है–
योग्यता आधार बनाने वालो
आर्थिक रेखा खिंचवाने वालो
जन-सम्पत्ति में आग लगाने वालो
रेल-पथ अवरोध कराने वालो
क्या तुम सड़क किनारे बैठ
फटा-जूता भी सी पाओगे?[18]
कवि की दृष्टि में मंडल के खिलाफ सवर्ण छात्रों का आंदोलन सांप्रदायिक मनोवृत्ति वाली राजनैतिक पार्टियों का षडयंत्र था। कवि ने ‘षडयंत्र के वृक्ष’ कविता में यह ठीक ही कहा–
षडयंत्र के वृ़क्ष पर
उगा है विषैला सुमन
जिसकी सुगंध पाकर।
हो रही है, नयी पीढ़ी दिशा भ्रमित
झुलसी जा रही है आग में
आत्मदाह के नाम पर।
हत्याएं की जा रही हैं
किशोरमय उम्र की
कुछ राजनीतिक पार्टियां
भुगतान पा रही हैं इनकी मृत्यु का।
अंधेरों की ओट में-
सांप्रदायिक मनोवृत्तियां
अपना गुल खिला रही हैं।[19]
इसी विचार की एक लंबी कविता ‘जो तुमने कहा’ है, मंडल के खिलाफ कमंडल के आंदोलन पर सवाल खड़े करती है। कवि पूछता है–
और कब तक चलेगा
यह जुल्म और सितम का सैलाब
कि एक भाई भूखा सोये
दूसरा भाई पेट भरकर खाना फेंके।
एक भाई नभ को छुए
दूजा भाई जमीन में धंसे।[20]
आगे, वह हिंदुओं के इस उन्माद को दलितों की प्रगति को अवरुद्ध करने वाला बताते हुए कहता है–
इस कटे-मरे शरीर ने
अपने अधिकारों की ली है अंगड़ाई।
हम पहुंच न सकें मंजिल तक
सारे देश में खोद दी है खाई।[21]
अंत में, कवि ने योग्यता की बात करने वाले आरक्षण-विरोधियों से दो-टूक शब्दों में बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पूछे हैं–
योग्यता का प्रश्न चिन्ह लगाने वालो
अगर तुम्हीं योग्य थे
तो क्यों तुमने सोमनाथ का मंदिर लुटवाया?
क्यों तुमने पाकिस्तान बनवाया?
क्यों तुमने विदेशियों के कब्जे में
मातृभूमि के दिल का टुकड़ा काबिज करवाया?[22]
नवें दशक में दलित कविता ने जिस वैचारिकी के लिये संघर्ष किया था, उसकी एक बड़ी राजनैतिक उपलब्धि भी है, जिसे हम उस समय की रेडिकल दलित राजनीति के उभार में देख सकते हैं।
श्यौराज सिंह बेचैन का दूसरा कविता–संकलन
1994 में सूरजपाल चौहान का कविता-संग्रह ‘प्रयास’ प्रकाशित हुआ। जैसा कि नाम से ध्वनित होता है, कवि के रूप में चौहान का यह सचमुच पहला प्रयास था। इसलिये इस संग्रह की कविताओं में दलित कविता का कोई संघर्ष दिखाई नहीं देता, जबकि यह वह समय था, जब दलित साहित्य के उभार ने साहित्य के सिंहासन पर विराजमान द्विजों में अपने वर्चस्व को लेकर चिन्ता, भय और बौखलाहट पैदा कर दी थी। वे दलित साहित्य को नकारने के लिये तमाम तरह के सवाल खड़े करके निरर्थक बहसें चला रहे थे। एक सवाल, जो इन बहसों के केंद्र में सबसे ज्यादा था, वह था सहानुभूति और स्वानुभूति का सवाल। दलित लेखक द्विजों के दलित-विषयक लेखन को सहानुभूति का लेखन कहते थे, जबकि दलित लेखन स्वानुभूति का लेखन था, जिसमें अनुभूति की प्रामाणिकता थी। इसी आधार पर इन बहसों में इन सवाल पर खूब चर्चा होती थी कि गैर दलित, दलित साहित्य क्यों नहीं लिख सकता, या दलित साहित्य लिखने के लिये क्या दलित होना जरूरी है? इस सवाल का मजाक बनाते हुए आज भी यहां तक कह दिया जाता है कि क्या घोड़े पर लिखने के लिये घोड़ा बनना पड़ेगा? सभी दलित लेखक इन सवालों से जूझ रहे थे और अपने विरोधियों को सटीक जवाब दे रहे थे। इसके विपरीत सूरजपाल चौहान ‘प्रयास’ में राष्ट्रीय वंदना कर रहे थे–
यह जन्मभूमि है
कृष्ण और गौतम की
नानक, संत कबीर,
राम मर्यादा पुरुषोत्तम की
इस देव भूमि भारत को
शत शत मेरा प्रणाम।
वर्ष 1995 में श्यौराज सिंह ‘बेचैन’ के दूसरे कविता-संग्रह ‘क्रौंच हूं मैं’ में हम कवि को इन सवालों से टकराते हुए देखते हैं। उन्होंने ‘क्रौंच हूं मैं’ शीर्षक कविता में इस सवाल का बहुत ही सटीक जवाब दिया है कि सवर्णों के दलित लेखन में अनुभूति की प्रामाणिकता क्यों नहीं है? आदिकवि वाल्मीकि ने रामायण में बहेलिया द्वारा क्रौंच पक्षी के वध का मार्मिक वर्णन किया है। इसी बिंब को आधार बनाते हुए बेचैन ने दलित वेदना को रेखांकित किया है। इस कविता में वे कहते हैं–
आदि कविता
क्रौंच का वध देखकर पैदा हुई थी।
मैं परंतु
आदि कवि के वंशजों में से नहीं हूँ।
वाल्मीकि मैं नहीं हूं,
क्रौंच हूं मैं।[23]
यहां वाल्मीकि सहानुभूति का लेखन करने वाले सवर्ण लेखक का प्रतीक है और ‘क्रौंच’ स्वयं दलित का प्रतीक है, जो अपनी पीड़ा का स्वयं अनुभव कर रहा है। वाल्मीकि ने क्रौंच पक्षी के दुख से द्रवित होकर जो कविता रची, वह सहानुभूति की मार्मिक अभिव्यक्ति है, इसमें संदेह नहीं, परंतु वह क्रौंच की अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति नहीं है, क्योंकि क्रौंच की पीड़ा और ही है। वह कवि की दृष्टि में यह है–
आंख में अपराधियों के
तैरते हैं चित्र।
वह शिकारी आज का अभियुक्त।
दंड भोगे बिन रहा वह मुक्त।[24]
यदि शोषक और अत्याचारी मुक्त घूमता है, तो सहानुभूति के लेखन से दलित को क्या लाभ? कवि अंत में कहता है–
स्वयं पीड़ित-
स्वयं ही हूं साक्ष्य।
प्रेक्षकों पर है नहीं विश्वास।[25]
कवि आदिकवि वाल्मीकि को प्रेक्षक बताते हुए कहना चाहता है कि दलितों पर सहानुभूति-परक लेखन प्रेक्षक का लेखन है, वह वास्तविक और यथार्थ-परक लेखन नहीं है। इसी बात को कवि अपनी एक अन्य कविता ‘आप और खास’ में और भी बेहतर ढंग से कहता है–
आम आदमी पर खास आदमी
कविता लिख देता है।
खास आदमी पारितोषिक लेता है।
पारितोषिक मिठास में सना होता है।
कविता में असीम दर्द भरा होता है।
यह खास आदमी
इतना क्यों दुखी होता है,
देखकर निरक्षरता,
भूख और दरिद्रता?[26]
कवि ने बहुत ही सही सवाल उठाया है कि खास आदमी आम आदमी की गरीबी और भूख को देखकर क्यों दुखी होता है, जबकि वह उसे दूर करने के लिये कुछ भी नहीं करता? कवि इसका जवाब भी बहुत सही देता है–
आम आदमी उद्दीपन ही नहीं रहा तो
कौन करेगा प्रेरित उसको
इसलिये वह मानता है
कि आम को बस ‘आम’ रहना चाहिए।
आम को खास होने से रोक देना चाहिए।
हो सके तो खास को
आम में बदल देना चाहिए।[27]
दलित कविता का यही संघर्ष हमें बेचैन की ‘मशीनों का समय’ कविता में दिखायी देता है–
तब बहेलिया वध करता था
और प्रेक्षक कविता।
अब बहेलिया वध से ज्यादा
कविताएं करता है।
तब कविता संत्रास जन्य थी
अब कविता अभ्यास।[28]
जब शोषक श्रेणी के लोग ही कविता करने लगे हैं, तो दलित कविता को उनका समर्थन कैसे मिल सकता है? कवि ने बहेलियों और प्रेक्षकों की कविताओं के बिंब को एक अन्य कविता ‘जुल्म जारी भी है’ में शोषण के प्रपंच के रूप में चित्रित किया है–
अब उसके खेत का
टुकड़ा कुतरने में लगा है भूमिधर
उसकी बरबादी का
जिम्मेदार पटवारी भी है।
वह मजूरी गांव में देखे
या भागे शहर को।[29]
कवि इस शोषण को ‘पशुओं की गर्दन पर आरा’ की संज्ञा देते हुए ‘फरेब नहीं’ कविता में इस प्रकार अपना विचार रखता है–
यह कविता नहीं
शब्दों की जोड़-तोड़ है
कतारबद्ध लोगों का नारा है।
पूंजीवाद का कविता में हस्तक्षेप
श्रमिकों का शोषण, स्त्रियों का वस्तुकरण
दलितों और अवामी कवियों की गर्दनों पर
वैसे ही है जैसे वधस्थल में
पशुओं की गर्दन पर आरा है।[30]
लेकिन कवि गुलामियों के अंत के लिये अपने संघर्ष के सफर को जारी रखता है। यथा ‘समूह गान’ कविता की ये पंक्तियां–
गुलामियों के खात्मे की
जिद किये हुए हैं हम
नहीं रुकेंगे अब हमारे
साथियों के ये कदम।
उठें कि रस्मे रूढ़ियों की,
बंदिशें हटा सकें।
उठें कि साफ स्वस्थ
नव समाज हम बना सकें।[31]
क्रमश: जारी
संदर्भ :
[1] सिंधु घाटी बोल उठी (कविता संग्रह), डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर, राष्ट्रीय प्रकाशन समिति, 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली- 9, प्रथम संस्करण- 1990, पृष्ठ 81-82
[2] वही, पृष्ठ 82-83
[3] आग और आंदोलन (कविता संग्रह), मोहनदास नैमिशराय, भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्ध विहार, आंबेडकर भवन, नयी दिल्ली, संस्करण- प्रथम, सन् 2000, देखिये, कवि का वक्तव्य ‘दो शब्द’।
[4] वही
[5] वही, पृष्ठ 11, 12 एवं 13
[6] वही, पृष्ठ 14
[7] वही, पृष्ठ 20
[8] वही, पृष्ठ 24-25
[9] वही, पृष्ठ 33
[10] वही, पृष्ठ 36
[11] वही, पृष्ठ 38
[12] वही, पृष्ठ 57
[13] वही, पृष्ठ 70
[14] वही, पृष्ठ 75
[15] वही, पृष्ठ 44
[16] वही
[17] वीणा के नूपुर (कविता संग्रह)- हरकिशन सन्तोषी, नव साहित्य अकादमी, नयी दिल्ली, प्रथम संस्करण- 1991, पृष्ठ 20
[18] वही, पृष्ठ 57
[19] वही, पृष्ठ 59
[20] वही, पृष्ठ 61
[21] वही, पृष्ठ 63
[22] वही, पृष्ठ 67
[23] क्रौंच हूँ मैं (कविता संग्रह)- श्यौराज सिंह बेचैन, सहयोग प्रकाशन, मयूर विहार, फेज-1, दिल्ली-91, संस्करण, प्रथम- 1995, पृष्ठ 20-21
[24] वही
[25] वही
[26] वही, पृष्ठ 28-29
[27] वही, पृष्ठ 29
[28] वही, पृष्ठ 35
[29] वही, पृष्ठ 36
[30] वही, पृष्ठ 39
[31] वही, पृष्ठ 36
(संपादन : नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in