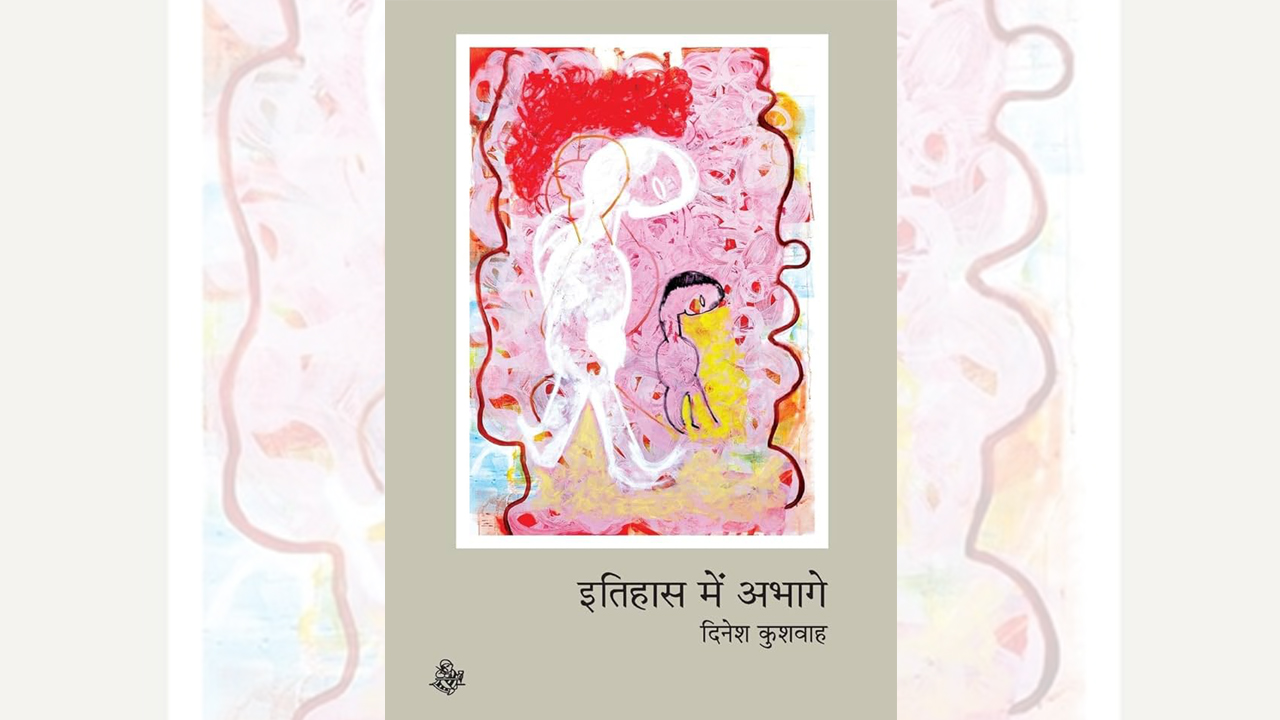रजत रानी मीनू ने अपना कविता संकलन ‘पिता भी तो होते हैं मां’[1] मुझे 4 फ़रवरी, 2018 को भेंट किया था। संयोग से यह मीनू जी के जन्म की तिथि भी है, और मेरे जन्म की भी। मैं चार साल इतिहास और दर्शन के अपने अध्ययन-लेखन के अलावा अनुवाद के शौक को पूरा करने में इतना व्यस्त रहा कि मीनू जी की कविताओं को ही नहीं, किसी भी कविता-संकलन को पढ़ने का मन नहीं बना सका। पर जब 2022 के उत्तरार्द्ध में फारवर्ड प्रेस में ‘दलित कविता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य’ लेखमाला शुरू हुई, तब कुछ नए कविता-संकलनों को भी पढ़ने का मन बना। और मीनू जी के कविता संकलन पर नजर गई।
मैं किसी भी कविता-संकलन की भूमिका पढ़ने में बहुत कम रूचि लेता हूं, पर कवि के ‘दो शब्द’ जरूर पढ़ता हूं। मीनू ने ‘सबब और सिलसिला’ शीर्षक से अपने ‘दो शब्द’ लिखे हैं, जिसे पढ़ने के बाद मैं उनकी दो बातों से अवगत हुआ, एक, उनकी कविताओं की रचना-प्रक्रिया से; और दो, उनकी आलोचनात्मक प्रतिभा से। उन्होंने लिखा है कि उन पर कवि श्यौराज सिंह ‘बेचैन’ की कविताओं का प्रभाव है,[2] जो स्वाभाविक भी है। बेचैन जी उनके जीवनसाथी हैं। उनकी काव्य-प्रतिभा से प्रभावित होकर ही उनके प्रति उनमें प्रेम पैदा हुआ था, जिसकी परिणिति जीवन-भर साथ रहने में हुई। बेचैन जी की कविताओं पर लोकमानस का प्रभाव है, इसलिए उनमें लोक-ऊर्जा और लोकरस भरपूर है। लेकिन मीनू की कविताएं उनके परिवेश के यथार्थ से उपजी हैं, इसलिए उनमें सामाजिक विद्रूप और विषमताओं के विरुद्ध विद्रोह और संघर्ष का भाव है। यह भाव उनकी लगभग सभी कविताओं में दिखाई देता है।
उन्होंने अपने ‘दो शब्द’ में कालीकट के एक महिला-सम्मेलन का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने सवर्ण महिलाओं के सरोकारों के साथ दलित महिलाओं के सरोकारों की बेहद संजीदगी से तुलनात्मक विवेचना की है। उनका विचारोत्तेजक तर्क है, “दलित स्त्री पितृसत्ता से ज्यादा जातिसत्ता से पीड़ित है। गैर-दलित स्त्रियों का बहनापा शाब्दिक तो खूब है, लेकिन बौद्धिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने की दिशा में शून्य है। इसलिए एक सवर्ण स्त्री की मुक्ति और एक दलित स्त्री की मुक्ति के रास्ते समान नहीं हैं।”[3] सवर्ण और दलित स्त्री की सामाजिकता के बीच की यही खाई अपने आप नहीं बनी, बल्कि इसे ब्राह्मणों की वर्णव्यवस्था ने जानबूझकर निर्मित किया है, ताकि द्विज वर्ग हमेशा शासक वर्ग बना रहे।
जब देश मुगलों और अंग्रेजों का गुलाम था, तब भी द्विज वर्ग आज़ाद था और शान से जीता था। कैथरीन मेयो ने 1929 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ‘स्लेव्स ऑफ दि गॉड्स’ में एक सरकारी अस्पताल की अंग्रेज महिला डाक्टर के हवाले से, कलकत्ता की एक ब्राह्मण स्त्री श्रीमती शरतचंद्र बनर्जी के ड्राइंग रूम यानी बैठकखाने का चित्र इस तरह खींचा है– “वह एक शाही सोफे पर तनकर बैठी हुई थी। सोफे पर फ़्रांसीसी कपड़ा मढ़ा हुआ था और सोने का पानी चढ़ा हुआ था। उसका एक पैर शानदार स्टूल पर रखा हुआ था। बेहद भव्य साटन मढ़ी कुर्सियां थीं। नया एक्समिन्स्टर गलीचा था। दीवारों पर लंदन के रीजेंट स्ट्रीट के फोटो टंगे हुए थे। जर्मन स्टैच्यू के आलीशान जोड़े थे। बेल्जियम के कांच की ढेरो कलाकृतियां कमरे में सजी हुई थीं। एक ऐसे कमरे में, जिस की बेजान ईंटों की दीवार पर पेंट से मिथ्या खिड़कियां बनाई गई थी। और उसके बंद दरवाजे के पीछे पुराने नंगे गरीब लोगों के घर थे।”[4]
अपनी बात में मीनू ने दो और सम्मेलनों का जिक्र किया है, जिनमें हिंदी की दो सुप्रसिद्ध ब्राह्मण लेखिकाओं मैत्रेयी पुष्पा और अल्पना मिश्र के विचारों के प्रति अपना प्रतिरोध दर्ज किया है। मैत्रेयी का कथन था कि स्त्री की मुक्ति पति के न रहने पर ही है। अपवाद छोड़ दें, तो मीनू का विरोध सही है, दलित स्त्री की मुक्ति पति के रहते ही है। “पति के न रहने पर उसके पास न आय का जरिया रहता है, न उसकी यह मानसिकता है। उसकी कमाई उसके पति के हाथ-पांव ही हैं।”[5] अल्पना मिश्र ने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में कहा कि “आज स्त्री शिक्षित होकर इतनी समर्थ हो गई है कि काम वाली बाई रख लेती है। गाड़ी धुलने वाला रख लेती है। यानि शिक्षित होकर वह रोजगार देने वाली बन गई है।” इस प्रकार की बात जब भी कही जाती है, तो यह बात मुझे भी दलित-विरोधी लगती है, क्योंकि काम वाली बाई या गाड़ी धोने वाला कोई ब्राह्मण-ठाकुर नहीं होता, बल्कि दलित ही होता है। सत्ता द्वारा भी दलितों को अनपढ़ बनाए रखने की साजिश इसीलिए की जाती है, जिससे वे सवर्णों के घरों में गुलामी करके अपनी रोजी कमाएं। इसलिए मीनू लिखती हैं कि अल्पना मिश्र जैसी सवर्ण स्त्रियां ऐसा ही सोच सकती हैं। “यह स्थिति एक वर्ग विशेष स्त्री की है, पर मेरी चिंता उन तमाम दलित स्त्री-पुरुषों को लेकर थी, जो आज भी बाई या काम वाला भाई बनने को मजबूर हैं। उनके बच्चे स्कूल जाने के बजाए गाड़ी धोने या जूते पॉलिश करने जैसे काम कर रहे हैं।”
उन्होंने सही सवाल उठाया कि “क्या यह सच्चाई नहीं है कि एक भंगिन या चमारिन बिना जाति छिपाए इन सवर्ण साहिबाओं के घरों में बाई का काम भी नहीं पा सकती हैं? यदि किसी उदारवादी महामानव ने उसे अपने घर काम पर रख भी लिया, तो तब भी एक सवाल यह है कि क्या उसकी यह स्थिति आज़ाद नागरिक की स्थिति है? क्या उसे भी शिक्षा-संस्कृति, कला-साहित्य और ज्ञान-विज्ञान आदि के क्षेत्रों में विकास के मौके मिल पा रहे हैं, जिस तरह सवर्ण स्त्रियों को मिले हैं?”[6]

इस रचना-प्रक्रिया को जानने के बाद, यह स्पष्ट हो जाता है कि सवर्ण स्त्री की सोच कभी भी दलित-मुक्ति के प्रश्न को नहीं समझ सकी। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि क्यों सवर्ण स्त्रियों के काव्य में स्त्री-स्वाधीनता देह की स्वाधीनता और यौन-उन्मुक्तता से आगे नहीं जाती? चाहे अमृता प्रीतम हों, अनामिका हों, रमणिका गुप्ता हों, गगन गिल हों या सविता सिंह या कात्यायनी, वंदना मिश्र हों या अर्चना श्रीवास्तव, ये सब पितृसत्ता के विरोध में जरूर हैं, पर जातिव्यवस्था के विरोध में नहीं हैं। उनके सामाजिक सरोकार बस इतने ही हैं कि वे अन्याय, अत्याचार, बलात्कार और हिंसा का विरोध करती हैं, पर वे इनके मूल में कुंडली मारकर बैठे हुए ब्राह्मणवाद से लड़ने को तैयार नहीं हैं। सवर्ण लेखिकाओं के मन में यह विचार आता ही नहीं कि दलित स्त्री या आदिवासी स्त्री दोयम दर्जे की नागरिक क्यों बना दी गई है? किसी सवर्ण विचारक ने प्रश्न उठाया था कि दलित ने अपनी दासता को अपनी नियति क्यों मान लिया है? पर उसके पास इसका उत्तर नहीं था। यह प्रश्न डॉ. आंबेडकर ने भी उठाया था, पर उनके पास इसका उत्तर था। और यह उत्तर जब उन्होंने अपना शरीर बेचने वाली दलित स्त्रियों को बताया, तो उन स्त्रियों के भीतर एक आग धधकने लगी थी। गरीबी और बेबसी क्यों है, उसका उत्तर आंबेडकर से पहले किसी ने सोचा ही नहीं था। आंबेडकर के विचार ने ऐसी चेतना जगाई कि पत्थरों में भी चिंगारियां फूट गईं। यही चेतना दलित कवियों को इतिहास और समाज को न दक्षिण-न वाम, बल्कि उस तीसरे नजरिए से देखने की दृष्टि देती है, जो किसी भी सवर्ण के पास नहीं है। रजत रानी मीनू की कविताएं इसी चेतना से लैस है। वह अपनी लंबी कविता ‘आदिवासी’ में सवर्ण लेखकों की आंखों में आंखें डालकर पूछती हैं–
तुम मुझ पर
कभी कविता लिखते हो
तो कभी कहानी, और कभी उपन्यास
पत्र-पत्रिकाओं में पाते हो कवरेज
बनकर पक्षधर खासमखास
और लूटते हो वाहवाही।
कभी तुमने मुझसे पूछा
कि मुझे और मेरे बच्चों को क्या चाहिए?
उजड़े जंगल या बसी हुईं बस्तियां?
मुझे क्या चाहिए?
जहालत भरा पिछड़ापन, अववंचन
या उन्नत शिक्षा, बेहतर जीवन?
तुम दिखाते हो सहानुभूति मुझसे
और रखते हो मुझे यथास्थिति में।[7]
यह सीधी लड़ाई का वह सूत्र है, जो डॉ. आंबेडकर ने दिया था। दलितों और आदिवासियों को यथास्थिति में रखने वाले लोग उनसे किस तरह सहानुभूति रख सकते हैं? उस सहानुभूति का क्या कोई अर्थ है, जिसमें उनके लिए अप्रत्यक्ष घृणा और उपेक्षा का भाव रहता है? इसी कविता में वह आगे प्रश्न करती हैं–
बताओ तो क्या मिला
इन अड़सठ सालों में मुझे?
मैंने नहीं जानी आज़ादी क्या होती है?
मेरी स्त्रियां रहती हैं अभी भी अर्धनग्न।
मेरे बच्चे घूमते हैं जानवरों की तरह
जानवरों के बीच, जानवरों से ही,
चिड़ियां, चूहे खाकर जीते हैं।[8]
और इस कविता का अंत डा. आंबेडकर की क्रांति-चेतना से होता है। यथा—
तुम मत लड़ो, मेरी मुक्ति की लड़ाई
मत सिखाओ मेरे बच्चों को क्रांति का पाठ
क्योंकि, क्रांति वो नहीं, जो तुम बताते हो,
क्रांन्ति वो है, जिसकी शिक्षा रूपी राह
बाबासाहेब ने दिखाई थी।[9]
दलित कविता की ताकत यही चेतना है, जिसमें बाबासाहेब की बताई हुई राह और दृष्टि है। वह कहते थे कि सवर्णों के बताए हुए मार्ग में सवर्णों का ही विकास है, दलितों का नहीं। जैसे बिल्लियां चूहों की रक्षा नहीं कर सकतीं, उसी तरह सवर्ण भी दलितों के हितैषी नहीं हो सकते।
मीनू की कविताओं के दो रूप हैं, एक, आत्मानुभूतियों का, जो वैयक्तिक है, उनका स्वयं का भोगा हुआ, और दूसरा, सामाजिक, जिसे वह अपने इर्द-गिर्द, अपने परिवेश में देखती हैं। इस तरह उनके सृष्टा का उद्भव उनके भोक्ता और द्रष्टा दोनों स्वरूप से हुआ है। अक्सर दलित साहित्य के सवर्ण आलोचक कहते हैं कि दलित साहित्य आत्मकथाओं के दायरे से बाहर नहीं निकल रहा है। इस टिप्पणी के पीछे उनका जो भी कारण हो, हालांकि एक कारण साफ़ नजर आता है कि दलित आत्मकथाओं से उन्हें यह पता चल जाता है कि सवर्णों ने दलितों के साथ कैसा व्यवहार किया था; पर हकीकत में दलित लेखकों के ये अनुभव ही हिंदुओं के धार्मिक और सांस्कृतिक समाज को समझने में उनकी सहायता करते हैं। ये अनुभव उनकी कविताओं और कहानियों को ताकत प्रदान करते हैं।
मीनू की आत्मकथात्मक कविताओं में पहली कविता ‘मां को याद करते हुए’ है, और दूसरी कविता ‘पिता भी तो होते हैं मां’ है। इसके बाद और भी कुछ कविताएं हैं, जैसे : ‘मम्मी बनते पापा’, ‘बदल रहा है जेएनयू’, ‘स्कूल के वे दिन’। मीनू की स्मृतियों में उनकी मां की छवि शायद धुंधली है। इसलिए ‘मां को याद करते हुए’ उनकी सबसे छोटी कविता है, सिर्फ चार पंक्तियों की, जिसे इस संकलन का समर्पण कहा जा सकता है। हालांकि समर्पण उन्होंने “उन दलित माताओं को किया है, जो तमाम अवरोधों के बीच स्त्री शिक्षा और स्त्री अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं।” मां को याद करते हुए वह सिर्फ इतना लिखती हैं–
न उस मां के जाने का बोध था
न इस मां के आने का बोध था
मासूम शैशव कैसा आईना था
वक्त मेरे जीवन का अपरिचित मेहमान था।[10]
जाहिर है कि ‘उस मां’ के जाने के बाद मीनू ने पिता में ही मां की छवि को देखा। एक बच्ची के लिए पिता ने ही मां की भी भूमिका निभाई, जिसे उन्होंने पूरी शिद्दत से ‘पिता भी तो होते हैं मां’ कविता में अभिव्यंजित किया है। यथा–
मैंने पापा की आंखों में देखा
अपनी मां का चेहरा
पापा मां ही तो होते हैं,
ऐसा महसूसा।
पापा ने सिखाया
उठना-बैठना, पढ़ना-लिखना
सिलना-बुनना
खाना पकाना, रहना-सहना
वे सुलाते थे मुझे
अपने सीने से लगाकर
मम्मी की तरह।
मेरे कपड़ों को धोते थे अपने हाथों से
करते थे मेरे कपड़ों पर इस्त्री
नहलाते थे मुझे रगड़-रगड़ कर
मेरी चोटियां गूंथते थे
बालों में तेल लगाकर
खाना खिलाते थे
अपने हाथों से निवाला तोड़-तोड़कर
तभी मिलती थी उनको तृप्ति।[11]
पिता पर हिंदी में कई कविताएं लिखी गई हैं। यद्यपि, सभी कवियों की कविताओं को पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन, उदय प्रकाश, गगन गिल, मंगलेश डबराल, चंद्रकांत देवताले की कविताएं मैं देख चुका हूं। हालांकि उनमें किसी में भी मां के रूप की कल्पना नहीं है। यह रूप हम मीनू की कविता में ही देखते हैं। जाहिर है, संवेदना का यह आयाम उनकी निजी अनुभूति के कारण ही कविता में आया। इस संवेदना का विस्तार उनकी एक और कविता ‘मम्मी बनते पापा’ में भी हुआ है। वह कहती हैं–
पापा मुझमें हैं
मैं पापा में हूं
उठते-बैठते, सोते-जागते
हर पल पापा रहते हैं
मेरी यादों में और मैं बसती हूं
उनकी स्मृतियों में।
पापा मम्मी का पर्याय नहीं हैं
पर मम्मी का विकल्प बन जाते हैं।[12]
मीनू के लिए इस कविता की रचना जितनी मार्मिक रही होगी, उतना ही मार्मिक एक पाठक के लिए इसका पाठ भी है। इसमें संवेदना के स्तर पर करुणा का वह रस है, जो किसी को भी भावविह्वल का सकता है। यथा–
जब मम्मी हुई थीं निष्प्राण
उनकी लाश रखी थी
विद्युत संस्थान के उस घर में
पड़ोसन को दूध का भगोना पकड़ाते हुए
भरी आवाज़ में कहा था—
‘भाभी जरा दूध गर्म करके बच्ची को पिला दो।’
वे मुझे रखना चाहते थे अनभिज्ञ
मम्मी की अनुपस्थिति से
पर मुझे पता था
मम्मी सो गई थीं
न जागने वाली नींद में।
न आ सकेगा अब उनका हाथ मेरे गालों पर
नहीं जान सकूंगी मैं मम्मी की ममता।
पर, पापा महसूस नहीं होने देना चाहते
कोई कमी कोई खालीपन।[13]
निजी अनुभूतियों का एक महत्व है कि उनसे जीवन और परिवेश की बेहतर समझ मिलती है, जो बड़ी-बड़ी किताबों से नहीं मिलती। कविता को बहुत सारे लेखकों ने अपने-अपने ढंग से परिभाषित किया है। अगर अनुसंधान किया जाए, तो इस विषय पर बहुत सी किताबें भी मिल सकती हैं। पर उनसे कविता को नहीं समझा जा सकता। और, जहां तक दलित कविता का प्रश्न है, उसे परिभाषित करने वाला कोई ग्रंथ नहीं बना। दलित कविता का अर्थ और उसका सृजन पहली बार दलितों ने ही किया। यह आकस्मिक नहीं है कि लगभग हर दलित कवि ने, रजत रानी मीनू ने भी, कविता को उस ढर्रे से अलग किया है, जो मुख्यधारा की कविता की परंपरा रही है। उनकी दृष्टि में कविता ‘कथित मान्यताओं के अनुसार मन बहलाव का साधन मात्र’ नहीं है, जिसमें कल्पनाएं होती हैं, जिससे “श्रोता आह्लादित हों/ सुनें और हाथ झाड़ सभागार से चलते बनें/ जैसे धूल से सने हाथों को झाड़ता है सभ्य इंसान।” वह लिखती हैं–
यह कविता नहीं हो सकती।
कविता एक क्रांति है
मात्र शब्दों का जाल नहीं।
कविता मन-बहलाव का साधन नहीं।
कविता बदलाव का दूसरा नाम है।
कविता एक स्त्रीलिंगी शब्द है,
जिसमें समाया है
पूरा का पूरा विश्व परिवार।
कविता एक संवेदना का सार है।
कविता मनुष्यता से मनुष्यता का प्यार है।[14]
मीनू ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि कविता स्त्रीलिंगी शब्द है, जिसमें पूरा विश्व समाया हुआ है। स्त्री का दूसरा नाम सृजक भी है, इसलिए सृजन उसके हर कर्म में समाया हुआ है, जिससे विश्व का निर्माण होता है।
मीनू की ‘आत्मबोध’ कविता इस सृजन को अच्छे से व्यक्त करती है। यथा–
दोपहर में दो पल मिले फुरसत के
ढूंढ़ रही थी वह अपनी उस कविता को
जो सुबह बनाते-खिलाते समय आई थी परी सी
मन में अनेक खुशियां समेटे
ढूंढ़ने की कोशिश की थी उस कहानी को
जो दोपहर में रोटियां सेकते हुए दिखी थी
मन को पंख लग गए थे
ढूंढ़ रही थी उपन्यास के उस पात्र को
जो शाम का चाय-नाश्ता बनाते समय
आए थे उसके पास
जो संजोए थे उसने मौलिक चिंतन से
वे कर रहे थे गुफ्तगू उससे।[15]
लेकिन वे कहां रह पाए उसके पास–
वे सब खो गए
अपनों की तरह कुम्भ मेले में।
मगर वे दर्द दे गए
दर्द भी नया न था,
अभ्यस्त थी वह सहने की।[16]
यह विडंबना ही है कि जो स्त्री सृजनशील है, परंपरा ने उसकी स्वाधीनता के सारे दरवाजे बंद रखे थे। और जो स्वाधीनता विश्व के स्त्रीवादी आंदोलनों ने उसे दी, वह बहुत आधुनिक है, और दलित स्त्री तो उसके दायरे में थी ही नहीं। दलित स्त्री की स्वाधीनता पर अभी भी ब्राह्मणवादी सत्ता का पहरा है। इसलिए यह आकस्मिक नहीं है कि दलित स्त्री पर हुए अत्याचार सवर्ण समाज में हलचल पैदा नहीं करते, लेकिन यदि सवर्ण स्त्री कहीं जुल्म या हिंसा की शिकार होती है, तो मुख्यधारा की सारी मीडिया उसके लिए आवाज़ उठाता है। सवर्ण वर्ग दलित के लिए आवाज़ नहीं उठाता। इससे यह साबित होता है कि दलित स्त्री ने अभी अस्तित्व ही नहीं पाया है। ‘क्यों नहीं हिलता पत्ता एक भी’ कविता में मीनू ने दलित स्त्री के अनस्तित्व को ही केंद्र में रखा है। यथा–
हमारे साथ जब होता है बलात्कार
सामूहिक बलात्कार—
तब क्यों हिलता नहीं पत्ता एक भी?
और जब तुम्हारे साथ हुआ बलात्कार
तब क्यों हिल गई संसद भी?
चीख उठी महिला सांसद बलात्कार के खिलाफ
क्यों उड़ गई महिला आयोग की चैन की नींद?
आज क्यों उठी बलात्कारियों को
सजा-ए-मौत की मांग
कल क्यों मौन थीं तुम?[17]
मीनू कहती हैं कि अगर सवर्णों ने जुल्म को जुल्म समझा होता, और हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई होती, तो दलित को भी जीने का संबल मिल गया होता। यथा–
कारण मालूम है मुझे
क्योंकि तुम हो आभिजात्य सवर्ण
और मैं ठहरी दलित।
यदि हजारों बालाओं के साथ
किए जा रहे बलात्कारों पर
तुम खामोश नहीं रही होतीं,
तो तुम्हारे बोलने से मिल जाता
मेरी आवाज़ को थोड़ा संबल
आज तुम्हारी बच्ची के साथ
भी नहीं होता बलात्कार।[18]
मगर सवर्ण पुरुषों की नजर में दलित स्त्रियों की इज्जत का कोई मूल्य ही नहीं है। जमीदारों की यह घृणित प्रथा तो आज़ादी के बाद तक कुछ ग्रामीण इलाकों में प्रचलित थी, जिसमें दलित बहू का डोला पहले ठाकुर के घर उतरता था, और उसकी पहली सुहागरात ठाकुर मनाता था। सवाल सिर्फ इज्जत का ही नहीं है, बल्कि दलित की अशिक्षा, गरीबी, बेबसी और घृणित जिंदगी सबका जिम्मेदार भारत का यही सवर्ण वर्ग है, जिसकी सारी सत्ता दलित को सदैव अपनी अधीनता में ही रखने की रही है। इस यथार्थ की बहुत साफ़ और बेबाक अभिव्यक्ति हमें मीनू की ‘तुम हो’ कविता में मिलती है। यथा–
मेरी मिचीं आंखें, भिंचे गाल
दुबला शरीर तुम हो
आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर की जगह
मेरे अंगूठे के निशान तुम हो
मेरे मैले कपड़े, टूटी चप्पलें तुम हो
दूध के लिए बिलखते मेरे बच्चे
भूखा पेट तुम हो
टूटी चारपाई, फटी रजाई
टूटी छान के जिम्मेदार तुम हो।[19]
दलितों की बेबसी के जिम्मेदार द्विजों ने इसीलिए परिवर्तन के किसी आंदोलन को, किसी आवाज़ को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जो व्यवस्था कायम की, उसने दलितों को न पढ़ने दिया, न स्वतंत्रता से न खाने दिया, न पहनने दिया और न सिर पर छत डालने दी। उन्होंने दलितों के साथ ऐसे व्यवहार किए, जैसे वे विधर्मी और दूसरे देश के नागरिक हों। ‘मेरा दर्द’ कविता में मीनू ने ऐसे दो दृश्यों का मार्मिक चित्रण किया है। पहला दृश्य इस तरह है–
एक दलित बाला बैठी उदास
काश मेरी भी कोई सुनता
मैं भी पढ़ना चाहती हूं
आगे बढ़ना चाहती हूं
मगर मेरी सवर्ण शिक्षिका ने
लिख दिया था मेरे माथे पर
काली स्याही से ‘तू चमारी है
तू नहीं पढ़ सकती।’
तमाशा बनी थी मैं
गिड़गिड़ाई थी पढ़ना है मुझे।[20]
वह पूछती हैं, “क्यों नहीं पहुंची/ मेरी खबर देशी-विदेशी अखबारों तक?” मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी बुआ, मेरी मौसी, मेरी मां/ किसी को भी नहीं पढ़ने दिया मेरी तरह।‘[21]
मीनू ने यह प्रश्न सवर्णों के साथ-साथ दलित अभिभावकों से भी पूछा है। सवाल यह नहीं है कि दलित अभिभावक अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सके। कारण यह नहीं है कि वे गरीब थे, बल्कि कारण यह है कि ब्राह्मणी व्यवस्था में दलितों के लिए शिक्षा की इजाजत ही नहीं थी। वे चाहते थे और उन्होंने चाहा भी था, लेकिन सवर्ण शिक्षकों को दलितों का पढ़ना गंवारा नहीं था। मीनू कहती हैं–
ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई
स्वामी अछूतानंद चीखते रहे
समझाते रहे, पढ़ो, अपना हक छीनो
हम हिंदवासी हैं, मूलनिवासी हैं
पर हमारी वर्णभेदी व्यवस्था ने
रोक दी मेरी शिक्षा।[22]
इस कविता के दूसरे दृश्य में सवर्ण आततायियों द्वारा दलित स्त्रियों के दैहिक और यौन शोषण का चित्रण है। इसमें एक दलित बाला है, जिसे सवर्ण जानवर खींचकर खेतों में ले जाते हैं और बंदूक के बल पर उसके साथ बदसलूकी करते हैं। यथा–
मेरे मां-बापू विवश थे
रोये थे, गिड़गिड़ाए थे
अपने मालिकों से गुहार लगाई थी
पर वे बंदूक ताने खड़े थे मेरी झुग्गी के बाहर
जुबान खोली तो उड़ा देंगे पूरा गांव
मिर्चपुरा, साढूपुरा आदि की तरह।[23]
वह पूछती हैं– “कहां चली गई थी मेरे देश की कानून-व्यवस्था?/ क्यों उदासीन है व्यवस्था मेरे प्रति?”[24]
यह व्यवस्था दलित जातियों के प्रति आज भी उदासीन है, हालांकि भारतीय गणतंत्र को कायम हुए आधी सदी गुजर चुकी है, लेकिन दलितों का उत्थान और विकास अभी भी सरकारों और ब्राह्मणों के रहमोकरम पर निर्भर करता है। ठीकठाक शैक्षिक योग्यता होने के बाद भी दलित जातियों के लोगों को नौकरी मिलने की गारंटी नहीं है। इस व्यथा को मीनू ने ‘साक्षात्कार’ कविता में इस तरह व्यक्त किया है–
वे करते हैं आतंकित बोर्ड में बैठकर
रचते हैं जीवन के आधार
हम सबकी किस्मत के सर्जनहार।
वर्णव्यवस्था के खोल में घुसकर।
रहते हैं सचेत सावधान
व्यवस्था को यथावत बनाए रखने के लिए।[25]
सवर्णों ने इस अलोकतांत्रिक व्यवस्था को यथावत बनाए रखकर उन असंख्य लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को यथावत बनाए रखने का षड्यंत्र रचा है, जो उनकी वर्णव्यवस्था के दायरे से बाहर हैं। इसी व्यवस्था के कारण दलित जातियों के लोग आज भी नहीं जानते कि उनके अधिकार क्या हैं? मीनू ने इस अर्थबोध की एक लंबी कविता ‘रैदास की संतानो’ लिखी है। यह कविता इस दृष्टि से और भी अर्थपूर्ण है कि यह उन दलितों को भी सबक सिखाती है, जो जानबूझकर ब्राह्मणवाद के भक्त बने हुए हैं और नहीं जानते कि उसी के कारण उनकी दुर्गति हो रही है। इस कविता में रैदास की संतान शब्द मोची के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कवियित्री कहती है–
ओ! रैदास की संतानों
चप्पल में कील ठोकने के बजाए
क्यों नहीं ठोक देते कील
पास बैठे पंडित जी के हृदयहीन सीने में
जो वर्णव्यवस्था के अंगरक्षक हैं
भेदभाव के संरक्षक हैं।[26]
लेकिन पंडित जी के हृदयहीन सीने में कील ठोकने का साहस तो तब हो, जब उस मोची में चेतना हो। अगर उसमें चेतना होती, तो वह मोची का काम ही क्यों करता? अगर मेहतर में चेतना होती, तो वह कब का मैला उठाने का गंदा काम छोड़ चुका होता। यह चेतना ही है, जो अभी असंख्य दलितों में पैदा ही नहीं हुई है। इसलिए ऐसे मोची या मेहतर या खटिक या अन्य दलित जातियों के लोग पंडितों की ही सेवा-पूजा करते रहते हैं। यथा–
अरे, तुम तो गर्व करते हो अपने आप पर
जब तुम्हारे पास पंडित जी बैठते हैं
तुम दौड़ पड़ते हो अपना काम छोड़ [27]
उनकी सेवा में।[28]
मीनू कहती हैं, ऐसे लोग अज्ञानी हैं। वे नहीं जानते कि उन्हीं ब्राह्मणों की वजह से वे नाली पर बैठे हुए हैं। यथा–
तुम उन्हीं की कृपा से ठोक रहे हो कील
वे ही कहते हैं, सब पढ़ गए तो कौन गांठेगा जूता?
क्या तुमने कभी सोचा, जानने की कोशिश की
उनके बेटे-बेटियां क्या करते हैं?
वे पढ़ते हैं देश-विदेश में,
वे नेता, अभिनेता, शिक्षक, वाइस चांसलर हैं
तुमने कभी सोचा ठंडे दिमाग से
तुम कहां हो? तुम कौन हो? तुम्हें क्या मिला?
अपमान, जलालत, बहिष्कार, तिरस्कार, गरीबी
गुलामों सा जीवन पीढ़ी-दर-पीढ़ी।[29]
आगे मीनू ने मोचियों के सामाजिक यथार्थ का जो चित्र खींचा है, वह वर्णव्यवस्था के समर्थक सवर्णों के मन में तो नहीं, पर संवेदनशील पाठकों के मन में जरूर करुणा जगा सकता है। किसी भी शहर में जूते गांठने वाले मोची प्राय: बदबूदार गंदे नाले या नाली के पास बैठते हैं। कहीं-कहीं तो उनके पीछे सार्वजनिक पेशाबघर होता है, जहां लोगों का पेशाब रिसकर उनके पास तक बहता है। डॉ. मंजू देवी ने अपनी शोध पुस्तक ‘आजादी पर उठते सवाल : नाली पर मोची’ में मोचियों की सामाजिक, आर्थिक और कर्मस्थली का वह आंखों देखा वर्णन किया है, जो मार्मिक होने के साथ-साथ भयावह भी है। उसी दृष्टि से मीनू बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती हैं–
तुम्हारी कर्मस्थली और तुम्हें देखकर
कहीं से नहीं लगता है
तुम इसी देश के नागरिक हो
और देश विकासमान है।[30]
डॉ. आंबेडकर ने भी अपने एक निबंध में सवर्ण और दलित के बीच दो पृथक राष्ट्रों जैसी दूरी बताई थी। यह भारतीय जीवन का घृणित सच है। दलित जहां भी रहते हैं, बहुत ही निरीह प्राणियों की तरह बेबस और लाचार बनकर एक ही देश में, एक ही कानून के तहत अजनबियों की तरह रहते हैं। विकास की धारा उनकी बस्तियों में नहीं पहुंचती। और इसका एकमात्र कारण यह है कि देश की शासन-सत्ता उन्हीं सवर्णों के हाथों में है, जो दलित जातियों को अशिक्षा, अज्ञानता, गंदगी और जलालत-भरे माहौल में रखना चाहते हैं। मीनू ने इसे एक और कविता ‘मरघट से गुजर कर’ में बेहतरीन बिंब के साथ चित्रित किया है। इस कविता में दो राष्ट्रों की पहचान साफ नजर आती है। यथा–
मैं बस से उतरी
सड़क भरी थी छोटे-बड़े वाहनों से
मैं किनारे खड़ी डरी-डरी थी
खड़ी अट्टालिकाएं ललाट ऊंचा किए।
फिर एक पग आगे बढ़ी।
मुझको दिखी छोटी मुहल्ला सी कालोनी
जिसमें नंगे-अधनंगे चिल्लपों करते बच्चे-औरतें
वस्त्र हैं मैले-कुचैले और वे अपने-अपने काम में मशगूल।
मैं आगे बढ़ी, उनके पास पहुंची दूजी ओर।
गंदला पानी, मच्छरों, मक्खियों और बीमारियों का स्रोत
लबालब एक जोहड़।[31]
कवियित्री ने जिस बस्ती का चित्रण किया है, वह एक मरघट के पास वाली बस्ती है, और वहां के निवासी चलती-फिरती जिन्दा लाशें हैं। कवियित्री लिखती है–
ये लोग मरघट वासी हैं?
क्या ये मरकर भूत हैं या शव सरीखे
ये रहते हैं मरघट में?
या मरघट इनमें रहता है?
क्या ईश्वर देख रहा है इन्हें?
या ये ही राह देख रहे हैं उसके आने की?[32]
वे भले ही कुछ सुख पाने के लिए ईश्वर की राह देखते हों, क्योंकि सरकार उनकी नहीं है। पर सच यह है कि कोई ईश्वर भी उनको नहीं देखता, क्योंकि सरकार की तरह ईश्वर भी उनका नहीं है।
रजत रानी मीनू सिर्फ उपेक्षित, शोषित, पीड़ित, अधिकारविहीन स्त्री और दलित की चीख को ही कविता में शब्द नहीं देती हैं, बल्कि उन चेहरों को भी बेनकाब करती हैं, जो उस चीख का कारण हैं। उनकी कविताओं में शब्दों की सादगी है, पर वे मार दूर तक करते हैं। वह सीधे-सरल शब्दों में कविता करती हैं, व्यर्थ में कल्पना से बिंब और प्रतीक नहीं गढ़तीं, बल्कि सहज स्वाभाविक रूप से अपनी बात कहती हैं। उनकी सभी कविताएं एक वैचारिकी निर्मित करती हैं। उसमें हम कबीर-रैदास, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, स्वामी अछूतानंद और डॉ. आंबेडकर की क्रांतिकारी परंपरा को देखते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनके कविता-कर्म में उनकी ऊर्जा इतिहास से नहीं, आंखों देखे यथार्थ से सृजित हुई है। उनका यह संपूर्ण संकलन बेहद पठनीय और विचारोत्तेजक है। अंत में मैं उनकी कविता ‘चीख’ की इन पंक्तियों से उनके ‘इतिहास और यथार्थ’ को रेखांकित करना चाहूंगा–
मैं ढूंढती हूं लोकतंत्र को इक्कीसवीं सदी में
मुझे चारों तरफ दिखता है सोलहवीं सदी का समाज
जहां जीवित रखे हैं अपने पुराने मूल्यों को
सामंती सोच को
राजतंत्र को अपने मन में।[33]
[1] रजतरानी मीनू, पिता भी तो होते हैं माँ (कविता-संकलन), वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2015
[2] वही, पृष्ठ 8
[3] वही, पृ. 9
[4] कैथरीन मेयो, स्लैव्स ऑफ दि गोड्स, हरकोर्ट, ब्रेस एंड कम्पनी, न्यू योर्क, 1929, पृष्ठ 229
[5] रजतरानी मीनू, उपरोक्त, पृ. 9
[6] वही, पृ. 10-11
[7] वही, पृ. 116-117
[8] वही, पृ. 117-118
[9] वही, पृ. 120
[10] वही, पृ. 27
[11] वही, पृ. 30-31
[12] वही, पृ. 34
[13] वही, पृ. 37-38
[14] वही, पृष्ठ 53-54
[15] वही, पृ. 168
[16] वही, पृ. 169
[17] वही, पृ. 39
[18] वही, पृ 39-40
[19] वही, पृ. 41
[20] वही, पृ. 45
[21] वही, पृ. 46
[22] वही, पृ. 46
[23] वही, पृ 46-47
[24] वही, पृ. 47
[25] वही, पृ. 50
[26] वही, पृ. 159
[27]32. वही, पृ. 76
[28] वही।
[29] वही, पृ. 159-160
[30] वही, पृ. 163
[31] वही, पृ. 42-43
[32] वही, पृ. 43
[33] वही, पृ. 76
(संपादन : नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in