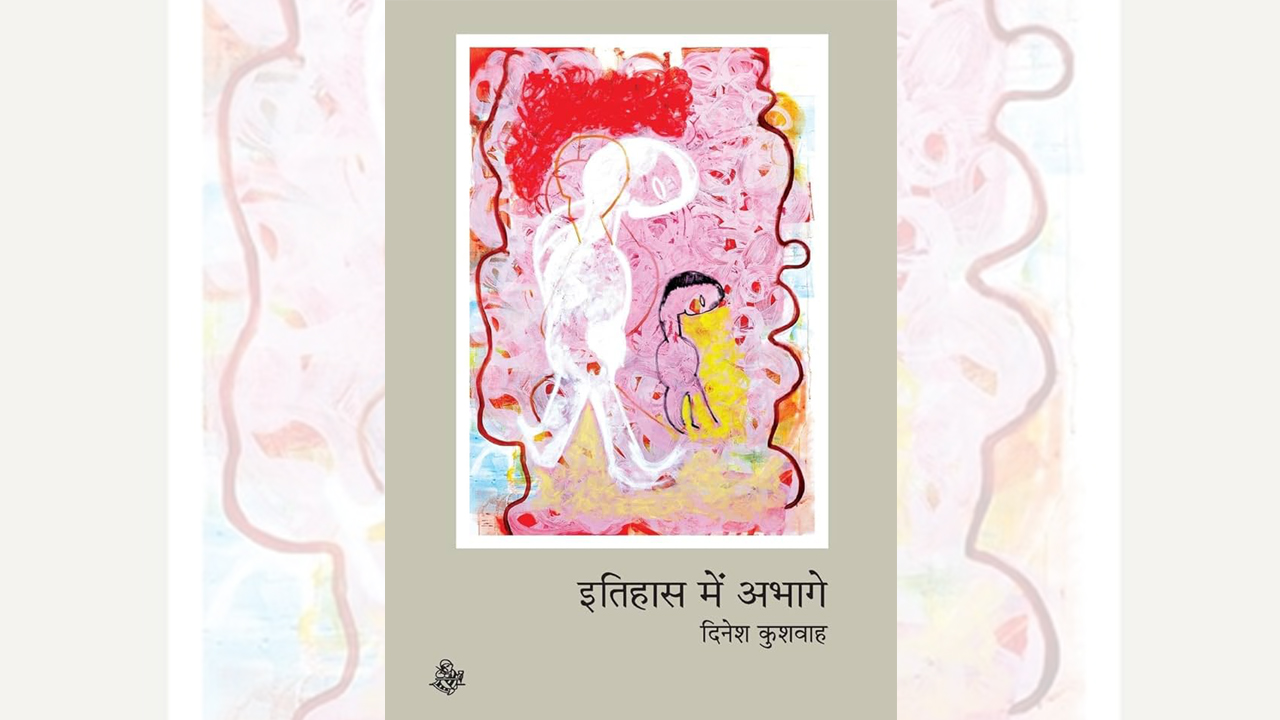कांचा आइलैय्या शेपर्ड की हाल ही में हिंदी में प्रकाशित पुस्तक ‘हिंदुत्व-मुक्त भारत की ओर’ को पढ़ते हुए, पहला विचार दिमाग में यह आया कि आदिवासियों तथा दलित-पिछड़ी जातियों पर हिंदू धर्म का कुछ भी उपकार नहीं है; यहां तक कि उनके विकास में भी उसका योगदान नहीं है। हां, अगर कुछ योगदान हिंदू धर्म का इन समुदायों पर है, तो वह उनके ज्ञान-विज्ञान, शिल्प और कला-कौशल के दमन और विनाश में है। तकनीकी तौर पर हिंदू धर्म का योगदान केवल ब्राह्मणों, ठाकुरों और वैश्यों के उत्थान और विकास में है और वह दिखाई भी देता है; यह मनुस्मृति के अध्ययन से भी हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है।
आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग भारत का वैज्ञानिक वर्ग है। मिट्टी और लोहे के बर्तन तथा औजार बनाना, पशु पालना, उनके चारे की व्यवस्था करना, उनको स्वस्थ रखना, दूध निकालना, दूध से मक्खन घी और छाछ बनाना, जमीन को उपजाऊ बनाकर खेती करना, बीज बनाना, पौध तैयार करना, लोगों के भरण-पोषण के लिए अनाज का उत्पादन करना, लोगों को सुंदर बनाने के लिए उनके दाढ़ी-बाल बनाना, पशुओं की खाल निकालना, उसे साफ़ करके उसे जूते और विभिन्न वस्तुएं बनाने के उपयोग में लाना, कपास से सूत बनाने के लिए करघा बनाना, कपड़ा बुनना, दरी-चादर और रजाई बनाना, इंटें पाथना, उन्हें पकाना, घरों का निर्माण करना, नालियां बनाना, लकड़ी काटना, उससे दरवाजे पीढ़े और खटिया बनाना, क्या उन्हें हिंदू धर्म ने सिखाया था? निश्चित तौर पर नहीं। प्रत्युत, हिंदू धर्म के निर्माता द्विजों ने अपने को जिंदा रखने के लिए इन उत्पादनों का उपयोग किया था। जब आधुनिक चिकित्सा और स्वास्थ्य-सेवाएं भारत में नहीं आईं थी, तब ये ही वर्ग घरों में नवजात शिशुओं का जन्म कराते थे, और उनके पोषण तथा विकास के लिए औषधियां बनाते थे। ये स्वभावत: वैज्ञानिक समुदाय थे, जिनके शिल्प-विज्ञान के विकास में हिंदू धर्म का कोई योगदान नहीं है।
कांचा आइलैय्या शेपर्ड के अनुसार ये हिंदुत्व-मुक्त समुदाय हैं। इसमें संदेह नहीं कि लेखक ने भारतीय समाज का जो अध्ययन किया है, वह समाजशास्त्र की दुनिया में पहला अध्ययन है, जिसने आदिवासियों, दलितों और पिछड़ी जातियों को एक नई पहचान दी है। उन्होंने अपने अध्ययन की यात्रा आदिवासी समाज से शुरू की है, जिसे वह ‘अवैतनिक शिक्षक’ का दर्जा देते हैं। इसके बाद वह दलित वर्ग को लेते हैं, जिन्हें ‘सबाल्टर्न वैज्ञानिक’ की संज्ञा देते हैं। शूद्र श्रेणियों को वह ‘सामाजिक चिकित्सक’ के रूप में देखते हैं। इसी तरह वह वैश्यों को ‘सामाजिक तस्कर’ और ब्राह्मणों को ‘आध्यात्मिक फासीवादी’ और ‘बौद्धिक गुंडों’ के रूप में देखते हैं, जो बेहद गौरतलब और विचारोत्तेजक है। लेखक ने अपने अध्ययन में इन श्रेणियों के बारे में क्या कहा है, इसका एक संक्षिप्त अवलोकन आवश्यक है।
पहला अध्याय आदिम जनजातियों पर है, जिसका लेखक ने ‘बिना भुगतान के शिक्षक’ नाम रखा है। लेखक का मत है कि जनजातीय लोगों ने ही हमारी संस्कृति और सभ्यता की बुनियाद रखी– “उन्होंने हमें सिखलाया कि हमें जिंदा रहने के लिए क्या खाना और क्या पीना चाहिए।” उनके अनुसार, “कंद-मूलों और फलों की कई किस्में हैं, जिन्हें जनजातीय लोग जानते हैं कि वे खाने के योग्य हैं। कंद या जड़, जो हम खाते हैं, कच्चा या पकाया हुआ, इनकी उत्पत्ति जनजातीय ज्ञान में है। जनजातीय लोगों के पास कुछ ऐसे जड़-आहारों का ज्ञान है, जो सूखे और अन्य कठिन स्थितियों में उन्हें जिंदा रख सकते हैं। यह ज्ञान अब उनके अपने ज्ञान-तंत्र के अंदर सीमित रह गया, क्योंकि उनके ज्ञान को प्रामाणिक नहीं माना गया।”
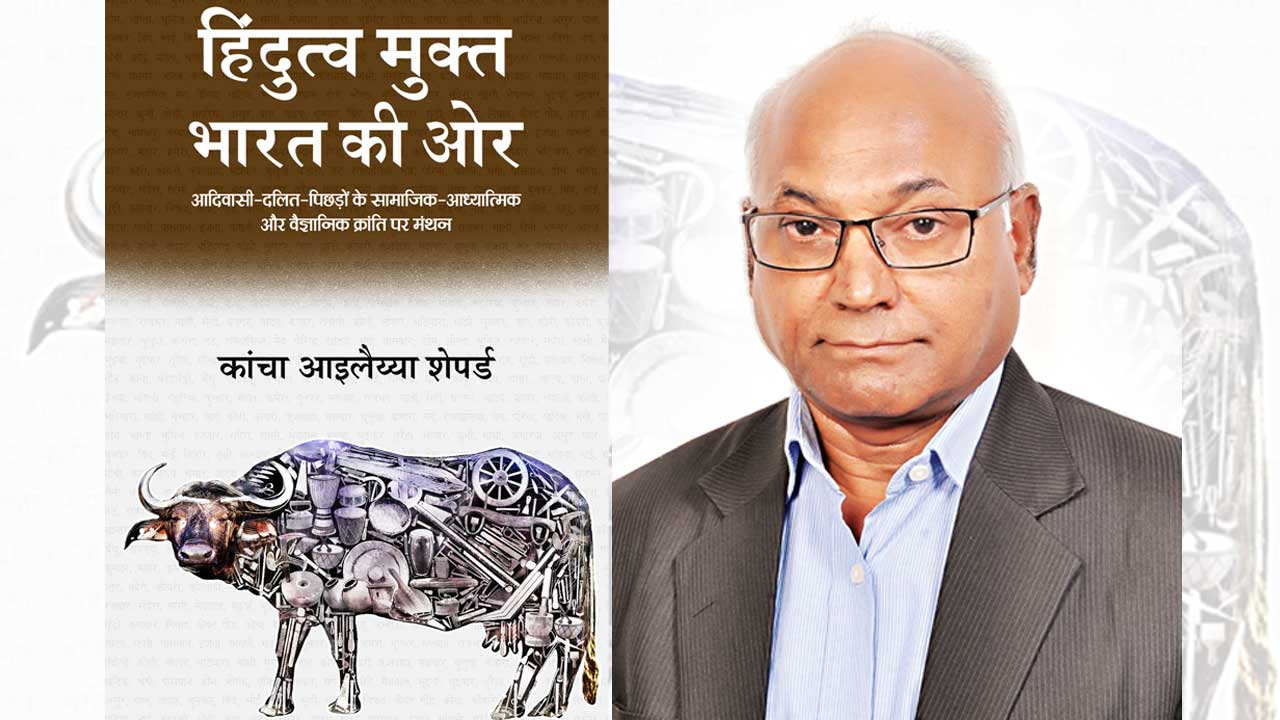
लेखक ने उशिल्लू नामक कीट के आहार का जिक्र किया है। उनके अनुसार, “उशिल्लू बरसात के मौसम में ही प्रकट होते हैं। जनजातीय लोगों ने उशिल्लू कीट को खाने योग्य इसलिए चुना, क्योंकि उनको खाना उनका ऊर्जा-स्तर बढ़ा देता है। वर्षा ऋतु में शिकार करने के स्थल भीगे और दलदली हो जाते हैं। जिन जानवरों का वे सामान्य रूप से शिकार करते हैं, वे घनी हरी झाड़ियों और जंगलों का फायदा उठाकर भाग जाते हैं। हालांकि वर्षा ऋतु में वे पर्याप्त जड़-आहार खाते हैं, लेकिन यह फलों का मौसम नहीं होता। इसलिए उन्होंने उशिल्लू और यिप्पा फूलों के उत्कृष्ट मिश्रण की खोज की।”
इसी प्रकार जनजातीय लोगों ने कई पेय पदार्थों की भी खोज की। लेखक लिखता है, “गोंड, कोया, लम्बाडा और कोंडारेड्डी के खानपान के महत्वपूर्ण अंश थे– स्वाभाविक और कृत्रिम तरीके से बनाए हुए मादक पेय पदार्थ। जनजातीय ज्ञान-व्यवस्था के क्षेत्र में पेड़ से रस निचोड़ना नियमित रूप से फल, जड़ एवं मकरंद एकत्रित करने का हिस्सा है। ताड़ी और इआटा बहुत लोकप्रिय पेय पदार्थ हैं। कुछ जनजातियां नीम के पेड़ से भी एक मादक पेय निकालने में माहिर हैं।”
किताब का दूसरे अध्याय का शीर्षक ‘सबाल्टर्न वैज्ञानिक’ है। इस अध्याय में लेखक का कहना है कि तेलुगु भाषी क्षेत्र में किसी भी गांव की शुरुआत मडिगावाड़ा से होती है। लेखक के अनुसार मडिगा उत्तरी भारत के चमार हैं– “मडिगावाड़ों ने खाल को चमड़े में और चमड़े को वस्तुओं में बदलने की एक पूरी प्रक्रिया का विकास किया। इस प्रक्रिया के लिए एक ऐसे मस्तिष्क की आवश्यकता थी, जो चमड़े के अशुद्ध होने के मिथक से मुक्त होकर इसे एक कुटीर उद्योग के रूप में आरंभ कर सके। भारत में इस कुटीर उद्योग को स्थापित करने का कौशल मडिगाओं अर्थात चमारों ने हजारों साल से अर्जित किया।”
उनके वैज्ञानिक कौशल का उल्लेख करते हुए लेखक ने लिखा है, “जिस पद्धति से मृत पशु की देह से खाल उतारी जाती है, उसमें भी कौशल-आधारित विशिष्ट ज्ञान की प्रक्रिया शामिल होती है। खाल में बिना कोई छेद किए उतारने के लिए हाथों और चाकू का उच्च कौशल-युक्त प्रयोग जरूरी है, जो सामान्य प्रयोगों के माध्यम से पूर्णता तक पहुंचा। भीगी खाल को सड़ने से बचाने के लिए नमक की उपयोगिता का आविष्कार भी मडिगा/चमारों द्वारा सदियों पहले कर लिया गया था। खाल को नमक लगाकर तंगेडू नामक पेड़ की छाल के चूर्ण के घोल में डुबोकर रखा जाता है। यह प्रक्रिया पंद्रह दिनों तक चलती है। हर दिन इस पानी का खट्टापन जांचा जाता है। हर गुजरते दिन तंगेडू के रासायनिक तत्व खाल में जज्ब हो जाते हैं, और धीरे-धीरे खाल कड़ी होकर चमड़े में बदल जाती है।” लेखक आगे कहता है, चमड़े से उपयोगी चीजें बनाने के लिए मडिगाओं ने जिस ज्ञान का इस्तेमाल किया, वह रचनात्मक भी था और वैज्ञानिक भी। लेखक के अनुसार, “मडिगाओं ने ही चमड़े के काम को लौह तकनीक से जोड़ा। उन्होंने कच्चे लोहे को पिघलाने के लिए कोलिमी यानी चमड़े की धौंकनी बनाई, जो लुहार की पूरी कार्य-प्रणाली का केंद्र बनी। चमड़े की धौंकनी एक आधुनिक उपकरण था, जिसके निर्माण में भौतिकी का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत शामिल था कि खाली स्थान हवा को अपने भीतर खींचता है। धौंकनी के प्रारूप में एक क्रांतिकारी बदलाव तब आया, जब बोरे के भीतर एक छोटा छेद बनाकर अंदर की तरफ से एक चमड़े का वाल्व उसमें सिल दिया गया। जब बोरे को ऊपर से दबाया जाता, वाल्व उठ जाता और बाहर की हवा उसके अंदर आ जाती। जैसे ही वाल्व बंद होता, हवा भट्ठी के अंदर चली जाती।”
चमारों का दूसरा आविष्कार, लेखक के अनुसार, चमड़े की बाल्टी का निर्माण है। लेखक लिखता है कि “भारत में सिंचाई का काम शुरू में कुंओं से होता था, जिसमें कुंओं से पानी निकालने के लिए बाल्टी की जरूरत होती थी। मडिगाओं ने चमड़े को गोल आकारों में सिलकर कई किस्म की बाल्टियां तैयार कीं, जिनमें पानी को बाहर निकालने के लिए एक पाइप भी पूंछ की तरह बना होता था।” लेखक कहता है कि मडिगाओं की बाल्टियां हमारी आज की बाल्टियों और टबों आदि की पूर्वज हैं। इन पंक्तियों के लेखक, यानी मैंने स्वयं उन्नीस सौ सत्तर के दशक में भिश्तियों को चमड़े की मश्कों से मुस्लिम घरों में पानी की आपूर्ति करते देखा है। तब नगरपालिकाओं में भी सड़कों पर छिड़काव के लिए भिश्तियों को ही नियुक्त किया जाता था। ये मश्कें बकरी या भेड़ की खाल की बनी होती थी, और उन्हें चमार कारीगर तैयार करते थे।”
कांचा आइलैय्या लिखते हैं कि कृषि-कार्य के उपयोग में आने वाली चमड़े की रस्सियों तथा पट्टों के अलावा चमड़े के थैले भी मडिगाओं ने बनाए, जिनका उपयोग अनाज को ले जाने और सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। “चार हजार साल पहले जूते/चप्पल बनाकर मडिगा/चमारों ने खेती और रिहाइश के लिए भूमि को अपने अनुकूल बनाने के रास्ते का भी एक बड़ा कांटा दूर कर दिया था, क्योंकि शीतोष्ण जंगलों में बिना जूतों के प्रवेश करना बहुत कठिन था।”
कांचा आइलैय्या लिखते हैं कि संगीत के उपकरण बनाने में भी मडिगा/चमारों का बहुत बड़ा योगदान है। असल में पानी और पाता (गायन) दलित संस्कृति का हिस्सा है और ‘चदायु’ और ‘संध्या’ (पाठ और प्रार्थना) ब्राह्मण संस्कृति का। मडिगाओं ने डप्पू अर्थात डफली का निर्माण किया। वह कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आदिवासियों ने संगीत-यंत्रों की रचना नहीं की। उन्होंने भी अपने संगीत-यंत्र बनाए, लेकिन वे उन्हीं तक सीमित रह गए, जबकि डप्पू की पहुंच सभी समुदायों तक बनी, जिनमें ब्राह्मण भी शामिल थे। डप्पू लकड़ी और चमड़े से बना वाद्य है। इसे बनाने के लिए लकड़ी की एक खपच्ची को मोड़कर गोल कर लिया जाता है, और चमड़े की रस्सी से उसे बांध दिया जाता है। फिर खपच्ची में छेद करके चमड़े को उसमें एक तरफ सिल दिया जाता है। जैसे-जैसे चमड़ा सूखता है, वह तन जाता है और जरा-सा छूने पर भी संगीतमय ध्वनि उत्पन्न करता है। वह आगे लिखते हैं, “डोलू और जग्गू नामक वाद्य, जिन्हें यादव/कुरुमा समुदाय के लोग बजाते हैं, डप्पू से मिलते-जुलते ही हैं। मडेला, जिसका प्रयोग कर्नाटक संगीत में किया जाता है, और तबला भी डप्पू के ही ऋणी हैं।”
इस अध्याय को पढ़ते हुए मुझे याद आया कि मेरे रामपुर शहर में भी जाटवों का एक मुहल्ला है, जहां के जाटव कारीगर तबला बनाने और चमड़े से मढ़ने का काम करते हैं। उनके इसी काम की वजह से इस मुहल्ले का नाम ‘तबलचियान’ पड़ा। इन जाटव कारीगरों के बनाए गए तबले भारत में ही नहीं, विदेशों में भी मशहूर हैं।
‘उत्पादक सैनिक’ के रूप में लेखक ने आंध्र प्रदेश के मालावाड़ा के मालाओं का उल्लेख किया है। ये महाराष्ट्र में महार हैं। लेखक लिखता है कि मालाओं ने “बतौर सैनिक और भूमि-अभियंता दोनों रूपों में ग्रामीण समुदाय को प्रकृति के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाने में सहयोग किया है।” लेखक के अनुसार, रक्षा के संबंध में मालाओं की धारणा क्षत्रियों से भिन्न थी। क्षत्रिय राज्य की रक्षा में विश्वास करते थे, जबकि माला ग्रामीणों की सुरक्षा करते थे।
इसके बाद लेखक ने चाकलियों का जिक्र किया है, जिन्हें धोबी कहा जाता है। इस समुदाय को लेखक ने ‘सबाल्टर्न नारीवादी’ की संज्ञा दी है। उन्होंने लिखा है कि “धोबी/चाकली शूद्र समाज की पहली सीढ़ी हुए, जिन्हें बावजूद उनकी काबिलियत के, मूर्ख का ख़िताब दिया गया, जबकि चाकलियों का ज्ञानाधार वह प्राथमिक आधार है, जिस पर पूरे शूद्र समाज को गर्व करना चाहिए।” लेखक के अनुसार सदियों पहले चाकलियों ने ही कपड़े धोने के लिए मिट्टी के साबुन की खोज की थी। तेलुगुदेशम में इस साबुन को ‘चाऊडू माटी’ कहते हैं। (हिंदी क्षेत्र में इसे ‘रे’ बोलते हैं) किंतु ‘सिर्फ मिट्टी के साबुन से कपड़ों में मौजूद संक्रामक कीटाणु समाप्त नहीं होते थे। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने कपड़ों को उबालने की तकनीक की खोज की। लेखक लिखता है कि चाकलियों/धोबियों ने व्यक्तिगत सौंदर्य के साथ सामाजिक सौंदर्य को भी अपना लक्ष्य बनाया। गांव की सामूहिक सुंदरता तभी संभव थी, जब वहां के निवासियों के कपड़े साफ़-सुथरे हों। लेखक के अनुसार, चाकली समुदाय के नारीवाद का संबंध कपड़ों की धुलाई से है। वह लिखता है, “किसी भी चाकली पुरुष में किसी भी अन्य भारतीय पुरुष के मुकाबले स्त्री-सुलभ गुण ज्यादा होते हैं। स्त्री-यौनिकता की उसकी समझ औसत हिंदू पुरुष के मुकाबले कहीं ज्यादा मूलगामी होती है। लेकिन इस समझ को सम्मान के काबिल नहीं समझा गया; न इसे सामाजिक दृश्यता मिली, न उसका आर्थिक आधार मजबूत हुआ।”
किताब का पांचवां अध्याय ‘सामाजिक चिकित्सक’ है, जिसमें मांगली अर्थात नाई समुदाय के समाज-विज्ञान का वर्णन किया गया है। कांचा आइलैय्या लिखते हैं, “मांगली सामाजिक चिकित्सक थे, जो मनुष्य की शारीरिक संरचना का ज्ञान रखते थे और यह जानते थे कि कैसे शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखा जाए। … बालों को काटने, शरीर की हजामत, नाखून काटने और उन्हें रगड़कर सुंदर बनाने की प्रथा वे सेवाएं थीं, जिन्हें नाइयों ने सदियों से प्रदान कीं। यह कार्य मनुष्य को पशु से अलग करता है, क्योंकि पशु अपने शरीर की हजामत नहीं कर सकते।” आगे लेखक ने बहुत ही विचारणीय बात कही है कि ब्राह्मणवाद ने सन्यासी प्रथा को जन्म देकर नाईगीरी को अध्यात्म-विरोधी कहकर नाइयों को सन्यासी ब्राह्मणों का शरीर स्पर्श करने पर रोक लगा दी। परिणामत: शरीर पर जितने लंबे बाल, वह उतना ही बड़ा सन्यासी, जिसके जितने बिना धुले बाल, वह उतना दैवीय साधु हुआ। इस संन्यास के विरुद्ध सातवीं ईसा पूर्व शताब्दी में जैन धर्म ने विद्रोह किया। बौद्ध धर्म ने भी अपने भिक्षुओं के लिए मुंडन को आवश्यक बताया। इससे नाईगीरी के विकास को बल मिला।
कांचा आइलैय्या शेपर्ड की किताब का एक और महत्वपूर्ण अध्याय यादव समुदाय पर है, जिसका नाम ‘मांस और दूध के अर्थशास्त्री’ है। वह लिखते हैं कि पशुपालन अर्थव्यवस्था के केंद्र में चार किस्म के पशु हैं– गाय-बैल, भैंसें, भेड़ें और बकरियां। दूध देने वाले पशु के रूप में भैंसों को भारतीय नागरिक समाज में लाने का श्रेय यादवों को जाता है। लेकिन यादवों का स्थान हिंदू समाज में सर्वोच्च नहीं है। यादवों को कृष्ण का वंशज माना जाता है। इस संदर्भ में कांचा आइलैय्या ने बहुत ही रोचक प्रश्न उठाया है कि “पशुपालक होते हुए अगर कृष्ण गीता लिख सकते हैं, तो यादवों को भी शिक्षा पाने और किताबें लिखने का अधिकार मिलना चाहिए था। ऐसा होता तो अब तक भारत की ज्यादातर जनसंख्या शिक्षित हो चुकी होती, हर गड़रिया और पशुपालक शिक्षित हो गया होता, जैसा कि उन देशों में हुआ, जहां मानव-समानता कम-से-कम आध्यात्मिक स्तर पर तो रही है।”
आगे लेखक ने यादवों के सशक्त वैज्ञानिक, तकनीकी और अर्थशास्त्रीय ज्ञान पर प्रकाश डाला है, जो दिलचस्प होने के साथ-साथ विचारोत्तेजक भी है।
सातवां अध्याय ‘गुमनाम अभियंता’ नाम से है, जिसमें लेखक ने गौड़, कमसली, कम्मारी और चंद्रांगी आदि कामगार जातियों के अभियंत्रण ज्ञान का प्रभावशाली चित्रण किया है। लेखक के अनुसार ताड़ी निकालने का काम करने वाले दलित जातियों के लोगों का अभियंत्रण कौशल ऐसे पेड़ों की खोज से शुरू होता है, जिनसे ऐसा तरल पदार्थ टपकता है, जो पीने योग्य हो और हाजमा ठीक करता हो। लेखक लिखता है कि ताड़ का पेड़ बिना टहनियों का लंबा पेड़ होता है, जिस पर छिपकली की तरह चढ़ा जाता है। ऊपर चढ़कर वह उस हिस्से को काटता है, जिससे ताड़ी का रस टपकता है। वहां वह घड़ा लटकाता है। यह अद्भुत तकनीक का काम है, जिसमें शुरूआती चरण में उस पेड़ का व्यवस्थित अध्ययन भी शामिल है।
इसके बाद लेखक ने इसी अध्याय में अभियंत्रण कौशल के तीन अन्य समुदायों—लोहार, बढ़ई और सुनार का जिक्र किया है। लोहारगिरी एक ऐसा कौशल है, जिसके बल पर ही भारतीय सभ्यता का विकास हुआ, और कृषि क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति हुई। लोहा पिघलाने के लिए लोहार के द्वारा बनाई गई भट्ठी अद्भुत विज्ञान है, जो चर्मकार और लोहार के मिश्रित ज्ञान से बना उपकरण है। इसी तरह बैलगाड़ी का निर्माण बढ़ई का ही आविष्कार है। मेरे विचार में अगर भारत की शिल्पकार जातियों को ब्राह्मणों ने शिक्षा से वंचित न किया होता, तो रेल, कार और हवाईजहाज का आविष्कार भी भारत में ही हुआ होता। क्या कुम्हार के चाक और भट्ठी को भुलाया जा सकता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाने और पकाने की वैज्ञानिक पद्धति का अद्भुत उदाहरण है? क्या सुनारों की कला के बिना आभूषणों का निर्माण हो सकता था? जब आज की तरह गहने बनाने की अत्याधुनिक मशीनें नहीं थीं, तब सुनार किस तरह से सुंदर आभूषण बनाते थे? वह ज्ञान उन्हें किसी विश्वविद्यालय से नहीं मिला था, अपितु उनकी अपनी महान परंपरा से मिला था। “गहना निर्माण के परंपरागत तरीके में एक ग्रामीण सुनार सोने को एक कुल्हिया में बैठाता है, और उसे कोयले की एक छोटी अंगीठी पर रखता है। वह मुंह से फूंकने वाली फुंकनी का इस्तेमाल करता है। वह अपने फेफड़ों पर जोर देकर तब तक फूंकता रहता है, जब तक कुल्हिया में रखा सोना पिघल न जाए। उसके बाद सुनार पिघले हुए सोने को धागों के रूप में फैलाता है, और उन धागों को सुंदर आभूषणों में ढाल देता है।”
किताब का सबसे महत्वपूर्ण और सनसनीखेज अध्याय ‘सामाजिक तस्कर’ है, जिसे एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में भी अलग से छापा गया था, और जिसके विरोध में लेखक के विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था। इस अध्याय में ऐसा क्या है कि इसका विरोध हुआ? तो इसका उत्तर यह है कि कांचा आइलैय्या ने इस अध्याय में वैश्य वर्ग अर्थात बनियों को सामाजिक तस्कर की संज्ञा दी है। यह अपने आप में एक ऐसा शब्द है, जिसे बनियों ने अपने अपमान के रूप में लिया।
कांचा आइलैय्या के अनुसार, तस्कर वह होता है, जो किसी चीज को गुप्त रूप से नियम के विरुद्ध छिपाकर रखता है या बाहर ले जाता है। चूंकि, हिंदू वर्णव्यवस्था ने व्यापार की संपूर्ण प्रक्रिया को वैश्य समुदाय को ही सौंपा, और ऐसा ब्राह्मणों ने आध्यात्मिक माध्यमों से स्वयं को उनके धन का उपयोग करने के अधिकार को स्वीकृत करके किया, इसलिए उपरोक्त अर्थ में तस्करी के सभी रूपों का आरंभ बनियों ने ही किया। लेखक के अनुसार गुप्त धन की अवधारणा बनिया अर्थशास्त्रियों द्वारा विकसित की गई थी। गुप्त धन को अक्सर भूमि में गाड़कर रखा जाता था, जो बिना किसी सामाजिक उपयोग के भूमिगत ही रहता था। मजबूर लोगों को कर्ज देकर ब्याज में उनकी संपत्ति कब्जे में लेने, अधिकारियों को रिश्वत देकर टैक्स की चोरी करने, जमाखोरी, मिलावट और घटतोली के द्वारा भ्रष्टाचार करने आदि सारे अवैध आर्थिक कर्मों की शुरुआत बनियों द्वारा ही की गई। लेखक का कहना है कि विश्व के किसी भी देश से अधिक अथाह भूमिगत धन भारत में है, जो काला धन भी कहलाता है। मंदिरों के तख्खानों में बंद स्वर्ण-धन भी किसी सामाजिक उपयोग में नहीं आता। इसमें भी अधिकांश रूप से बनियों का ही गुप्त धन है। लेखक कहता है कि ब्राह्मणों ने धन के माध्यम से पूजा का एक तरीका ईजाद किया और बनिया सामाजिक रूप से तस्करी किए हुए धन को मंदिरों पर खर्च करने के लिए मौजूद थे। इस प्रकार, हिंदू मंदिर आज की तारीख तक ब्राह्मण और बनिया इन दो भ्रष्ट जातियों के खेल के मैदान हैं। लेखक का स्पष्ट मत है कि गुप्त धन अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने का एक विशिष्ट बनिया तरीका था, जिसने सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध व्यापक आर्थिक विनाश किया।
लेखक ने दसवें अध्याय में ब्राह्मणों को ‘आध्यात्मिक फासीवादी’ मानते हुए लिखा है कि “भारत के ब्राह्मणों ने जिस आध्यात्मिक फासीवाद की स्थापना की, उसमें अन्य धर्मों की तरह अपने विकास-क्रम के दौरान अपने आपको बदलने की व्यवस्था नहीं है। इसी ने दुनिया की सबसे भयावह बीमारी– मानव-अस्पृश्यता को जन्म दिया।” उन्होंने लिखा कि ब्राह्मणों के आध्यात्मिक फासीवाद का स्रोत उनके द्वारा निर्मित देवी-देवता हैं, जिन्हें उन्होंने युद्ध करने, और अपने विरोधियों की हत्या करने का काम सौंपा। उनके अनुसार इस फासीवाद का मूल तत्व असमानता है। इसलिए कोई भी ब्राह्मण जातिगत भेदभाव के उन्मूलन की बात नहीं करता। लेखक ने राजनीतिक और आध्यात्मिक फासीवाद में अंतर करते हुए लिखा है कि राजनीतिक फासीवाद जो सोचता है, स्पष्ट शब्दों में कहता है। किंतु राजनीतिक तानाशाह को बदलने की गुंजाइश रहती है, जबकि आध्यात्मिक फासीवाद को बदलने की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि वह जो सोचता है, वह नहीं कहता। लेखक के अनुसार, “यह तथ्य कि ब्राह्मणों ने ईसाई मिशनरियों से शिक्षा पाई, सिद्ध करता है कि ब्राह्मण बहैसियत एक जाति जो भी सीखते हैं, सिर्फ अपने हित में सीखते हैं, और अपने आध्यात्मिक फासीवाद में कोई बदलाव नहीं करते।”
लेखक ने अध्याय के अंत में लिखा है कि ब्राह्मणवाद का बना रहना दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। इससे लड़ने के लिए दलित-बहुजनों को आगे आना होगा। पर लेखक का निष्कर्ष है कि “दलित-बहुजन समाज के परिवर्तनकारी विमर्श को लाने का प्रयास ब्राह्मणवाद के विरोध के चलते, हो सकता है कि यहां एक गृहयुद्ध की शुरुआत हो जाए, जिसे ब्राह्मणवाद ने इतिहास के किसी भी मोड़ पर और किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया।”
बारहवें अध्याय में लेखक ने गृहयुद्ध के लक्षण और स्थितियों पर विचार किया है, और लिखा है कि भारत गृहयुद्ध की ओर जा सकता है। उनका मत है कि जिस तरह पश्चिम में गृहयुद्धों ने गरीबों की स्थितियों को बदल दिया, उसी प्रकार भारत के दलित-बहुजन समाज में बदलाव के लिए भी एक ऐसे गृहयुद्ध की आवश्यकता है, जो हिंदुत्व-मुक्त भारत के निर्माण के लिए हो। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ऐसे गृहयुद्ध की ओर संकेत नहीं करतीं हैं, क्योंकि दलित-पिछड़ा बहुजन समाज अपनी हिंदू पहचान के साथ ब्राह्मणवादी जाल में फंस चुका है।
लेकिन फिर भी दलित-बहुजनों को इस किताब को अवश्य ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह उन्हें उनकी अस्मिता और उनके इतिहास से तुलनात्मक रूप से अवगत कराती है। हालांकि यह किताब तेलुगु भाषी क्षेत्र के समाज पर आधारित है, पर पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगता कि यह संपूर्ण भारत के समाज का सच नहीं है।
समीक्षित पुस्तक : हिंदुत्व मुक्त भारत की ओर
लेखक : कांचा आइलैय्या शेपर्ड
प्रकाशक : फारवर्ड प्रेस, नई दिल्ली
मूल्य : पांच सौ रुपए
(संपादन : राजन/नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in