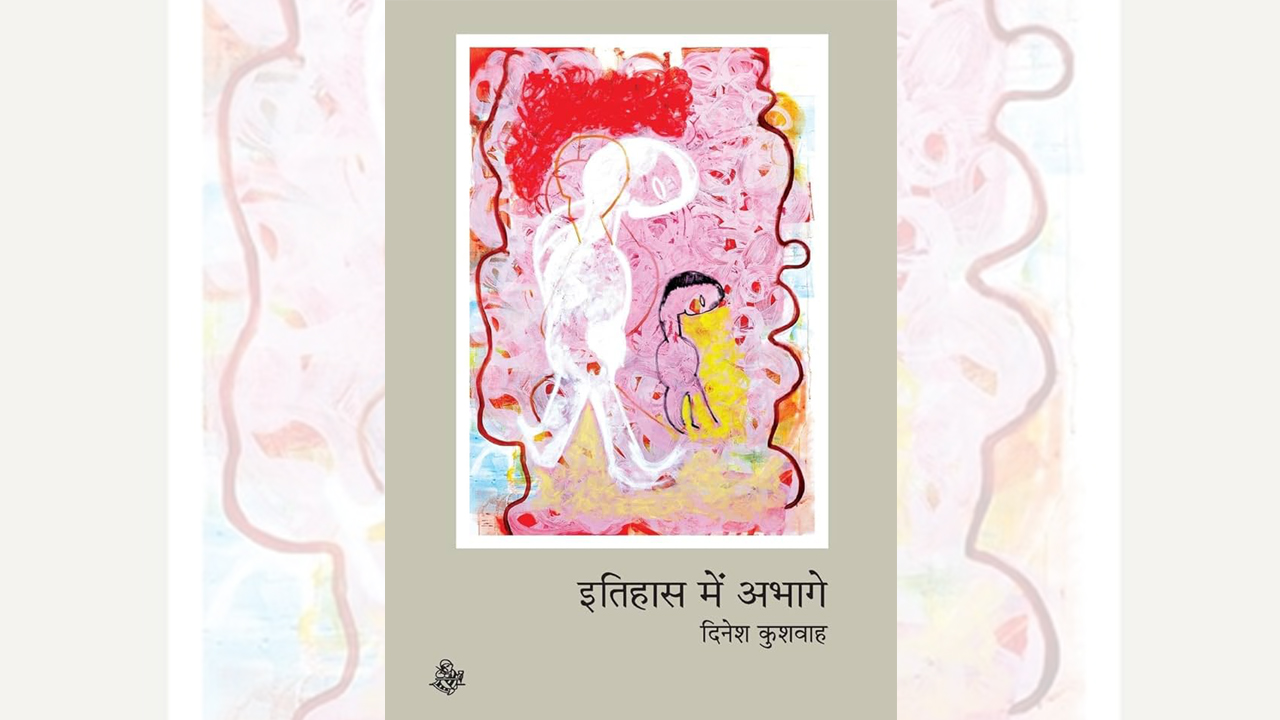डॉ. रामविलास शर्मा ने अपने एक निबंध में लिखा है– “प्रचीन भारत में भरत, कोसल और मगध, इन तीनों गण-समाजों की निर्णायक भूमिका थी। भरत गण यज्ञवादी संस्कृति का उपासक था। मगध गण इसका परम विरोधी था। मगध की आधार भूमि से ही जैन और बौद्ध धर्म का प्रवर्तन हुआ।…. मगध और भरत गणों के बीच में पड़ते थे कोसल। ये लोग कर्मकांडी नहीं थे और वेद-विरोधी मतों के प्रचारक भी नहीं थे। ये लोग मुख्यतः कवि और कविता-प्रेमी जन थे। महाभारत और रामायण, इन दोनों महाकाव्यों का घनिष्ठ संबंध कोसल गण से है।… वाल्मीकि तमसा के किनारे रहते थे। वह आदि कवि के रूप में विख्यात हैं। रवींद्र नाथ ठाकुर की ‘भाखा ओ छंद’ नाम की कविता में वाल्मीकि नारद से कहते हैं, ‘अब तक देवताओं का काव्य लिखा गया है, मैं अपने काव्य में मनुष्य को अमर करूंगा।’”
डॉ. शर्मा आगे लिखते हैं– “रवींद्रनाथ ने बड़े मर्म की बात पकड़ी। वाल्मीकि उस काव्य-परंपरा को जन्म दे रहे थे, जो देवोपासक नहीं, बड़ी गहराई से मानवतावादी है। उनके काव्य के आरंभ में किसी देवता की वंदना नहीं है। वह घोषित करते हैं कि यह काव्य द्विजों के लिए ही नहीं, शूद्रों के लिए भी है। उनके चरितनायक राम अपने मनुष्य होने की सगर्व घोषणा करते हैं।”
अतः कहना न होगा कि कोसल की आधार-भूमि महाभारत के रचयिता वेदव्यास के साथ-साथ वाल्मीकि के काव्य-दर्शन और मूल्यों के अध्ययन की समस्या को भी सरल करती है। शायद, इसीलिये वाल्मीकि की विचारधारा मिश्रित विचारधारा है। वह वैदिक चिंतन-परंपरा का उल्लंघन भी नहीं करते हैं और अवैदिक भौतिक विचारधारा को अपने मानवतावाद का अंग भी बनाते हैं। वह किस ओर अधिक गए हैं, प्रवृत्ति की ओर या निवृत्ति की ओर? इस पर बहस हो सकती है, लेकिन समग्रतः उनका दृष्टिकोण समन्वयवाद ही है और इस समन्वय में उनका मानवतावाद सामंती मूल्यों से टकराता हुआ, बड़ी सफाई से प्रगतिवाद की ओर उन्मुख हो गया है।
वाल्मीकि के जीवन-मूल्य धार्मिक हैं और धर्म से उनका तात्पर्य है– “आहुं: सत्यं हि परमं धर्म धर्मविदो जनाः” अर्थात, धर्मज्ञ लोग सत्य को ही सर्वश्रेष्ठ बतलाते हैं। यह है वाल्मीकि की परिभाषा। जो सत्य का उद्घाटन करता है, वही धर्म का पालन करता है। कर्मकांडों में धर्म नहीं है, और न सब कुछ त्याग कर भगवान का भजन करने में धर्म है। ऐसे धार्मिकों पर तो उनका रोष है। वह ऐसे सब लोगों के लिये दुःखी हैं, जो भौतिक सुख का परित्याग कर धर्म की शरण में चले जाते हैं। ऐसे लोग कोई सुख न उठाकर केवल दुःख भोग कर ही नष्ट हो जाते हैं–
अर्थ धर्मपरा ये ये तांस्ताशोचामि नेतरान्।
ते हि दुःख मिह प्राप्य विनाशं प्रेत्य लेभिरे।।
धर्म तो अर्थ-सुख का साधन है– “धर्मादर्शः प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखम्।” परंतु अर्थ-सुख से धर्म की उपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। अर्थवान होकर अनैतिक रहना भी निंदनीय है और धर्मवान होकर निर्धन रहना भी हेय है। वैज्ञानिक प्रगतिवाद का यह बीजारोपण वाल्मीकि भारतीय साहित्य में पहले ही कर चुके थे।
धर्म, अर्थ और काम– इन तीनों को जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार किया गया है। धर्म से अर्थ की और अर्थ से काम की उत्पत्ति होती है। काम शरीर की आवश्यक मांग है, जिसकी उपेक्षा संभव नहीं है। परंतु अनैतिक काम भोग-विलास है, जो काम का अशिव रूप है। वाल्मीकि के अनुसार अशिव काम में डूबा हुआ मनुष्य धर्म और अर्थ का परित्याग कर दशरथ की भांति विपत्ति में पड़ता है–
अर्थधर्मौ परित्यज्य यः काममनुवर्तते।
एवमापद्यते क्षिप्रं राजा दशरथी यथा।।
क्योंकि काम के लोभी पुरुषों में ये तीन बुराइयां आवश्यक रूप से होती हैं– झूठ बोलना, पर-स्त्री-गमन करना और दूसरों के प्रति बिना वैर के ही क्रूर बर्ताव करना। यथा–
त्रीण्येव व्यसनान्यत्र काम जानि भवन्त्युत।
मिथ्या वाक्यं तु परमं तस्ताद् गुरुतरावुभौ।।
परदाराभिगमनं विना वैरं च रौद्रता।।
यहां वाल्मीकि को मध्यम-मार्गी समझना चाहिए। मध्यम-मार्ग से धर्म, अर्थ और काम के सेवन में अभ्युदय है और इस अभ्युदय का नाम ही मोक्ष है।
वाल्मीकि के नैतिक मूल्य भी जबर्दस्त हैं। माता, पिता और गुरु की सेवा का उपदेश तो सभी ने किया है। माता और पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है– “एष धर्मश्च सुश्रोणि पितुर्मातुश्च वश्यता।” यह उतनी अहम बात नहीं है, जितनी यह कि प्रत्यक्ष देवता- माता, पिता और गुरु के रहते हुए, अप्रत्यक्ष देवताओं की आराधना कैसे की जा सकती है? यथा–
अस्वाधीनं कथं दैवं प्रकारैरभिराध्यते।
स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुम्।।
क्योंकि, इन प्रत्यक्ष देवताओं के समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस पृथ्वी पर नहीं है– “नान्यदस्ति शुभापांगे तेनेदयभिराध्यते।” लेकिन, यह भी स्मरणीय है कि “जो गुरु घमंड में आकर कर्तव्य-अकर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और कुमार्गी हो जाय, वह फिर सेवा का नहीं, दंड का पात्र हो जाता है।” यह साहसपूर्ण निर्भीक अभिव्यक्ति भी हम वाल्मीकि में ही पाते हैं–
गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः।
उत्पथं प्रतिपन्नस्य कार्ये भवति शासनम्।।
धर्म के उपदेशकों का सर्वाधिक बल निष्काम कर्म पर रहा है। निष्काम कर्म अपनी जगह ठीक हो सकता है। लेकिन, वाल्मीकि का मत है कि वह मूर्ख ही है, जो फल पर विचार किये बिना ही कर्म करता है–
गुरुलाघवमर्थानमारम्ये कर्मणा फलम्।
दोषं वा यो न जानति स बाल इति होच्यते।।
कर्म दो ही होते हैं– शुभ और अशुभ। उसी के फलस्वरूप मनुष्य सुख या दुःख भोगता है–
यदा चरति कल्याणि शुभं वा यदि वाशुभम्।
तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः।।
यह वाल्मीकि के मानवतावाद का आशावादी रूप है, जो कल्याण की ओर अग्रसर है, लोक के भी और स्वयं के भी।
उनका संपूर्ण आग्रह लोक-कल्याण पर है। जो लोक के लिये क्रूर और आततायी है, यदि वह तीनों लोकों का ईश्वर भी हो, तो भी सांप की तरह मारा जाता है–
उद्वेजनीयो भूतानां नृशंसः पापकर्मड्डत्।
त्रयाणामपि लोकनामीश्वरोऽपि न तिष्ठति।।
कर्म लोकविरुद्ध तु कुर्वाणं क्षणदाचर।
तीक्ष्णं सर्वजनो हन्ति सर्प दुष्टमिवागतम्।।
ऐसे पापियों के साथ मैत्री भी ठीक नहीं है। पाप से घृणा करो, लेकिन पापी से नहीं, वाल्मीकि इस विचार के नहीं हैं, क्योंकि, पापी खुद तो डूबता ही है, दूसरों को भी लेकर डूबता है। वाल्मीकि के अनुसार, जैसे सांप वाले सरोवर में रहने वाली मछलियां सांप के साथ ही मारी जाती हैं, वैसे ही पापी के संसर्ग में आकर पापरहित मनुष्य भी मारा जाता है। लोक-कल्याण की इतनी जबर्दस्त हिमायत अन्यत्र दुर्लभ है–
अकुर्वन्तोऽपि पापानि शुचयः पाप संश्रयात्।
परपापैर्विनश्यन्ति मत्स्या नागह्नदे यथा।।
क्रोध, मनुष्य में सबसे बड़ा दुर्गुण है, जिसकी सभी निंदा करते हैं। वाल्मीकि भी क्रोध को क्षमा से शांत करने को कहते हैं– “यः समुत्पतितं क्रोधं क्षमयैव निरस्यति।” और, जिसने क्रोध को शांत कर लिया, वही वीर है– “कोपमार्येण यो हन्ति स वीरः पुरुषोत्तमः।” लेकिन, दूसरी ओर वाल्मीकि की यह भी स्वीकारोक्ति है कि क्रोध-रहित मनुष्य निष्क्रिय ही रहते हैं। जिनमें शत्रुओं के प्रति क्रोध रहता है, उनसे सभी भय खाते हैं– “निश्चेष्टाः क्षत्रिया मन्दाः सर्वेचण्डस्य विभ्यति।” है न नीत्शे की टक्कर का सिद्धांत!

वाल्मीकि की वाणी में दैव की आलोचना भी है और समर्थन भी। यह चौंकाने वाली बात हो सकती है। जब अंध-विश्वास और निरर्थक कर्मकांडों में धन लुटाने की बात चली तो वाल्मीकि चार्वाक के भौतिकवाद को आगे ले आए, जो बहुत जरूरी था। आखिर, धन की बरबादी भी तो लोककल्याण के विरुद्ध है। लेकिन, जीवन की स्वाभाविकता में वाल्मीकि दैववादी ही हैं–
गुण दोषौ न निश्चित्य त्यक्तवा दैव व्यपाश्रयम्।
करिष्यामीती यः कार्यमुपेक्षेत् स नराधमः।।
दुनिया के सभी धर्मो में चोरी को जघन्य पाप माना गया है। वाल्मीकि भी विभीषण के मुख से कहला देते हैं कि दूसरों का धन लूटने वाला दुरात्मा होता है– “परं स्वहरणे युक्तं … त्याज्यमाहुर्दुरात्मान्।” वाल्मीकि से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि वह निर्धनता का स्रोत खोजते। आखिर, प्रश्न तो धनिकों के धन की सुरक्षा का था, और धर्मादा का, जिससे उनके आश्रम की व्यवस्था होती थी।
लेकिन, जहां मौका मिला, वहां वाल्मीकि के कवि ने सत्य का बड़ी निर्भीकता से पक्ष भी लिया है। हनुमान अशोक वन में पहुंच कर राक्षसियों का वध करना शुरु कर देता है, क्योंकि उसके लिये वे सब पापी थीं। पर, सीता के मुख से वाल्मीकि ने बड़े मार्के की बात कहला दी है– “कोई पापी हो या पुण्यात्मा, किसी का भी अमंगल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं, जिसने कभी पाप न किया हो।” यथा–
पापानां वा शुभानां वा वधार्हाणामथापि वा।
कार्यं कारूण्यमार्येण न कश्चिन्ना पराध्यति।।
और, इसी में यह रहस्य भी बड़ी चतुराई से वाल्मीकि छोड़ गए हैं कि अशोक वन में बंदिनी सीता सुखी थी या दुखी? अगर सीता दुखी होती तो उसका स्वर कुछ और होता। लेकिन बिना यह भेद खोले वाल्मीकि ने चुटकियां लीं हैं और उसी में वह अपनी बात को बड़ी बारीकी से कह गए हैं। लेकिन स्मरण रहे कि यह वचन सामाजिक यथास्थितिवाद का भी समर्थन करता है।
वाल्मीकि के काव्य में जो सामंती मूल्य हैं, उनके साथ जबर्दस्त संघर्ष है और इस संघर्ष में उनका जनवाद आंशिक रूप में नहीं, पूर्ण रूप में सफल हुआ है। राम अपने पिता के श्राद्ध के लिये प्रवृत्त होते हैं और लोकायतिक जाबालि कहता है कि यह सब ढोंग है। पर, व्यवस्था बड़ी मजबूत है। सब कुछ जानते हुए भी राम में हिम्मत नहीं कि उसको नकार दें। व्यवस्थित मर्यादाएं और मर्यादित व्यवस्थाएं– इनका दृढ़ता से पालन ही राम को अभीष्ट था। इसी प्रकार जब राम राक्षसों का वध करते हैं, तो सीता कहती हैं कि बिना अपराध के किसी प्राणी को मारना अच्छा काम नहीं है– “अपराध बिना हन्तु लोको वीर न मंस्यते।” लेकिन, राम जवाब देते हैं कि मैं सब कुछ त्याग सकता हूं, पर व्यवस्था को नहीं छोड़ सकता–
अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां सीते सलक्ष्मणम्।
न तु प्रतिज्ञा संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्य विशेषता।।
वाल्मीकि की दृष्टि में दो प्रकार के मित्र होते हैं– एक वह, जो अपने मित्र के अर्थ-प्राप्ति में तत्पर होता है और दूसरा वह, जो सत्य एवं धर्म के ही आश्रित रहता है– “मित्रं ह्यर्थगुण श्रेष्ठं सत्यधर्मपरायणम्।” मित्रता की इससे उत्तम परिभाषा दूसरी नहीं हो सकती। आज की दुनिया में पैसे के बहुत यार मिल जाएंगे, लेकिन सत्य और धर्म पर आश्रित रहने वाला पैसे के सामने शत्रु ही होता है। इसमें वाल्मीकि ने बड़ी बारीकी से सामाजिक उत्कर्ष की भावना को स्थापित किया है।
“स्त्री शूद्रो नाधीयताम”– स्त्री और शूद्रों को विद्या नहीं देनी चाहिए, यह श्रुति है। मगध गण समाज में भले ही शूद्रों के साथ मानवता का व्यवहार रहा हो, लेकिन भरत गण समाज में तो शूद्र घृणा के ही पात्र थे। और, नारी? उसकी स्थिति तो सभी समाजों में एक समान निम्न थी। सत्य और धर्म सिर्फ पुरुषों के लिये था, नारी का सत्य और धर्म तो सर्वत्र पति-भक्ति ही था। नारी के अंदर की क्षमताओं को तत्कालीन पुरुष-समाज ने नहीं पहचाना था। तब, वाल्मीकि भी क्या कर सकते थे? मनु महाराज का अनुसरण करते हुए वह भी कौसल्या से कहला देते हैं कि नारी की केवल तीन शरण हैं– पति, पुत्र और पिता। उसके लिये चौथी कोई शरण नहीं है–
गतिरेका पतिर्नार्या द्वितीया गतिरात्मजः।
तृतीय ज्ञातयो राजश्चतुर्थी नैव विद्यते।।
वाल्मीकि यह कैसे कहते कि नारी की सबसे बड़ी शरण वह स्वयं है। मर्यादित पुरुष नारी का अभ्युदय कैसे देख सकते थे?
लेकिन, वाल्मीकि के सृष्टा-रूप में मर्यादाओं के साथ-साथ प्रगतिशीलता भी है, क्योंकि उनका कवि मूल रूप से सीता की वेदना का द्रष्टा और भोक्ता था। सीता राम से कहती है– “भर्तुर्भाग्यं तु नार्येका प्राप्नोति पुरुषर्षभ।” इसमें कवि सिर्फ यही नहीं कहता कि नारी पति के भाग्य का अनुसरण करती है, वरन् इस एक वाक्य में वह नारी का दर्द भी उड़ेल देती है। कुछ मुट्ठी भर आधुनिकताओं की बात छोड़ दीजिये, भारत का नारी-समाज आज भी इस दर्द को ही जी रहा है। लंका-विजय के बाद, सीता जब राम के समक्ष आती है, तो विभीषण पर्दे के विचार से लोगों को हटाना शुरु कर देते हैं। तब, राम कहते हैं कि घर, वस्त्र और चहारदीवारी आदि वस्तुएं स्त्री के लिये पर्दा नहीं हुआ करती हैं– “न गृहाणि न वस्त्राणि न प्राकारस्तिरस्क्रिया।” यह प्रगतिशीलता ही है, जो वाल्मीकि ने पर्दा को नारी का आभूषण नहीं बताया।
राजनीतिक संदर्भों में वाल्मीकि का शब्द-निरूपण तत्कालीन राज्य-व्यवस्था की विद्रूपताओं का चित्रण है, जो संकेत करता है कि राजा के होते हुए भी तत्कालीन समाज अराजक स्थिति में था। कहीं अध्यात्म में डूबे शासक राज्य की भौतिक अभिवृद्धि की उपेक्षा कर रहे थे, और कहीं चरम भोगवाद धर्म की अनुभूतियों को नष्ट कर रहा था। राम और रावण, दोनों एक दूसरे की योजनाओं को जान लेते थे, यह गुप्तचर-व्यवस्था की प्रत्यक्ष कमजोरियां थीं। वाल्मीकि के राजनीतिक विचारों में विरोधाभास है। यह विरोधाभास दो व्यवस्थाओं के बीच है। इसलिए कवि वहां नहीं हैं, वह दोनों के मध्य में हैं, उनके द्वंद्वात्मक रूप में है।
वाल्मीकि ने आदर्श राज्य की परिकल्पना की है, जहां प्रजा की सुरक्षा, संरक्षा और खुशहाली हो, जहां धर्म और अर्थ, दोनों की अभिवृद्धि हो। जनता के प्रतिकूल चलने वाले राजा से राज्य की रक्षा नहीं हो सकती– “न चाति प्रतिकूलेन नाविनीतेन राक्षस।” ऐसा राज्य अपने शासक के कार्यों के साथ ही नष्ट हो जाता है– “स तु वै सह राज्येन तैश्च कार्येर्विनश्यति।” व्यवस्था कैसी भी हो, पर जनता का हित सर्वप्रमुख है। जहां जनता का हित उपेक्षित है, वहां जनता द्वारा व्यवस्था भी उपेक्षित हो जाती है। राजनीति में एक व्यक्ति का कर्म पूरे राष्ट्र को प्रभावित करता है– “व्यसनं स्वामिवैगुण्यात् प्राप्नुवन्तीतरे जनाः।” इसलिए लोकप्रिय शासन वही है, जो स्थूल आंखों से सोता है, लेकिन नीति की आंखों से सदैव जागता है–
नयनाभ्यां प्रसुप्तो वा जागर्ति नयचक्षुषा।
व्यक्त क्रोध प्रसादश्च स राजा पूज्यते जनैः।।
बौद्ध-दर्शन को छोड़ दें, तो समूचा भारतीय दर्शन नित्यवादी है। यानि, सब कुछ शाश्वत, सृष्टि भी और सृष्टि की क्रियाएं भी। जो दिखाई पड़ने वाला परिवर्तन है, वह भ्रम तथा माया है, जिसके वशीभूत होकर मनुष्य दुःख-चक्र में फंसा हुआ है। इसलिए माया का त्याग और ईश्वर की आराधना इन दो कर्मों में ही मानव की मुक्ति है। इसके विपरीत, बुद्ध अनित्यवादी थे। उनके यहां सब कुछ परिवर्तनशील है। जीवन घटनाओं का विच्छिन्न प्रवाह है, सृष्टि जल-तरंगों के समान है, जो पल-पल पैदा होती और पल-पल नष्ट होती है। सारी वस्तुएं अशाश्वत हैं, इसलिए न आत्मा है और न परमात्मा।
नित्यवाद व्यवस्था का दर्शन है और अनित्यवाद उसके विरोध का दर्शन है। एक में सामंती मूल्य हैं और दूसरे में मानवतावाद है। एक में अनुभूति की गहन कल्पनाएं हैं और दूसरे में विवेक की उच्चतम अनुभूतियां हैं। एक में आदर्शों का आध्यात्मिक अभ्युदय है और दूसरे में यथार्थ की वेदनाओं से गुजरता हुआ विज्ञान है। एक में परलोक का आकर्षण है और दूसरे में जीवन का सौंदर्य है। एक आदेश देता है कठोरता के साथ, दूसरा उपदेश देता है मैत्री के साथ। एक का मूल मंत्र है– व्यवस्था को धारण किये रहो और दूसरे का मंत्र है– धर्म बेड़े की भांति पार उतारने के लिए है। पार उतरने के बाद धर्म को भी उतार फेंको।
किसी ने लिखा है कि वाल्मीकि नित्यवाद और अनित्यवाद के बीच में स्थित हैं। पर, बीच का कोई मार्ग भी तो हो। उनका अपना अलग ही मार्ग है। बुद्ध ने गरीबी के स्रोत को सामंती व्यवस्था में खोज लिया था, लेकिन राजाओं के भय से वह गरीबी को मिटाने का अभियान नहीं चला पाए थे। फिर, क्या राज्य की सहायता से संचालित आश्रम के कवि मात्र से नित्यवादी दर्शन के विरोध की आशा की जा सकती थी? बुद्ध की भांति वाल्मीकि भी जानते थे कि मानव की मुक्ति माया के त्याग और ईश्वर की आराधना में नहीं है, इसलिए उनका मानवतावाद, जहां पलायनवाद का संदेश देता है, वहां उनके कवि की मजबूरी ही समझिए। और, उनकी मजबूरी को समझना बड़ा आसान है, यदि आप शंबूक की घटना को समझ लें। शंबूक चले थे व्यवस्था का विरोध कर, नए समाज का निर्माण करने, पर न तो व्यवस्था ध्वस्त हुई और न नए समाज का निर्माण हुआ, उनका सिर जरूर धड़ से अलग हो गया। सिर कटा कर शहीद होना वाल्मीकि के लिये उतना महत्व नहीं रखता, जितना यह कि उन्होंने समाज-व्यवस्था और मानव के संघर्ष को बिंब रूप में चित्रित किया। पाठक की सहानुभूति किसके प्रति उत्पन्न होती है, व्यवस्था के प्रति या मानव के संघर्ष के प्रति? यदि मानव के संघर्ष के प्रति पाठक का मन संवेदित होता है तो कवि अपने कर्म में असफल नहीं कहा जाएगा।
आइए, हम उनके कुछ दर्शन-सूत्रों पर भी विचार करें। राम भरत से कहते हैं ki समस्त संग्रहों का अंत विनाश है और सांसारिक उन्नतियों का अंत पतन है– “सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छयाः।” तब, क्या मनुष्य उन्नति करना छोड़ दे? सामंती व्यवस्था को दृढ़ता देने वाले ये विचार आपको वाल्मीकि-वाणी में अनेक स्थलों पर मिलेंगे। दूसरों की गाढ़ी कमायी पर ऐश करने वालों के लिये यह दर्शन सूत्र बड़े काम का है, और दौलत पैदा करने वालों की गरीबी का मुख्य कारण भी यही दर्शन है। इसलिए, वाल्मीकि बड़ी सावधानी से जाबालि के मुंह से सामंती राम के कानों में ये शब्द भी डलवा देते हैं कि इस लोक के सिवाय दूसरा कोई लोक नहीं है, अतः जो प्रत्यक्ष है, उसी का आश्रय लीजिए– “प्रत्यक्षं यत् तदातिष्ठ परोक्षं पृष्ठतः कुरू।” जाबालि का मत राम को स्वीकार नहीं था। लेकिन, राम को स्वीकार कराने के लिए तो वाल्मीकि ने काव्य-रचना नहीं की थी।
लक्ष्मण ने राम से कहा– “जिनमें अधर्म प्रतिष्ठित है, उनके तो धन बढ़ रहे हैं और जो धर्माचरण करने वाले हैं, वे क्लेश में पड़े हैं। इसलिए यह धर्म और अधर्म दोनों निरर्थक हैं।” यथा–
यस्मादर्था विवर्धन्ते येष्वधर्मः प्रतिष्ठितः।
क्लिश्यन्ते धर्मशीलाश्च तस्मादेतौ निरर्थकौ।।
क्या एक सामंती पुरुष धर्म का विरोध कर सकता है? यह है वाल्मीकि का कवि-कौशल। लक्ष्मण निर्णय करते हैं कि जो धर्म दुर्बलों के लिये है, उसका सेवन ही अनुचित है–
अथवा दुर्बलः क्लीबो बलं धर्मोऽनुवर्तते।
दुर्बलो हृतमर्यादो न सेव्य इति मे मतिः।।
धर्म और दुर्बलता का अटूट संबंध है। जहां दुर्बलता है, वहीं धर्म है और वहीं निर्धनता है। वाल्मीकि के लिये धर्म भले ही अभिशाप न हो, पर निर्धनता जरूर अभिशाप है। अर्थ पर उनका आग्रह देखिए– “अर्थ से वंचित लोगों की सारी क्रियाएं उसी तरह छिन्न-भिन्न हो जाती हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु में छोटी-छोटी नदियां सूख जाती हैं। जिसके पास धन है, संसार में वही श्रेष्ठ है, वही पंडित है और उसी के सारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं। हर्ष, काम, धर्म, क्रोध आदि सब धन होने से ही सफल होते हैं। धर्म और तपस्या में लगे हुए लोगों का जीवन अर्थाभाव के कारण ही नष्ट हो जाता है। यथा–
अर्थेन हि विमुक्तस्य पुरुषस्याल्पचेतसः।
विच्छिद्यन्ते क्रियाः सर्वा ग्रीष्मे कुसरितो यथा।
यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः।
यस्यार्थाः स पुमांल्लोके यस्यार्थाः स च पण्डितः।
हर्षः कामश्च दर्पश्च धर्मः क्रोधः शमो दमः।
अर्थादेतानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते नराधिप।
येषां नश्यत्ययं लोकश्चरतां धर्मचारिणाम।
वाल्मीकि की यह स्थापना स्वांत: सुखाय और अस्मिता बेचकर स्तुति-गान करने वाले लेखकों की समझ में नहीं आएगी। जिनके जीवन का निर्वाह धर्मादा से होता हो, वे कला के लिये कला का विकास क्यों न करें? मालूम पड़ता है, वाल्मीकि की वाणी बहरे कानों में पड़ी, नहीं तो करोड़ों-करोड़ों लोग, जिन्हें धर्म से बांधकर अर्थ से वचिंत कर दिया गया है, आज प्रगति के पथ पर होते।
वाल्मीकि सामंतों के नहीं, जनता के कवि थे। जन-वेदना ही उनके काव्य का आधार है। आज जब हम समाजवाद की ओर अग्रसर हुए हैं और धर्म की वैज्ञानिक चेतना को अपनाते हुए एक नए समाज की रचना पर विचार करते हैं, तो मेरा अपना मत है कि वाल्मीकि-वाणी उसमें विरोधी नहीं बनेगी।
(संपादन : नवल/अनिल)