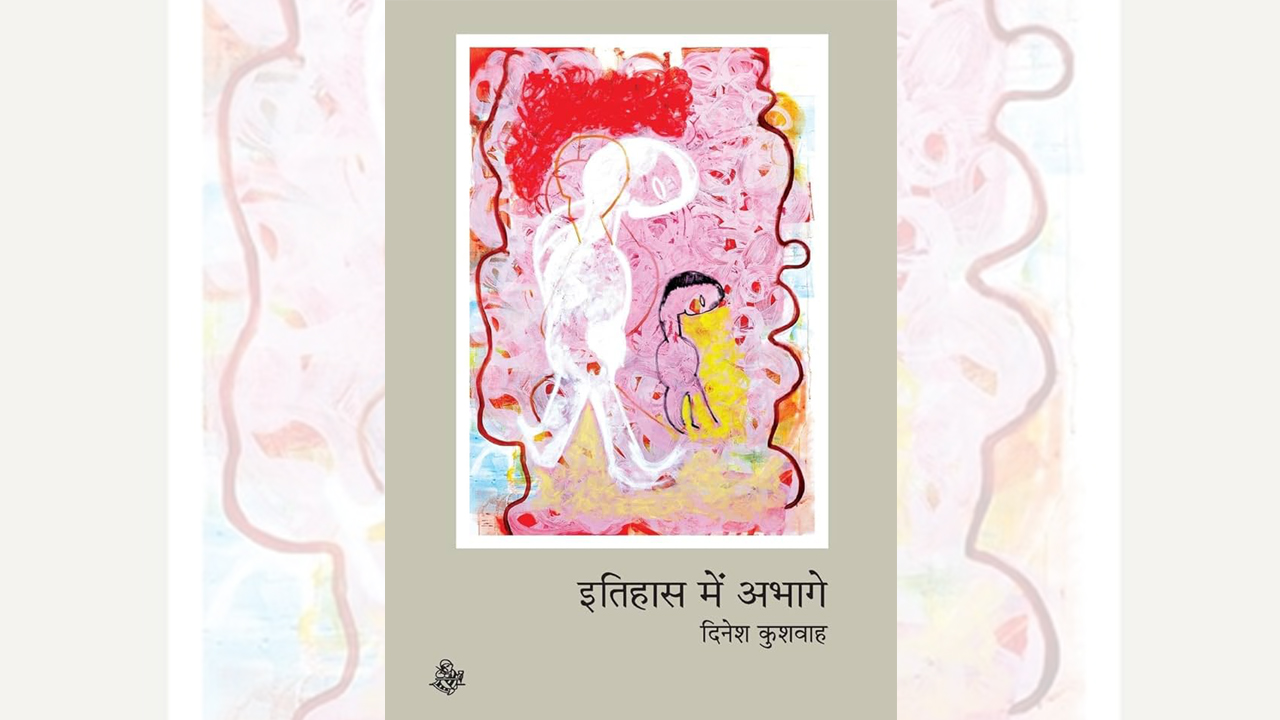दलित विमर्श पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें हिंदी में हैं, पर, प्रियंका सोनकर की इसी वर्ष प्रकाशित ‘दलित स्त्री विमर्श : सृजन और संघर्ष’ संभवत: दलित स्त्री विमर्श की पहली पुस्तक है। इस विषय पर कोई दूसरी पुस्तक मेरे देखने में नहीं आई।
इस पुस्तक में चार खंड हैं, जिनमें पहले खंड में जाति-विरोध की परंपरा, प्रेमचंद की दलित चेतना और दलित साहित्य के संघर्ष और स्वरूप पर चर्चा की गई है। दूसरे खंड में दलित स्त्री विमर्श की व्याख्या करते हुए कुछ व्यक्तित्वों, जैसे बुद्ध-काल की थेरियों, मध्यकालीन संत कवयित्रियों, कुछ क्रांतिकारी दलित वीरांगनाओं एवं डॉ. आंबेडकर के स्त्री आंदोलन के बारे में प्रकाश डाला गया है। तीसरा खंड दलित स्त्री विमर्श की अवधारणा, अश्वेत नारीवादी आंदोलन, दलित स्त्री विमर्श की वैचारिकी और सैद्धांतिकी तथा दलित स्त्री के रचनात्मक साहित्य पर आधारित है। और अंतिम चौथे खंड में शोषण, संघर्ष, देवदासी, बहुजुठाई, 1859 का चानार विद्रोह, तेभागा आंदोलन, मथुरा आदिवासी आंदोलन, फूलन देवी का संघर्ष और भगाणा आंदोलन को चर्चा के केंद्र में रखा गया है।
विमर्श और संघर्ष दो अलग-अलग चीजें हैं। पहले कौन, विमर्श या संघर्ष? यह पहले अंडा या मुर्गी वाला जटिल प्रश्न नहीं है। किसी भी समाज में संघर्ष पहले आता है, और विमर्श या साहित्य बाद में। यह बात स्त्री-विमर्श पर भी लागू होती है। यह संघर्ष ही है, जिसके गर्भ से विमर्श और साहित्य पैदा होता है। संघर्ष सिर्फ अन्याय से लड़ने के लिए या अपना अधिकार पाने के लिए ही नहीं होता, बल्कि जीने के लिए भी होता है। जिजीविषा ही वास्तव में संघर्ष है। इस दृष्टि से दलित स्त्री का जीवन एक संघर्ष के सिवाय कुछ नहीं है। वह सुबह से शाम तक जीने के लिए ही संघर्षरत रहती है। संघर्ष से होने वाले अनुभव जब व्यक्ति में एक जाग्रत चेतना का निर्माण करते हैं, तभी विमर्श का जन्म होता है। लेकिन साहित्य तब अस्तित्व में आता है, जब शिक्षा उस चेतना से जुड़ती है। चूंकि भारत में दलितों के लिए शिक्षा के द्वार शताब्दियों बाद मुसलमानों और अंग्रेजों के शासन में खुले। इसलिए निचले वर्गों का विमर्श और साहित्य भी इन्हीं दो कालखंडों में प्रकाश में आया। कबीर, रैदास, मीराबाई, जोतीराव फुले, सावित्रीबाई फुले और आंबेडकर जैसे विमर्शकार इन्हीं कालखंडों में हो सकते थे, इससे पूर्व उनके होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन दलित स्त्री-शिक्षा तो और भी बाद की घटना है, भारत को आज़ादी मिलने के भी दशकों बाद की।
हालांकि, प्रियंका सोनकर दलित स्त्री-विमर्श की पहली यात्रा बुद्ध-काल की थेरियों की गाथाओं से मानती हैं। यह विचारणीय भी है, क्योंकि निस्संदेह बुद्ध ने समानता, स्वतंत्रता और करुणा की देशना में स्त्री-स्वतंत्रता को प्रमुखता दी थी। इसलिए लेखिका ने दूसरे खंड से दलित स्त्री विमर्श के इतिहास को ठीक ही दर्ज किया है। उन्होंने लिखा है कि दलित स्त्री विमर्श की ऐतिहासिक जड़ें बुद्ध-संघ में शामिल स्त्रियों के विमर्श में हैं। उनके अनुसार, “वे बहुत ही सहज-सरल ढंग से और निर्भीकतापूर्वक अपने मनुष्य होने के अहसास को कथा-कहानियों के माध्यम से व्यक्त करती हैं। स्त्री-मुक्ति की कामना करती हुईं ये थेरियां कविता-कहानियों से इतिहास रचती हैं। मन, तन, वचन की पीड़ा से मुक्त जाति, वर्ण, लिंग और समाज के बंधनों से स्वतंत्र होकर वे गा उठती हैं—
यहां इस शिला पर बैठी
मैं पूर्ण मुक्ति का अनुभव कर रही हूं
स्वाधीनता का वातावरण
मेरी आत्मा और शरीर को
आच्छादित किए हुए हैं।”
(प्रियंका सोनकर, दलित स्त्री विमर्श : सृजन और संघर्ष, प्रलेक प्रकाशन, मुंबई, पृष्ठ 73)
प्रियंका सोनकर ने सही कहा है कि जिस नारी को पुरुष-प्रधान समाज में किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था, उसे सभी प्रकार के अधिकारों की अधिकारिणी बनाना, यथा– ज्ञान प्राप्त करने, ज्ञान का उपदेश देने का अधिकार देना बहुत क्रांतिकारी बात थी।

बुद्धकाल के बाद लेखिका ने दलित स्त्री-विमर्श का दूसरा पड़ाव मध्यकालीन दलित संत कवयित्रियों के काव्य में माना है। इनमें एक संत कवयित्री पंद्रहवीं सदी की कश्मीर की कवयित्री ललदेह या ललद्यद हैं। सुभाष राय के अनुसार, ललद्यद की रचनाओं का पहला परिचय 1730 ईस्वी में लिखित ‘तारीख़े कश्मीर’ में मिलता है। उनके ऊपर पहला महत्वपूर्ण काम ग्रियर्सन ने किया था। सुभाष राय ने ललद्यद की एक वाख (रचना) का उल्लेख किया है, जिसमें वह कहती हैं कि “गोरस प्रछाम सासि लटे/ यस नु केंह वनान तस क्या नाव?/ परछाँ परछाँ थसिस तु लूसस/ केंह नस निशि क्या नाव द्राव।” वह कहती हैं कि “गुरु से मैंने हज़ार बार पूछा कि जिसे ‘कुछ नहीं’ कहते हैं, उसका नाम क्या है? पूछते-पूछते मैं थक गई और मुरझा गई। आख़िर में मैं समझी कि ‘कुछ नहीं’ से ही कुछ न कुछ निकलता है।” सुभाष राय ने इसकी व्याख्या नहीं की है। लेकिन ललद्यद की इस वाख का अर्थ बौद्ध-दर्शन के शून्यवाद में खुलता है। यह उन पर बौद्धधर्म के प्रभाव को प्रमाणित करता है, जो न केवल सम्राट अशोक के समय में कश्मीर का प्रमुख धर्म था, बल्कि उससे पहले से ही वहां व्यापक रूप में मौजूद था, और पड़ोस में लद्दाख, तिब्बत और चीन तक फैला हुआ था। शून्यवाद के प्रवर्तक बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन कुषाण काल के दौरान कश्मीर में रहते थे। ललद्यद के बारे में अधिकांश विद्वानों का मत यही है कि वह ब्राह्मणी थीं। सुभाष राय की सहमति भी इसी मत से है। लेकिन उनके जीवन के कुछ विवरण इससे मेल नहीं खाते। जैसे उनका निर्गुणवाद, तीर्थों, कर्मकांडों और शास्त्रों का विरोध। ललद्यद और अक्क महादेवी, दोनों ने ही देह की नग्नता को स्वीकार किया था। लेकिन कहा जाता है कि समाज द्वारा उनको निर्वस्त्र कर अपमानित किया गया था। सुभाष राय ने यह भी लिखा है कि लोकभाषा कश्मीर के निम्नजनों की भाषा मानी जाती थी। लेकिन इस भाषा को शक्तिशाली माध्यम बना देने का श्रेय ललद्यद नाम की स्त्री को जाता है। (दिगंबर विद्रोहिणी अक्क महादेवी, पृष्ठ 44-47) प्रियंका सोनकर ने ललद्यद को दलित जाति का माना है। उन्होंने परशुराम चतुर्वेदी की पुस्तक ‘उत्तर भारत की संत परंपरा’ के हवाले से लिखा है कि लल्ला या लाल (ललद्यद) कश्मीर की रहने वाली एक ढेढ़वा मेहतर जाति की स्त्री थी, जो सामाजिक दृष्टि से निम्न स्तर वाले परिवार से थी, लेकिन बहुत उच्च विचार रखती थी। इनके विषय में प्रसिद्ध है कि यह शैव संप्रदाय का अनुसरण करने वाली एक भ्रमणशील भंगिन थी। (प्रियंका सोनकर, उपरोक्त, पृष्ठ 76)
इस क्रम में सोनकर ने मध्यकाल की दूसरी दलित स्त्री संत महाराष्ट्र की जनाबाई (1258-1350) का उल्लेख किया है। भक्ति मार्ग की बहुज्ञानी उपेक्षिता संत जनाबाई भक्ति-काव्यधारा की महान कवयित्री थीं। कहा जाता है कि वह मातृ-पितृविहीन अनाथ थीं और संत नामदेव के घर सेविका के रूप में रहती थीं। प्रियंका सोनकर ने जनाबाई की जाति का उल्लेख नहीं किया है। लेकिन साक्ष्य बताते हैं कि उनका जन्म मातंग जाति में हुआ था, जो महाराष्ट्र की एक अछूत जाति है। कहा जाता है कि जनाबाई के माता-पिता बचपन में ही गुजर गए थे और एक अनाथ के रूप में नामदेव ने उनको आश्रय दिया था। नामदेव को कुछ विद्वानों ने क्षत्रिय वर्ण का बताया है, तो कुछ उन्हें दर्जी जाति का मानते हैं। लेकिन वास्तव में वह दर्जी या दूसरी जाति के शूद्र थे। अगर वह उच्च वर्ण के होते, तो मातंग जाति की जनाबाई को अपने घर में कभी आश्रय नहीं दे सकते थे। यद्यपि, जनाबाई के काव्य पर नामदेव का प्रभाव माना जाता है; लेकिन उनकी भक्तिप्रधान कविताओं को, जो लगभग 350 भजन के रूप में हैं, प्रियंका सोनकर ने भक्तिधारा के विरुद्ध एक अलग धारा माना है, जिसमें ईश्वर भी एक साधारण मनुष्य के रूप में आया है। इस संबंध में उन्होंने जनाबाई का यह पद उद्धृत किया है—
जना फर्श बुहार रही है
और भगवान कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं
अपने सर पर रखकर दूर ले जा रहे हैं
भक्ति से विजित
ईश्वर नीचा काम कर रहे हैं
जना बिढोबा से कहती है
मैं तुम्हारा क़र्ज़ कैसे उतारूंगी। (वही, पृष्ठ 78)
प्रियंका सोनकर ने जनाबाई के स्त्री-मुक्ति विमर्श को रेखांकित करते हुए लिखा है कि मध्यकाल में जनाबाई ने स्त्रियों के ऊपर लादे गए तमाम शिकंजों और वर्जनाओं को दूर फेंककर स्वतंत्र जीवन जीने का मार्ग दिखाया था।
मध्यकाल की अन्य दलित स्त्री कवयित्रियों में उन्होंने बंगाल की धोबी जाति की रामी का उल्लेख किया है, जिसने ब्राह्मण कवि चंडीदास से प्रेम-विवाह किया था। पर बाद में चंडीदास उसे छोड़कर अपने ब्राह्मण-परिवार में वापस चले गए थे। उनके अनुसार, उनकी कविता का नमूना इस तरह है—
तूफ़ान को उन लोगों के सर पर गिर जाने दो
जो अपने घरों में छिपे अच्छे लोगों को कोसते हैं
मैं और ज्यादा इस अन्याय की भूमि पर नहीं रह सकती
मुझे वहां जाना है, जहां यातनाएं न हों। (वही, पृष्ठ 80)
अन्य कवयित्रियों में उमा, मीरा, कमाली, सहजोबाई, दयाबाई, फूलाबाई, पुली बाई, दोतुलम्मा और लखम्मा आदि के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा लेखिका ने की है, जिनका काव्य मध्यकाल के ब्राह्मण-विमर्श में एक अलग स्त्री-स्वर है।
दलित स्त्री-विमर्श की तीसरी यात्रा में लेखिका ने 1857 की कुछ दलित वीरांगनाओं का उल्लेख किया है, जिनमें झलकारीबाई, महाबीरी देवी, ऊदादेवी, आशादेवी, अजीवनबाई आदि पर चर्चा की है। इसके पश्चात उन्होंने दलित स्त्री-विमर्श की चौथी मंजिल में स्त्री-शिक्षा की प्रथम पाठशाला के रूप में सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, मुक्ताबाई और दुर्गाबाई; इन चार स्त्रियों के अवदान पर प्रकाश डाला है। निस्संदेह ये स्त्रियां भारत में स्त्री-नवजागरण की क्रांतिकारी स्तंभ थीं। रमाबाई ब्राह्मण थीं, पर उन्होंने हिन्दू धर्म को त्याग दिया था, जिसे वह स्त्री-मुक्ति में बाधक मानती थीं। उन्होंने स्त्री-मुक्ति के लिए स्त्री-शिक्षा और विधवा स्त्रियों के उत्थान की दिशा में आजीवन कार्य किया था। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली स्त्री शिक्षिका थीं, तो मुक्ताबाई उन्हीं के स्कूल में शिक्षित महिला थी, जिन्होंने अपने लेखों और कविताओं के माध्यम से ब्राह्मणवाद के खिलाफ जागरण किया था। दुर्गाबाई बीसवीं सदी में उत्तर भारत में आदि हिंदू आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी अछूतानंद की जीवनसंगिनी थीं, जिन्होंने उनसे प्रेरणा लेकर सिरसागंज में विद्यालय खोला था और दलित लड़कियों को शिक्षित करने का प्रयत्न किया था। इन स्त्रियों का, जैसा कि लेखिका ने लिखा है, स्त्री-मुक्ति के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
दलित स्त्री विमर्श के पांचवें स्तंभ के रूप में लेखिका ने डॉ. आंबेडकर के स्त्री आंदोलन, हिंदू कोड बिल और दलित राजनीति में मायावती के योगदान का उल्लेख किया है। लेकिन इस विषय में उनका विश्लेषण आलोचनात्मक है, जो उन्हें एक जागरूक आलोचक साबित करता है।
मसलन, डॉ. आंबेडकर के महिला आंदोलन पर प्रकाश डालते हुए लेखिका लिखती हैं कि बाबासाहेब आंबेडकर के नेतृत्व में चलाए गए महिला आंदोलन का महत्वपूर्ण समय 1930 और 1940 के दशकों का है। हालांकि उनके अनुसार, आंबेडकर ने महिला आंदोलन की शुरुआत 1920 में ही कर दी थी, जब कोल्हापुर नरेश शाहूजी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय बहिष्कृत परिषद की सभा में पहली बार दलित महिलाओं ने भाग लिया था। इस सभा में तुलसाबाई बनसोडे तथा रुकमनीबाई ने स्त्री-शिक्षा पर अनिवार्य रूप से जोर दिया था। 1928 में बंबई में महिला मंडल की स्थापना हुई थी, जिसका अध्यक्ष रमाबाई आंबेडकर को बनाया गया था। बाबासाहेब के नेतृत्व में चलने वाले मंदिर-सत्याग्रह में भी दलित महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। इसी तरह 1929 में पुणे के पार्वती मंदिर में प्रवेश के लिए बाबासाहेब आंबेडकर और तानुबाई के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने आंदोलन किया था। लेखिका ने दलित महिलाओं के संघर्ष और आंदोलन के 1940 तक के विवरण दिए हैं, जो बाबासाहेब के स्त्री-मुक्ति विमर्श को समझने के लिए बेहद विचारणीय हैं।
इस खंड में प्रियंका सोनकर ने 1980 के दशक में उत्तर प्रदेश में उभरे कांशीराम और मायावती के बहुजन-आंदोलन पर भी महत्वपूर्ण चर्चा की है। इसमें उन्होंने ख़ास तौर से स्त्री-मुक्ति के संदर्भ में मायावती की राजनीति को केंद्र में रखा है। उन्होंने पहली दलित मुख्यमंत्री के रूप में मायावती के राजनीतिक उत्थान की प्रशंसा की है, लेकिन उन्होंने यह भी बताया है कि मायावती दलित समाज की महिलाओं के लिए प्रेरणा क्यों नहीं बन सकीं, और अपने शासन-काल में दलित महिलाओं के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे सकीं। उन्होंने लिखा है कि मायावती ने ब्राह्मणवाद से गठबंधन करके न केवल दलित आंदोलन को, बल्कि दलित महिलाओं के मुक्ति-संघर्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है। उन्होंने आगे लिखा है कि बाबासाहेब आंबेडकर ने जिस ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद को दलितों का दुश्मन माना था, मायावती ने उन्हीं के विकास की राजनीति की। बहुजन राजनीति पर लेखिका का विश्लेषण निस्संदेह काबिलेगौर है।
तीसरा खंड इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यह दलित-स्त्री-विमर्श की अवधारणा, अश्वेत नारीवादी आंदोलन और दलित स्त्री विमर्श से उसके संबंध, दलित स्त्री-विमर्श की वैचारिकी और सैद्धांतिकी तथा दलित लेखिकाओं के रचनात्मक साहित्य पर चर्चा करता है।
दलित साहित्य की अवधारणा और दलित स्त्री-विमर्श की अवधारणा में केवल इस बिंदु पर भिन्नता है कि एक स्त्री अपने मन और मुक्ति को जितने अच्छे से समझती है, या समझ सकती है, उतना पुरुष उसकी न वेदना को समझ सकता है और न उसकी मुक्ति की अवधारणा को ही। इसलिए सोच, पीड़ा और उपचार की दृष्टि से स्त्री-साहित्य ज्यादा प्रामाणिक है, अपेक्षाकृत उस साहित्य के, जो स्त्री के बारे में पुरुष द्वारा लिखा गया है। इसलिए दलित स्त्री लेखन ने अपनी अलग राह चुनी। लेकिन यह दिलचस्प है कि प्रियंका सोनकर ने स्त्री विमर्श को रेखांकित करने के लिए पुरुष लेखक बजरंग बिहारी तिवारी और सुभाष गाताडे के चिंतन को अपना आधार बनाया, जबकि कई दलित स्त्री लेखिकाओं के चिंतन मौजूद हैं। उन्हें 2006 में प्रकाशित हेमलता महिश्वर की पुस्तक ‘स्त्री लेखन और समय के सरोकार’ का अवलोकन करना चाहिए था, जो दलित साहित्य में दलित स्त्री विमर्श की महत्वपूर्ण पुस्तक है। रमणिका गुप्ता का स्त्री-विमर्श भी इस संदर्भ में उल्लेख करने योग्य था।
प्रियंका सोनकर लिखती हैं कि दलित स्त्री-विमर्श पर बात करते हुए सबसे पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि पश्चिम में जो अश्वेत नारीवादी आंदोलन चला, वह वास्तव में क्या है और नब्बे के दशक में चले दलित स्त्री विमर्श से क्या उसकी कोई समानता है? लेकिन इतनी जल्दी डॉ. आंबेडकर द्वारा चलाए गए स्त्री आंदोलन से उसकी असमानता अनुभव करना आश्चर्यजनक है।
प्रियंका सोनकर का मानना है कि जिस तरह से अश्वेत लेखिकाओं की आत्मकथाओं ने अमेरिका के संपूर्ण विमर्श को बदल दिया था, उसी तरह दलित स्त्रियों की आत्मकथाओं ने भी परिवर्तन लाने में सहायता की। अश्वेत स्त्रियां यहां रंगभेद की शिकार रही हैं, वहीं दलित स्त्रियाां जातिगत भेदभाव की। (वही, पृष्ठ 137)
दलित स्त्री विमर्श की वैचारिकी और सैद्धांतिकी के तहत प्रियंका सोनकर ने कई नारीवादी महिला कार्यकर्ताओं और लेखकों के संदर्भ दिए हैं, लेकिन वह अपने स्तर पर कोई वैचारिकी निर्मित नहीं कर सकीं, जिसकी उनसे अपेक्षा थी। वह यहां इसी मत को दोहराती हैं कि जहां स्त्रीवाद सवर्ण स्त्रियों के खेमे तक सीमित है, वहां दलितवाद को पुरुषों के खेमे तक सीमित कर दिया गया है, जिसमें दलित स्त्री को जगह न मिलने के कारण ही दलित स्त्री-विमर्श का जन्म हुआ है।
लेकिन दलित स्त्री विमर्श क्या है? इसके उत्तर में वह रजनी तिलक के मत का समर्थन करती हैं, कि नारीवादी इतिहास में अपने वजूद को न पाकर दलित स्त्रियां स्वयं ही अपने संघर्षों के इतिहास को लिखने में जुट गईं। उन्होंने दलित स्त्री विमर्श को सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई और बाबासाहेब आंबेडकर से प्रभावित माना है। लेकिन उसके प्रतिमानों और सिद्धांतों पर कोई चर्चा उन्होंने नहीं की है, जो शोधार्थियों के लिए निराशापूर्ण हो सकता है।
इस खंड के अंत में लेखिका ने कुछ दलित लेखिकाओं की आत्मकथाओं, कविताओं, कहानियों और अन्य रचनाओं तथा पत्रिकाओं का एक विवरण प्रस्तुत किया है। यह भी सिर्फ एक विवरण भर ही है, जबकि कुछ महत्वपूर्ण कृतियों का विवेचन आवश्यक था।
पुस्तक का चौथा और अंतिम खंड इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसमें कुछ घृणित सामाजिक प्रथाओं और दलित स्त्रियों के विद्रोहों पर चर्चा की गई है। इसमें लैंगिक शोषण पर भी एक चर्चा है, जिसमें लेखिका ने डॉ. तेज सिंह, उमा चक्रवर्ती, मोहनदास नैमिशराय, राजेंद्र यादव, कांचा आइलैय्या शेपर्ड के विचारों और सुशीला टाकभौरे, बेबी कांबले, कौसल्या बैसंत्री, तुलसी राम, डॉ. धर्मवीर और बेबी हालदार की आत्मकथाओं के हवाले से समाज और घरों में होने वाले लैंगिक भेदभाव का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। इसके बाद लेखिका ने दलित स्त्रियों के साथ घटित बलात्कार के स्वरूप का वर्णन किया है और बलात्कार की कई श्रेणियां गिनाई हैं। यथा, जमींदार बलात्कार, अधिकारी वर्ग और जाति बलात्कार। यह विवरण उन्होंने राधा कुमार की पुस्तक ‘स्त्री-संघर्ष का इतिहास’ के आधार पर दिया है। कुछ अन्य स्रोतों से भी उन्होंने दलित स्त्रियों के साथ हुईं बलात्कार की कुछ घटनाओं का वर्णन किया है। इनमें एक घटना उत्तर प्रदेश के शाहपुर गांव की है, जहां एक दलित महिला शौच के लिए खेत में गई, तभी गांव के ऊंची जाति के नत्थू सिंह ने उसके साथ बलात्कार किया। उसने जब इसका जिक्र अपने पति से किया, तो नत्थू सिंह और उसके पुत्र ने स्त्री के घर में घुसकर उसके पति को मारा, जिससे डरकर वह गांव छोड़कर भाग गया। पीड़ित महिला जब गुहार लगाने अन्य घरों में गई, तो नत्थू सिंह ने उसे वहां से खींचकर नंगा करके पूरे गांव में घुमाया। किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की, और पुलिस ने भी उसकी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। इसी तरह लेखिका ने मणिमाला के हवाले से मध्य प्रदेश की दो घटनाओं का जिक्र किया है। इनमें एक दलित महिला थी और दूसरी आदिवासी। उन दोनों महिलाओं को भी नंगा करके घुमाया गया था। दलित महिलाओं के मामले में महिला आयोग भी प्राय: निष्क्रिय रहता है। लेखिका के अनुसार इसके दो कारण हैं, एक यह कि इन आयोगों में दलित प्रतिनिधित्व प्राय: नहीं होता और सवर्ण महिलाएं ही पदाधिकारी होती हैं, जिनका वर्ग-चरित्र दलितों के प्रति पक्षपातपूर्ण और संवेदनहीन होता है।
देवदासी प्रथा पर चर्चा करते हुए लेखिका ने इसे ठीक ही मंदिरों में दलित स्त्री का वेश्यात्मक चढ़ावा नाम दिया है। लेखिका के अनुसार पूना में देवदासियों की संख्या लगभग छह हजार और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में दस हजार है। हालांकि देवदासियों की संख्या इससे भी कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि इस घृणित प्रथा का पूर्ण उन्मूलन अभी तक नहीं हुआ है। अगर देवदासी प्रथा ब्राह्मण पुजारियों ने अपनी अय्याशी के लिए स्थापित की थी, तो ठाकुर ज़मींदारों ने अपनी वासना के लिए ‘बहू जुठाई’ प्रथा कायम की थी, जो भारत के सभी गांवों में नहीं, तो अधिकांश गांवों में प्रचलित थी। यह प्रथा दलित स्त्रियों का सिर्फ यौन-शोषण ही नहीं करती थी, बल्कि उनके आत्मगौरव को भी कुचलती थी। इस प्रथा के तहत निम्न जातियों की नवब्याहता दुल्हनों के डोले ठाकुर जमींदार की हवेली पर उतरते थे। उनकी पहली रात ठाकुर के साथ होती थी। हालांकि, इस अध्याय में इस प्रथा पर लेखिका ने कोई विशेष चर्चा नहीं की है, लेकिन दलित स्त्री-संघर्ष की दृष्टि से दलित जाति की नादर स्त्रियों के प्रतिरोध पर लेखिका ने महत्वपूर्ण चर्चा की है। यह भारतीय समाज की बहुत ही क्रूर और घृणित परंपरा थी, जिसके अंतर्गत केरल के त्रावणकोर में नादर स्त्रियों को अपने स्तनों को ढंकने की इजाजत नहीं थी। इसलिए वे शरीर के ऊपरी हिस्से को नग्न रखती थीं। इतना ही नहीं, जो स्त्री अपने स्तनों को ढंकने का प्रयास करती थी, उससे राज्य स्तन-टैक्स वसूलता था। इस असभ्य परंपरा के बारे में संज्ञान पहली बार ईसाइयों ने लिया। ईसाई मिशनरियों ने जब उनके बीच ईसाई धर्म का प्रचार किया और कुछ नादर स्त्रियों ने ईसाई धर्म अपनाया, तो उन्होंने अपना शरीर ढंकना शुरू किया। पहली बार 1814 में अंग्रेजों के शासन में त्रावणकोर के दीवान कर्नल मुनरो ने सभी ईसाई नादर और अन्य नादर स्त्रियों को ब्लाउज पहनने का आदेश निकलवाया। लेखिका के अनुसार, इस आदेश के बावजूद उच्च वर्ण के पुरुष अपनी ताकत के सहारे नादर स्त्रियों को अपने स्तन नग्न रखने के लिए बाध्य करते रहे। आठ साल बाद फिर सरकार द्वारा स्तनों को ढंकने का आदेश निकाला गया, जिसके बाद कुछ नादर स्त्रियों ने शालीन कपड़े पहनने शुरू किए। लेकिन ब्राह्मणों और सामंतों का दबाव अभी भी विरोध में था। प्रियंका सोनकर ने लिखा है कि इस पूरे आंदोलन का सीधा संबंध न सिर्फ स्त्री-मुक्ति की लड़ाई से था, बल्कि भारत की आज़ादी के इतिहास से भी जुड़ा है। केरल के नारायण गुरु और अन्य सुधारकों और अवर्ण स्त्रियों के प्रतिरोध तथा अंग्रेजों के दबाव के परिणामस्वरूप अंतत: त्रावणकोर के राजा को 26 जुलाई, 1859 को इस प्रथा को समाप्त करने का आदेश जारी करना पड़ा। भारत का ब्राह्मणवाद और सामंतवाद दलित स्त्रियों के प्रति कितना क्रूर था, ऐसी शर्मनाक प्रथाएं इसका प्रमाण हैं।
पुस्तक के अंत में प्रियंका सोनकर ने वर्गीय आर्थिक शोषण और दलित स्त्री-संघर्ष पर विस्तार से चर्चा की हैं, जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण स्त्री-आंदोलनों तथा संघर्षों का वर्णन किया है। इनमें चानार विद्रोह, तेभागा और तेलंगाना आंदोलन, मथुरा आदिवासी आंदोलन, भगाणा आंदोलन, फूलन देवी का संघर्ष और भंवरी देवी प्रकरण शामिल हैं। हालांकि लेखिका ने इन आंदोलनों से अपने पाठकों को परिचित कराते हुए उनमें वामपंथी आंदोलनों पर भी संक्षिप्त चर्चा की है, जो जरूरी भी थी, लेकिन जिस आलोचनात्मक विश्लेषण की यहां दरकार थी, उसका अभाव अखरता है।
(संपादन : राजन/नवल/अनिल)