 दलित पत्रकारिता को कैसे परिभाषित किया जाए? इसकी तीन संभावित परिभाषाएं हो सकतीं हैं। पहली, दलितों के लिए पत्रकारिता; दूसरी दलित पत्रकार और तीसरी दलितों के लिए दलित पत्रकार। दलित पत्रकारिता का अर्थ देश और लोकतंत्र के लिए पत्रकारिता के रूप में लिया जाना चाहिए। दलित मीडिया का ढांचा खड़ा करने के कई प्रयास हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने अपने अभियान के लिए मीडिया की अहमियत को बखूबी समझा और इसलिए अखबार निकाले। डा. आम्बेडकर ने भी यह अहमियत समझी थी। लेकिन न तो डा. आम्बेडकर और ना ही कांशीराम के द्वारा निकाले गए अख़बारों के नाम में ‘दलित’ शब्द था। कांशीराम ने ‘दि ऑप्रेस्ड इण्डियन’ निकाला और अन्य अखबारों के भी ऐसे ही नाम थे। महात्मा गांधी ने अपने अखबार का नाम ज़रूर ‘हरिजन’ रखा था , क्योंकि उन्हें वर्ण व्यवस्था के साथ संसदीय सत्ता के तालमेल की स्थितियां तैयार करनी थीं।
दलित पत्रकारिता को कैसे परिभाषित किया जाए? इसकी तीन संभावित परिभाषाएं हो सकतीं हैं। पहली, दलितों के लिए पत्रकारिता; दूसरी दलित पत्रकार और तीसरी दलितों के लिए दलित पत्रकार। दलित पत्रकारिता का अर्थ देश और लोकतंत्र के लिए पत्रकारिता के रूप में लिया जाना चाहिए। दलित मीडिया का ढांचा खड़ा करने के कई प्रयास हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने अपने अभियान के लिए मीडिया की अहमियत को बखूबी समझा और इसलिए अखबार निकाले। डा. आम्बेडकर ने भी यह अहमियत समझी थी। लेकिन न तो डा. आम्बेडकर और ना ही कांशीराम के द्वारा निकाले गए अख़बारों के नाम में ‘दलित’ शब्द था। कांशीराम ने ‘दि ऑप्रेस्ड इण्डियन’ निकाला और अन्य अखबारों के भी ऐसे ही नाम थे। महात्मा गांधी ने अपने अखबार का नाम ज़रूर ‘हरिजन’ रखा था , क्योंकि उन्हें वर्ण व्यवस्था के साथ संसदीय सत्ता के तालमेल की स्थितियां तैयार करनी थीं।
ये उदाहरण मात्र इस बातचीत को आगे बढ़ाने और विस्तार में जाने से बचने के लिए दिए गए हैं। संसदीय राजनीति के लिए वोटो का आधार बनाने और एक वैचारिक-सांस्कृतिक आंदोलन की निरंतरता सुनिश्चित करने की जद्दोजहद में कुछ बुनियादी फर्क होते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों में परिवर्तन के लिए वैचारिक और सांस्कृतिक संघर्ष और संसदीय सत्ता के जरिये बदलाव की प्रक्रिया – दोनों में उस कड़ी की खोज की जा जानी चाहिए, जो कि उनके ठहराव और फिसलन के कारणों को स्पष्ट कर सके। जोतिबा फूले, पेरियार एवं डा. आम्बेडकर का अलग-अलग मूल्यांकन इसमें सहायक हो सकता है। संसदीय राजनीति का समाज परिवर्तन के औजार के रूप में प्रयोग के सम्बन्ध में बाबू जगजीवन राम और डां. आम्बेडकर के अलग-अलग दृष्टिकोण की समझ भी इसमें मददगार हो सकती है।
इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि मीडिया के एक ऐसे ढांचे के निर्माण, जो संविधान के उद्देश्यों व संकल्पों को साकार दे सके, की उपेक्षा कर महज तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने को प्राथमिकता क्यों दी गयी। ‘द ऑप्रेस्ड इण्डियन’ के सितंबर 1980 के संपादकीय में कांशीराम लिखते हैं कि ‘जय भीम’, ‘निर्णायक भीम’ व ‘भीम पत्रिका’ के संपादकों को बाबू जगजीवन राम ने अपनी उजली छवि बनाने के लिए ऐसे समय पर आर्थिक मदद दी जब हिन्दू जातिवादी प्रेस उनकी उपेक्षा कर रही थी। यह गौरतलब है कि ‘द ऑप्रेस्ड इण्डियन’, जहाँ वैचारिक सिद्दांत की जरूरत पर बल देता है वहीं ‘जय भीम’ जगजीवन राम की तात्कालिक जरूरतों की पूर्ति करने के माध्यम के रूप में सीमित हो जाता है।
इसी संपादकीय में कांशीराम लिखते है कि बाबू जगजीवन राम, डा. आम्बेडकर की धर्मपरिवर्तन की अवधारणा से कभी सहमत नहीं हुए क्योंकि उन्हें यह स्पष्ट नहीं था कि अछूतों का मूल क्या है। जगजीवन बा
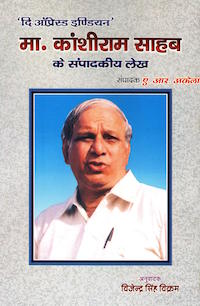
संपादक : एआर अकेला
प्रकाशक : आनंद साहित्या सदन, छावनी, अलीगढ
पृष्ठश संख्या : 274
मूल्य : 150 रूपये
संपर्क : 9319294963
बू ने दलित-शोषित समाज की पत्रिकाओं के संपादकों से कहा था कि वे इस बात पर शोध करें कि अछूतों की उत्पति कहां से हुई थी। हिन्दू जातिवादी प्रेस की उपेक्षा के कारण जगजीवन राम को ‘जय भीम’ की जरूरत महसूस हुई।
पूरे देश और लोकतंत्र के लिए मीडिया के ढांचे के खड़े नहीं होने की वजहें बहुत साफ है। ए आर अकेला ने ‘द ऑप्रेस्ड इण्डियन’ के सम्पादकियों का संकलन निकाला है। उससे पहले उन्होंने कांशीराम के भाषणों के संकलन निकाले हैं और आगे भी कांशीराम के साहित्य को एक जगह लाने की उनकी लंबी योजना है। इन सम्पादकियों को पढऩे से यह महसूस होता है कि बुनियादी बदलाव के लिए मीडिया के ढांचे को विकसित करने की कोशिश कैसे तात्कालिक संसदीय जरूरतों के आगे बिखरने लगती है। महज यह कहने से कि ब्राह्मण-बनिया प्रेस जातिवादी और दलित विरोधी है, देश और लोकतंत्र के लिए मीडिया का ढाँचे खड़ा नहीं हो जायेगा। संसदीय पार्टियों को सामाजिक आधार की जरूरत होती है और उसमें जाति का घटक महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन मीडिया के ढांचे के लिए एक गतिशील वैचारिक अवधारणा जरूरी है। बहुसंख्यक जातियों के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि कैसे इस देश में जातिवाद और उसकी सत्ता के पीछे संचार का पूरा ढांचा हर पल सक्रिय रहता है। संचार के इस ढांचे में रोज छपने वाले समाचारपत्र, दिन भर खबरें उगलने वाली समाचार एजेंसियां और हर पल शोर मचाने वाले इलेक्ट्रोनिक चैनल शामिल है। वे उनकी जीवनचर्या को बेहद सीमित दायरे में समेटे रखने में कामयाब रहे हैं। वे उन्हें बेहद छोटे दायरे में पढऩे और नौकरीपेशा बनाए रखते हैं।
भारतीय समाज व्यवस्था में वर्चस्व रखने वाली जातियों का संचार का एक व्यवस्थित ढांचा है। इसीलिए तमाम तरह के बदलावों के बावजूद वे खुद को टिकाए हुए हैं। यदि बहुसंख्यक जातियों, जो कि तमाम तरह के शोषण, उत्पीडऩ और गैरबराबरी की शिकार हैं, के संचार ढांचे का अध्ययन करें तो वे एक खास तरह के ढांचे में बंधीं हुई हैं। एक विशेष तरह की पत्रकारिता लगातार उनके दमन, उत्पीडऩ और गैरबराबरी की कहानियां उन्हें सुनाती रहती है। लेकिन यह पत्रकारिता केवल संसद तक उनकी कल्पनाओं और इरादों को ले जाती है।
जिस तरह एक राजनीति अपने संसदीय जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने की हर संभव कोशिश करता है, उसी तरह एक सांस्कृतिक योद्धा, बुनियादी परिवर्तन के वैचारिक औजार तैयार करता रहता है। इस फर्क को इस उदाहरण से समझा जा सकता है। कांशीराम जुलाई 1979 में अपने संपादकीय में लिखते हैं कि -दंगों में एक विशेष पहलू यह भी देखने को मिला कि मुसलमानों को अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के विरूद्ध खड़ा करने की कोशिश की गई। अलीगढ़ में मुस्लिमों और जाटवों (चमारों) को भिड़ाने का प्रयास किया गया। जमशेदपुर में अनुसूचित जनजातियों को मुस्लिमों के विरूद्ध खुलकर भड़काया गया तथा नादिया जिले में पिछड़ी जातियों के गुंडे मुस्लिमों से भिड़ गए।’
कांशीराम की वैचारिक दृष्टि स्पष्ट है। लेकिन उन्हें भी अपनी संसदीय जरूरतों के लिए, जिस आरएसएस की दंगों में भूमिका उन्होंने देखी थी, उसी की संसदीय शाखा के साथ सरकार बनाने के लिए तालमेल करना पड़ा।
फारवर्ड प्रेस के जुलाई, 2015 अंक में प्रकाशित





