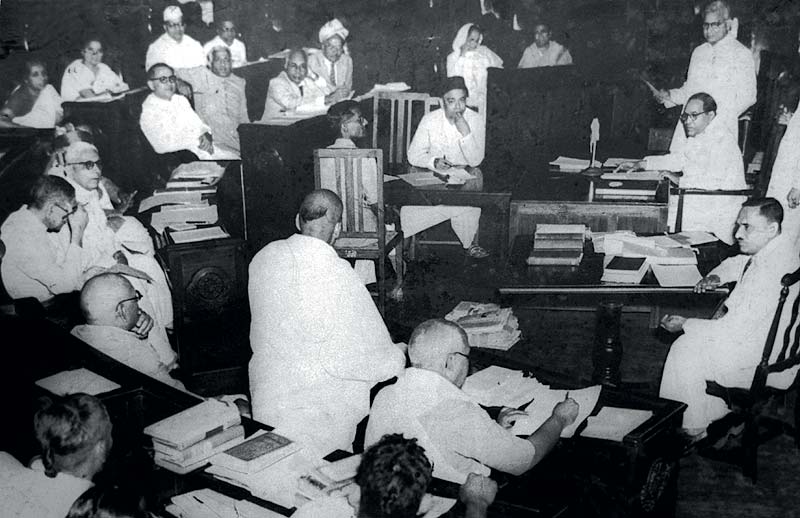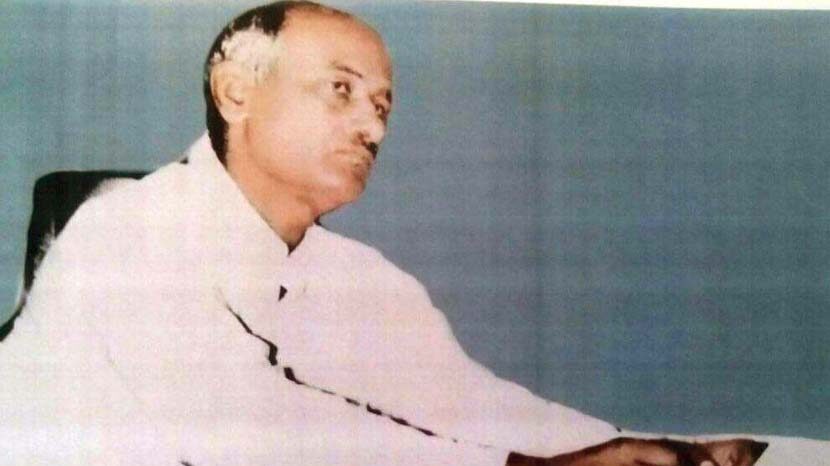रैदास जयंती पर विशेष
ऐसा माना जाता है कि संत रैदास का जन्म 1398 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 में हुई। उनका जन्म काशी (बनारस) में चर्मकार परिवार में हुआ था। बहुजन-श्रमण परंपरा के अन्य कवियों की तरह रैदास के मन में भी अपनी जाति और पेशे को लेकर कोई हीनताबोध का भाव नहीं है, इसके उलट वे अपनी जाति पर गर्व करते हैं। जातीय श्रेष्ठता का दंभ पालने वाले उंची जातियों को ललकारते हुए कहते हैं—
कह रैदास खलास चमारा।
जो हम -सहरी सो मीत हमारा।।
या वे यह कहते हैं—
ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार।
अपनी जाति पर गर्व करने का यह अर्थ नहीं है कि रैदास जाति-व्यवस्था में विश्वास करते थे। वे जाति-व्यवस्था और उंच-नीच की अवधारणा को पूरी तरह खारिज करते थे। वे जाति-व्यवस्था को मनुष्यता को खा जाने वाली चीज मानते थे। वे जाति व्यवस्था के संदर्भ में लिखते हैं—
जात-पात के फेर मह उरझि रहे सब लोग।
मानुषता को खात है, रैदास जात का रोग।।
वे यह भी कहते हैं कि जाति एक ऐसी बाधा है, जो आदमी को आदमी से जुडने नहीं देती है। वे कहते हैं एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से तब तक नहीं जुड़ सकता, जब तक जाति का खात्मा नहीं हो जाता—
रैदास ना मानुष जुड़े सके जब लौं जाय न जात
कबीर की तरह रैदास भी साफ कहते हैं कि कोई उंच या नीच अपने मानवीय कर्मों से होता है, जन्म के आधार पर कोई उंच या नीच नहीं होता। वे लिखते हैं—
रैदास जन्म के कारने होत न कोई नीच।
नर कूं नीच कर डारि है, ओछे करम की नीच।।
वे कहते हैं कि असल में वह व्यक्ति नीच है, जिसके हद्य में संवेदना नहीं है, करूणा नहीं है—
दया धर्म जिन्ह में नहीं, हद्य पाप को कीच।
रविदास जिन्हहि जानि हो महा पात की नीच।
उनका मानना है कि व्यक्ति का आदर और सम्मान उसके कर्म के आधार पर करना चाहिए, जन्म के आधार पर कोई पूज्यनीय नहीं होता है—
रैदास बाभन मत पूजिए जो होवे गुन हीन।
पूजिए चरन चंडाल के जो हो गुन परवीन।।
ब्राह्मणवादी द्विज आलोचको ने रैदास को सगुण मार्गी कवि ठहराने की कोशिश किया। उनके वेद-पुराणों में विश्वास रखने वाले कवि के रूप में चित्रित किया, जबकि सच्चाई इसके उलट है, स्वंय रैदास ने कहा है कि उन्होंने चारो वेदों का खण्डन किया है—
चारो वेद किया खंडौति, ताकौ विप्र करे डंडौति

वे निर्गुण ई्श्वर में विश्वास करते थे, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसके रहने कोई जगह नहीं है, जिसका कोई आकार-प्रकार नहीं है, जो सब जगह विराजमान है। वे सहज स्वरूप नाम देते हैं—
मन ही ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊं सहज स्वरूप।
तोडूं न पाती, पूजूं न देवा। सहज समाधि करूं हरि सेवा।।
वे मानते हैं कि ईश्वर को पाने का एक ही तरीका है, वह गरीबों की निरंतर सेवा। उनका कहना है कि जो व्यक्ति निरंतर गरीबों की सेवा में लगा रहता है, वह ईश्वर से मिलने की आशा कर सकता है—
दीन दुखी के सेव में लाग रह्यो रविदास।
निशिवासर की सेव सौ प्रभु मिलन की आस।।
गरीबों के प्रति रैदास के मन में कितनी हमदर्दी है, कितनी संवेदना इसका अंदाज इस बात से लगता है कि वे उसी व्यक्ति को सबसे सच्चा योद्धा मानते हैं, जो गरीबों हित में अपने प्राण त्यागता है—
दीन दुखी के हेत जऊ, वारै अपने प्रान।
रविदास वह नर सूर को सांचा सूरा जान।।
बहुजन-श्रमण परंपरा के अन्य कवियों की तरह रैदास भी हिंदू-मुस्लिम के बीच कोई भेद नहीं करते। दोनों के पाखण्ड को उजागर करते हैं। वे साफ शब्दों में कहते हैं कि न मुझे न तो मंदिर से कोई मतलब है, न मस्जिद से, क्योंकि दोनों में ईश्वर का वास नहीं है—
मस्जिद सो कुछ घिन नहीं मन्दिर सो नहीं प्यार।
दोउ अल्ला हरि नहीं कह रविदास उचार।।
रैदास मंदिर-मस्जिद से अपने दूर रखते हैं, लेकिन हिंदू-मुस्लिम दोनों से प्रेम करते हैं, दोनों के बीच कोई भेद नहीं करते हैं—
मुसलमान से दोस्ती हिन्दुवन से कर प्रीत।
रविदास ज्योति सभ हरि की सभ हैं अपने मीत।
वे मनुष्य-मात्र के एकता और भाईचारे में विश्वास रखते हैं। वे मानते हैं कि सभी मनुष्य एक हैं। मनुष्यों के बीच जाति या धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं करना चाहिए—
रविदास सभहिं है एक ब्राहमन मुल्ला सेख।
सभका करता एक है, सभकू एकहि पेख।।
रैदास बार-बार इस बात पर जोर देते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों में कोई भेद नहीं है। जिन तत्वों से हिंदू बने हैं, उन्हीं तत्वों से मुसलमान। दोनों के जन्म का तरीका भी एक ही है—
हिन्दू तुरूक महि नाहि कछु भेदा दुई आयो इक द्वार।
प्राण पिण्ड लौह मास एकहि रविदास विचार।।
ब्राह्मणवादी द्विज परंपरा के विपरीत बहुजन-श्रमण परंपरा के कवि श्रम की संस्कृति में विश्वास करते हैं। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को श्रम करके ही खाना खाने का अधिकार है। वे परजीविता से घृणा करते थे—
रविदास श्रम कर खाइए है, जो-लौ-पार बसाय।
नेक कमाई जौ करई कबह न निष्फल जाय।।
रैदास श्रम करते जीवन-जीने को सबसे बड़ा मूल्य मानते हैं। घर-बार छोड़कर वन जाने या सन्यास लेने को ढोंग-पाखण्ड मानते हैं—
नेक कमाई जउ करइ गृह तजि बन नहिं जाय।
रैदास अभिमानी ब्राह्मण की तुलना में श्रमिक को ज्यादा महत्व देते है—
धरम करम जाने नहीं, मन मह जाति अभिमान।
ऐ सोउ ब्राह्मण सो भलो रविदास श्रमिकहु जान।।
रैदास पराधीन जाति और समाज में पैदा हुए थे, पराधीनता के दर्द को अच्छी तरह महसूस करते थे। पराधीन मनुष्य की क्या स्थिति होती है, कैसे हर व्यक्ति हिकारत की नजर से देखता है। पराधीन आदिमी की स्थिति को उन्होंने इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है—
पराधीन का दीन क्या, पराधीन बेदीन।
रविदास परा अधीन को सभेही समझै हीन।।
वे पराधीनता से मुक्ति के लिए आह्वान करते हैं—
पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत।
रविदास दास पराधीन से कौन करै है प्रीत।।
बहुजन-श्रमण परंपरा वर्चस्व की संस्कृति में विश्वास नहीं करती है। यह परंपरा सबसे लिए न्यायपूर्ण समाज का स्वप्न देखती रही है, सबके लिए स्वतंत्रता और समता की कामना करती है। मनुष्य-मनुष्य के बीच बंधुता की चाह रखती है। रैदास भी एक ऐसे समाज का स्वप्न देखते हैं, जिसमें किसी तरह का दुख नहीं हो, असन्तोष नहीं हो और किसी प्रकार का अन्याय न हो। सुख हो, शान्ति हो और बंधुता हो। ऐसी जगह को वे बेगमपुर नाम देते हैं—
बेगम पुरा सहर को नाउ।।
दूख: अंदोह नही तह ठाउ।।
न तसवीस खिराजु न माल ।।
खउफ न खता न तरस जवाल ।।१।।
अब मोहि खूब वतन गह पाई ।।
ऊहां खैर सदा मेरे भाई ।।१।। रहाउ ।।
काइम दाइम सदा पातिसाही ।।
दोम न सेम एक सो आही ।।
आबादान सदा मसहूर ।।
ऊहां गनी बसहि मामूर ।।२।।
तिउ तिउ सैल करहि जिउ भावै ।।
महरम महल न को अटकावै ।।
कहि रविदास खलास चमारा ।।
जो हम सहरी सु मीत हमारा ।।३।।२।।
रैदास संत परंपरा के कवि हैं। इन संत कवियों के काव्य का आधार बौद्ध धम्म की मानवीय करूणा और समता की विचारधारा रही है। कंवल भारती के शब्दों में कहें तो,’ संत काव्य का वास्तविक आधार बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के पतन के बाद जो बुद्ध वचन परंपरा से जन-जीवन में संचित थे, संत काव्य उन्हीं की अभिव्यंजना हुई है। इसका सबसे प्रबल प्रमाण यह है कि सन्तों का साहित्य जीवन की स्वीकृति का साहित्य है, उसमें पीड़ित जन का आक्रोश और आवेश, सुखी समाज की आकांक्षा, और शोषक श्रेणी के प्रपंचों पर आघात है, और सबसे बढ़कर समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की स्पष्ट अभिव्यक्ति है।
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +919968527911, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें :
बहुजन साहित्य की प्रस्तावना
जाति के प्रश्न पर कबीर
चिंतन के जन सरोकार
महिषासुर : मिथक व परंपराए