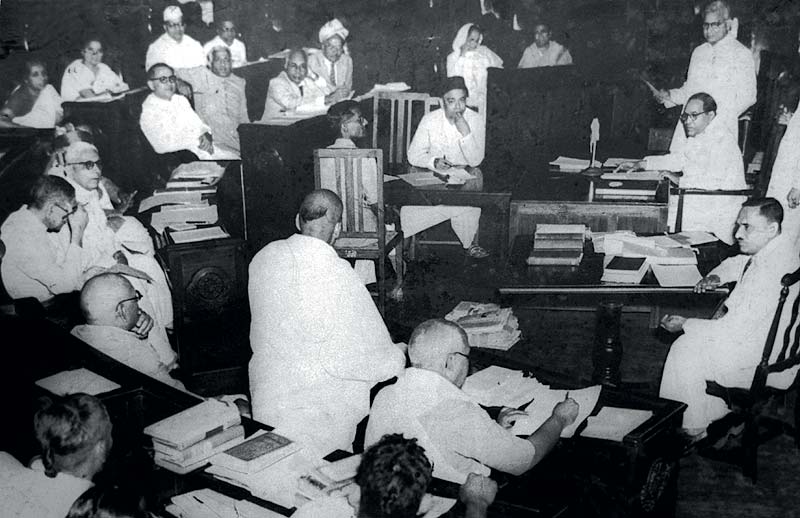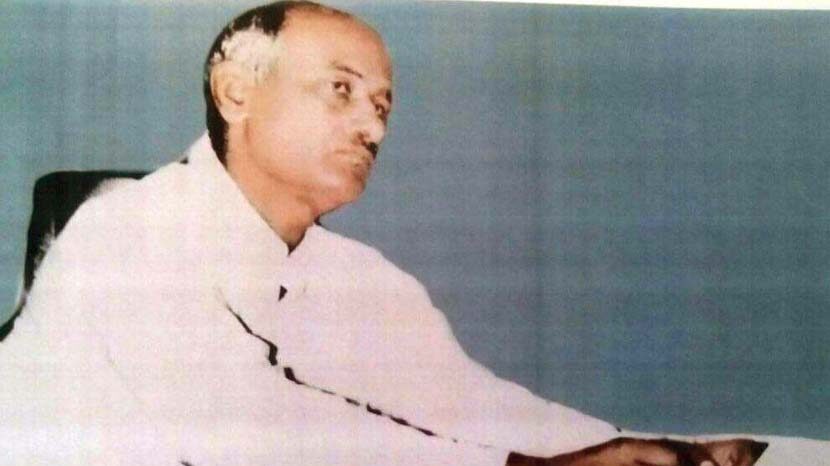“मैं मानव-मात्र की समानता में विश्वास करता हूं. मेरे हिसाब से धर्म का अभिप्रायः ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करना है, जिनसे न्याय की स्थापना हो. दिलों में एक-दूसरे के प्रति दया, ममता, करुणा तथा प्रेम का उजियारा हो, ऐसे कर्तव्य करना जिनसे हमारे आसपास के प्राणी अधिकाधिक सुखी रह सके”—थॉमस पेन
“तुम उस समय तक अच्छा समाज नहीं गढ़ सकते जब तक तुम्हें पर्याप्त राजनीतिक अधिकार न हों. न ही तुम उस समय तक अपने राजनीतिक संकल्पों तथा विशेषाधिकारों पर अमल कर सकते हो, जब तक तुम्हारा सामाजिक तंत्र तर्क और न्याय-भावना पर केंद्रित न हो. तुम उस समय तक अच्छा आर्थिक ढांचा खड़ा नहीं कर सकते जब तक सामाजिक ढांचा बेहतर न हो. यदि तुम्हारा धर्म नैतिक आधार पर कमजोर और भटकाव-युक्त है तो तुम स्त्री तथा अन्य वर्गों के लिए समानतायुक्त वातावरण नहीं बना सकते. अन्योन्याश्रितता महज दुर्घटना नहीं, कुदरत का नियम है.”—महादेव गोविंद रानाडे
आज देश में लोकतंत्र है. चुनावों के दौरान करीब एक अरब नागरिक अलग-अलग और एक साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं. उसके आधार पर हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का दावा कर सकते हैं. हालांकि कुछ कमजोरियां भी हैं. हमारे यहां भूख है, गरीबी है, भीषण समाजार्थिक असमानता तथा बेरोजगारी है. नेता सब्जबाग दिखाते हैं. सरकारें बनती हैं. जनाकांक्षाओं को पूरा किए बगैर चली भी जाती हैं. उनका शिकार समाज के निम्न-मध्यम, गरीब और विपन्न लोगों को होना पड़ता है. फिर भी चुनावों के दौरान सर्वाधिक भागीदारी इन्हीं लोगों की रहती है. लोकतंत्र से सर्वाधिक उम्मीद भी इसी वर्ग को है. यह उम्मीद नहीं होती, सपने नहीं होते. सपनों को पहचानने, उन्हें पूरा करने की हसरत तथा संघर्ष करने का जज्बा नहीं होता—यदि महात्मा जोतीराव फुले और डॉ. आंबेडकर नहीं होते. भारत को आधुनिक राज्य बनाने में इन दो महापुरुषों का सर्वाधिक योगदान रहा है.

दोनों अलग-अलग समय में जन्मे. जो फुले का समय है वह डॉ. आंबेडकर का नहीं है. जिस वर्ष आंबेडकर का जन्म हुआ, उससे कुछ महीने पहले फुले दुनिया छोड़ चुके थे. फिर भी लगता है जैसे सबकुछ योजनाबद्ध हो. ओलंपिक के उन खिलाड़ियों की भांति जिनमें एक पूरे संकल्प और इरादे के साथ मशाल लेकर दौड़ता है, फिर उसे आगे वाले खिलाड़ी के हाथों में सौंपकर अंर्तध्यान हो जाता है. दोनों का संघर्ष अपने समाज के अलावा समय के साथ भी है. अतएव बिना उनके इतिहास को जाने, बगैर उस समय की पड़ताल किए—उनके योगदान को समझ पाना असंभव है.
जोतीराव फुले द्वारा स्थापित पाठशाला में पढ़ने वाली एक लड़की ने प्रदेश में महार और मांग जातियों की दुर्दशा पर एक निबंध लिखा था. निबंध इतना मार्मिक था कि मराठी समाचारपत्र ‘ज्ञानोदय’ ने 15 फरवरी 1855 के अंक में उसपर एक समाचार प्रकाशित किया. इस घटना का उल्लेख धनंजय कीर ने ‘महात्मा ज्योतिबा फुले’ में किया है. उसमें पेशवाई के अन्याय के विरोध में आक्रोश है, तो अंग्रेजी शासन के प्रति सहानुभूति की झलक भी है. निबंध उस समय के शूद्र एवं अतिशूद्रों की मनोस्थिति का दस्तावेज है—
‘‘ब्राह्मण कहते हैं, वेदों पर उनका विशेषाधिकार है. केवल वही उनका अध्ययन कर सकते हैं. इससे पता चलता है कि हमारा कोई धर्मग्रंथ नहीं है. यदि वेद ब्राह्मणों की रचना है तो उनके अनुसार आचरण करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है. हमें धर्मग्रंथों को पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं है. कहना पड़ेगा कि हमारा कोई धर्म नहीं है. हम बिना धर्म के हैं. हे ईश्वर! तू ही बता, तूने हमारे लिए कौन-सा धर्म बनाया है, जिससे ब्राह्मणों की तरह हम भी उसका पालन कर सकें.
पहले हम इमारतों की नींव तले दफना दिए जाते थे. शिक्षा सदनों में जाने की हमें अनुमति नहीं थी. यदि कोई ऐसा करे तो उसकी गर्दन नाप दी जाती थी. आज बाजीराव द्वितीय आकर देखे कि अछूत और शूद्र लड़के-लड़कियां स्कूल जा रहे हैं तो ईर्ष्या और क्रोध से उसका दिमाग फट जाएगा—‘अरे! यदि महार और मांग पढ़-लिख जाएंगे तो क्या ब्राह्मण उनकी सेवा करेगा? क्या ब्राह्मण बच्चे उसके लिए बोझा ढोकर लाएंगे? परमात्मा ने हमें ब्रिटिश राज्य की सौगात दी है. आज हमारे कष्टों में कमी आई है. अब कोई हमें परेशान नहीं कर सकता. कोई हमें फांसी नहीं चढ़ा सकता. कोई हमें जिंदा नहीं जला सकता. हमारी संतान सुरक्षित है. हम अपना शरीर ढक सकते हैं. चादर ओढ़ सकते हैं. आज हर किसी को अपने ढंग से जीने की आजादी है. कोई बंधन नहीं, किसी प्रकार का अंकुश नहीं है. कोई प्रतिबंध भी नहीं हैं. यहां तक कि हमें बाजार जाने की भी आजादी है.’’
उसी अखबार ने आगे लिखा था—‘‘वे(अछूत) किसी न्यायालय के भीतर नहीं जा सकते. रोगी का इलाज कराने के लिए उन्हें अस्पताल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है. किसी सराय में नहीं ठहर सकते. न ही प्रदेश की सार्वजनिक सड़कों पर आने-जाने की अनुमति उनको है. किसान-शिल्पकार की हैसियत से उन्हें सदैव घाटा उठाना पड़ता है, क्योंकि बाजार में दुकान की सीढ़ियां चढ़ने की अनुमति उन्हें नहीं है. मजबूरी में उन्हें अपना माल दलालों के हाथों ओने-पौने भाव बेचना पड़ता है. कुछ तो इतने पतित मान लिए गए हैं कि उनसे कुछ काम नहीं लिया जा सकता….वे केवल भिक्षा के सहारे जीते हैं. भीख मांगने के लिए भी वे सड़क का प्रयोग नहीं कर सकते. उन्हें सड़क से दूर, ऐसी जगह जहां से कोई देख न ले, खड़ा होना पड़ता है. लोगों को आते-जाते देख दूर खड़े-खड़े गुहार लगाते हैं. दया करके यदि कोई दूर से ही भीख उछाल देता है, तो वे उसपर झपट नहीं पड़ते. बल्कि वे वहीं खड़े-खड़े उस समय तक प्रतीक्षा करते हैं, जब तक भीख देने वाला आंखों से ओझल न हो जाए. उसके जाते ही भीख को उठाकर वहां से भाग जाते हैं.’’[1]
कदाचित वह पहला अवसर था जब कोई अछूत बालिका अपने कष्टों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त कर रही थी; और समाचारपत्र उसकी पीड़ा को सार्वजनिक कर रहा था. उससे पहले शूद्र और अतिशूद्र अपने कष्टों के बारे में बताना तो दूर सोचना तक नहीं जानते थे. उनके लिए सबकुछ नियतिबद्ध, दैवी आदेश जैसा था. शोषण एवं दमन से मुक्ति के लिए ईश्वर की विशेष अनुकंपा की कामना की जाती थी. कहा जाता था कि ईश्वरीय अनुकंपा तभी संभव है जब वे उन कर्मों का निर्वाह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें, जो उनके लिए वर्ण-व्यवस्था द्वारा निर्धारित किए गए हैं. इस तरह दमन और शोषण का सोचा-समझा विधान था. खासकर अश्पृश्यता को लेकर. देवेंद्र कुमार बेसंतरी ने केरल का उदाहरण दिया है—‘नंबूदरी ब्राह्मण नायर जैसे सवर्णों से 32 फुट की दूरी से, नायर इढ़वा लोगों से जो अगम्य थे, परंतु जिनका सामाजिक ढांचे में बहुत ऊंचा स्थान था, 64 फुट कर दूरी से और इढ़वा जाति के लोग अछूतों पुलवा, परेया से सौ फुट की दूरी पर ही अपवित्र हो जाते थे.’(संदर्भ-भारत के सामाजिक क्रांतिकारी, देवेंद्र कुमार बेसंतरी, पेज, 136). ऐसे परिवेश में शूद्र अपने लिए भला कैसे मान-सम्मान की उम्मीद करता! नाउम्मीदी के बीच वे अपना जीवन जीने को विवश थे. पुरोहित वर्ग इसे भाग्यदोष अथवा पूर्व कर्मों का फल कहकर भरमाए रखता था. उत्पीड़न से मुक्ति का एक रास्ता धर्म-परिवर्तन भी था. लेकिन वह भी निरापद न था. जाति प्रथा के विषाणु बाकी धर्मों में भी प्रवेश कर चुके थे. धर्मांतरित व्यक्ति को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था. यह दुर्दशा क्यों हुई? इसपर फुले ने विचार किया है. शूद्रों-अतिशूद्रों की अशिक्षा का मामला उनके लिए कितना महत्त्वपूर्ण था, वह इससे भी पता चलता है कि ‘किसान का कोड़ा’ पुस्तिका की भूमिका की शुरुआत ही उन्होंने इन शब्दों से की है—‘विद्या न होने से बुद्धि न रही, बुद्धि के न रहने से नैतिकता का हृास हुआ, नैतिकता न रहने से गतिशीलता का लोप हुआ, गतिशीलता के अभाव में धन-दौलत दूर होते गए, धन-दौलत के न रहने से शूद्रों का पतन हुआ. इतना अनर्थ एक अविद्या के कारण हुआ.’
डॉ. आंबेडकर ने बुद्ध और कबीर के अलावा फुले को भी अपना गुरु माना. दलितों की दुर्दशा का मूल कारण अशिक्षा है. दलित युवाओं को शिक्षा का महत्त्व समझाते हुए उन्होंने लिखा—‘शिक्षा शेरनी का दूध है. जो भी पीता है, दहाड़ने लगता है.’ डॉ. आंबेडकर आजीवन दलितों को शिक्षित होने, संगठित रहने तथा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आवाह्न करते रहे.
उस समय के सभी सुधारवादी अंग्रेजी शिक्षा से प्रेरित थे. नई ज्ञान-चेतना, जिसके मूल में जॉन लाक, वाल्तेयर, रूसो, बैंथम, मार्क्स, थॉमस पेन जैसे महान दार्शनिकों की प्रेरणाएं थीं—से लबरेज होकर उन्होंने भारतीय समाज की कुरीतियों को समझा तथा उनसे संघर्ष किया था. बदले में यथास्थितिवादियों का विरोध और उत्पीड़न सहा. अपने-अपने क्षेत्र में वे सब कमोबेश सफल भी रहे. लेकिन उनके कार्यक्षेत्र का दायरा सीमित था. डॉ. आंबेडकर के मतानुसार उनके प्रयास केवल परिवार-सुधार तक सीमित थे.[2] समाज सुधार की दिशा में बहुत आगे बढ़ने की इच्छाशक्ति उनमें नहीं थी. राजा राममोहनराय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद जैसे महापुरुषों द्वारा चलाए जा रहे सुधारवादी आंदोलनों का प्रभाव जनता पर पड़ा था. लेकिन सीमित अर्थों में. हेनरी वर्नर हंपटन ने ‘ब्रह्मसमाज’ के संस्थापक राजा राममोहनराय को भारत में सुधारवादी आंदोलन का शिखर पुरुष घोषित करने के साथ-साथ, उन सीमाओं का उल्लेख भी किया है, जिनके पीछे उनके जन्मगत संस्कार थे. हंपटन के अनुसार राजा राममोहनराय, ‘अपने समय से बहुत आगे थे. लेकिन जहां तक शूद्रों की शिक्षा का सवाल है उनका मानना था कि शिक्षा ऊपर से शुरू होकर नीचे तक जानी चाहिए. इस प्रकार आरंभ में धीरे-धीरे, आगे चलकर तेजी से वह जनसाधारण तक पहुंच जाएगी. इस मामले में वे अपने समय की प्रचलित मान्यताओं के समर्थक थे. प्रकारांतर में वे उन लोगों में से थे जो बहुत आशावादी थे.’[3] हंपटन ने इसे फिल्ट्रेशन का सिद्धांत कहा है.
‘ब्रह्म समाज’ प्रकट में समाज के जाति-आधारित विभाजन की आलोचना करता था. वर्ण-विभाजन को लेकर उसे कोई शिकायत न थी. उसके द्वारा निर्धारित पूजा-विधानों में पुरोहित की भूमिका केवल ब्राह्मण निभा सकता था. जिसे ऊपर ‘फिल्ट्रेशन का सिद्धांत’ कहा गया है, अर्थशास्त्र की भाषा में उसे ‘ट्रिकिल डाउन थियरी’(रिसाव का सिद्धांत) कहा जाता है. उसके अनुसार समृद्धि ऊपर से नीचे की ओर निस्सरित होती है. गोया समाज को अपने स्वार्थ के अनुसार चलाते आए लोग सुधार को भी अपने स्वार्थानुसार नियंत्रित कर लेते हैं. इसकी सबसे अच्छी व्याख्या डॉ. आंबेडकर ने 1936 में ‘जात-पांत तोड़क मंडल’ के महाधिवेशन के लिए अपने दिए न जा सकने वाले अध्यक्षीय भाषण में की थी. विधवा विवाह, सती प्रथा उन्मूलन, बाल-विवाह की रोकथाम आदि भारतीय समाज की प्रमुख समस्याओं जिनसे भारतीय समाज उन दिनों जूझ रहा था, को उन्होंने ‘हिंदू परिवार का सुधार’ कार्यक्रमों तक सीमित माना था. उनका विश्वास था कि वास्तविक सुधार किसी मसीही कृपा द्वारा संभव नहीं है. उसकी पुनर्रचना केवल समाज के पुनर्गठन द्वारा संभव है(जातिप्रथा का उन्मूलन). वे जानते थे कि शिखर पर मौजूद लोग अपने विशेषाधिकारों को एकाएक छोड़ने को तैयार न होंगे. केवल संगठित शक्ति द्वारा उन्हें काबू में लाया जा सकता है. यह तभी संभव है जब लोग अपने कष्ट, शोक, विपन्नता के प्रति संवेदनशील हों. उनके पीछे निहित कारणों को समझते हों. ऐसे प्रश्नों की ओर लोगों का ध्यान न जाए, इसके लिए धर्म को बीच में लाया जाता है. इस साजिश को फुले ने सबसे पहले समझा था. यह मानते हुए कि दूसरों के भरोसे आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, उन्होंने निचली जातियों के युवक-युवतियों की पढ़ाई के लिए स्कूल खोले. सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाए. धर्म के नाम पर आडंबर फैला रहे ब्राह्मण पुरोहितों को चुनौती दी.
फुले ने जो कहा और जितना लिखा, बहुत बड़ा हिस्सा केवल दो मुद्दों पर केंद्रित है. पहला धर्म के नाम पर ब्राह्मणों द्वारा फैलाए जा रहे आडंबरों का विरोध, दूसरा शूद्र-अतिशूद्र के लिए शिक्षा पर जोर. दोनों मुद्दे बेहद चुनौतीपूर्ण थे. व्यवस्था के शिखर पर कुंडली मारे बैठी शक्तियां खुद को बदलने के लिए तैयार न थीं. जिस ‘फिल्ट्रेशन थियरी’ पर राजा राममोहनराय तथा उनके सहयोगियों की उम्मीदें टिकी थीं, वह नाकाम सिद्ध हुई थी. भारतीय समाज में शिक्षा की स्थिति का आकलन करने के लिए 1882 में ‘इंडियन एजुकेशन मिशन’ की स्थापना की गई थी. अपने अध्ययन के दौरान मिशन ने पाया कि कस्बों और शहरों में शिक्षा में सुधार हुआ था. लेकिन गांवों में वैसे ही हालात थे. शहरों में भी शिक्षा का जितना लाभ ऊंची जातियों ने उठाया था, शूद्रों, अतिशूद्रों तक उतना लाभ नहीं पहुंच पाया था. शिक्षा विभाग में अधिकांश अध्यापक ब्राह्मण थे. वे निचली जातियों के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव बरतते थे. यह बात कमोबेश उस समय के प्रमुख सुधारवादियों पर भी लागू थी. उच्च वर्गों से आए सुधारवादी सुधार तो चाहते थे, लेकिन हिंदू धर्म की मूल संरचना में छेड़छाड़ का न तो उनमें साहस था, न वैसी इच्छाशक्ति. इसीलिए थोड़े अंतराल के पश्चात हिंदू समाज में वही विकृतियां दुबारा पनपने लगती थीं. सती प्रथा पर कानूनी रोक 1829 में ही लग चुकी थी, मगर समाज उस विकृति से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाया था. मुंबई के समाचारपत्र ‘टेलीग्राफ एंड कुरियर’ में नवंबर 1852 में भुज की एक घटना छपी थी—
‘एक स्त्री को बलात् सती के लिए ले जाया जा रहा था. वह बचने के लिए चीख-चिल्ला रही थी. अंग्रेज अधिकारियों ने उसे बचाने का प्रयत्न किया. लेकिन साथ जा रहे ब्राह्मणों ने उसे जबरदस्ती खींचकर पुनः चिता पर बिठा दिया. युवती आगे चीखे-चिल्लाए नहीं इसके लिए उन्होंने उसके सिर पर प्रहार कर उसे बेहोश कर दिया फिर उसी अवस्था में चिता पर लिटाकर आग जला दी गई.’[4]
विकृति केवल सती प्रथा तक सीमित नहीं थी. प्रसिद्ध उपयोगितावादी दार्शनिक जेम्स मिल ने ‘ब्रिटिश भारत का इतिहास’ तथा अमेरिकी लेखिका कैथरीन मेयो ने ‘मदर इंडिया’ में भारतीय समाज की दुर्दशा का वर्णन किया है. उसके अनुसार पूरा भारतीय समाज घोर जातिवाद और आडंबरों में फंसा था. अनगिनत अंधविश्वास थे. एक अंधविश्वास यह भी था कि गंगा किनारे मृत्यु होने पर मोक्ष प्राप्त होता है. इसलिए बीमार परिजनों को मरणासन्न अवस्था में गंगा किनारे छोड़ देना धार्मिक कर्तव्य माना जाता था. बंगाल में तो यह मान्य प्रथा बन चुकी थी. माना जाता था कि गंगा किनारे मृत्यु होने पर आत्मा सीधे स्वर्ग की ओर प्रयाण कर जाती है. उस समय ‘कलकत्ता रिव्यू’ में ऐसे अनेक समाचार प्रकाशित हुए थे, जिसमें रोगी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए उसे मरने के लिए गंगाघाट भेज दिया जाता था. कुछ धर्म-भीरू वृद्धाएं गेहूं या चावल के दाने रात-दिन गिनती रहती थीं. एक लाख की गिनती पूरी होने पर उन्हें दान कर दिया जाता था. तरह-तरह बत्तियां बांटकर दान करने की भी प्रथा थी. कई बार यह मानते हुए कि गाय की सेवा ही मुक्ति दिला सकती है, गाय को अनाज खिलाया जाता. फिर उसके गोबर और मूत्र को श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया जाता था. पुजारी वर्ग ऐसे पाखंडों को बढ़ावा देता था. सरकार उनकी अनेक कुरीतियों पर प्रतिबंध लगा चुकी थी. तथापि अशिक्षा और रूढ़ियों में फंसा धर्मभीरू भारतीय समाज उनसे बाहर निकल ही नहीं पा रहा था.
महाराष्ट्र में 1827 तक एक प्रथा थी कि शंकराचार्य आगमन पर दक्षिणा के रूप जो भी मांग लें उसे देना यजमान का कर्तव्य बन जाता था. इस कुरीति के बारे में किसी ने पूना के कलेक्टर से शिकायत कर दी तो उसने तत्काल उसपर प्रतिबंध लगा दिया. दान का निर्णय शंकराचार्य की मर्जी के बजाय दानदाता की इच्छा पर छोड़ दिया गया. विधवाओं का मुंडन करना, उन्हें शुभ घोषित कर घर के किसी अंधेरे कोने में रहने के लिए विवश कर देना. अच्छा खाने, पहनने और रहने पर प्रतिबंध लगा देना—उन दिनों के स्त्री जीवन की त्रासदी थी. अगर कोई विधवा गलती से परपुरुषगमन करते हुए पकड़ी जाए तो दोष जानलेवा हो जाता था. 1854 में ऐसे ही एक मामले का शंकराचार्य द्वारा फैसला करने का एक उदाहरण है. घटना के अनुसार मुंहमांगी दक्षिणा का भरोसा होने के पश्चात शंकराचार्य ने विधवा के शुद्धिकरण का आश्वासन दिया. शंकराचार्य के पैर का अंगूठा विधवा स्त्री के सिर पर रखकर उसे पंच-गव्य से स्नान कराया गया. इस बीच लड़की के पिता ने बताया कि उसकी बेटी गर्भवती है, शुद्धिकरण के दौरान इसका भी ध्यान रखा जाए. इसपर शंकराचार्य क्रोधित हो गए. पुरुष हजार बदचलनी करे. इंद्र और विष्णु जैसे देवता दूसरों की पत्नियों के साथ बलात्कार करते फिरें. उससे धर्म की हानि नहीं होती. यदि स्त्री भूलवश भी कुछ कर दे तो ‘वैकुंठ लोक’ संकट में पड़ जाता है. अंतत: मनोवांछित दक्षिणा की शर्त पर शंकराचार्य ने विधवा के ‘उद्धार’ की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली. उन्होंने युवती को खोखले पेड़ के तने में रखकर आग लगाने का विधान किया. लड़की के पिता से कहा कि ‘अग्निपरीक्षा’ के बाद भी यदि उसकी बेटी बची रहती है तो उसका सिर मुंडवाने तथा एक सहस्र ब्राह्मणों को भोज कराने के उपरांत उसका शुद्धिकरण संभव है.
यह भी पढ़ें : जाति का विनाश : वह भाषण जिसे बाबा साहब को देने नहीं दिया गया
ऐसा नहीं कि इन घटनाओं का हिंदू समाज के भीतर कोई विरोध नहीं था. यहां तक कि सवर्णों में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो सामाजिक विकृतियों का विरोध करते थे. लेकिन उन लोगों की संख्या बहुत कम थी. 94 प्रतिशत जनता अशिक्षित थी. बाकी 6 प्रतिशत किसी न किसी रूप में उस व्यवस्था से लाभान्वित थे. वे सरकार और समाज के शीर्षस्थ पदों पर थे. बेहद जटिल सामाजिक ताने-बाने में फंसा आम आदमी केवल कराह सकता था. आडंबरों का बोलबाला था. तरह-तरह के भय दिखाकर पंडे-पुरोहित उसे लूटते रहते थे—
‘प्रत्येक नागरिक राज्य को कर देने से ज्यादा ब्राह्मणों को दान करता है. जन्म से लेकर मृत्युपर्यंत, वह भू-देवता ब्राह्मणों का पोषण करने में लगा रहता है. जातक के जन्म के समय ब्राह्मण को भोजन कराना जरूरी माना जाता है, नहीं तो बच्चे के आजीवन कंगाल बने रहने की संभावना रहती है. जन्म के सोलहवें दिन घर के शुद्धीकरण की रस्म मनाई जाती है, उसमें भी ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है. कुछ दिन बाद बच्चे के नामकरण के नाम पर फिर ब्राह्मण को दक्षिणा. तीसरे महीने मुंडन की रस्म होती है, ब्राह्मण पुनः दक्षिणा लेने पहुंच जाता है. उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार. शिशु जब पहली बार अन्न चखता है, तब भी ब्राह्मण को भुगतान किया जाता है. बालक चलने लगता है तो एक बार फिर ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है. साल-भर बाद बालक का जन्मदिवस आ जाता है. ब्राह्मण को फिर भोग के लिए आमंत्रित किया जाता है. वह आता है और दक्षिणा के साथ वापस लौटता है. सात वर्ष का होने पर बालक का शिक्षा संस्कार होता है. उस समय भी ब्राह्मण को भोज और दक्षिणा के लिए आमंत्रित किया जाता है.’[5]
उपनयन के बाद भी अनेक संस्कार थे, जिनसे हिंदुओं को गुजरना पड़ता था. सामाजिक संबंध और मर्यादाओं के निर्वहन के लिए बहुत जरूरी था. ‘किसान का कोड़ा’ में फुले ऐसी कई स्थितियों का वर्णन करते हैं, जिनमें पुरोहित द्वारा यजमान को डराकर, प्रलोभन देकर तरह-तरह से धन ऐंठते रहते थे. अधिकांश के लिए वही जीवन है. धर्म, संस्कृति और परंपरा के नाम पर वे अत्याचार को चुपचाप सह लेते हैं. लोगों को धर्म और ईश्वर का भय दिखाना पंडित का पुश्तैनी धंधा है. उस को जमाए रखने के लिए वह नए-नए देवता गढ़ता है. कर्मकांड की अमर-बेलि चढ़ाता है. परंपराओं का मनमाना विश्लेषण तो आम बात है. हालात जो भी हों, धर्म लोगों के विवेक पर पर्दा डालता है. लोगों की अज्ञानता तथा धर्म के बहाने भीतर पैठाए गए डर की मदद से पंडित पूरे समाज पर राज करता आया है. जनसंख्या की दृष्टि से वह अल्पसंख्यक है. मगर संगठन के आधार पर सबसे ताकतवर. अनगिनत जातियों, उपजातियों में विभाजित शूद्र-अतिशूद्र संख्या-बहुल होकर भी शक्ति-विपन्न बने रहते थे. दूसरी ओर ब्राह्मण के मुंह से निकले प्रत्येक शब्द को ज्ञान मान लिया जाता था. लोकश्रुति के अनुसार रामानंद नहीं चाहते थे कि कबीर को दीक्षा दें. मगर धुन के पक्के कबीर बनारस के गंगा घाट की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए. रामानंद का वहां से रोज आना-जाना था. उस दिन घाट की सीढ़ियों से गुजरते रामानंद का पैर कबीर से टकराया. मुंह से निकला—‘राम-राम.’ अनायास निकले उन शब्दों को ही कबीर ने गुरुमंत्र मान लिया. यह कहानी समाज की मानसिकता को दर्शाती है. भला कबीर जैसे औघड़ ज्ञानी को ब्राह्मण गुरु की क्या आवश्यकता थी! इसकी आवश्यकता तो उन चेले-चपाटों को थी, जिन्होंने कबीर को गुरु बनाकर मठ स्थापित किए थे. लोग मठों को पूजें, उनके शिष्यत्व को स्वीकारें इसके लिए कबीर को गुरु परंपरा के प्रति समर्पित दिखाना जरूरी था.
परिवर्तन की आहट उनीसवीं सदी के आरंभ में ही मिलने लगी थी. जून 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे आत्मसमर्पण के साथ पेशवाई का अंत हो चुका था. उस लड़ाई में अछूत सैनिकों की बड़ी भूमिका थी. उनके लिए वह अस्मिता और आत्मसम्मान की लड़ाई थी. इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के मात्र आठ सौ सैनिक बाजीराव द्वितीय के लगभग 28,000 सैनिकों पर भारी पड़े थे. उसके साथ ही देश का अधिकांश हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो चुका था. तीस करोड़ भारतीयों का कुछ हजार अंग्रेजों के अधीन हो जाना शर्म की बात थी. परंतु धर्म, जाति, क्षेत्रीयता के आधार पर बंटे समाज के लिए तो यह नियतिबद्ध जैसा था. उससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था. सत्तापक्ष से असंतुष्ट लोग स्वार्थ के वशीभूत हो, विदेशी आक्रामकों का साथ देते आए थे. कुछ ऐसे लोग भी अंग्रेजों के समर्थन में थे, जो योरोप की औद्योगिक क्रांति से प्रभावित थे. उनमें से अधिकांश के वाणिज्यिक हित अंग्रेजों से जुड़े थे. उस समय तक भारतीय उद्योग असंगठित था. व्यापारी वर्ग उत्पादों को देश-देशांतर तक पहुंचाने का काम करता था. अंग्रेजों के आने से इस वर्ग की महत्त्वाकांक्षाएं बढ़ी थीं. व्यापारियों के कंपनी के समर्थन में आने का सीधा असर रजबाड़ों की अर्थव्यवस्था पर पड़ा था. वे विरोध का सामर्थ्य गंवा चुके थे. शूद्रों-अतिशूद्रों के लिए पेशवाई का पराभव मुक्ति-संदेश जैसा था. उधर ‘चार्टर अधिनियम-1813’ के अनुसार देश की बागडोर अप्रत्यक्ष रूप से इंग्लेंड के हाथों में जा चुकी थी. कंपनी के अधिकार घटे थे. चीन को चाय और अफीम आदि के निर्यात के अलावा बाकी मामलों में उसे ब्रिटिश संसद की मंजूरी लेनी पड़ती थी.
जन-सहानुभूति हासिल करने के लिए कंपनी ने चार्टर अधिनियम द्वारा जो व्यवस्था लागू की थी, वह भारतीय सभ्यता के तब तक के इतिहास में सबसे मौलिक एवं क्रांतिकारी थी. उसके दो प्रावधान शूद्रों तथा अतिशूद्रों के लिए विशेष महत्त्वपूर्ण थे. उनमें पहला था—सभी के लिए समान कानून, जिसने स्मृतियों की ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था. दूसरा था—सभी वर्गों के लिए समान शिक्षा. उसके लिए भारत से होने वाली आय में से न्यूनतम एक लाख रुपये आधुनिक शिक्षा पर खर्च करना. शूद्रों-अतिशूद्रों ने उनका जोरदार स्वागत किया था. उनके लिए वह परीकथाओं में दिखने वाले चमत्कार जैसा था. चेटरसन ने उसके बारे में लिखा है—‘महत्त्वपूर्ण यह नहीं है कि परीकथाओं में राक्षस होते हैं. महत्त्वपूर्ण यह जान लेना है कि राक्षस को पराजित किया जा सकता है.’
पेशवाओं की पराजय से उनका आत्मविश्वास बढ़ा था. लगने लगा था कि ब्राह्मणवाद अपराजेय नहीं है. उसे पराजित किया जा सकता है. आने वाला समय तो अवसरों के लाभ उठाने का था. समान शिक्षा और एक जैसा कानून भारतीय सभ्यता के ज्ञात इतिहास में अद्वितीय थे. युगांतरकारी बदलाव की नींव रखने वाले. अंग्रेजों से पहले इस देश में बड़े-बड़े सम्राट हुए. किसी ने भव्य मंदिर बनवाए, किसी ने किले. नाम चलाने के लिए किसी-किसी ने कुएं, बावड़ियां भी बनवाईं. यहां तक कि धर्मशाला और गौशाला के नाम पर भी खर्च किया जाता था. लेकिन शिक्षा की जरूरत किसी ने भी नहीं समझी. नालंदा और तक्षशिला जैसे विद्यालयों के बारे में पढ़ना-सुनना किसी को भी रोमांचित कर सकता है. लेकिन वे उस कालखंड की निर्मितियां हैं, जब ब्राह्मण धर्म सबसे कमजोर था. ब्राह्मण वर्चस्व के दौर में शिक्षा आश्रम-भरोसे बनी रही. आश्रमों में केवल उच्च वर्ग के विद्यार्थी प्रवेश पा सकते थे. क्षत्रियों और वैश्यों को भी उतना पढ़ाया जाता था जितना उनके काम के लिए आवश्यक हो. शूद्रातिशूद्रों के लिए शिक्षा पर पूरा प्रतिबंध था. अगर वे पढ़ना चाहें तो उसके लिए दंड का घोषित विधान था. एकलव्य, कर्ण, शंबूक के किस्से आज भले ही ब्राह्मणवाद की आलोचना के काम आते हों, उन दिनों इनका उपयोग उसके महिमामंडन के लिए किया जाता था. अशिक्षित लोग मनमानी व्याख्याओं पर विश्वास भी कर लेते थे.
फुले कदम-कदम पर शिक्षा की जरूरत पर बल देते हैं. बल्कि ऐसा कोई अवसर ही नहीं है जब शूद्र-अतिशूद्रों की अशिक्षा उनकी चिंता का विषय न रही हो. शूद्रों की अशिक्षा के लिए ब्राह्मण को ही जिम्मेदार माना है—
‘ऐसे दुष्ट लोगों को अध्यापक बनाते
बच्चे वे गैरों(सवर्णों) के ही पढ़ाते
स्वजाति के बच्चे(को) गलती करने पर बार-बार समझाते
शिक्षा यत्नपूर्वक देते
परजाति के बच्चे गलती करते, थप्पड़-मुक्का मारते
जोर से कान ऐंठते
शूद्र बालक के मन को घायल करके भगा देते.’(पांवड़ा, शिक्षा विभाग के ब्राह्मण अध्यापक)
नए कानून यथास्थितिवादियों की ओर से उसका भी विरोध भी हुआ. आरोप लगाया गया कि आधुनिक शिक्षा के नाम पर सरकार निचली जातियों का ईसाईकरण करना चाहती है. मगर सरकार को समाज के बहुसंख्यक वर्ग का समर्थन हासिल था. अंग्रेजी शासन को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए उसे भारत के परंपरागत शासकों से अलग दिखना था. इसलिए सुधारवाद का सिलसिला आगे बढ़ता गया.
इन्हीं परिस्थितियों में फुले का जन्म हुआ. तारीख थी, 11 अप्रैल 1827. पिता फूलों के व्यवसायी थे. सुखी-समृद्ध परिवार था. मगर शूद्र के लिए आर्थिक समृद्धि सामाजिक मान-सम्मान का आधार नहीं बनती. फुले के पिता पारंपरिक विचारों के थे. अपने बुद्धि-विवेक से उन्होंने व्यापार को ऊंचाई तक पहुंचाया था. जो सहज प्राप्य था, वे उसी से खुश थे. किंतु बचपन से ही स्वाभिमानी फुले को उससे संतुष्टि न थी. फिर परिस्थितियां ऐसी बनती गईं कि उन्हें युग-निर्माण के ऐसे रास्तों पर उतरना पड़ा जहां पोंगापंथी ब्राह्मणों से सीधा टकराव था. एक घटना से फुले के सामने समाज में व्याप्त जाति-व्यवस्था का घिनौना रूप एकाएक सामने आ गया. पिता गोविंदराव की दुकान पर ब्राह्मण युवक मुंशीगिरी करता था. उसके साथ फुले की गहरी मित्रता थी. उसने फुले को अपने विवाह पर आमंत्रित किया. दूल्हे का मित्र होने के नाते विवाह के दौरान फुले हर आयोजन में उसके साथ थे. एक आयोजन में केवल ब्राह्मण हिस्सा ले सकते थे. यह बात न तो फुले को मालूम थी, न उनके मित्र ने बताया था. फुले सहज भाव से अपने मित्र का साथ दे रहे थे. इस बीच कोई देखते ही चिल्लाया—‘अरे! वह तो शूद्र है. उसे यहां किसने आने दिया?’ इसी के साथ चीख-पुकार मच गई. समाज का क्रूर जातिवादी चेहरा एकाएक सामने आ गया. किशोर ज्योतिबा को अपमानित होकर लौटना पड़ा. उस दिन उन्हें पता चला कि मनुष्य अपने बुद्धि-विवेक और परिश्रम से आर्थिक दैन्य को मिटा सकता है. लेकिन जाति का कलंक एक बार लग जाए तो उससे मुक्ति पाना असंभव है. जातिभेद का सामना डॉ. आंबेडकर को भी करना पड़ा था. उनके पिता सेना में सूबेदार थे. अछूत होने के कारण बालक आंबेडकर के साथ स्कूल में भेदभाव किया जाता था. यहां तक कि जब वे विदेश से खूब पढ़-लिखकर वापस लौटे तब भी मुंबई में उन्हें कोई कमरा देने वाला न था. एक पारसी महिला ने उन्हें कमरा दिया था. लेकिन जब उसे उनकी जाति के बारे में पता चला तो उसने तत्काल घर खाली करने का हुक्म सुना दिया. कार्यालय में चपरासी उन्हें पानी लाने में संकोच करता था. इन प्रसंगों के बारे में दलित साहित्य का विद्यार्थी भली-भांति जानता है. महसूस करता है. क्योंकि वे स्वयं ऐसे ही उत्पीड़न को झेलकर बड़े हुए हैं. जातीय भेदभाव की वह न तो पहली घटना थी, न ही आखिरी. लेकिन स्वाभिमानी फुले को जो उससे चोट पहुंची वह बड़ी थी. पेशवाई शासन की क्रूरता के बारे में सुनते आए थे. अब वह नहीं था. कानून की निगाह में अब सभी बराबर थे. लेकिन लोगों की मानसिकता ज्यों की त्यों थी. आखिर क्यों? फुले ने न केवल इसे समझा, बल्कि उसके समाधान के लिए आगे बढ़कर पहल भी की.
इसके अतर्निहित कारण को समझना बहुत मुश्किल भी नहीं था. अंग्रेज इस देश के शासक बन चुके थे. शासन कैसे चलाया जाएगा, मागदर्षक सिद्धांत कौन-से होंगे—इसकी लिखित व्यवस्था थी. अशिक्षित शूद्रों के लिए उन्हें समझना भी कठिन था. इसलिए वे उनके किसी काम के न थे, जब तक उसे समझ न सकें. ब्राह्मण पढ़-लिख सकते थे, इसलिए जोड़-तोड़ द्वारा स्वार्थ-सिद्धि का कोई न कोई उपाय वे खोज ही लेते थे. न हो तो शास्त्रों का हवाला देकर अपना उल्लू सीधा करते रहते थे. फुले समझ चुके थे कि दलितों की दुर्दशा का कारण गरीबी न होकर अशिक्षा है. नए प्रावधानों का लाभ उठाते हुए उन्होंने स्कूल-कॉलेज खोले. मुश्किलें वहां भी थीं. स्कूल चलाने के लिए अध्यापकों की आवश्यकता थी. उस समय के अधिकांश अध्यापक ब्राह्मण थे. उनके लिए शूद्रों की शिक्षा-दीक्षा निषिद्ध और धर्म-विरुद्ध कर्म था. फुले द्वारा स्थापित स्कूलों में अध्यापन के लिए वे भला क्यों तैयार होते! कहते हैं, जहां चाह वहां राह. दृढ़ इच्छाशक्ति के आगे बाधाएं सिर झुकाए मौन समर्पण कर देती हैं. फुले ने अपनी पत्नी को तैयार किया. सावित्री बाई फुले की देखा-देखी दूसरी महिलाओं में भी उत्साह जगा. दबंगों के भय से फुले के परिजनों ने उन्हें घर से निष्कासित कर दिया था. उस मुश्किल घड़ी में फातिमा शेख और उसके पति उस्मान शेख सामने आए. उन्होंने फुले दंपति को रहने के लिए आश्रय दिया. फातिमा शेख ने घर-घर जाकर माता-पिताओं को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी लड़कियों को स्कूल भेजें. उसके लिए यथास्थितिवादियों का विरोध सहा. वैसे भी राष्ट्र निर्माण की राह आसान नहीं होती. समाज सुधार की दिशा में फुले द्वारा किए जा रहे कार्यों से यथास्थितिवादी बेहद नाराज थे. पेशवाई के पराभव से वे हताश अवश्य थे, लेकिन पीठ पीछे हमला करने, नए-नए षड्यंत्र रचने में उनका कोई सानी न था. ऐसे ही षड्यंत्रकारियों ने एक बार फुले पर जानलेवा हमले की योजना बनाई थी. फुले सावधान थे. उस समय तक महार और मांग फुले के साथ आ चुके थे. विरोधियों के सामने पीछे हटने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था.
धीरे-धीरे शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने लगी. मगर दूसरी समस्याएं सिर उठाए थीं. सती-प्रथा दबे-छिपे रूप में जारी थी. बिना दांपत्य संबंधों के जन्मी संतान की देखभाल का भी मसला था. लोकलाज से बचने के लिए स्त्रियां ऐसे बच्चों को जन्म लेते ही मार देती थीं. आड़े वक्त में परिजन मदद से हाथ खींच लेते थे. समस्या को देखते हुए फुले ने प्रसूतिग्रहों की स्थापना की. सामाजिक दृष्टि से अवैध कहे जाने बच्चों की देखभाल के लिए शिशु सदन खोले. उनमें किसी भी धर्म, जाति की महिलाएं जा सकती थीं. लोकलाज के भय से नवजात शिशु को अपने साथ न ले जाना चाहे तो शिशु-सदन उसकी देखभाल करता था. अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा देना भी क्रांतिकारी कदम था. सबसे बड़ी समस्या रूढ़ियों की थीं. समाज धर्म के नाम पर तंत्र-मंत्र और कर्मकांडों में फंसा हुआ था. पुजारी लोगों को तरह-तरह से भरमाकर, लूटने में लगा रहता था. फुले ने अपने समाज को जाग्रत करना शुरू किया. धार्मिक कर्मकांडों की निस्सारता पर खुलकर लिखा. सभाएं कीं. इश्तहार निकाले. इससे ब्राह्मण समाज उनसे नाराज रहने लगा. यहां तक कि जानलेवा हमला भी उनपर किया गया. उस समय तक महार और मांग युवकों का संगठन फुले के समर्थन में आ चुका था. इससे षड्यंत्रकारियों के मनसूबे धरे के धरे रह गए.
समाज सुधार के क्षेत्र में फुले द्वारा किए जा रहे अनथक उपायों से प्रभावित होकर उच्च जातियों के उदारमना लोग भी उनके साथ समाज सुधार के क्षेत्र में आए थे. उनमें से कुछ को फुले ने अपनी स्कूल समितियों का सदस्य बनने का अवसर दिया था. इसे इरादों की कमजोरी कहिए या सामाजिक बहिष्कार की धमकी का डर, सवर्ण सदस्य बीच में ही अपनी राह बदल लेते थे. अक्टूबर 1853 के अंतिम सप्ताह में मुंबई में एक सभा का आयोजन किया था. उद्देश्य था हिंदू समाज की विकृतियों को दूर करना और उसके लिए आवश्यक सुधारवादी कार्यक्रम लागू करना. उसमें प्रगतिशील ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया था. सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए पंडित गंगाधर आप्टे को चुना गया. जो उस समय सुधारवादियों में गिने जाते थे. आप्टे को ब्राह्मण समाज के विरोध का अनुमान था. इसलिए सभा में उपस्थित होने का आश्वासन देने के बावजूद वे नियत दिन गायब रहे. सम्मेलन की अध्यक्षता भवानी विश्वनाथ ने की. बैठक में परंपरावादी ब्राह्मणों ने सुधारवादी कार्यक्रमों का इतना जबरदस्त विरोध किया कि बैठक को बेनतीजा समाप्त करना पड़ा. यह अकेला उदाहरण नहीं है. ‘एनीहिलेशन ऑफ कास्ट’ में डॉ. आंबेडकर ने सवर्ण नेताओं की मानसिकता पर विस्तार से लिखा है. जाति-व्यवस्था के विरोध में फुले जहां सीधी बात कहते या संकेत-भर करते हैं, वहीं आंबेडकर अपनी मान्यताओं के समर्थन में अकाट्य तर्क जुटाते हैं. उन्हीं ग्रंथों से जिनके बल पर ब्राह्मण जनसाधारण को भरमाते आए थे. बावजूद इसके रचनात्मक कार्यों को देखा जाए तो फुले आंबेडकर के गुरु सिद्ध होते हैं.
सामाजिक न्याय के पक्ष में बढ़ते दबाव को देख कांग्रेस ने ‘सोशल कांफ्रेंस’ नामक संगठन का गठन किया था. वह संगठन केवल दिखावे के लिए था. सवर्ण नेता राजनीति में तो रुचि लेते थे, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की ओर से मुंह मोड़े रहते थे. इसलिए कांग्रेस के अधिवेशनों में जहां नेताओं की भीड़ उमड़ पड़ती थी, वहीं ‘सोशल कांफ्रेस’ के पंडाल खाली रह जाते थे—‘जनता की उदासीनता देख नेताओं ने ‘सामाजिक सम्मेलन’ का विरोध करना आरंभ कर दिया. ‘सामाजिक सम्मेलन’ के अधिवेशन कांग्रेस के पंडाल में हुआ करते थे. मगर तिलक के विरोध के पश्चात कांग्रेस ने अपना पंडाल देना बंद कर दिया. दोनों के बीच नफरत इस कदर बढ़ी कि ‘सोशल कांफ्रेस’ ने जब अपना अलग पंडाल लगाना चाहा तो दूसरे पक्ष के नेताओं ने उसे जलाने की धमकी दे डाली. धीरे-धीरे ‘सोशल कांफ्रेस’ कमजोर पड़कर समाप्त हो गई.’(इन्हीलेशन आफ कास्ट : डॉ. आंबेडकर). 1892 में हुए ‘सोशल कांफ्रेस’ के अंतिम सम्मेलन में अध्यक्ष पद से बोलते हुए डब्ल्यू. सी. बनर्जी ने जो कहा, उससे कांग्रेसी नेताओं की मानसिकता को समझने में मदद मिल सकती है. कांग्रेस की भविष्य की राजनीति की झलक भी उसमें है, जिसे गांधी सहित उस समय के सभी बड़े नेता अपने आचरण और भाषणों में दोहराते रहते थे. बनर्जी ने कहा था—‘मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो कहते हैं कि जब तक हम सामाजिक पद्धति में सुधार नहीं कर लेते, तब तक हम राजनीतिक सुधार के योग्य नहीं हो सकते. मुझे इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं दीखता. क्या हम राजनीतिक सुधार के योग्य इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारी विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता. और दूसरे देशों के सापेक्ष हमारी लड़कियां कम उम्र में ब्याह दी जाती हैं. या हमारी पत्नियां और पुत्रियां हमारे साथ मोटरगाड़ी में बैठकर हमारे मित्रों से मिलने नहीं जातीं? या इसलिए कि हम अपनी बेटियों को आक्सफोर्ड और कैंब्रिज नहीं भेजते.’(एनीहिलेशन आफ कास्ट : डॉ. आंबेडकर).
वह परिवर्तन विरोधी वक्तव्य था, जो तत्कालीन कांग्रेसी नेताओं की मानसिकता को दर्शाता है. प्रकारांतर में वह सामाजिक न्याय की मांग को दबाए रखने का प्रयास था. अंग्रेजों द्वारा सामाजिक सुधार के लिए उठाए गए कदमों से भारतीय समाज का सवर्ण तबका खासा आहत था. उसके लिए देश की स्वयंप्रभुता इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं थी, जितनी सामाजिक यथास्थिति बनाए रखने की चाहत. इस संबंध में हमें 1942 में गांधी द्वारा ‘अंग्रेजो भारत छोड़ो’ आंदोलन के समय दिए गए ऐतिहासिक भाषण को याद करना चाहिए. उस समय तक कांग्रेस यह मान चुकी थी कि अंग्रेज भारत छोड़ने वाले हैं. सुरक्षित खेल खेलने के अभ्यस्त गांधी ने अपने ‘करेंगे या मरेंगे’ भाषण में अंग्रेजों से भारत को जैसा है उसी हालत में छोड़कर चले जाने का आह्वान किया था. ताकि शूद्रों और अतिशूद्रों की समाज-सुधार की मांग को, जिसे आरंभ से ही अंग्रेजों की सहानुभूति प्राप्त थी, किसी न किसी बहाने हमेशा-हमेशा के लिए टाला जा सके. जबकि फुले, आंबेडकर, पेरियार जैसे नेता आरंभ से ही जानते थे कि एक न एक दिन अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा. इसलिए जब तक वे देश में हैं, तब तक सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे अनुकूल समय है. दलितों और शूद्रों को उसका लाभ उठाना चाहिए. उस समय तक भारत आधुनिकीकरण की ओर बढ़ चुका था. जनता सांप्रदायिक द्वेष को बिसराकर राष्ट्रीय हितों के लिए एक हो चुकी थी. ‘तृतीय रत्न’ नाटक का सूत्रधार फुले की इन्हीं भावनाओं को अभिव्यक्त करता है—
‘ब्राह्मणों ने शूद्र-अतिशूद्रों पर जो शिक्षा बंदी लगाई थी, उसको समाप्त करके, उनको शिक्षा का मौका प्रदान करके होशियार बनाने के लिए भगवान ने इस देश में अंग्रेजों को भेजा है. शूद्र-अतिशूद्र पढ़-लिखकर होशियार होने पर वे लोग अंग्रेजों का अहसान नहीं भूलेंगे. फिर वे लोग पेशबाई से भी सौ गुना ज्यादा अंग्रेजों को पसंद करेंगे. आगे यदि मुगलों की भांति अंग्रेज लोग भी इस देश की प्रजा का उत्पीड़न करेंगे तो शिक्षा प्राप्त बुद्धिमान शूद्र-अतिशूद्र पहले जमाने में हुए जवांमर्द शिवाजी की भांति अपने शूद्र-अतिशूद्र राज्य की स्थापना करेंगे और अमेरिकी लोगों की तरह अपनी सत्ता खुद चलाएंगे. लेकिन ब्राह्मण-पंडों की दुष्ट और भ्रष्ट पेशवाई को आगे कभी आने नहीं देंगे. यह बात जोशी-पंडों को भली-भांति समझ लेनी चाहिए.’[6]
नई शिक्षा ने अनेक सुधारवादी आंदोलनों को जन्म दिया था. फुले को धर्म से गुरेज न था. यहां तक कि कर्मकांड में भी हिस्सा ले सकते थे. बशर्ते उसमें पुरोहित की भूमिका कोई गैर-ब्राह्मण निभा रहा हो. सत्यशोधक की नियमावलि में इस बात पर जोर दिया गया था कि शूद्र-अतिशूद्र रूढ़ियों और कर्मकांडों का बहिष्कार करें. जिन कर्मकांडों को वे परंपरासम्मत और आवश्यक मानते हैं, उनमें ब्राह्मण पुरोहित की अनिवार्यता न हो. धर्म के नाम पर आंबेडकर की भी यही नीति थी. फुले को उम्मीद थी कि नई ज्ञान-चेतना से सराबोर हो शूद्र-अतिशूद्र पुरोहितों की चालबाजियों को समझेंगे और धर्म को किनारे कर देंगे. इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म की आलोचना तो की लेकिन उससे बाहर आने का आह्वान नहीं किया. बल्कि उस समय के सभी बड़े हिंदू नेताओं जिनमें तिलक भी थे, के साथ मिलकर काम करते रहे. आंबेडकर मान चुके थे कि हिंदू धर्म का बदलना नामुमकिन है. क्योंकि जैसे-जैसे स्वतंत्रता निकट आ रही थी, सांप्रदायिक शक्तियां निरंतर उग्र हो रही थीं. धार्मिक कूपमंडूकता में भी वृद्धि हो रही थी. फिर भी हिंदू धर्म में सुधार के लिए उन्होंने लंबी प्रतीक्षा की थी. पूरी तरह निराश होने के बाद ही बौद्ध धर्म स्वीकार किया था. उस समय तक राजा राममोहन राय और केशवचंद सेन के आंदोलन को 130 वर्ष गुजर चुके थे. इसके बावजूद सवर्ण नेताओं की मानसिकता में बहुत अधिक बदलाव नहीं आया था. उनका चिंतन अतीतोन्मुखी था. भारत के प्राचीन गौरव के नाम पर वे उन दिनों की बार-बार याद दिलाते थे, जो उनके हिसाब से ब्राह्मणवाद के चरमोत्कर्ष के दिन थे. ताकि उनके माध्यम से निरंतर कमजोर पड़ती जा रही वर्ण-व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया जा सके. जबकि फुले और आंबेडकर के प्रयासों से शूद्रों एवं अतिशूद्रों के बड़े वर्ग में जागरूकता आ चुकी थी. डॉ. आंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार करके एक तरह से हिंदू धर्म का ही भला किया था. उस समय तक धर्मांतरण के माध्यम से समाजार्थिक स्वतंत्रता की चाहत रखने वालों के लिए इस्लाम और ईसाई धर्म सबसे लोकप्रिय हुआ करते थे. डॉ. आंबेडकर के धर्मांतरण के पश्चात इस्लाम और ईसाई धर्म की ओर अंतरण लगभग रुक-सा गया. हिंदू धर्म से उत्पीड़ित-हताश लोग बौद्ध धर्म को अपनाने लगे. फलस्वरूप भारतीय बौद्ध धर्म जो मूल का था, चलन में आ गया.
फुले का जिक्र हो तथा उनकी पुस्तकों ‘गुलामगिरी’ तथा ‘किसान का कोड़ा’ उल्लेख से वंचित रह जाए—यह नामुमकिन है. यूं तो उनकी सभी पुस्तकें बेमिसाल हैं. वे उनके चिंतन और रचनात्मक कार्यों की एकता को दर्शाती हैं. इनमें वे अपने विचारों को एकीकृत रूप में प्रस्तुत करते हैं. लेकिन ये दोनों पुस्तकें उनके चिंतन और कर्म का प्रतिनिधि संग्रह कही जा सकती हैं. पांच छोटे-छोटे अध्यायों में फैली ‘किसान का कोड़ा’ में उन्होंने व्यापारियों द्वारा किसान और शिल्पकार वर्ग के बहुविध शोषण का खुलासा किया है. उनमें धर्म और संस्कृति के नाम पर ब्राह्मणों द्वारा शोषण तो शामिल है ही, मंडी में बिचैलियों द्वारा किसानों की ठगी पर भी उनकी नजर गई है. इस पुस्तक में फुले ने अंग्रेजी राज्य की खुलकर प्रशंसा की है. उसे पेशवाई शासन से श्रेेष्ठ बताया है. इसके साथ-साथ ही उन अंग्रेज अधिकारियों की आलोचना भी की है जो अपनी काहिली या ब्राह्मणों के प्रभाव में आकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़े रहते हैं. योरोप की औद्योगिक क्रांति की प्रशंसा करते हुए उन्होंने अंग्रेजों की यह कहकर आलोचना की है कि वे भारतीय प्रजा से धन ऐंठकर अपने मुल्क पहुंचाने में लगे रहते हैं. इस विषय पर दादा भाई नौरोजी ने भी लिखा है. उनका प्रसिद्ध भाषण ‘पावर्टी इन इंडिया’ 1876 का है, जबकि ‘किसान का कोड़ा’ 1882 में लिखी गई. फुले पर नौरोजी का कितना प्रभाव था, यह बता पाना तो कठिन है, लेकिन इससे इतना साफ हो जाता है कि उस समय तक अंग्रेजों की व्यापार नीति की आलोचना होने लगी थी. ‘किसान का कोड़ा’ में फुले उसे अपनी शैली में प्रस्तुत करते हैं. नौरोजी की पुस्तक जहां अर्थशास्त्रीय महत्त्व रखती है, वहीं फुले अंग्रेजों द्वारा देश के आर्थिक शोषण के साथ-साथ वर्गीय शोषण को भी उठाते हैं. इसलिए ‘किसान का कोड़ा’ का अर्थशास्त्र के साथ-साथ समाज-वैज्ञानिक महत्त्व भी है. पुस्तक से फुले की व्यापक दृष्टि का भी पता चलता है. खेती के विकास के लिए वे बांध बनाने, नए बीज अपनाने, बिचौलिए दुकानदारों पर पाबंदी लगाने, यहां तक कि किसानों के प्रशिक्षण की मांग भी सरकार से करते हैं. वे बौद्ध धर्म तथा उसके अनुयायियों की प्रशंसा करते हैं.
व्यक्तिमात्र की स्वतंत्रता की मांग करते हुए मार्टिन लूथर किंग ने कहा था—‘मैं मानता हूं कि सभी मनुष्य एक समान हैं. मेरा एकमात्र सपना है कि मेरे छोटे-छोटे बच्चे एक दिन ऐसे राष्ट्र के नागरिक होंगे जहां उनकी पहचान चमड़ी के रंग के बजाय उनके चारित्रिक गुणों के आधार पर तय की जाएगी.’
कुछ ऐसा ही सपना फुले का भी था. ‘गुलामगिरी’ और ‘किसान का कोड़ा’ दोनों में उन्होंने गणतंत्र की प्रशंसा की है. जूलिस सीजर की वे यह कहकर आलोचना करते हैं कि उसने अपने देश में गणतंत्र को कुचलकर सत्ता हासिल की थी. थाॅमस पेन का प्रभाव भी उनपर था. आगे चलकर आंबेडकर ने भी हिंदू प्रतीकों और मिथों की आलोचना की. काफी सोचने-समझने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया. संविधान के माध्यम से वे भारत में गणतंत्र के प्रस्तोता बने. ‘किसान का कोड़ा’ में फुले ने बौद्ध धर्म तथा गणतंत्र की जैसी प्रशंसा की है, उससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि अपने-अपने समय के इन दोनों महामानवों के बीच विचार और कर्म की दृष्टि से कितना ज्यादा साम्य था.
‘किसान का कोड़ा’ को पढ़ते हुए यह बात भी सामने आती है कि शूद्रों-अतिशूद्रों की मुख्य समस्या गरीबी नहीं है. असली समस्या गरीबी के कारण को न समझ पाने की है. समाज के प्रमुख उत्पादक शिल्पकार और किसान हैं. लेकिन अपनी आय को अपनी मर्जी से खर्च करने का सत्साहस उनमें नहीं है. उनकी आय का बड़ा हिस्सा धार्मिक-सामाजिक कर्मकांडों पर खर्च होता है. आड़े समय पर किसानों को कर्ज लेना पड़ता है. फसल के समय महाजन और बिचैलिए उनकी फसल का बड़ा हिस्सा हड़प लेते हैं. जो बचता है, उसे भी अपनी मर्जी से, अपने विकास के लिए खर्च करना, उनके लिए संभव नहीं होता. शादी-विवाह, श्राद्ध, मुंडन, उपनयन जैसे अनेक संस्कार हैं, जो बेहद खर्चीले, मगर पूरी तरह अनुत्पादक हैं. वे लोगों की आर्थिक विपन्नता और बौद्धिक विकलांगता दोनों को बढ़ाते हैं. सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि व्यक्ति इनके चंगुल से निकल ही नहीं पाता. शिक्षा के अभाव में आम आदमी वही करता है, जो पुरोहित उन्हें बताता है. उसकी मानसिक संरचना पष्चगामी है. ‘तृतीय रतन’ नाटक में ब्राह्मण पुरोहित द्वारा अशिक्षित जनता के बहुआयामी शोषण को दर्शाया गया है. यह नाटक बताता है कि ब्राह्मण पुरोहित अशिक्षित जनता को कदम-कदम पर किस तरह भरमाते हैं. धर्म और अनीति का भय दिखाकर उनका धन लूटने में लगे रहते हैं. कोई ऐसा सामाजिक अनुष्ठान नहीं है जिसमें ब्राह्मण की मौजूदगी और उसके द्वारा दान-दक्षिणा के नाम पर गरीब जनता से धन न ऐंठा जाता हो. धर्म के नाम पर उन्हें इतना डराया जाता है कि कर्ज लेकर भी कर्मकांडों में लिप्त रहते हैं. इस उम्मीद से कि अंततः देवता उनपर कृपा करेगा. फिर उनके सारे दलिद्दर नष्ट हो जाएंगे. होता इसका उलटा है. दुख-दलिद्दर तो मिटना तो दूर, महाजन का कर्ज सिर पर चढ़ जाता है. उसे चुकाने के लिए वे जमींदार के घर बेगार करते रहते हैं. संक्षेप में ‘किसान का कोड़ा’ भारतीय किसान और मजदूर के जीवन का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है.
फुले की दूसरी महत्त्वपूर्ण पुस्तक का पूरा शीर्षक है—‘गुलामगिरी’ (ब्राह्मणधर्म की आड़ में होने वाली). छोटी-सी पुस्तिका को उन्होंने ‘संयुक्तराष्ट्र के सदाचारी जनों को जिन्होंने गुलामों को दासता से मुक्त करने के कार्य में उदारता, निष्पक्षता और परोपकार वृत्ति का प्रदर्शन किया था, के लिए सम्मानार्थ समर्पित’ किया गया है. भारत में इसे अपने विषय की इकलौती पुस्तक; जिसे आधार पुस्तक भी कहा जा सकता है. ‘सांस्कृतिक वर्चस्ववाद’ के विरुद्ध संघर्ष के इतिहास में इस पुस्तक का ठीक वही स्थान है, जो दुनिया-भर के मजदूर आंदोलनों के इतिहास में ‘कम्यूनिस्ट मेनीफेस्टो’ का है. धर्म के नाम पर फैलाए गए आडंबरों तथा निरर्थक कर्मकांडों का विरोध संत रविदास और कबीर ने भी किया था. उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए फुले ‘गुलामगिरी’ के माध्यम से उन मिथों पर सीधे प्रहार करते हैं, जो शताब्दियों से जनसमाज की बौद्धिक विकलांगता का कारण बने थे. जो छोटी-छोटी बात पर शूद्रों, अतिशूद्रों को ब्राह्मणों पर निर्भर बनाते थे. उनकी मदद से ब्राह्मण शिखर की दावेदारी करते हुए शेष तीनों वर्गों को अपना दासानुदास बनाए रखता था. वर्ण-व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण इस पृथ्वी के समस्त सुख-साधनों का एकमात्र स्वामी-संरक्षक है. क्षत्रिय का कर्तव्य उसकी रक्षा करना, वैश्य का धर्म कमा कर देना है. शूद्र-अतिशूद्रों के लिए मात्र ‘निष्काम सेवा’ निर्धारित है. पूजा-पाठ जैसे अनुत्पादक कार्यों के लिए मुंह-मांगी दक्षिणा लेना ब्राह्मण का एकाधिकार मान लिया जाता है. मजदूर अपने श्रम का मूल्यांकन स्वयं करना चाहे तो शास्त्र-विरुद्ध कहकर उसकी मांग को दबा दिया जाता है. क्षत्रिय और वैश्य ब्राह्मण के शीर्षत्व को स्वीकार करके संपत्ति के संरक्षक-संग्राहक बन सकते हैं. परंतु चौथे वर्ण को संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं है. इस वर्ग को जिसमें किसान, शिल्पकार, मजदूर आदि आते हैं, जिन्हें मार्क्स ने प्रमुख उत्पादक शक्ति माना है. बुद्धकालीन भारत में उनका यह स्थान और अपेक्षित मान-सम्मान सुरक्षित था. ब्राह्मण प्रभुत्व वाला तंत्र उन्हें न केवल वर्ण-विशेष के दायरे में कैद कर देता है, अपितु आजीविका के चयन के अधिकार के साथ-साथ उनसे श्रम और श्रमोत्पाद संबंधी समस्त अधिकार छीन लेता है. उत्पादक वर्ग विरोध न करे, उसके लिए जन्म-पुनर्जन्म, कर्मफल और पाप-पुण्य जैसी पश्चगामी व्यवस्थाएं हैं. ‘अवतारवाद’ की सैद्धांतिकी इन्हें पुष्ट करने के लिए ही गढ़ी गई है. ‘गुलामगिरी’ के माध्यम से फुले इसी पर प्रहार करते हैं.
‘गुलामगिरी’ संवाद की शैली में लिखी गई पुस्तक है. यह उन दिनों की प्रचलित शैली थी. यह जानते हुए कि अनपढ़ जनता प्रतीकों और मिथों से ही प्रेरणा लेती है, उन्हीं का हवाला देकर ब्राह्मणादि सवर्ण खुद को देव-सभ्यता का उत्तराधिकारी मानते आए हैं; तथा कुछ गिने-चुने मिथ शूद्रों-अतिशूद्रों की शारीरिक-मानसिक दासता का कारण हैं—फुले उनकी जड़ पर प्रहार करते हैं. आर्य बाहर से आए थे. यह उन दिनों स्थापित सत्य था. मैक्समूलर, विंसेंट स्मिथ, रिस डेविस, जॉन मार्शल जैसे विद्वानों का यही विचार था. इस दृष्टि से ब्राह्मणों को विदेशी मूल का बताना फुले की मौलिक स्थापना नहीं थी. मौलिक था, वाराह, कच्छप, नरसिंह जैसे कथित अवतारों के विवेचन से उस ऐतिहासिकता की खोज करना जिसके पीछे आर्य-अनार्य संघर्ष की अनेक कहानियां छिपी हैं. मिथों में उलझकर उनका वास्तविक इतिहास कहीं लुप्त चुका है. अनेकानेक मिथों पर टिकी प्राचीन भारतीय संस्कृति की आलोचना करते हुए फुले उस इतिहास की झलक दिखाते हैं, जिसकी कालावधि के बारे में ठोस जानकारी भले ही न हो, मगर वह सत्य के अपेक्षाकृत करीब है. यह असल में कांटे से कांटा निकालने की कोशिश है. जो सच हो न हो, मगर अपने सरोकारों के आधार पर सच के बहुत करीब दिखता है. देरिदा को ‘विखंडनवाद’ का आदि व्याख्याता माना जाता है. फुले उसका प्रयोग ‘गुलामगिरी’ में देरिदा से लगभग एक शताब्दी पहले करते हैं. उसी को अपना प्रस्थान-बिंदू बनाकर डॉ. आंबेडकर हिंदू धर्म की जटिल पहेलियों की विवेचना करते हैं. दोनों के निष्कर्ष आधुनिक दलित-बहुजन विमर्श की आधार सामग्री हैं. भारतीय संदर्भ में ‘गुलामगिरी’ ‘सांस्कृतिक विखंडनवाद’ की पहली पुस्तक है; तथा फुले ब्राह्मणों के ‘सांस्कृतिक आधिपत्य’ को चुनौती देने वाले पहले बहुजन नेता. दक्षिण भारत में उनकी प्रेरणा द्रविड़ आंदोलन के रूप में फलीभूत होती है. पेरियार उनके संघर्ष को नई ऊर्जा और वैचारिक चेतना के साथ आगे बढ़ाते हैं. ‘गुलामगिरी’ में फुले ने हिंदुओं की अवतारवादी धारणा का जोरदार खंडन किया है. पुस्तक का महत्त्व इससे भी आंका जा सकता है कि ब्राह्मणवाद के विरोध में जिन सांस्कृतिक प्रतीकों तत्वों का हवाला दिया जाता है, लगभग वे सभी इसमें मौजूद हैं. कुल मिलाकर बहुजन दृष्टि से फुले भारत के पहले और मौलिक इतिहासकार हैं. इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का मूल्य 12 आना था. निर्धन तथा शूद्रातिशूद्रों के लिए उसकी कीमत मात्र छह आना रखी गई थी. इसके पीछे भी फुले की दूरदृष्टि थी. उद्देश्य यही था कि जो गरीब तथा शूद्र-अतिशूद्र ‘गुलामगिरी’ को पढ़ना चाहते हैं, पैसे की कमी उसमें बाधा न बने.
फुले के समय तक सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी उजागर नहीं हुई थी. संस्कृत ग्रंथों से केवल यही तथ्य सामने आता है कि बाहर से आने वाली प्रजाति, जिसने स्वयं को ‘आर्य’ घोषित किया था, का स्थानीय प्रजातियों से जोरदार संघर्ष हुआ था. समुद्र और पहाड़ियों द्वारा सुरक्षित अनार्य अपेक्षाकृत सुख और शांतिपूर्ण जीवन जीने के अभ्यस्त थे. इसके प्रमाण सिंधू सभ्यता से प्राप्त हो चुके हैं. लाखों वर्ग किलोमीटर में फैली सिंधू सभ्यता के उत्खनन से पुरात्वविदों को भंडारगृह, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, मूर्तियां, मुद्राएं, अनाज, मापन यंत्र आदि प्राप्त हुए हैं, लेकिन हथियार के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिला है. उस सभ्यता का पराभव 1750 ईस्वी पूर्व के आसपास प्राकृतिक कारणों से हुआ था. आर्यों के भारत पहुंचने(1500 ईस्वी पूर्व) तक वह नष्टप्रायः अवस्था में थी. बचे-खुचे सिंधुवासी हतोत्साहित होकर जंगलों में बिखर चुके थे. असंगठित और शांतिप्रिय अनार्यों को पराजित करना आसान था. अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए आर्यों ने स्थानीय निवासियों के दिमाग को कब्जाना शुरू कर दिया था. उन्होंने काल्पनिक नायक इंद्र को केंद्र बनाकर मंत्र रचे. उसे उन पुरों का विनाशक घोषित किया, जो उनके आगमन से शताब्दियों पहले खंडहरों में बदलने लगे थे. सिंधू सभ्यता के आरंभिक अध्येता सुप्रसिद्ध पुरातत्वविद् जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक ‘मोहनजोदड़ो एंड इंड्स सिविलाइजेशन’(1931) में एक अध्याय सिंधुवासियों की धार्मिक मान्यताओं पर शामिल किया है. मार्शल का शोध उस सभ्यता को भारत की जनसंस्कृति के करीब रखता है, जो निश्चय ही ब्राह्मणेत्तर संस्कृति थी. ये तथ्य यदि फुले के सामने होते तो वे उनका उपयोग निश्चित रूप से वर्चस्वकारी ब्राह्मण संस्कृति के विखंडन हेतु करते. जातीय श्रेष्ठता का दंभ आर्यों से तीन हजार वर्ष बाद आने वाले अंग्रेजों में भी था, लेकिन उसके मूल में योरोपीय पुनर्जागरण की बेमिसाल उपलब्धियां थीं. जिसमें मानवीय गरिमा और मान-सम्मान पर जोर दिया गया था. मशीन-केंद्रित उत्पादन प्रणाली सामंतवाद के अत्याचारों से मुक्ति का भरोसा दिलाती थी. इसलिए शताब्दियों से आर्थिक-सामाजिक विषमता का दंश झेल रही जातियों ने उनका स्वागत किया था. फुले अंग्रेजी शासन की प्रशंसा करते हैं. वहीं, आर्थिक-सामाजिक शोषण के शिकार वर्गों की स्वतंत्रता के लिए पर्याप्त कदम न उठाने के कारण वे उसकी आलोचना भी करते हैं.
फुले की रचनाएं सीधे संवाद करती हैं. उनकी भाषा किसान-मजदूर की खरखरी भाषा है. मराठी में प्रशस्ति काव्य को पावड़ा कहा गया है. फुले ने कई पावड़े लिखे हैं. लेकिन वे निरे प्रशस्ति काव्य नहीं है. उनके सरोकार मानवीय हैं और सामाजिक न्याय की भावना पर खरे उतरते हैं. शिवाजी की गौरवगाथा को याद दिलाता एक पावड़ा है. एक अन्य पावड़े में वे निर्माण विभाग के अधिकारी की रिश्वत के बारे में बात करते हैं. ब्राह्मण अध्यापक अछूत विद्यार्थियों के साथ पक्षपात करते हैं. उन्हें पढ़ाने से बचते हैं. फुले इसकी पोल खोलते हुए शिक्षा अधिकारी से निवेदन करते हैं कि वह शिक्षा विभाग में शूद्र और अतिशूद्र विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इसी वर्ग के अध्यापकों की नियुक्ति करे. किसान की उपज का बड़ा हिस्सा मंडी में दलाल खा जाते हैं. इसलिए एक पावड़ा उसकी दुर्दशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी है. ‘गुलामगिरी’ में परिशिष्ट के रूप में ‘ब्राह्मण कर्मचारी इंजीनियरिंग विभाग में किस प्रकार धांधली मचाते हैं’—इस विषय पर एक पांवड़ा दिया गया है, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण कर्मचारियों की स्वार्थपरता और काहिली के साथ-साथ अंग्रेज अधिकारियों पर भी तंज कसा है—
‘ब्राह्मण बड़ी चतुराई करते. लिखने में कौशल दिखलाते. कुनबी को दिन-दहाड़े लूटते. हाजिरी-बही ले फैल(कार्यस्थल) पर जाते….फैल में जो हों शूद्र औरतें उनसे बरतन मंजवाते. बेगारी मजदूरों से फिर अपना बिस्तर हैं लगवाते. पागल से कुन्बी को पाकर उससे अपने पैर दबवाते. खूब मजे से खुर्राटे भरते. अपनी जात के बाम्हन को फैल पर काम को हैं ले जाते….किसान का लहू चूस-चूसकर मोटे-ताजे हैं बन जाते. जितना ये घी-शक्कर हैं उड़ाते, सब किसान के ऊपर.’
भाषा और अध्ययन की दृष्टि से डॉ. आंबेडकर फुले की अपेक्षा समृद्ध हैं. उनकी भाषा एक दार्शनिक और वैज्ञानिक की भाषा है. जो तर्क करती है; तथा उनके समर्थन में जरूरी प्रमाण भी देती है. फुले की भाषा की भांति उनके तर्क भी सीधे-सपाट हैं. डॉ. आंबेडकर का लेखन उनके विशद् अध्ययन का स्वतः प्रमाण है. ब्राह्मणवाद के विरुद्ध पिछड़े और दलित वर्गों में चेतना जगाने में फुले के लेखन का बड़ा योगदान है. उससे प्रेरणा लेकर दलित और पिछड़े समुदायों के सैकड़ों बुद्धिजीवी आगे आए. उन्होंने अनेकानेक आंदोलनों को जन्म दिया. सांस्कृतिक वर्चस्व से मुक्ति हेतु ग्राम्शी ने सर्वहारावर्ग से अपने बुद्धिजीवी पैदा करने का आवाह्न किया है. ऐसे चिंतक जिनकी मेधा स्वतंत्र हो, जो अभिजन बुद्धिजीवियों के मानसिक दास न हों. अपने विचार-कर्म से फुले, ग्राम्शी से आधी शती पहले ही इसे चरितार्थ करते नजर आते हैं. एक किसान की तरह वे भविष्य के दलित आंदोलन के लिए जमीन तैयार करते हैं.
फुले के समय भारतीयों, विशेषकर शूद्रों के लिए राजनीति में आने के अवसर कम थे. स्वयं फुले ने भी उस दिशा में कभी प्रयास नहीं किया. वे राजनीतिज्ञों यहां तक कि अंग्रेजों से भी दूरी बनाए रहे. निष्पक्ष बुद्धिजीवी की तरह जब आवश्यक समझा, तब अंग्रेजी शासन की प्रशंसा की और जहां कुछ आपत्तिजनक नजर आया, तत्काल आलोचना से भी बाज नहीं आए. राजनीति से प्रत्यक्ष संबंध न रखने के बावजूद शूद्रातिशूद्रों में संगठन और संघर्ष की प्रेरणा जगाने में फुले का योगदान अपने समकालीन किसी भी नेता से कहीं अधिक है. अच्छा शिष्य गुरु की शिक्षा को ज्यों का त्यों नहीं अपनाता, बल्कि उसको निरंतर परिवर्धित-परिमार्जित करता जाता है. जिस आंदोलन को फुले खड़ा करते हैं, डॉ. आंबेडकर उसे और अधिक मजबूती, साहस, ईमानदारी और संकल्प के साथ आगे बढ़ाते हैं. अंततः अपनी अप्रतिम मेधा, अनथक संघर्ष तथा प्रतिबद्धता के बल पर उसे एक अंजाम तक पहुंचाने में सफल सिद्ध होते हैं. डॉ. आंबेडकर राजनीति की महत्ता को समझते थे. उन्होंने दलितों का आवाह्न किया कि अपने अधिकारों के लिए राजनीति में खुलकर हिस्सा लें. फुले के समय तक अस्मितावादी राजनीति का वातावरण नहीं बना था. वक्त की नजर और समाज की जरूरतों को पहचानते हुए उन्होंने खुद को सामाजिक सुधार तक सीमित रखा था. पहले पंद्रह वर्ष वे मुख्यतः शिक्षा-सुधार को समर्पित रहे. शूद्रातिशूद्र विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले. लेकिन राजनीति से दूरी बनाए रखी. डॉ. आंबेडकर राजनीति की ताकत तथा जरूरत को समझते थे. उनकी सक्रियता समाज और राजनीति, दोनों क्षेत्रों बराबर बनी रही.
अच्छा नागरिक के लिए अच्छे समाज का होना आवश्यक है; और एक अच्छा समाज ही अच्छे राज्य का गठन कर सकता है. इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य का विवेक स्वतंत्र हो. प्रत्येक मनुष्य को अपने निर्णय खुद लेने की स्वतंत्रता हो. उसके लिए शिक्षा भी चाहिए और सहयोगपूर्ण वातावरण भी. इसी सपने के साथ फुले अपने आंदोलन की शुरुआत करते हैं. जिसे डॉ. आंबेडकर उसी निष्ठा एवं समर्पण के साथ आगे बढ़ाते हैं. आधुनिक भारत के निर्माण में दोनों की भूमिका अद्वितीय है. प्रतिक्रियावाद के इस दौर में जो लोग इन दोनों के योगदान को नकारने की कोशिश में हैं, उन्हें फ्रैड्रिक डगलस की यह चेतावनी याद रखनी चाहिए—‘जहां न्याय की अवमानना होती है, जहां जहालत और गरीबी है, जहां कोई भी समुदाय यह महसूस करे कि समाज सिवाय उसके दमन, लूट तथा अवमानना के संगठित षड्यंत्र के सिवाय कुछ नहीं है—वहां न तो मनुष्य सुरक्षित रह सकते हैं, न ही संपत्ति.’
(कॉपी संपादन : एफपी डेस्क)
[1] Dhanajay Keer in Mahatama Jyotiba Phule
[2] एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, संतराम बीए द्वारा अनूदित, पृष्ठ 8.
[3] Henry Verner Hampton in Biographical Studies of Education in India.
[4] Dhanajay Keer in Mahatama Jyotiba Phule
[5] Katherine Mayo, Mother India(1937), page 64.
[6] तृतीय रत्न, नाटक, फुले, ज्योतिराव फुले रचनावली, अनुवाद डॉ. एल. जी. मेश्राम ‘विमलकीर्ति’ पेज—47
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें
मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया
दलित पैंथर्स : एन ऑथरेटिव हिस्ट्री : लेखक : जेवी पवार