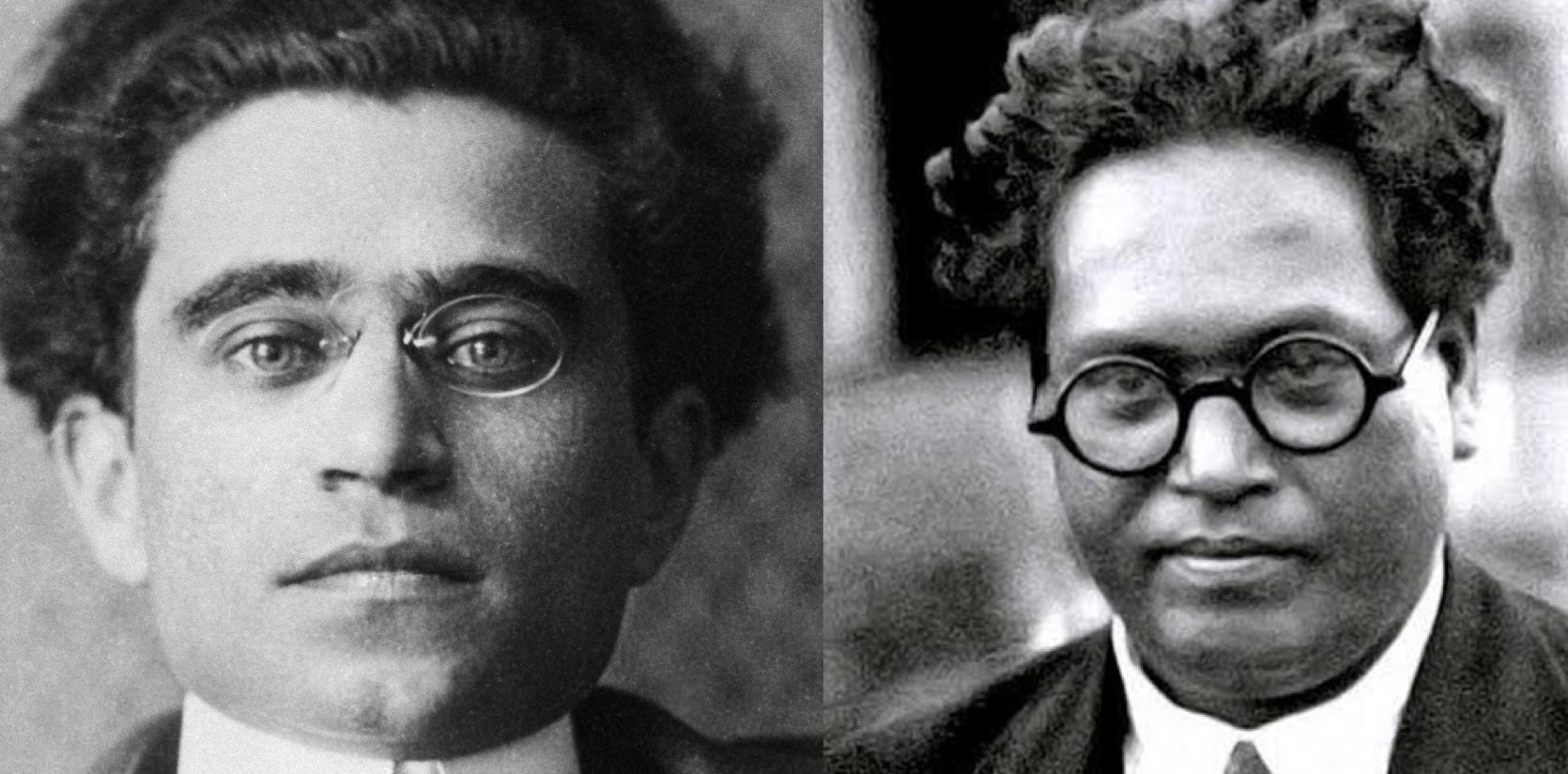जन-विकल्प
सिंधु सभ्यता का आखिरकार पतन हो गया। जिस सभ्यता के विकसित होने में सैंकड़ों वर्ष लगे, जो कम-से-कम छह सौ वर्षों तक अपने उत्कर्ष पर रही, वह धीरे-धीरे पझाने[1] लगी और फिर तो ऐसा समय भी आया जब उसके भौतिक निशान भी ओझल हो गए। इतिहासकारों ने 2600 ईस्वीपूर्व से लेकर 1900 ईस्वीपूर्व तक इसका उत्कर्ष-काल माना है। सभ्यताओं को अपना वितान समेटने में भी समय लगता है। यह माना गया है कि 1750 या अधिक से अधिक 1500 ईस्वीपूर्व इसकी आखिरी सीमा है। उसके बाद इस सभ्यता के निशान नहीं दृष्टिगोचर होते। यह एक ट्रेजेडी थी या इतिहास का सख्त फैसला, इसे लेकर विमर्श होते रहे हैं और होते रहेंगे। लेकिन यह अजीब बात लगती है कि ग्रामीण सभ्यता विकसित होकर नगर सभ्यता बनती है और पुनः ग्रामीण सभ्यता में लौट आती है। उन्नीसवीं सदी के जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहते थे, मानव विकसित होकर महामानव (सुपरमैन) नहीं बना, तो नीचे आकर फिर वानर जैसा जीव हो जायेगा। सिंधु-सभ्यता के मामले में बहुत कुछ ऐसा ही हुआ।
जहां उत्थान की कहानी होगी, वहां पतन की भी कहानी होगी। लेकिन सैंकड़ों या हजारों साल पुरानी किसी सभ्यता की कहानी हम या तो लिखित साक्ष्य के आधार पर कह सकते हैं, या फिर पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। जैसा कि बतलाया जा चुका है हड़प्पावासियों की लिपि तो थी, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए लिखे आधार पर कुछ कहना मुश्किल है। वह लिपि अब तक एक पहेली बनी हुई है और जाने कब सुलझेगी। लेकिन इस सभ्यता से जुड़े दर्जनों स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्य चुपचाप एक कहानी कह जाते हैं। हमने देखा है कि सभ्यता का विस्तार हड़प्पा से नीचे दक्षिण-पूरब की ओर होता है, तो ज्यों-ज्यों हम बढ़ते हैं, पक्की ईंटों के इस्तेमाल का धीरे-धीरे अभाव होने लगता है। दैमाबाद, जो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी के किनारे अवस्थित इस सभ्यता का दक्षिण में आखिरी ठिकाना है, में प्राप्त घर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से सर्वथा भिन्न हैं। वहां की दीवारें मिटटी और गारा मिला कर बनाई हुई पायी गयी हैं। इसमें वनस्पतियों का भी इस्तेमाल होता था। इसी तरह यहां के मृदभांडों की डिजायन भी कुछ भिन्न, या कहें हड़प्पा के मुकाबले कमतर किस्म की हैं। पूर्व सभ्यता के ह्रास का पता इन सब से चलता है। पंजाब के रोपर, हरियाणा के बनावली और उत्तरप्रदेश के आलमगीरपुर में प्राप्त पुरातात्विक अवशेष भी नगरीय तत्वों की अपेक्षा ग्रामीण तत्वों की प्रचुरता की गवाही देते हैं। कुल मिला कर यह बात साफ़ होती है कि एक या कुछ नगर भले ही बाढ़, महामारी या किसी बाह्य आक्रमण से अचानक खत्म हो जाएं, पूरी सभ्यता धीरे-धीरे ढलान की तरह उतरी और फिर ख़त्म हो गयी। हम इस विषय-बिंदु पर भी बात करेंगे कि क्या इस सभ्यता का कोई प्रभाव बाद के समाजों पर किसी रूप में दीखता है?

लेकिन सब से पहले हम उस बहुचर्चित और बहुप्रचारित कहानी की ओर देखें, जो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास का ककहरा बन गया है। कहानी यह है कि भारत के बाहर से आये आर्यों ने आक्रमण कर के हड़प्पा-वासियों और उनकी सभ्यता-संस्कृति को को तहस-नहस कर दिया। बाहर की व्याख्या अनेक लोगों ने अनेक तरह से की है। कोई इन्हें मेसोपोटामिया से आया हुआ बतलाता है, तो कोई उत्तरी ध्रुव प्रदेश से। रूस से लेकर अफगान तक की चर्चा होती है। लेकिन इस बात पर लम्बे समय तक सहमति बनी रही कि आर्यों और सिन्धुवासियों के बीच युद्ध हुआ और इसमें सिंधु वासी पराजित और तबाह हो गए। उनके नगर और दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए आदि-आदि। इस कहानी के प्रस्तावक पुरातत्वविद रामप्रसाद चंद थे, जो सर जॉन मार्शल की टीम में अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने ऋग्वेद में वर्णित पुर को हड़प्पा के नगर के रूप में देखा और वहीं उल्लिखित हरियूपिया नामक जगह को हड़प्पा बना दिया। चंद का कहना था कि आर्यों ने इसलिए आक्रमण किया कि हड़प्पा संस्कृति के पणि – जो वैश्य-व्यापारी थे, उनके वैदिक आचरणों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने इंद्र को पुरों अर्थात नगरों को विनष्ट करने वाले पुरंदर के रूप में देखा, जो ऋग्वेद का मुख्य देवता या नायक है। इस तरह युद्ध की एक कहानी गढ़ दी गयी। लेकिन इस विषय पर काम करने वाले एक भारतीय इतिहासकार नयनजोत लाहिरी के अनुसार बाद में रामप्रसाद चंद ने अपने दावे को वापस ले लिया, क्योंकि उनके पास ऋग्वेद के भाषिक आख्यान के अलावा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं था।
यह भी पढ़ें – सिंधु सभ्यता का विस्तार : हड़प्पा से आलमगीरपुर तक
लाहिरी के शोध के अनुसार आर्य आक्रमण वाले इस सिद्धांत को 1947 ई. में एक ब्रिटिश पुरातत्वविद रोबर्ट एरिक मोर्टिमर व्हीलर (1890-1976) ने एक बार फिर नए सिरे से उठाया और एन्सिएंट इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में मोहनजोदड़ो में प्राप्त 37 कंकालों को अपना पुरातात्विक साक्ष्य बनाया। ये साक्ष्य मोहनजोदड़ो में प्राप्त कब्रगाह एच में पाए गए हैं। व्हीलर का कहना था कि एक जगह इतने कंकाल आक्रमण में मारे गए लोगों के हैं। इन सब का आर्यों द्वारा कत्लेआम हुआ। हालांकि बाद में रामप्रसाद चंद की तरह व्हीलर भी विचलित हुए और बाढ़ आदि कारकों को नज़रअंदाज न करने की बात भी की; लेकिन आर्य आक्रमण को सभ्यता के विनष्ट होने के मूल कारण पर वह जोर देते रहे। रामप्रसाद चंद और व्हीलर के मत इतिहासकारों पर तब तक प्रभावशाली बने रहे, जब तक 1953 में पांडुरंग वामन काणे (1880-1972) ने इसका जोरदार खंडन नहीं किया। पी.वी. काणे, जो ‘धर्मशास्त्र का इतिहास’ के प्रसिद्ध लेखक और 1963 में ‘भारत-रत्न’ प्राप्त विद्वान थे, ने 1953 के इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में अध्यक्ष पद से आर्य आक्रमण वाली सैद्धांतिकी को चुनौती दी। काणे वेदों और अन्य हिन्दू धर्मशास्त्रों के आधिकारिक विद्वान थे और उनका कहना था कि ऋग्वेद का स्वरुप और चरित्र धार्मिक है, और उसके एक रचना-काल पर भी सर्वानुमति नहीं है, ऐसे में बिना किसी पुरातात्विक साक्ष्य के आप इतिहास सम्बन्धी राय नहीं स्थापित कर सकते। काणे की मान्यत्ता को 1964 में जार्ज डेल्स और 1997 में ब्रज बासी लाल ( बी.बी. लाल) ने रेखांकित किया।

यह ध्यान देने योग्य है कि आर्य आक्रमण वाला सिद्धांत उस काल में गढ़ा गया जो पूरी दुनिया में लड़ाई-झगड़ों के लिए जाना जाता है। यह दूसरे विश्वयुद्ध के इर्द-गिर्द का समय है और ऐसे समय में मनुष्य का नजरिया अमूमन हर चीज को लड़ाई-झगडे की भावना से देखने का हो जाता है। लेकिन आज हम इस बिंदु पर अधिक तटस्थता से विचार कर कर सकते हैं। आर्य आक्रमण वाले विचार को स्वीकार करने में किसी को क्या बाधा हो सकती है, यदि इसमें कुछ सच्चाई हो। लेकिन प्रथम दृष्टया यह अजीब बात लगती है कि एक ऐसे सभ्य-विकसित समाज पर जो तकनीकी तौर भी काफी समृद्ध हो, जिन्हे समुद्री रास्तों का ज्ञान और यात्राओं के अनुभव हों, जो इतनी बड़ी सभ्यता का वितान गढ़ सकते हों, जो सुरक्षित घरों और नगरों में निवास करते हों; अचानक एक खानाबदोश चरित्र की टोली से इतनी बुरी तरह पराजित कर दिए जाते हों। हड़प्पावासी जब अपने नगरों को दुर्गनुमा चारदीवारियों से घेर रहे थे तभी उन्हें सुरक्षा का संज्ञान था। संभव है, उन पर हमले हुए हों और उनसे बचने के लिए उन लोगों ने दुर्ग की घेराबंदी की हुई थी। इस बात के भी कोई प्रमाण नहीं हैं कि आर्यों के पास कोई सेना थी। इसलिए कि अमूमन सेना के पीछे एक व्यवस्थित राजसत्ता का होना आवश्यक जान पड़ता है। यदि राजसत्ता न हो, तब भी कोई ऐसी व्यवस्था तो होनी ही चाहिए जो इस संगठन का भरण-पोषण कर सके, जैसे आधुनिक ज़माने में ईस्ट इंडिया कम्पनी सेना रखती थी। इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं कि आर्यों के पास कोई राजसत्ता उन इलाकों में थी, जहां से इनके आने की बातें कही जाती हैं। ऐसे में उनका आक्रमण घुसपैठिया-उचक्का की तरह ही संभव होगा। ऐसे छिट-पुट आक्रमणों से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे आक्रमण दो तरह की स्थितियां विकसित करेंगे। पहला तो यह कि सिंधु निवासियों में प्रतिरक्षा की भावना और तकनीक विकसित करेंगे और आक्रमण तीव्र या जोरदार होने पर उन्हें पीछे हटने के लिए विवश करेंगे। तब आर्यों की तकनीक इतनी विकसित तो नहीं ही होगी कि हड़प्पावासियों को एक ही बार जल, थल दोनों मार्गों से काट दिया गया और वे एकबारगी ख़त्म कर दिए गए। ऋग्वेद के उल्लेखों से ही यह जानकारी मिलती है कि इंद्र प्रायः हड्डियों के हथियारों से संघर्ष करता था और वैदिक उल्लेख ही उन्हें उनके विरोधी असुरों के समक्ष निरीह बतलाते थे। दधीचि के अस्थिदान से लेकर कई प्रसंग उनकी दयनीयता का बोध कराते हैं। लेकिन यह सब भी सिंधु सभ्यता के पतन के बहुत बाद की कहानी है। ईसा-पूर्व 1750 तक सिंधु सभ्यता का पतन हो चुका था। मैक्समूलर के अनुसार ऋग्वेद का समय 1500 ईस्वीपूर्व है। अतएव इंद्र-पुरन्दर की कथा सिंधु-सभ्यता के बाद के किसी संघर्ष की ओर इंगित करता है। इन्हे सिंधु सभ्यता से नहीं जोड़ा जा सकता।

सिंधु सभ्यता का पतन भौगोलिक और पर्यावरणीय कारणों से होने की संभावना अधिक जान पड़ती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का इलाका शुष्क वायुमंडल वाला है। चार-पांच हजार वर्षों में थोड़ा परिवर्तन तो संभव है, लेकिन बहुत बड़े परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। अभी जैसा पर्यावरणीय ढांचा है, लगभग इसी तरह का उन दिनों भी होगा। ऐसे इलाकों में, यदि वहां से नदियां रुख फेर लें, या उनका बहाव दूर हो जाय, तब वहां जल संकट तो उपस्थित होगा ही, पर्यावरण तथा अन्य संकट भी उपस्थित हो जायेंगे। उपिंदर सिंह ने अपनी किताब ‘प्राचीन एवं मध्यकालीन पूर्व भारत के इतिहास’ में इस सभ्यता के पतन के कारणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए पर्यावरण-विशेषज्ञ गुरदीप सिंह के 1971 में राजस्थान की झीलों पर आये अध्ययन को उद्धृत किया है। गुरदीप सिंह के अध्ययन के अनुसार वर्तमान समय में राजस्थान के झीलों की तरह अति प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के विनष्ट होने का कारण भी शुष्क जलवायु है। यह भी संभव है कि प्रकृति का अत्याधिक दोहन करने से मिटटी में लवण की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ने लगी और फिर उसकी उर्वरा शक्ति इतनी कमजोर हो गयी कि पर्याप्त अन्न-उत्पादन में अक्षम हो गयी। जितनी मात्रा में ईंटों का इस्तेमाल हुआ है उससे यह भी पता चलता है कि उन्हें पकाणे के लिए लकड़ियों का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ और इस प्रक्रिया में उतनी ही रफ़्तार से जंगलों का कटाव भी हुआ। जंगलों के विनष्ट होने से मौसम, खासकर वर्षा प्रभावित हुई। वर्षा ने नदियों के प्रवाह को प्रभावित किया। अर्थात इसका कई स्तरों पर प्रभाव पड़ा। सभ्यता के अचानक विनष्ट होने के सिद्धांत के पीछे आक्रमण की जगह भीषण बाढ़ को भी रखा जा सकता है। वायुमंडल की आर्द्रता कम होने और शुष्कता बढ़ने से कई प्रकार की व्याधियां भी विकसित हुई होंगी। संभव है तय ठिकाने और नगर छोड़कर लोग सुरक्षित अथवा अधिक अनुकूल स्थानों पर खिसकने लगे।

हमारा निष्कर्ष यही है कि सिंधु सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से न होकर बाढ़, महामारी और मौसम के बदलते मिजाज के कारण हुआ। इतनी पुरानी सभ्यता पर जब कोई समुचित लेख या साक्ष्य मौजूद न हो, हम कुछ अनुमान ही कर सकते हैं। लेकिन अनुमानों की भी वैज्ञानिकता और तार्किकता होती है। हमें यह तो देखना ही होगा कि कौन सा अनुमान अधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण है। संभव है भविष्य में इस सम्बन्ध में कुछ अधिक प्रमाण-साक्ष्य मिलें और अधिक आधिकारिक स्तर पर इस सम्बन्ध में कुछ कहने की स्थिति में हम हों।
(कॉपी संपादन : नवल)
[1] पझाना मगही शब्द है। इसका मतलब चमक खोना अथवा प्रभावहीन होना है।
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें
मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया