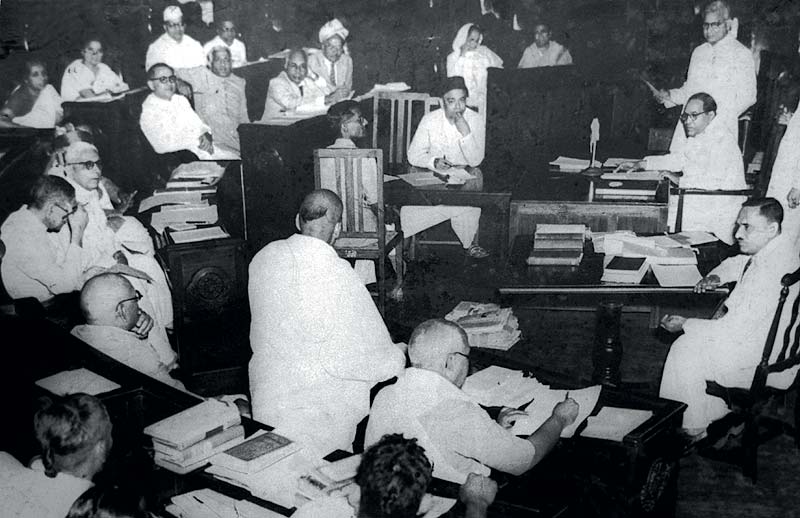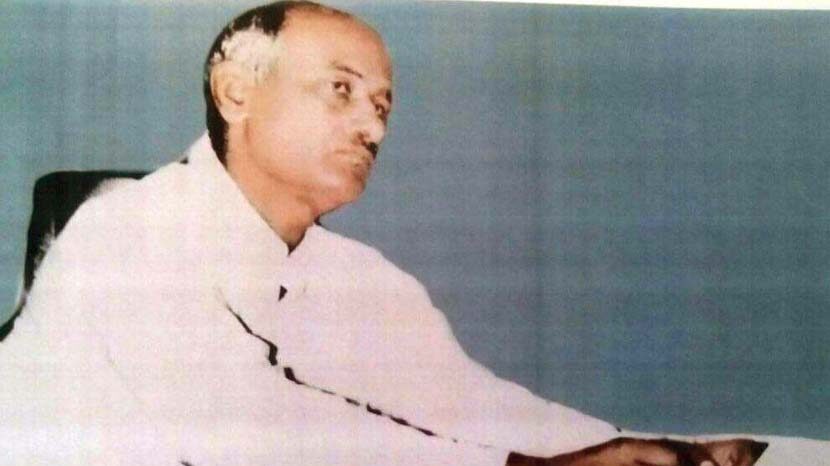जोतीराव फुले (11 अप्रैल, 1827 – 28 नवंबर 1890) पर विशेष
महान वे नहीं होते जो धारा के विपरीत बहते हैं। महान वे होते जो धारा को अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं। शुरू में अकेले होते हैं। धीरे-धीरे पूरा कारवां बन जाते हैं। जहां से गुजरते हैं, वहां उनके पैरों के निशान बन जाते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाते हैं। जोतीराव फुले ऐसी ही शख्सियत थे। एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। उनका वर्ण था शूद्र, जिन्हें ‘मनुस्मृति’ के विधान के हिसाब से न शिक्षा प्राप्त करने की आजादी थी और न अपनी मर्जी का पेशा चुनने की। धन-संपत्ति जुटाकर सुखी जीवन जीने का सपना देखने तक का उन्हें अधिकार नहीं था। लेकिन वक्त बदल चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में ‘दासता उन्मूलन अधिनियम-1833’ और मैकाले द्वारा प्रस्तुत ‘मिनिट्स ऑन एजुकेशन’ (1835) लागू किये जा चुके थे। यह मनुस्मृति-आधारित सामाजिक व्यवस्था को बदलने वाली एक महान पहल थी जिसमें जॉन स्टुअर्ट मिल की उल्लेखनीय भूमिका रही।
जीवन परिचय
फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। 1848 में मात्र 21 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। वे मृत्युपर्यंत वे लोगों के लिए काम करते रहे। वर्ष 1840 में उनका विवाह मात्र 9 वर्ष की सावित्रीबाई फुले से हुआ। वे पढ़ना चाहती थीं। परंतु उन दिनों लड़कियों को पढ़ाने का चलन नहीं था। शिक्षा के प्रति पत्नी की ललक देख जोतीराव फुले ने उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। लोगों ने उनका विरोध किया। परंतु फुले अड़े रहे।
अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत उन्होंने स्कूल खोलकर की। उन दिनों ब्राह्मण अध्यापक शूद्रों के स्कूल में पढ़ाने को तैयार नहीं होते थे। आड़े वक्त में सावित्रीबाई को दी गई शिक्षा काम आई। फुले ने उन्हें अध्यापन का प्रशिक्षण दिलवाया। उसके बाद अगले तीन वर्षों में पति-पत्नी ने 18 स्कूलों की स्थापना की। उनमें से तीन स्कूल लड़कियों के लिए थे। फुले के स्कूलों को सरकार की ओर से बहुत मामूली अनुदान राशि प्राप्त होती थी। इसके बावजूद उनके विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सरकारी और भाषायी स्कूलों से बेहतर था। 16 अक्टूबर 1851 को सरकार की ओर से फुले के बुधवार पैठ स्थित स्कूल का निरीक्षण किया गया। बहुत कम समय में स्कूल की प्रगति देख उसकी बहुत प्रशंसा हुई। कुछ महीने बाद पूना कॉलेज के सुपरिटेंडेंट मेजर केंडी ने भी फुले दंपत्ति द्वारा संचालित स्कूलों का दौरा किया। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा था—‘मैं वहां अध्ययनरत विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता और प्रगति देखकर बेहद प्रसन्न हूं।’
फुले भारत के पहले समाज सुधारक नहीं थे। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बालशास्त्री जांभेकर जैसे नेता उनसे पहले ही सुधारवादी आंदोलनों की शुरुआत कर चुके थे। फुले के समय में भी स्वामी दयानंद, गोपालहरी देशमुख ‘लोकहितवादी’, केशवचंद सेन, रामकृष्ण परमहंस जैसे सुधारक सामाजिक उत्थान के काम में जुटे थे। किंतु फुले तथा उनकी दृष्टि में मूलभूत अंतर था। राजा राममोहन राय सहित ऊंची जातियों से आए सुधारवादी मानते थे कि पहले ऊपर के वर्गों का विकास हो। उनकी देखा-देखी निचले वर्ग भी सुधरते चले जाएंगे। यह विचार अर्थशास्त्र की ‘ट्रिकिल डाउन थ्योरी’ जैसा था, जिसके अनुसार माना जाता है कि समृद्धि ऊपर से नीचे की ओर रिसकर आती है। इस सोच में दो कमियां थीं। पहली परिवर्तन के लिए समाज में परिवर्तन की इच्छा का होना आवश्यक है। निचले वर्गों में परिवर्तन की इच्छा जगे, इस दिशा में ऊंची जाति से आए समाज-सुधारकों का कोई प्रयास न था। उलटे वे उसे दबाने में लगे रहते थे। जबकि फुले के सत्यशोधक समाज ने हाशिये पर पड़े समाजों में चेतना लाने का काम किया, जो उन दिनों सर्वथा उपेक्षित थे।

फुले पर थॉमस पेन जैसे आधुनिक विचारकों का असर था। वे एक हद तक मार्टिन लूथर से भी प्रभावित थे। पेन मनुष्य के अधिकारों के प्रबल हिमायती थे। अपनी पुस्तक, ‘मनुष्य के अधिकार’ में पेन ने लिखा था, ‘मनुष्य, मनुष्य की संपत्ति नहीं है; न ही अनुगामी पीढ़ियां पूर्वगामी पीढ़ियों की संपत्ति हैं….प्रत्येक पीढ़ी को अपने युग की आवश्यकता के अनुसार काम करने का पूरा अधिकार है और होना चाहिए….मनुष्य के समान अधिकार का अर्थ है कि सभी मनुष्य एक कोटि के हैं। परंतु, भारत में शूद्र-अतिशूद्र उन दिनों दोहरी पराधीनता का शिकार थे। राजनीतिक स्तर पर शेष भारतवासियों की भांति वे भी अंग्रेजों के अधीन थे। सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर पर उन्हें ब्राह्मणों सहित कथित ऊंची जातियों का आदेश मानना पड़ता था। इस कारण विचार से बदलाव के औजार की तरह काम लेना और भी मुश्किल था।
क्रांतिधर्मा लेखक
शूद्रातिशूद्र आधुनिक विचारों के आलोक में अपनी स्थिति की समीक्षा कर सकें, इसके लिए फुले शिक्षा-क्रांति की शुरुआत 1848 में कर चुके थे। इन वर्गों को सांस्कृतिक वर्चस्व से बाहर लाने के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों तथा उनके आडंबरों से बाहर निकालना आवश्यक था। धर्म और संस्कृति के नाम पर जनसाधारण को किस तरह मूर्ख बनाया जाता है, यह दर्शाने के लिए 1855 में फुले ने ‘तृतीय रत्न’ नाटक की रचना की। नाटक में उन्होंने बताया कि ब्राह्मण पुरोहित अशिक्षित जनता को किस तरह कदम-कदम पर भरमाते हैं। धर्म और अनीति का भय दिखाकर उनका धन लूटने में लगे रहते हैं। कभी डर तो कभी प्रलोभन के माध्यम से उन्हें कर्मकांडों के लिए मजबूर किया जाता है। कभी-कभी तो वे कर्ज लेकर भी कर्मकांडों का निर्वाह करते हैं। उससे दुख-दलिद्दर मिटना तो दूर, महाजन का कर्ज सिर पर चढ़ जाता है। उसे चुकाने के लिए उन्हें जमींदार के घर बेगार करनी पड़ती है। ‘तृतीय रत्न’ शूद्रों के धार्मिक शोषण के विरुद्ध पहला शंखनाद था।
फुले के यही तेवर उनकी अगली पुस्तक ‘किसान का कोड़ा’ (1869) में भी दिखाई पड़ते हैं। इस रचना के सरोकार काफी बड़े हैं। फुले इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक शोषण के विभिन्न स्तरों पर विचार करते हैं। वे दर्शाते हैं कि हिंदुओं के विभिन्न त्योहार, तीर्थ-स्थल, पंचांग, सामाजिक संस्कार आदि और कुछ नहीं, केवल किसी न किसी बहाने आमजन से रुपये ऐंठने की ब्राह्मणवादी साजिश का नमूना हैं। वे बताते हैं कि किसानों की मुख्य समस्या गरीबी नहीं है। असली समस्या है गरीबी का कारण न समझ पाना। मंडी में बिचौलियों द्वारा किसानों की ठगी, पुरानी किस्म के बीज, अच्छे कृषि-यंत्रों और शिक्षा का अभाव जैसे कारण उनकी उत्पादकता पर प्रतिकूल असर डालते हैं। फुले ने अंग्रेजी राज्य की खुलकर प्रशंसा की और उसे पेशवाई शासन से श्रेष्ठ बताया। इसके साथ-साथ उन्होंने उन अंग्रेज अधिकारियों की आलोचना भी की है जो अपनी काहिली या ब्राह्मणों के प्रभाव में आकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़े रहते हैं।
यह भी पढ़ें : फुले-आंबेडकर की कला दृष्टि
विखंडनवाद यूं तो जाक देरीदा, फूको जैसे ख्यातिनाम चिंतकों के माध्यम से पिछली शताब्दी के अंतिम दशकों में चर्चा का विषय बना था, परंतु उसके बीजतत्व, जॉन लाक, देकार्त्त, इमानुएल कांट, हीगेल, फायरबाख, ब्रूनो बायर आदि चिंतकों के दर्शन में मौजूद थे। वे सभी विचारक अपने-अपने समय की स्थापनाओं का पुनर्पाठ कर, उसे युगीन संदर्भों में पेश कर रहे थे। फुले इस शैली का उपयोग ‘गुलामगिरी’(1873) में ब्राह्मणग्रंथों, प्रतीकों और परंपराओं के पुनर्पाठ के लिए करते हैं। तार्किक विश्लेषण के उपरांत वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पौराणिक आख्यानों की भांति आर्य श्रेष्ठता का दावा भी मिथक है। 1930 तथा उसके बाद सिंधु सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त जानकारियां, उनके निष्कर्षों की पुष्टि करती हैं। ‘गुलामगिरी’ आधुनिक दलित-बहुजन विचारधारा का बीजपाठ है। फुले से प्रेरणा लेकर बीसवीं शताब्दी में दलित-बहुजन विचारधारा का अलग-अलग दिशाओं में विस्तार हुआ। डॉ. आंबेडकर, पेरियार, स्वामी अछूतानंद जैसे बड़े-बड़े नेता और समाज सुधारक उभरे। लेकिन उत्तर से दक्षिण तक जहां-जहां भी अस्मिताकारी राजनीति ने अपनी पहचान बनाई, ‘गुलामगिरी’ में ब्राह्मण संस्कृति का पुनर्पाठ, किसी न किसी रूप में उन सबकी प्रेरणा बना रहा।
सत्यशोधक समाज की स्थापना और उद्देश्य
फुले हिंदू धर्म और उससे जुड़ी परंपराओं को अवैज्ञानिक मानते थे। वे आधुनिक शिक्षा, ज्ञान-विज्ञान और तर्क को महत्व देते थे। वे 25 वर्षों से समाज सुधार के काम में लगे थे। विरोधियों से अकेले ही लोहा लेते आए थे। परंतु अब उन्हें अपने आंदोलन को विस्तार देने और विचारों को विस्तार दी के लिए संगठन की जरूरत महसूस होने लगी थी। कुछ उत्साही युवाओं को साथ लेकर फुले ने एक संगठन बनाने का फैसला लिया। 24 सितंबर, 1873 को पुणे में, नए संगठन के गठन की घोषणा के अवसर पर, महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों से आए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था—
‘अपने मतलबी ग्रंथों के सहारे हजारों वर्षों तक शूद्रों को नीच मानकर ब्राह्मण, भट्ट, जोशी, उपाध्याय आदि लोग उन्हें लूटते आए हैं। उन लोगों की गुलामगिरी से शूद्रों को मुक्त कराने के लिए, सदोपदेश और ज्ञान के द्वारा उन्हें उनके अधिकारों से परिचित कराने के लिए; तथा धर्म और व्यवहार-संबंधी ब्राह्मणों के बनावटी और धर्मसाधक ग्रंथों से उन्हें मुक्त कराने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई है।’2
संगठन का नामकरण फुले ने स्वयं किया था। उसके प्रमुख सिद्धांत थे—ईश्वर एक और सर्वव्यापी है। वह ब्राह्मण पुरोहित के मंदिर में बंद नहीं है। धर्म और जाति से परे है, इसलिए सभी को बराबर मानता है। मनुष्य जाति से नहीं, अपने गुणों से श्रेष्ठ बनता है। सभी धर्मग्रंथ मानव-रचित हैं। ईश्वर न तो अवतार लेता है, न ही कर्मकांड, जप-तप, पूजा-पाठ आदि से प्रसन्न होता है। सभी धर्म बराबर हैं। पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म, भाग्य वगैरह ब्राह्मणों ने स्वार्थ-सिद्धि के लिए गढ़े हैं।
सत्यशोधक समाज के प्रभाव में आकर लोगों ने पुरोहितों से किनारा करना शुरू किया। इस पर पंडितों ने दूसरी चाल चली। वे लोगों को यह कहकर बरगलाने लगे कि संस्कृत देवभाषा है। किसी अन्य भाषा में की गई प्रार्थना ईश्वर को स्वीकार्य नहीं हो सकतीं। इसपर फुले ने समझाया कि—
‘यदि ईश्वर केवल संस्कृत ही समझता है, तो क्या ईसाई, मुसलमान, यहूदी आदि द्वारा उनकी भाषा में की जाने वाली प्रार्थनाएं उसकी समझ में नहीं आतीं? हमारे देश के संतों ने अपनी-अपनी भाषा में ईश्वर की जो प्रार्थनाएं की हैं, क्या वे भी ईश्वर तक नहीं पहुंची हैं?’
‘सत्यशोधक समाज’ पूरी तरह से गैर-राजनीतिक संगठन था। फुले के जनता पर प्रभाव तथा उनकी अनूठी कार्यशैली के फलस्वरूप उसे पांव जमाते देर न लगी। कुछ ही महीनों में मुंबई और पुणे के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी शाखाएं स्थापित होने लगी थीं। उसका प्रभाव महाराष्ट्र की लगभग सभी शूद्र ओर अतिशूद्र जातियों पर था। उन दिनों समाज में अनेकानेक कुरीतियां व्याप्त थीं। उनमें प्रमुख थीं—जातीय भेदभाव, छूआछूत, बाल वैधव्य, भ्रूण हत्या, विवाहादि अवसरों पर दिखावा, फिजूलखर्ची आदि। एक और समस्या विवाहेत्तर संबंधों से जन्मी संतान के पालन-पोषण की भी थी। लोकलाज के कारण ऐसे शिशुओं को प्रायः मार दिया जाता था। एक बार काशीबाई नामक विधवा एक धूर्त ब्राह्मण के संपर्क में आने से गर्भवती हो गई। समय आने पर उसने एक शिशु को जन्म दिया। लोकलाज और समाज के डरी काशीबाई ने शिशु की हत्या कर दी। मामला खुलने पर काशीबाई को जेल जाना पड़ा। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने, पुणे स्थित अपने घर में ‘मातृसदन’ बनाने की घोषणा कर दी। उस अनूठी पहल की भारत के तब तक के इतिहास में बानगी नहीं थी।
‘सत्यशोधक समाज’ का एक नियम था—शादी-विवाह, श्राद्ध-कर्म आदि के अनुष्ठानों के लिए ब्राह्मण पुरोहित को बुलाने की बजाए व्यक्ति स्वयं करे या फिर परिवार के सदस्यों के द्वारा संपन्न कराए। फिजूलखर्ची पर रोक लगे। बचे हुए धन का उपयोग बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाए। वे अकसर कहा करते थे—’विद्या के न होने से वुद्धि गई, बुद्धि के न होने से नैतिकता न रही। नैतिकता के लोप से गतिशीलता लुप्त हुई। गतिशीलता लुप्त होने से धन-दौलत गई। धन-दौलत न रहने पर शूद्रों का पतन हुआ, इतना अनर्थ एक अविद्या से हुआ।’3 आने वाले वर्षों में दर्जनों विवाह ‘सत्यशोधक समाज’ की नियमावलि के अनुसार संपन्न कराए गए। मृत्युभोज, भादों माह में हरतालिका लेना, ब्राह्मण को आटा देते समय उसके पैरों की पूजा करना, होलिका पूजन जैसी निरर्थक परंपराओं को बंद कर दिया गया।
आधुनिक भारत के इतिहास में 19वीं शताब्दी सही मायनों में परिवर्तन की शताब्दी थी। अनेक महापुरुषों ने उस शताब्दी में जन्म लिया। उनमें से यदि किसी एक को ‘आधुनिक भारत का वास्तुकार’ चुनना पड़े तो वे जोतीराव फुले ही होंगे। उनका कार्यक्षेत्र व्यापक था। स्त्री शिक्षा, बालिकाओं की भ्रूण हत्या, बाल-वैधव्य, विधवा-विवाह, बालविवाह, जातिप्रथा और छूआछूत उन्मूलन, धार्मिक आडंबरों का विरोध आदि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहां उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो।
संदर्भ
- थॉमस पेन, थॉमस पेन के राजनीतिक निबंध, संपादक नेल्सन एफ. एडकिंस, अनुवादक रामदेव दीक्षित, पृष्ठ-99
- जियालाल आर्य, ज्योतिपुंज महात्मा फुले, 2006, पृष्ठ 165
- महात्मा फुले, किसान का कोड़ा, महात्मा ज्योतिबा फुले रचनावली, विमलकीर्ति, पृष्ठ-289
(संपादन : नवल/अमरीश)