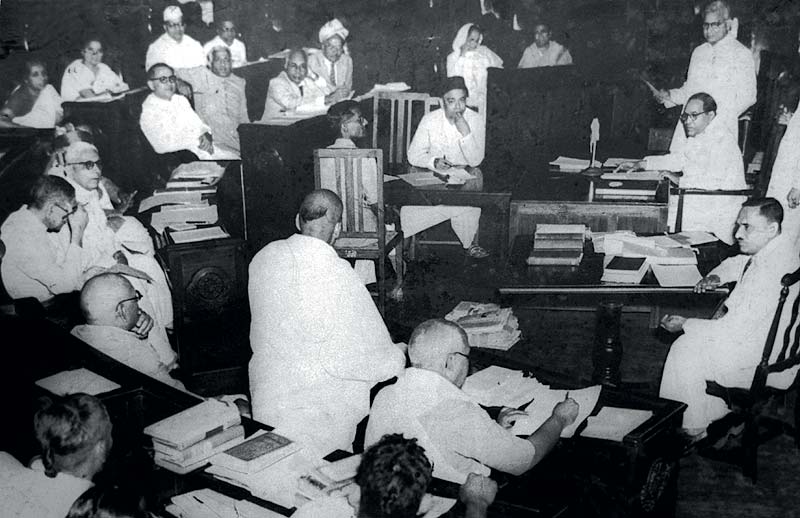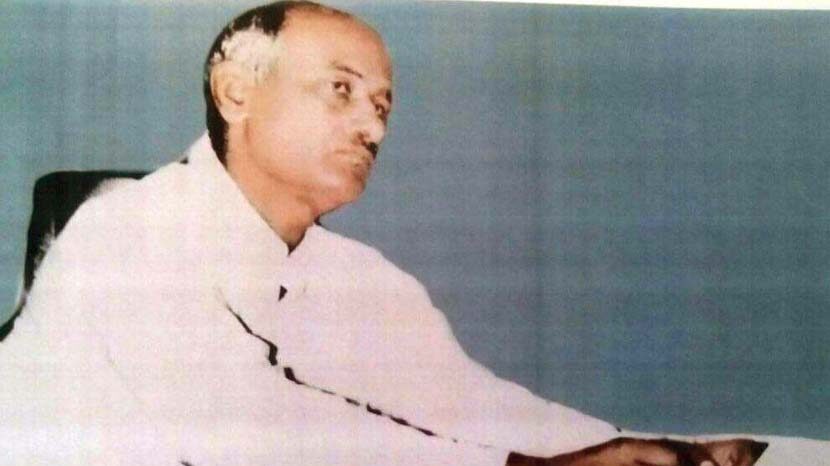क्या आप जानते हैं कि जालियांवाला बाग कांड के पहले भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गुजरात-राजस्थान की सीमा पर अवस्थित बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ में अंग्रेज सैनिकों द्वारा करीब पंद्रह सौ आदिवासियों की हत्या की घटना दर्ज है, जिसे इतिहास के पन्नों में यथोचित स्थान नहीं दिया गया है। जालियांवाला बाग कांड को अंगेजों ने 13 अप्रैल, 1919 को अंजाम दिया था। इसके करीब 6 साल पहले, 17 नवंबर, 1913 को राजस्थान-गुजरात सीमा पर स्थित बांसवाड़ा जिले में अंग्रेजों ने करीब 1500 भील आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया था। परंतु आदिवासियाें की इस शहादत को इतिहासकारों ने तवज्जो नहीं दी। मसलन, राजस्थान के इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे महज “भीलों का उत्पात” की संज्ञा दी है।
दक्षिणी राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बागड़ की मानगढ़ पहाड़ी, आदिवासी अस्मिता और उनके ऐतिहासिक बलिदान का स्मारक है। स्थानीय लोग इसे “मानगढ़ धाम” के नाम से जानते हैं। इस स्थान को राष्ट्रीय धरोहर बनाने की मांग बार-बार की जाती रही है। यहां तक कि लोकसभा में भी इसके लिए आवाज उठाई गई परंतु नतीजा सिफर रहा।
दरअसल, मानगढ़ गवाह है भील आदिवासियों के अदम्य साहस और अटूट एकता का, जिसके कारण अंग्रेजों को नाकों चने चबाने पड़े थे। हालांकि यह एकजुटता गोविंद गुरू के नेतृत्व में बनी थी, जो स्वयं लंबाडा (बंजारा समाज) के थे। इसके बावजूद गोविंद गुरू का जीवन भील समुदाय के लिए समर्पित रहा। खास बात यह है कि उनके नेतृत्व में हुए इस ऐतिहासिक विद्रोह के निशाने पर केवल अंग्रेज नहीं थे बल्कि वे स्थानीय रजवाड़े भी थे जिनके जुल्मों-सितम से भील समुदाय के लोग कराह रहे थे।

भील और लंबाड़ा समुदाय के लोगों की बहादुरी के कारण ही उन्हें रजवाड़ों और अंग्रेजों ने भी अपनी सेना में शामिल किया था। पूंजा भील, जिसे महाराणा प्रताप अपना दाहिना हाथ मानते थे, की छवि तो मेवाड़ के राजचिह्न तक में दर्ज है।
गोविंद गुरु और उनका सामाजिक चेतना का आंदोलन
यह बात तब की है जब 1857 के सैन्य विद्रोह को एक साल भी नही हुआ था। पूरा देश उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। ऐसे समय में गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर से करीब 23 किलोमीटर दूर बांसिया गांव में 20 दिसंबर, 1858 को एक लंबाडा (बंजारा) परिवार में हुआ। गोविंद गुरू बचपन से ही साधु प्रवृत्ति के थे। वे भील एवं लंबाड़ा लोगों पर जाने जाने अत्याचारों से आहत हो जाते थे। वे शोषण और दमन से मुक्ति की राह तलाश कर रहे थे।
वे यह समझ चुके थे कि जब तक शोषित समुदायों के लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए वे क्षेत्रीय आदिवासी बसाहटों (बस्तियों) में जाकर उन्हें संगठित करने लगे। वे लोगों को संदेश देते कि रोज स्नान करो, शराब मत पीओ, मांस मत खाओ और चोरी मत करो। वे श्रम को महत्व देते और कहते थे कि खेती करो और मजदूरी से पेट भरो। बच्चों की शिक्षा के लिए भी वे लोगों को प्रेरित करते और स्कूल खोलने का आह्वान करते। वे रजवाड़ाें और उनके द्वारा चलाायी जाने वाली अदालतों से दूर रहने की बात कहते थे। गोविंद गुरू बहुत ही सहज तरीके से लोगों को समझाते थे कि वे न तो जुल्म करें और न जुल्म सहें। वे लोगों को अपनी माटी से प्रेम करने का संदेश देते।
नए साहित्य का सृजन
गोविंद गुरू ने अपने सन्देश को लोगों तक पहुंचाने के लिए साहित्य का सृजन भी किया। वे लोगों को गीत सुनाते थे। मसलन,
तालोद मारी थाली है, गोदरा में मारी कोड़ी है (बजाने की)
अंग्रेजिया नई मानू नई मानूं
अमदाबाद मारो जाजेम है -2 कांकरिये मारो तंबू हे
अंग्रेजिया नई मानू नई मानूं
…….. धोलागढ़ मारो ढोल है, चित्तोड़ मारी सोरी (अधिकार क्षेत्र) है।
आबू में मारो तोरण है, वेणेश्वर मारो मेरो है।
अंग्रेजिया नई मानू. नई मानूं
दिल्ली में मारो कलम है, वेणेश्वर में मारो चोपड़ो है,
अंग्रेजिया नई मानू. नई मानूं
हरि ना शरणा में गुरु गोविंद बोल्या
जांबू (देश) में जामलो (जनसमूह) जागे है, अंग्रेजिया नई मानू. नई मानूं।।
इन पंक्तियों में गोविंद गुरू अंग्रेजों से देश की जमीन का हिसाब मांग रहे हैं और बता रहे हैं कि सारा देश हमारा है। हम लड़कर अपनी माटी को अंग्रेजों से मुक्त करा लेंगे। गोविंद गुरू अंग्रेजों (जिन्हें वे भूरिया कहते थे) की नीतियों को खूब समझते थे। वे इस बारे में लोगों यह गीत गाकर बताते थे–
दिल्ली रे दक्कण नू भूरिया, आवे है महराज।
बाड़े घुडिले भूरिया आवे है महराज।।
साईं रे भूरिया आवे है महराज।
डांटा रे टोपीनु भूरिया आवे हैं महराज।।
मगरे झंडो नेके आवे है महराज।
नवो-नवो कानून काढे है महराज।।
दुनियां के लेके लिए आवे है महराज।
जमीं नु लेके लिए है महराज।।
दुनियांं नु राजते करे है महराज।
दिल्ली ने वारु बास्सा वाजे है महराज।।
धूरिया जातू रे थारे देश।
भूरिया ते मारा देश नू राज है महराज।।
वैेसे कहने को तो यह एक भजन है और “राजा है महराज” जैसे टेक के होने के कारण यह समूह गीत की तरह गाया जाता था। परंतु यह भजन कम, राजनीतिक ककहरा ज्यादा है, जिसे स्कूल के मास्टर की तरह गोविंद गुरू सभी को रटाते थे। खास बात यह कि वे व्यापक एकता चाहते थे और इस कारण वे राजस्थानी हिंदी का उपयोग करते थे। वे जानते थे कि उनके सांस्कृतिक संदर्भ में यही (हिंदी) भाषा जनांदोलन की भाषा हो सकती है।
आदिवासियों की एकजुटता से हिलने लगी थीं रजवाड़ों की चूलें
उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा से लोग प्रभावित होने लगे और धीरे–धीरे दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और मालवा के आदिवासी संगठित होकर एक बड़ी जनशक्ति बन गए। अपने जनाधार को विस्तार देने के लिए गोविंद गुरू ने वर्ष 1883 में “संप सभा” की स्थापना की। भील समुदाय की भाषा में संप का अर्थ होता है – भाईचारा, एकता और प्रेम। संप सभा का पहला अधिवेशन वर्ष 1903 में हुआ।
दरअसल गोविंद गुरू राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश के आदिवासियों को शिक्षित बनाकर देश की मुख्य आवाज बनाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को समझने के लिए अध्ययन करना, चिंतन करना और संगठन स्थापित करना जरूरी है। इसी से शोषण व उत्पीड़न से निपटा जा सकेगा।
एक तरफ गोविंद गुरू के नेतृत्व में आदिवासी जागरूक हो रहे थे तो दूसरी ओर देशी रजवाड़े व उनकी संरक्षक अंग्रेजी हुकूमत आदिवासी एकता को अपने लिए खतरे के रूप में देखने लगी थी।
देशी राजे-महराजे सदियों से भीलों से बेगारी कराते आए थे। वे अब भी चाहते थे कि भील बेगारी करें। मगर भील अब जाग चुके थे। उन्होंने बेगारी करने से इंकार कर दिया। शराब नहीं पीने के गोविंद गुरू के आह्वान के कारण शराब कारोबारियों का धंधा ठप्प पड़ गया। इन ठेकों से अंग्रेजी हुकूमत को टैक्स के रूप में आमदनी होती थी जो बंद हो गई। सूदखोंरों के दिन भी लद चुके थे क्येांकि लोगों ने उनसे सूद पर पैसे लेने बंद कर दिया।
आदिवासियों में बढ़ती जागरूकता से देशी रजवाड़े प्रसन्न नहीं थे। उन्हें भय सता रहा था कि जागृत आदिवासी कहीं उनकी रियासतों पर कब्जा न कर लें। दूसरी और सूदखोरों व लालची व्यापारियों ने भी रजवाड़ों पर दबाव बनाया। देशी रजवाड़ों के समर्थन में अंग्रेजी हुकूमत भी आदिवासियों के खिलाफ हो गयी।
जब अंग्रेजों ने पंद्रह सौ से अधिक आदिवासियों की जान ले ली
गोविंद गुरू के नेतृत्व में आदिवासी एकजुट होकर बदलाव की राह पर अग्रसर थे। 7 दिसंबर, 1908 को संप सभा का वार्षिक अधिवेशन बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से सत्तर किलोमीटर दूर आनन्दपुरी के समीप मानगढ़ धाम में आयोजित हुआ। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। मानगढ़ उनका महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था।
सन 1913 में गाेविंद गुरू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आदिवासी मानगढ़ में जुटे। वे अपने साथ राशनपानी भी लाए थे। उनके विरोधियों ने यह अफ़वाह फैला दी कि आदिवासी रियासतों पर कब्जा करने की तैयारी में जुटे हैं।
उस समय गुजरात बंबई राज्य के अधीन था। बंबई राज्य का सेना अधिकारी अंग्रेजी सेना लेकर 10 नवंबर 1913 को पहाड़ी के पास पहुंचा। सशस्त्र भीलों ने बलपूर्वक आयुक्त सहित सेना को वापस भेज दिया। सेना पहाड़ी से थोड़ी दूर पर ठहर गई। 12 नवंबर 1913 को एक भील प्रतिनिधि पहाड़ी के नीचे उतरा और भीलों का मांगपत्र सेना के मुखिया को सौंपा मगर बात बन नहीं पाई। समझौता न होने से डूंगरपुर और बांसवाड़ा के रजवाड़ों ने अहमदाबाद के कमिश्नर को सूचित किया कि अगर जल्द ही “‘संप सभा’” के भीलों का दमन न किया गया तो वे उनकी रियासत लूटकर अपनी रियासत खड़ी करेंगे, जिससे अंग्रेजी सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अंग्रेज अधिकारी सतर्क हो गए। वे भीलवाड़ा की मांग से अवगत थे। इसलिए तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने मेवाड़ छावनी से सेना बुला ली। यह सेना 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहुंची और पहुंचते ही फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक कुल पंद्रह सौ लाशें गिरीं। गोविंद गुरु के पांव में गोली लगी। वे वहीं गिर पड़े। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। मगर बाद में फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। अच्छे चाल-चलन के कारण सन 1923 में उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद वे गुजरात के पंचमहल जिला के कंबोई गांव में रहने लगे। जिंदगी के अंतिम दिनों तक जन-कल्याण कार्य में लगे रहे। वहीं सन 1931 में उनका देहांत हो गया। आज भी पंद्रह सौ आदिवासियों की शहादत मानगढ़ पहाड़ी के पत्थरों पर उत्कीर्ण हैं। भीलों ने जिस धूनी को जलाया था, वह आज भी जल रही है।
(संपादन : नवल/गोल्डी/अमरीश)