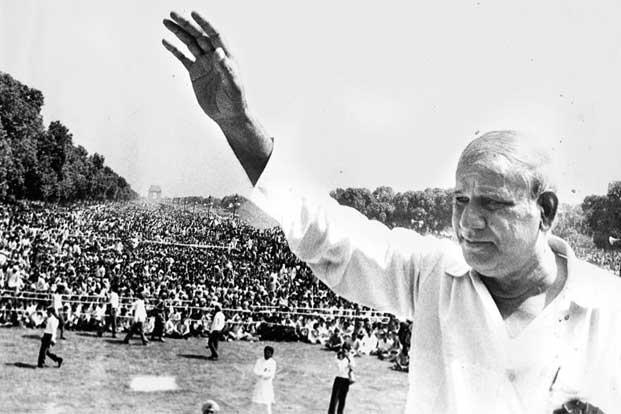पिछले हफ्ते जब यह स्तम्भ शुरू किया गया तो इसका आशय यह था कि शृंखलाबद्ध तरीके से इस बात पर विचार किया जाय कि पिछड़ों का साहित्य कैसा होगा और उसके स्रोत क्या होंगे? ज़ाहिर सी बात है कि यह विराट मानवीय जिज्ञासाओं और अन्वेषण की बात होगी जिसके कारण अनेक प्रचलित चीजें, स्थितियां, मान्यताएं और चरित्र अपने पुराने स्वरूप से अलग भी हो जाएंगे और उनकी जगह बहुत सी नई चीजें जुड़ सकती हैं। और अगर ऐसा न हो तो फिर कागज़ कारे करने का मतलब ही क्या? उससे बेहतर है कि गुल्ली-डंडा ही खेल लिया जाय। उससे मानसिक स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर रहेगा। इसीलिए पिछड़ों के मनोविज्ञान को संचालित करने वाले तमाम घटकों की ओर ध्यान ले जाने की कोशिश शुरू हुई। इस क्रम में सबसे पहले एक विशाल जनसमुदाय को पिछड़ों के रूप में चिन्हित करने का एजेंडा मुख्य है। पिछड़े मतलब हिन्दू समाज में धार्मिक एकता कायम करते हुए भी भू-अधिकार, नौकरियों तथा सत्ता में भागीदारी से वंचित समाजों के लोग। गैर हिन्दू धार्मिक दायरों में रहनेवाले वे लोग जो धर्म को तो कसकर पकड़े हुए हैं लेकिन अपने जीवन को अतार्किक नियतियों के आधार पर मानते आए हैं।
यह जकड़बंदी इतनी जटिल है कि वे अपनी अनंतकालीन वंचनाओं और दुखों के लिए न तो किसी भौतिक सत्ता को जिम्मेदार मानते हैं और न ही उसके खिलाफ कोई आवाज उठाते हैं। बल्कि अपनी गरीबी, शोषण और उत्पीड़न-दमन को गर्दन झुकाए स्वीकार किए चले आते हैं। इस दायरे में विशाल वन-प्रांतर, समुद्री किनारों और पर्वतीय क्षेत्रों में रहनेवाले लोग हैं जिनपर हिन्दू होने का बहुत ज्यादा दबाव थोपा नहीं जा सका लेकिन जो लंबे समय तक तिजारती-तंत्र के शिकार रहे। उनकी मामूली जरूरतों की पूर्ति के बहाने उनको कर्ज और ब्याज के भयानक जाल में फंसाकर उनके खून की अंतिम बूंद तक चूस ली गई। इस दायरे में वे आदिवासी लोग भी हैं जो पिछले कई दशकों से संघी प्रचारों के चंगुल में हैं, जिन्हें हिन्दुत्व की चाशनी चटाकर रामभक्त बनाने का प्रयास तो बहुत शातिरना तरीके से हुआ लेकिन वे बदहाली के उसी गर्त में हैं जहां वे सदियों तक रहते आए हैं। इस दायरे में वे आदिवासी हैं जिनके जंगलों और पहाड़ों को समूचा चबा जाने के लिए कॉर्पोरेट और सत्ता का सबसे भयानक गंठजोड़ चल रहा है, जिसके खिलाफ कॉर्पोरेट का आईटी सेल मीडिया सबसे घिनौनी और कुत्सित खबरें फैलाने में लगा हुआ है।
वास्तव में ब्राह्मण-बनिया-कॉर्पोरेट-सत्ता के निरंकुश और अपराजेय माने जाने वाले गंठजोड़ के शिकार समाजों-समुदायों-जातियों-जमातों को हम पिछड़ा मान रहे हैं, जो सिर्फ भारतीय आज़ादी के दौर से ही नहीं, पता नहीं इतिहास के किस मोड से बदहाली में जीते और समाज को अपना अनमोल योगदान करते हुये यहां तक आए हैं। उनकी ऐतिहासिक जीवन यात्रा, संघर्ष और दशा के माध्यम से न केवल उनकी वास्तविकता को जाना जाय बल्कि उनको नियंत्रित करनेवाली व्यवस्था के खिलाफ उनके प्रतिरोध और उसकी भाषा को भी जाना जाय। कुल मिलाकर इस उपक्रम का लक्ष्य पिछड़ों की व्यापकता को विखंडित करनेवाली ताकतों की पहचान के साथ ही उनको एकजुट करने के सकारात्मक विंदुओं और मुख्य घटकों की शिनाख्त करना है। इसके लिए उन असुविधाजनक और अलक्षित इलाकों तक जाने का भी उद्देश्य है जहां तक पहले तो नज़र ही बहुत मुश्किल से जाती है दूसरे अगर नज़र पड़े भी तो वहां से तथ्य निकाल लाना सबके वश की बात नहीं है।
मसलन पिछड़ों के साहित्य की खोज में जेल की कोठरियों की छानबीन, अदालती पराजयों का गहन अध्ययन, फांसी के फंदों और थानों की हवालातों के विश्लेषण से पिछड़ों का साहित्य खोजने की परिकल्पना की गई है। इसके साथ ही आदि लिपिकार पथरकटों, आदि आविष्कारक चरवाहों, किसानों, देशों के अन्वेषक और खोजी मल्लाहों, नाइयों, धोबियों, बुनकरों की ऐतिहासिक जीवन यात्राओं के अलावा विभिन्न घटनाओं के प्रभावों का गहन अध्ययन भी एक मुख्य परिकल्पना है और मुझे लगता है इन्हीं सब में एक विराट पिछड़ा साहित्य मौजूद है। वास्तव में यह बहुत रोमांचक और लोमहर्षक परिकल्पना है लेकिन इसका आधार थोथा रोमांटिसिज़्म नहीं है, बल्कि इसका आधार ऐतिहासिक भौतिकवाद और उसकी द्वंद्वात्मकता है।

संयोग से स्तम्भ के पहले लेख में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि विश्वविद्यालयों और दीगर संस्थानों के जरिए से शिक्षित-प्रशिक्षित होने वाले पिछड़े मुख्यधारा, जिसे उसकी संरचनामूलक विशेषताओं के कारण हिन्दू और उसमें भी केवल सवर्ण हिन्दू हितों की रक्षक धारा भी कहा जाना चाहिए, द्वारा थोपी गई साहित्यिक सामग्री और अवधारणाओं को न जाने कब से ढो रहे हैं। वास्तव में वह सामग्री उनके लिए फिजूल है इसीलिए उसे गोबर का टोकरा कहा गया और उसे फेंकने की अपील की गई। इस क्रम में कबीर के ढाई आखर के विभिन्न आयामों को रेखांकित किया गया और कबीर द्वारा कृष्ण को दिया गया विशेषण ‘काम को कीरा’ के बहाने कृष्ण के थोपे गए व्यक्तित्व की भी सख्त आलोचना की गई। इस बात को पढ़कर मेरे पास कई फोन आए और कुछ लोगों ने अपनी लिखित प्रतिक्रिया दी कि मैं कृष्ण की चरित्र हत्या कर रहा हूं। ज़्यादातर लोगों ने अपना गुस्सा इस बात पर जाहिर किया कि ले देकर उनके पास एक ही नायक है और मैं उसके चेहरे पर कालिख लगा रहा हूं।
मैं उन सभी लोगों से जानना चाहता हूं जो कृष्ण के नायक व्यक्तित्व को लेकर इतने आग्रही हैं कि सच्चाई का सामना होते ही गाली-गलौज करने लगते हैं कि कृष्ण का क्या चरित्र है जिसकी हत्या करना संभव है? अगर यौन संबंधी नैतिकताओं के आधार पर पूछूं तो यह पूछना चाहिए कि कृष्ण के पास चरित्र है कहां जो हत्या की बात उठे। तथाकथित मित्र वत्सलता की कसौटी पर कसा जाय तब कृष्ण का क्या चरित्र है जिसकी हत्या संभव है? श्रमजीवी अहीर स्त्रियों के साथ कृष्ण के व्यवहार से कृष्ण का कौन सा चरित्र उभर रहा है जिसकी हत्या हो सकती है? क्या कृष्ण के पास कोई चारित्रिक दृढ़ता है? कृष्ण किसका है? क्या यादवों ने अपने लिए किसी कृष्ण को गढ़ा है या वे तमाम निहित स्वार्थों द्वारा थोपे गए कृष्ण को लेकर ही उसकी पूजा कर रहे हैं और गौरवान्वित हो रहे हैं। क्या अत्यंत साधनसम्पन्न और शोषणकारी व्यवस्था में शामिल मुट्ठी भर यादवों का कोई ऐसा कृष्ण है जो खेतिहर मजदूरों, भूमिहीन, गृहविहीन, बेरोजगार और बदहाली में जीवन जी रहे यादवों का भी कृष्ण है? क्या कृष्ण कोई ऐसा वैचारिक सूत्र है जिससे किसी जाति या समुदाय को एक मजबूत धागे में बांधा जा सकता है? सवाल हजारों हैं जिनका जवाब उन यादवों को देना चाहिए जो मानते हैं कि कृष्ण उनके कबीले का आइकॉन है।
यह भी पढ़ें : बहस-तलब : पिछड़े करें अपने साहित्य की तलाश
मामला चूंकि आइकॉन का है इसलिए वेदों, पुराणों, महाभारत से लेकर सूरसागर, गीत गोविंद आदि सैकड़ों किताबों में कृष्ण को देखना चाहिए। हर जगह कृष्ण एक नहीं है। ऋग्वेद में एक लड़ता हुआ कृष्ण है। महाभारत में अपने ही लोगों को कौरव सेना में भेजकर मरवाता हुआ कृष्ण है तो सूर सागर में बक़ौल डॉ. धर्मवीर ‘कृष्णभक्ति का राधावाद’ है जो वस्तुतः यौन अपराधियों को अपराधबोध से मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करता है। अपनी पुस्तक ‘दलित चिंतन का विकास : अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर’ (2008) में संकलित लेख ‘डॉ. नामवर सिंह का दुख’ में एक जगह लिखते हैं – “डॉ. नामवर सिंह का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है –‘वह क्या है जिसकी प्रक्रिया इस्लाम के आने से पहले से ही शुरू हो गई थी और उसके बाद भी अबाधित गति से चलती रही? उनका उत्तर “लोक धर्म बनाम शास्त्र धर्म” की गुत्थमगुत्थी से निकला है। लोक धर्म में वे लोक जीवन, लोक, शक्ति और लोकसंस्कृति के नाम गिनाते हैं। लेकिन यह सपाट बयानी अधिक है। सपाट बयानी इसलिए क्योंकि इसमें ‘लोक बिगाड़’ का शब्द नहीं आया। असल में लोक के दो रूप थे – एक लोक सुधार और दूसरा लोक बिगाड़। आजीवक धर्म हमेशा लोक सुधार की बात सामने लाते थे लेकिन ब्राह्मण धर्म उसी जगह लोक-बिगाड़ करता रहता था। इस बिगाड़ के लिए वह अन्य विरोधी धर्मों में प्रच्छन्न रूप धारण कर घुस जाता था। बौद्ध धर्म का उसने खात्मा इसी विधि से किया। सिद्धों में जो कुछ वरणीय और श्रेष्ठ था, उसे वह नष्ट करता जा रहा था। जो मत पत्नी के रूप में स्त्री का सम्मान करना चाहता था, उसकी तुलना में उसने स्त्री को परकीया और रखैल बना दिया था। उसने सिद्ध नाथ, तंत्र, योग और शाक्त की तुलना में अपने राधावाद को आगे रख दिया था। वह लोक सुधार को मिटाता गया और लोक-बिगाड़ को बढ़ाता गया।” (पृष्ठ 45-46)
अब आसानी से वास्तविकता की ओर जाया जा सकता है। कृष्ण की ज़िंदगी में प्रक्षेप की जरूरत किसे थी? साक्ष्य बताते हैं कि ब्राह्मणों को, ताकि वे न केवल अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकें बल्कि अपने ब्राह्मणधर्म को सुरक्षित भी रख सकें। डॉ. धर्मवीर कहते हैं कि ब्राह्मण विवाह में विच्छेद की गुंजाइश नहीं है चाहे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनैतिक यौन सम्बन्धों को स्थापित किया जाय। और इसके लिए शास्त्र में ही नहीं, लोक का भी समर्थन चाहिए था, जिसके लिए अवतारवाद के माध्यम से एक ऐसा पात्र गढ़ना जरूरी था जो यौन सम्बन्धों में मर्यादित न हो। उसकी आड़ में सारे कुकर्म न केवल किए जाएं बल्कि उनका जायजीकरण भी किया जाय। और हम देखते हैं कि उन्होने इसके लिए एक अहीर के छोकरे को बलि का बकरा बना लिया। और हम यह भी देखते हैं कि उसके अलग-अलग चित्रण के लिए ब्राह्मणों कवियों की अनेक पीढ़ियों ने मुसलसल काम किया। व्यास जैसा फर्जी चरित्र हो या सूरदास जैसा रहस्यमय व्यक्ति या जयदेव जैसा कवि। सभी को अभीष्ट कामकला और रिश्तों की मर्यादा न समझनेवाला कृष्ण रचना था। जयदेव ने तो ‘गीत गोविंद’ में ऐसे ऐसे श्लोक रचे हैं कि उन्हें यहां रखना मुश्किल है लेकिन एक पद का भावार्थ बताना चाहूंगा जिसमें कहा गया है कि ‘गोपियों के कुचाग्रों से कृष्ण के तलवों में रक्त छलछला आया है।’ अब जरा ‘ब्रह्मवैवर्त पुराण’ में कृष्ण के चित्रण पर ध्यान लगाया जाय। प्रसंग मथुरा में कृष्ण के आने और कूबड़ी कुब्जा के साथ दैहिक संवाद का है –
‘त्यज निद्रां महाभागे शृंगारं देहि सुंदरि। पुरा शूर्पणखा त्वं च भगिनीं रावणस्य च ॥56॥
रामजन्मनि मद्धेतोस्त्वया कान्ते तपः कृतम। तपः प्रभावान्माँ कांतं भज श्रीकृष्ण जन्मनि॥57॥
अधुना सुखसंयोगं कृत्वा गच्छ ममाSSलयम । सुदुर्लभं च गोलोकं जरामृत्युहरं परम ॥58॥
मतलब यह कि श्रीभगवान कहते हैं – हे सुंदरी! निद्रा त्याग करके मुझे शृंगार (कामक्रीड़ा) प्रदान करो। हे सुंदरी! तुम पूर्वजन्म में रावण की बहन शूर्पणखा थी। हे कान्ते! तुमने रामवतार में मुझे प्राप्त करने हेतु तपश्चरण किया था। तपश्चरण के प्रभाव से मैं इस जन्म में श्रीकृष्णरूप में पति मिल गया। अब मेरे साथ सुख संभोग करके मेरे गृह गोलोक जाना। जो दुर्लभ तथा जरामृत्युहारी लोक है।
सुरतेर्विरतिर्नास्तिदंपति रतिपंडितौ। नानाप्रकार सुरतं बभूव तत्र नारद ॥61॥
स्तनश्रोणियुगं तस्या विक्षतं च चकार ह। भगवान्नखरेस्तीक्ष्णेर्दशनैरधरं वरम॥62॥
अर्थात ये दंपति रतिक्रीड़ा के पंडित थे। इनकी रमण क्रीड़ा में कोई विराम नहीं हो रहा था। नारद! श्रीकृष्ण तथा कुब्जा में अनेक प्रकार की सुरत क्रीड़ा होने लगी। श्रीकृष्ण ने तीक्ष्ण नखघात एवं दंताघात से कुब्जा के स्तनों तथा नितंबों को क्षत-विक्षत कर दिया। श्रीकृष्ण ने तदनंतर कुब्जा के श्रेष्ठ आधार का पान भी किया।
यह आपके नायक श्रीकृष्ण का चित्रण है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। यह कृष्णद्वैपायन महर्षि व्यास द्वारा लिखा बताया जा रहा है और जिस संस्करण से उद्धरण दिया गया है उसके भाषा भाष्यकार श्रीनाथ खंडेलवाल हैं। इसका अर्थ है यह किताब बहुत पुरानी है। क्या यादवों में से किसी ने इस पर आपत्ति की। क्या कभी उनको लगा कि यह उनके नायक और कुलपूर्वज की चरित्रहत्या करने की कोशिश है?
डॉ. धर्मवीर इस सबकी पृष्ठभूमि और निहितार्थों की व्याख्या इन शब्दों में करते हैं –“अब ब्राह्मणों को सिद्ध बनने की जरूरत नहीं रह गई थी। सिद्धों के डोम्बीवाद का काम कृष्ण भक्ति के राधावाद से चल निकला था। पहले वे तंत्र में अपने जारकर्म और बलात्कार की ओट ढूंढ रहे थे, अब उन्हें कृष्ण भक्ति में यह ओट मिल गई थी। उन्हें अपनी जार मनोवृत्ति को संतुष्ट करना है, वह सिद्ध बनकर हो या भक्त बनकर हो, इससे उन्हें ऐतराज नहीं है। उन्हें जारकर्म को युगानुकूल रूप देना है। सिद्धों की डोम्बी, चांडाली, बंगालन और बालरंडा कृष्ण भक्ति में गोपियां बन गई हैं। वहां और यहां सब जगह दलित जातियों की स्त्रियां हैं, इनमें से किसी के साथ विवाह नहीं किया जाता। इस दृष्टि से बिलकुल कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों के लिए उनका साहित्य एक निरंतर अविच्छिन्न प्रवाह है जिसमें ब्राह्म-विवाह में अनुमत उनके परकीया-सम्बन्धों के जारकर्म पर कोई रोकटोक नहीं है। (वही, पृष्ठ 46-47)
ब्राह्मणों ने कृष्ण को अपने हिसाब से रचा है और अपनी सुरक्षा में एक ऐसे पहाड़ की तरह खड़ा कर दिया है जिसको हटाने में यादव बिलकुल अक्षम हैं। वे थोपे गए और नकली कृष्ण के गहरे मोह में हैं। उन्हें गीता अपनी लगती है और इसपर उनको नाज है जबकि गीता एक संदिग्ध पुस्तक है। और उसके सारे निहितार्थ ब्राह्मणों के हित में हैं। जिस तरह कृष्ण ने अपने को कर्ता और अर्जुन को अकर्ता या माध्यम भर कहा है उसका खामियाजा उसके अपने ही बंधु-बांधवों के विनाश के रूप में निकलता है। लेकिन डॉ. धर्मवीर कहते हैं –“कृष्ण का अकर्तावाद अपराधी के पक्ष में जाता है, कारण, आधे अकर्त्तावाद को लागू नहीं किया जाता। पूरा अकर्तावाद हो तो समाज को भी इसका लाभ हो। कृष्ण की गीता का अकर्तावाद यही बताता है कि मेरे भक्त ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि थ्योरी में वह अकर्ता है।” (वही पृष्ठ 51)
बार-बार मुझे कबीर याद आते हैं – सांच कहूं तो मारन धावे, झूठा जग पतियाना। सांच क्या है? यह कि तुम मनुष्य हो लेकिन इसी से तुम्हें ऐतराज है। तुम भक्त, चेरा, गुलाम और अकर्ता बनते हो और उन सारी कपोल कल्पनाओं पर भरोसा बनाए हुये हो, जिनका कोई आधार ही नहीं है। लेकिन यह झूठ तुम्हारे सामने इतनी बार दुहराया गया है कि वह तुम्हारे खून में बस गया है। वही खून क्रमशः तुम्हारी पीढ़ियों के रगों में जा रहा है और सब के सब वही झूठ पतिया (सच मान) रहे हैं। इसलिए मैं जब सच कह रहा हूं कि तुम हो। तुम मनुष्य दुनिया के अनमोल रत्न हो तो तुम्हें भरोसा ही नहीं हो रहा है। तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं और तुम मेरे उपर ही हमला कर रहे हो। झूठा कहनेवाला इतनी खूबसूरती से कह रहा है कि तुम उसी में फंस गए हो। और ध्यान दो सैकड़ों जातियों का एक समुच्चय जो अपने को सबसे ऊंचा वर्ण और जन्मजात तुम्हारा गुरु होने का दावा कर रहा है वह लगातार तुम्हारे नायकों का किस्सा अपने फायदे के लिए रच रहा है। तुमसे कमा रहा है और तुम्हें झूठ परोस रहा है। तुम्हारा नायक उसका पांव धोकर पी रहा है और अपना सबकुछ दे दे रहा है। पगले। तुम भी तो उसी बनावटी नायक में खो गए हो।
लगता है कबीर यादवों को ही संबोधित कर रहे हैं कि कहां खोये हो। डॉ. आंबेडकर ने वर्णव्यवस्था के विधानों की संहिता ‘मनुस्मृति’ का दहन किया लेकिन क्या यादवों ने कभी ‘ब्रह्मवैवर्त पुराण’ जलाने की कोशिश की? क्या कभी उनको इस बात का खयाल आया कि कृष्ण का ऐसा चित्रण करने वाले लोगों का निहित स्वार्थ क्या था? क्या जिस व्यक्ति के पास कोई यौन नैतिकता ही नहीं है वह किसी समाज का नायक हो सकता है? उपरोक्त उद्धारित किए गए इकसठवें श्लोक में कहा गया है कि ‘ये दंपति रतिक्रीड़ा के पंडित थे। क्या थे मुझे नहीं पता लेकिन क्या वास्तव में ये दंपति थे। क्या कुब्जा से कृष्ण का विवाह हुआ था? जरा ढिठाई देखिये – “हे सुंदरी! तुम पूर्वजन्म में रावण की बहन शूर्पणखा थी। हे कान्ते! तुमने रामवतार में मुझे प्राप्त करने हेतु तपश्चरण किया था। तपश्चरण के प्रभाव से मैं इस जन्म में श्रीकृष्णरूप में पति मिल गया।” कबीर के शब्दों में ‘काम को कीरा’ कुब्जा के इस जन्म को तो कलंकित कर ही रहा है। पिछले जन्म को भी कलंकित कर रहा है। क्या यादवों को अपने नायक का ऐसा चित्रण आपत्तिजनक लगता है? आखिर वे स्त्री के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं? क्या उन्हें विवाह संस्था में भरोसा है और वे एकविवाही जीवन को महत्व देते हैं। उनमें कोई सामाजिक मर्यादा या नैतिकता है या कृष्ण की तरह ‘सोलह हजार रानियों के पति’ होना पसंद करते हैं?
हर व्यक्ति जो एक समय युवा होता है वह एक समय जिम्मेदार प्रौढ़ और घर का बुजुर्ग हो जाता है क्या वह अपनी वर्तमान और भावी बेटियों को ऐसे किसी आदमी के साथ विदा करना पसंद करते हैं जो लंगोट का कच्चा है और हर जगह छिनरपन पर उतर आता है? क्या ये स्त्रियां या ऐसी स्त्रियां कभी संपत्ति और सत्ता में हिस्सेदारी की मांग कर सकती हैं या उनकी नियति में केवल रास रचाना लिखा है? यह सवाल सभी यादवों से है कि उन्होंने ऐसे कृष्ण को इस दुनिया में रहने क्यों दिया है। इसके पीछे उनकी क्या मजबूरी है? उन्होने ऋग्वेद के उस कृष्ण को अपना क्यों नहीं माना जो इंद्र के साथ लोमहर्षक संघर्ष करता है, जिसे प्रख्यात भाषाविज्ञानी डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह किसानी परंपरा में देखते हैं?
कृष्ण को किसने गढ़ा है यह आज भी बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही क्यों गढ़ा यह भी एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही यह सबसे बड़ा सवाल है कि कृष्ण को यादवों ने किस रूप में अपनाया और क्यों अपनाया? क्या कोरी भावुकतावश या इसमें कोई तार्किक आधार है?
(संपादन : नवल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें
मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया