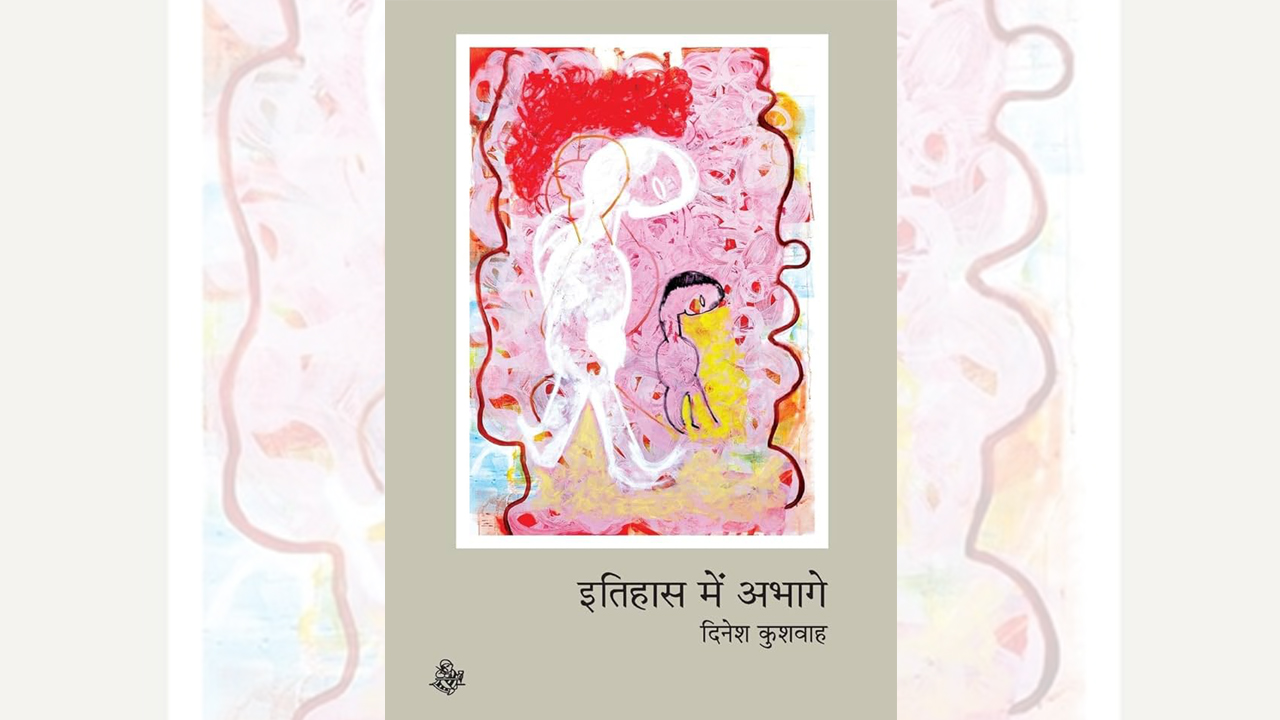पिछली कड़ी के आगे
जयप्रकाश कर्दम व ईश कुमार गंगानिया का कविता–संघर्ष
मलखान सिंह की कविता में ‘रोटी’ और ‘सम्मान’ की, जो लड़ाई हम देखते हैं, उसी का विकास हमें जयप्रकाश कर्दम के कविता-संग्रह ‘गूंगा नहीं था मैं’ में दिखाई देता हैं, जो 1997 में प्रकाशित हुआ था। तब करीब 39 साल के इस तरुण कवि को आंबेडकर के आंदोलन से जुड़कर जीवन के अनुभवों को कविता में अभिव्यक्त करने का साहस मिल गया था। वह गांव में पैदा हुआ और घोर गरीबी में उसकी परवरिश हुई। इस कवि ने गरीबी, भूख और अस्पृश्यता को अपने पूरे जिस्म पर महसूस किया। उसने उस परिवेश को देखा, जिसमें सवर्णों के आतंक से दलित जातियां सदैव भयभीत रहती थीं। कहने को देश आजाद था और कानून की नजर में सब समान थे। पर, हकीकत में ऐसा नहीं था। न अस्पृश्यता खत्म हुई थी, न उत्पीड़न और न बेगारी बंद हुई थी। अछूत जातियां आजाद भारत में भी डर-डर कर और जुबान बंद रखकर घुट-घुटकर जी रही थीं। पर, वे गूंगे नहीं थे।
कवि ने ‘गूंगा नहीं था मैं’ कविता में इसी अंतर्वेदना को अभिव्यक्त किया है। स्कूल में जाट के लड़के कहते– “अरे ओ मोरिया/ ज्यादै बिगड़ै मत/ कमीज कू पेंट में दबा कै मत चल।”[1]
उस समय भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के तेजतर्रार आंबेडकरवादी दलित नेता बी.पी. मौर्य के कांग्रेस और हिंदू-विरोधी भाषणों की धूम मची हुई थी। सवर्ण उनका नाम बिगाड़ कर ‘मोरिया’ कहकर अपनी घृणा प्रदर्शित करते थे। उस दौर में यह नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सवर्णों ने हर चमार का रखा हुआ था। कवि आगे कहता है, “मैंने चुपचाप अपनी कमीज/ पेंट से बाहर निकाल ली थी।” पर, कवि गूंगा नहीं था, जो प्रतिरोध नहीं कर सकता था। पर वह भयभीत था, क्योकि, कवि कहता है–
अगर मैं बोल जाता
जंगल की आग की तरह
यह बात फैल जाती कि
ढेढ़ों का दिमाग चढ़ गया है,
मिसल गढ़ी का एक चमार का लड़का
काजीपुरा के
एक जाट के छोरे से
अड़ गया है।
तुरत-फुरत स्कूल के
सारे सवर्ण छात्र
गोलबंद हो जाते,
कई दलित छात्रों के हाथ-पैर टूटते
और फिर
झगड़ा करने के जुर्म में
हम ही स्कूल से
‘रेस्टीकेट’ कर दिये जाते।[2]
यह ऐतिहासिक सत्य है कि सवर्णों के गढ़ में और उनकी दलित-विरोधी व्यवस्था में दलितों ने प्रायः चुप रहकर और बरदाश्त करके ही अपने विकास की सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। यदि वे आपा खो देते, तो आज जितने शिक्षित हैं, उसके आधे भी नहीं पढ़ पाते। हालांकि सवर्ण उन्हें इसीलिये अपमानिक करते थे कि वे ‘आपा’ खोयें, पर दलितों को उनके अभिभावकों ने समझाया हुआ था कि उन्हें इसी विरोधी माहौल को झेल कर आगे बढ़ना है, यदि तुम आपा खो बैठोगे, तो अनपढ़ ही रह जाओगे। और, निस्संदेह, जिन दलितों ने अपमान बरदाश्त नहीं किया, वे अपमान करने वाले सवर्ण अध्यापकों और छात्रों को मार-पीट कर भाग आये और अनपढ़ ही रह गये। इन गरीब दलितों को सवर्णों की व्यवस्था में क्या-क्या झेलना पड़ा, इसका मार्मिक वर्णन जयप्रकाश कर्दम ने ‘बेमानी है आजादी’ कविता में किया है। यथा–
नहीं निकल सकता जो आज भी
पहनकर नये कपड़े
नहीं निकल सकती जिसकी
घोड़ी पर बारात
नहीं बैठ सकता जो आज भी
सवर्णों के सामने खाट पर
साठ साल का बूढ़ा भी
दुध-मुंहे बच्चों तक को
मिमिया कर कहता है ‘बाप’।
नहीं कर सकता
अपनी इच्छा और पसंद का काम।
छोटे से कर्ज के बदले
लिख देता है
कई पीढ़ियों की जिन्दगी
साहूकार के नाम।
गांव की पंचायत है जिसकी सुप्रीम कोर्ट
जी रहा है जो स्वराज में भी
गुलामों सी जिन्दगी।[3]
डॉ. आंबेडकर ने इन पाबंदियों को ‘हिंदुओं का कोड’ कहा है, जो गांव में दलित जातियों पर सवर्णों द्वारा थोपा गया था। इस कोड का उल्लंघन करने पर, दलितों को कठोर दंड दिया जाता था। यह दंड अक्सर सामूहिक रूप से दलितों को दिया जाता था, भले ही कोड का उल्लंघन किसी एक दलित ने किया हो।[4]

डॉ. आंबेडकर ने इस कोड का उल्लेख आजादी से पूर्व की स्थिति में किया है, पर जयप्रकाश कर्दम ने इन सारी पाबंदियों का अनुभव उस समय किया है, जब भारत अपनी आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहा था। इसलिये, उन्होंने कविता के अंत में लिखा–
बेमानी हैं उसके लिये
आजादी और लोकतंत्र की बातें
व्यर्थ हैं संसद और संविधान
नहीं चाहिए उसे
नीति और धर्म की शिक्षा
नहीं चाहिए अध्यात्म का ज्ञान
उसे चाहिए रोटी और सम्मान।[5]
दलित के घर में गरीबी की क्या दशा थी और इसमें भी मुक्ति की जिजीविषा को किस तरह जिंदा रखा जा रहा था, उसका विशद वर्णन हमें कर्दम की ‘लालटेन’ कविता में मिलता है। कवि कहता है–
यूं गांव के दूसरे घरों में
बिजली थी, लेकिन
हमारे घर में सिर्फ यही लालटेन थी
यही लालटेन ‘दीए’ का काम करती
इसी लालटेन के उजाले में मां
काम से लौटकर/ गीले सूखे उपले
या लकड़ियों में धूं-धूंकर
सांझ का खाना पकाती
इसी लालटेन के उजाले में
हम सब खाना खाते।[6]
लालटेन का संबंध मां से भी कवि ने जोड़ा है–
इसी लालटेन की रोशनी में बैठकर मां
फटे-उधड़े कपड़ों को
हाथ से सिलती
घर में एक-एक पैसे की तंगी और
हफ्तों बिना छुकी-भुनी सब्जी भी
घर में नहीं बनने के बावजूद मां
लालटेन के लिये तेल की व्यवस्था
जरूर करती थी
कभी-कभी भूखी भी रह जाती थी
ऐसा कई बार हुआ था
पर तेल के अभाव में
घर में लालटेन नहीं जली हो
ऐसा कभी नहीं हुआ था।[7]
मां ही रोज शाम को लालटेन की चिमनी साफ करती थी। कवि ने मां के इस नियमित कार्य को पढ़ाई-लिखाई से भी जोड़ा है। यथा–
हम को वह
सिर्फ पढ़ने के लिये कहती
पढ़ाई-लिखाई ही तुम्हारी पूंजी है
पढ़-लिख लोगे तो कहीं
अच्छा हिल्ला पा जाओगे
नहीं तो तसले ढोवोगे
दूसरों की गुलामी करोगे।[8]
बच्चे पढ़-लिख गये, अच्छा हिल्ला पा गये, तसले ढोने से बच गये। इस उत्थान में सचमुच मां की महती भूमिका है। पर क्या मां को भी मुक्ति मिली। कवि ने यहां कविता को एक दूसरा मार्मिक मोड़ दिया है। भाइयों को सरकारी नौकरी मिल गयी। वे गांव छोड़कर शहर में जाकर रहने लगे। बहनें भी शादी होकर अपने-अपने घर चली गयीं। एक मां ही गांव में रह गयी। बेटों, बहुओं, नाती-पोतों सबसे अलग गांव के उस टूटे-फूटे घर में मां निपट अकेली है। कवि कहता है–
साल-छह महीने में
कोई भाई चला जाता है
सौ-दो सौ रुपये
या एकाध जोड़ा कपड़ा देकर
अपना कर्त्तव्य निभा आता है,
बाकी के दिन
वह भूखी रहती है कि नंगी
बीमार रहती है कि परेशान
भाइयों में से कोई भी
जाकर उसे नहीं देखता है
सबके जीवन में सवेरा है
लेकिन मां की जिंदगी में
आज भी अंधेरा है।[9]
इस दलित कविता ने ‘मां’ की वेदना को जो अमूर्त शब्द दिये हैं, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यह किसी एक दलित मां की पीड़ा नहीं है। वरन् अधिकांश दलित मांओं की जिंदगी के हिस्से में यही अंधेरा आया है। जयप्रकाश कर्दम ने इस कविता के माध्यम से उन दलित बेटों को संदेश दिया है, जो गांव की गरीबी से निकलकर अमीरी में आने के बाद मां को अपने जीवन से बाहर कर देते हैं।
कर्दम के संग्रह की कई कविताएं अपने आप में पूर्ण खंड-काव्य हैं। इनमें ‘कलिया की मौत’, ‘अक्करमासी’, ‘आज का रैदास’ उल्लेखनीय हैं। ‘कलिया की मौत’ में कवि ने एक दलित मां का वर्णन किया है, जो अपने पढ़े-लिखे हिल्ले से लगे बेटों की उपेक्षा से बेमौत मर जाती है। इस कविता में एक मां के आत्मसंघर्ष का चित्रण है। इस मां का नाम कलिया है, जिसका पति भरी जवानी में मर जाता है। दो साल का बेटा उसकी गोद में है, जिसकी बरबादी के डर से वह पुनर्विवाह नहीं करती है, जबकि उसके घर-गांव के लोग उस पर दबाव बनाते हैं कि अकेले किस तरह जिंदगी जियेगी और बेटे को पालेगी। लेकिन कलिया ने किसी की नहीं सुनी–
सह जिंदगी की त्रासदी, वैधव्य का दुख झेलकर।
बेटे को पाला लाड़ से कलिया ने हंसकर खेलकर।
घास खोदी, भैंस पाली, की मजूरी भी, मगर।
न कभी वह हार मानी, न कभी भटकी डगर।।[10]
बेटा बड़ा हो गया। पढ़-लिखकर नौकरी में आ गया। शादी भी हो गयी और वह पत्नी के साथ शहर में जाकर रहने लगा। मां गांव में अकेली रह गयी। शुरु में बेटा हर महीने मां से मिलने आता। पर, बाद में धीरे-धीरे उसका भी मिलने आना कम हो गया। एक दिन मां ने बेटे से कहा कि अब उससे अकेलापन नहीं सहा जाता। उसे भी अपने साथ शहर ले चल। इस पर बेटे को अपनी तथाकथित ‘हाई सोसाइटी’ का भय सताने लगता है। वह मां से कहता है–
साथ तो मैं ले चलूं लेकिन रखूं तुझको कहां?
ऊंची-ऊंची जातियों के लोग रहते हैं वहां,
सभ्य शिक्षित, हाइजेंटरी लोग, सब फारवर्ड हैं।
लेकिन मां तू तो निरी अशिक्षित और बैकवर्ड है।
इंगलिश हैं सब बोलते हिंदी उन्हें भाती नहीं।
लेकिन मां तुझको तो एबीसी भी है आती नहीं।
गर लोग पायेंगे तुझे अज्ञान की अनगढ़ धरा।
शान क्या मेरी रहेगी सोच मां तू ही जरा।।[11]
निस्संदेह, यह कल्पना हवाई नहीं है। हीनभावना के शिकार ऐसे दलितों की आज भी कमी नहीं है। कवि ने जिस दौर के दलित युवकों के मानसिक यथार्थ का यहां चित्र प्रस्तुत किया है, वह वस्तुतः दलितों के मध्यम वर्ग में रूपांतरण का दौर था। इसी समय एक नयी दुनिया में प्रवेश के साथ उनका संस्कृतिकरण भी हो रहा था। शहरों में वे जिस बड़ी समस्या से जूझ रहे थे, वह मकान की समस्या थी। वे जाति बताकर सवर्णों की बस्तियों में मकान नहीं पा सकते थे। उन्हें मकान लेने के लिये जाति छिपानी पड़ती थी। यह भी एक बड़ा कारण था, उनको गांव से अपनी दूरी बनाने और अपने अशिक्षित मां-बाप को अपने साथ न रखने का। उस समय जाति उनके लिये आज की तरह स्वाभिमान की चीज न थी। आज समय बदल गया है। दलित अस्मिता के इस दौर में आज न वह हीनभावना है दलितों में और न जाति छिपाने की उन्हें जरूरत पड़ती है। यह परिवर्तन डॉ. आंबेडकर के आंदोलन से आया है, जिसे कांग्रेस की राजनीति ने भरसक दबाने का काम किया था और उसकी हरिजन-नीति ने तो ऐसे हालात पैदा कर दिये थे कि डॉ. आंबेडकर की बात करने मात्र से दलितों की नौकरी खतरे में पड़ जाती थी। कलिया का बेटा इसी हीन ग्रंथी का शिकार है। पर, मां में कोई ग्रंथी नहीं है। उसे इतना मालूम है कि पढ़ाई-लिखाई आदमी को इंसान बना देती है। इसलिये बेटे की बात सुनकर कलिया को आघात लगता है–
उठ गया विश्वास उसका आज अपने लाल पर,
रोयी थी कलिया बहुत उस रात अपने हाल पर।[12]
बेटा शहर चला गया और फिर न लौटा। ममता तड़पती रही और बेटा ‘फारवर्ड’ बनकर मौज लेता रहा। कवि ने एक और चित्र प्रस्तुत किया कि मां ने–
एक दिन सपने में देखीं पुत्र की परछाइयां।
डर गया कलिया का मन, थी बज रही शहनाइयां।।
देखे कैसे पुत्र को जाकर, नहीं कोई उपाय।
चैन बिन देखे नहीं, व्याकुल थी कलिया, असहाय।।
जिंदगी भर की तपन, थी इंद्रियां भी थक गयीं।
तीन दिन ज्वर से तड़प, एक रोज कलिया मर गयी।।[13]
लोक-विश्वास है कि सपने में शहनाई बजते हुए या बारात चढ़ते हुए देखना किसी अपने की मौत का संकेत होता है। कलिया को सपने में शहनाईयां बजती दिखायी दीं, तो वह अपने पुत्र को देखने के लिये व्याकुल हो गयी। यह मां की ममता थी, जो बेटे के अनिष्ट की आशंका से तड़प रही थी। पर, तीन दिन बुखार में तड़पने के बाद उसी की मौत हो गयी। इस दलित मां के दुखद अंत पर कवि ने लिखा–
सोच ग्लानि से गलित हूं कलिया के अंजाम पर।
क्या यही पाया है हमने उन्नति के नाम पर।।
माता को माता कहने में भी शर्म आती है जिसे।
लानत है ऐसे पुत्र को, धिक्कार है शत-शत उसे।।
पर क्या कहें मां-बाप के अहसास को, विश्वास को।
ढो रहे अपने ही कंधों पर हैं अपनी लाश को।।[14]
दलित स्त्री की गरिमा को व्यक्त करने वाली कर्दम की एक कविता ‘अक्करमासी’ है। संभवत: यह कविता मराठी दलित लेखक शरण कुमार लिंबाले की आत्मकथा ‘अक्करमासी’ पढ़ने के बाद लिखी गयी प्रतीत होती है, क्योंकि ‘अक्करमासी’ शब्द मराठी भाषा का है, हिंदी में यह शब्द नहीं चलता। कोई हिंदी भाषी ‘अक्करमासी’ का अर्थ जानता भी नहीं, जब तक कि उसे बताया न जाय। इस कविता की आरंभ की पंक्तियां इस प्रकार हैं। यथा–
मुझे अक्करमासी कहकर
मेरा उपहास मत उड़ाओ
मेरे खून को मत खौलाओ
अपनी मां के कुकर्मों के कारण
नहीं हूं मैं अक्करमासी
मैं उसकी विवशता का परिणाम हूं।
पाटील की औलाद होकर भी
बाप से बेनाम हूं।[15]
इस कविता में पाटील जमींदार है और ‘अक्करमासी’ का अर्थ है– अवैध संतान, जिसे आम भाषा में ‘नाजायज’ कहते हैं। जमींदार द्वारा दलित स्त्री के यौन शोषण के के परिणामस्वरूप जिस ‘अक्करमासी’ का जन्म हुआ, उसे मां ने पाला-पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया-लिखाया और वह एक कवि के रूप में विख्यात हुआ। दुनिया उसे भले ही अक्करमासी कहे, पर वह अपनी मां को उसके लिये दोषी नहीं मानता है। वह उसके लिये उन सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को उत्तरदायी मानता है, जो भारतीय सामंतवादी व्यवस्था ने दलित जातियों के लिये उत्पन्न की थीं। इसलिये कवि कहता है–
व्यभिचारिणी होती मेरी मां
तो अपने जारकर्म की निशानी को
लेकर नहीं घूमती
वह अपना गर्भ गिरवाती
या पैदा होते ही मुझे चुपके से
किसी मंदिर की दहलीज पर
या कूड़े के ढेर पर फेंक आती।[16]
कर्दम ने इस कविता के द्वारा दलित लेखक डॉ. धर्मवीर को भी जबाव दिया है, जिनके चिंतन में दलित स्त्रियां रखैल, चरित्रहीन, कुलटा और व्यभिचारिणी के रूप में मिलती हैं। कर्दम ने शायद डॉ. धर्मवीर के लिये ही कविता के अंत में ये पंक्तियां कही हैं–
व्यभिचारिणी होती मेरी मां
तो खूब गुलछर्रे उड़ाती
नये-नये कपड़े और गहने पहन
मांग-पट्टी निकाल कर रहती
भूखी-नंगी रह
वह दर-दर की ठोकरें नहीं खाती
दो मुट्ठी अनाज के दानों के लिये
किसी पाटील के घर या खेत में
बेगार करने नहीं जाती।[17]
कर्दम ने डॉ. आंबेडकर के दर्शन को अपनी कविता का आधार बनाया है। इस वैचारिकी की उनकी एक कविता ‘आज का रैदास’ है। निश्चित रूप से यहां ‘रैदास’ शब्द एक मोची के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जो पंद्रहवीं शताब्दी के सन्त रैदास को भी अभिव्यंजित करता है। किंवदंतियों में संत रैदास जूते बनाने का काम करते थे, पर कर्दम का रैदास जूतियां गांठता है, अर्थात् फटी हुई जूतियों की मरम्मत करने का काम करता है। इस आधार पर इस कविता में संत रैदास और मोची रैदास की कोई तुलना नहीं है। यह कविता मोची रैदास की भविष्योन्मुखी दृष्टि को जरूर अभिव्यक्त करती है। इस कविता की तुलना यदि किसी कविता से हो सकती है, तो वह धूमिल की ‘मोची राम’ कविता से हो सकती है। मेरी दृष्टि में यदि कर्दम की ‘आज का रैदास’ कविता को धूमिल की कविता ‘मोची राम’ की तुलना में पढ़ा जायगा, तो जाति और वर्ग चेतना की दृष्टि यहां साफ हो जाएगी। धूमिल की कविता में मोची राम सिर्फ एक मोची है। उसके सिवा कुछ नहीं है। उसकी दृष्टि सिर्फ लोगों के फटे जूतों पर रहती है और उसकी दृष्टि पेशेवर है। उसके और आदमी के बीच सिर्फ जूता है और कुछ नहीं है। उसकी आंखों में न कोई सपना है और ना वह अपना कोई भविष्य गढ़ता है।
धूमिल की कविता ‘मोची राम’ में आरंभ की ये पंक्तियां दृष्टव्य हैं–
बाबू जी, सच कहूं मेरी निगाह में
न कोई छोटा है
न कोई बड़ा है
मेरे लिये हर आदमी एक जोड़ी जूता है।[18]
लेकिन कर्दम की कविता ‘आज का रैदास’ में मोची का संघर्ष सिर्फ पेट के लिये नहीं है, वरन् अपने सपनों को पूरा करने के लिये भी है। इस कविता में आरंभ की ये पंक्तियां विचारणीय हैं–
सड़क के किनारे
जूती गांठता है रैदास
पास में बैठा है उसका
आठ वर्ष का बेटा पूसन।[19]
पास बैठा पूसन रैदास की अगली पीढ़ी है। वह उसका भविष्य है, जिसका सपना है–
चाहता वह खूब पढ़ना
और पढ़-लिखकर आगे बढ़ना।[20]
पर, पढ़े कैसे? दरिद्रता ने उसका रास्ता रोक रखा है। कवि कहता है–
यूं उसका नाम
सरकारी स्कूल में दर्ज है
लेकिन वहां का भी
क्या कम खर्च है
कभी किताब कभी कापी और
कभी कपड़ों के अभाव में
नहीं जा पाता है पूसन प्रायः स्कूल
और आ बैठता है यहां
अपने पिता के पास।[21]
जिस जगह बैठकर पूसन के पिता जूतियां गांठते हैं, वहां कई पब्लिक स्कूलों की बसें आकर रुकती हैं। उनमें से तरह-तरह की ड्रेस पहने और कंधों पर बैग लटकाये संभ्रांत परिवारों के बच्चे उतरते हैं, जिन्हें देखकर पूसन की आंखों में सपने तैरने लगते हैं। वह अपने पिता से पूछता है–
पिताजी, क्यों नहीं बनाते तुम भी
मेरे लिये/ इनके जैसे कपड़े
क्यों नहीं भेजते मुझको भी
इनके ही जैसे स्कूल?[22]
पूसन के ये शब्द भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार करते हैं। इनमें हम डॉ. आंबेडकर के इन विचारों की झलक भी देख सकते हैं, जिनमें उन्होंने कहा था कि ‘भारत ने सिर्फ राजनैतिक लोकतंत्र स्वीकार किया है, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अभी भी यथास्थिति बनी हुई है।[23] कवि ने इसी विरोधाभास को पूसन और पब्लिक स्कूलों के बिंब में उतारा है। भारत में दोहरी शिक्षा प्रणाली अमीर और गरीब के लिये बनायी गयी प्रणाली है, जो विशेष रूप से दलित जातियों को पिछड़ा बनाये रखने की सुनियोजित नीति है। दलित जातियों के बच्चे भी अच्छे पब्लिक स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, तभी उनका समान विकास हो सकता है। आज के रैदास अपने पूसनों का सपना कैसे पूरा करें, जबकि उनकी गरीबी सरकारी स्कूलों की शिक्षा का खर्च भी उठाने में समर्थ नहीं है? कविता का अंत रैदास के इस आक्रोश से होता है–
अपनी भूख और बेबसी को
कोसता है, और
ईर्ष्या, ग्लानि और क्षोभ से भरकर
व्यवस्था के जूते में
आक्रोश की कील
ठोक देता है।[24]
यहां पुनः धूमिल की कविता उल्लेखनीय हो जाती है। उनकी कविता में मोची राम जूते में इसलिये कील ठोक देता है, क्योंकि जूते का मालिक उसे कम मजदूरी देता है। वहां वह पूरी तरह पेशेवर है। आक्रोश वहां भी है, पर वह व्यवस्था पर नहीं है। दलित कवि की कविता में रैदास व्यवस्था की जूती में कील ठोकता है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि वह उसे अपने वर्ग के लिये एक क्रूर व्यवस्था मानता है। यहां जाति-चेतना भी है और वर्ग-चेतना भी और यही दलित कविता का आंबेडकरवादी आधार है।
भारत में पूंजीवादी व्यवस्था ने विकास का मॉडल या विकास की संस्थाएं इस तरह विकसित की हैं कि उनका लाभ उच्च वर्गों को ही मिलता है। मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रबंधन की सारे संस्थान इसी तरह के हैं, जो उच्च वर्गों के हित में कायम किये गये हैं। दलित-पिछड़े वर्गों ने जब इन संस्थानों में अपने लिये आरक्षण की मांग की, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में उच्च वर्गों के लोग दलितों के विरोध में उग्र हो गये। धरना-प्रदर्शन, तोड़-फोड़, आगजनी, यहां तक कि सवर्ण छात्रों से आत्मदाह तक उन्होंने कराये। अखबारों और टी.वी. चैनलों पर विरोध पर बहसें चलाने से लेकर न्यायालयों में उसे रोकने के लिए याचिकाएं तक दाखिल की गयीं। नवें दशक के अंत तक पूरे देश का सामाजिक वातावरण दलित-विरोधी हो गया था।
‘गूंगा नहीं था मैं’ संकलन में ‘आरक्षण’ कविता इसी समय की है, जिसमें कर्दम ने दलितों और सवर्णों के आरक्षण पर तार्किक सवाल उठाये हैं। यथा–
तुम्हें खटकता है
सरकारी नौकरियों में मेरा आरक्षण
मेडिकल या इंजीनियरिंग कालेजों में
मेरा एडमिशन।
क्या कैपिटेशन फीस
यानी रिश्वत देकर एडमिशन लेना
उचित है?
क्या मंदिर की मोटी कमाई पर
ब्राह्मणों का एकाधिकार उचित है?
क्या यह सब आरक्षण नहीं है?[25]
सवर्णों के एकाधिकारवाद को तोड़ने के लिये दलित कविता का संघर्ष बहुत व्यापक है। यह व्यापकता हमें ‘मेरे अधिकार कहां हैं’ और ‘लाठी’ कविताओं में भी दिखायी देती है। ‘मेरे अधिकार कहां हैं’ कविता में कवि हिंदुओं से पूछता है–
शासन-सत्ता पर काबिज तुम
थाने-तहसील तुम्हारे हैं
तुम जाति-दंभ के अभिमानी
मुझसे घृणा व्यापार करो
वैषम्य-द्वेष के बीहड़ में
मैत्री की मीनार कहां है?[26]
कवि की दृष्टि में राष्ट्रवाद और रामराज्य का नारा भी सवर्णों के वर्चस्ववाद का नारा है। यथा–
तुम चाहो राम-राज्य आये
तुम श्रेष्ठ, शूद्र मैं बना रहूं
तुमको सारे अधिकार रहें
मैं वर्जनाओं से लदा रहूं।[27]
यहां ‘श्रेष्ठ’ शब्द सब तरह से ‘योग्य’ और ‘शूद्र’ शब्द ‘अयोग्य’ के अर्थ में आया है। और इस अर्थ में यह कविता शासन-सत्ता और विकास के क्षेत्रों में सवर्णों के वर्चस्ववाद पर तीखा प्रकार करती है। ‘लाठी’ कविता में कवि ने इस वर्चस्ववाद की पीड़ा का चित्रण किया है। गांव में खेती की सिंचाई के लिये चलने वाले पानी पर दलित के हक पर भी सवर्ण अपना ही हक समझता है और विरोध करने पर उसकी लाठी जुल्म करती है। कवि ने जुल्म का एक सजीव बिंब इस कविता मे उतारा है। यथा–
पानी का बार हमारा था
लेकिन, मढ़ैया का बदनी जाट
काट ले गया था पानी जबरन
अपने खेत में
प्रतिकार किया था मेरे पिता ने
तो उनकी कमर पर पड़ी थी लाठी
बहुत दिन तक
उस लाठी की चोट से
मेरे पिता और परिवार की
कमर दुखती रही।
मरते दम तक
उनकी कमर से
उस लाठी का दर्द नहीं गया।[28]
अगर दर्द चला जाता तो जुल्म की अनुभूति फिर कहां रहती? इस दर्द ने ही तो दलितों को यह अनुभूति दी कि इस देश में रहते हुए भी वे ‘पराये’ हैं, नागरिक होते हुए भी अनागरिक हैं और मनुष्य होते हुए भी गुलाम जैसे हैं। इस अनुभूति ने दलितों की अगली पीड़ी को विद्रोह का पाठ पढ़ाया। इस विद्रोह को कवि ने ‘दमन की दहलीज पर’ कविता में व्यक्त किया है। इस कविता में अनेक दलित-हत्याकांडों की झलक मिल जाएगी। सवर्ण शोषकों द्वारा दलितों के बर्बर दमन का लोमहर्षक चित्रण करने के बाद कवि अंत में कहता है–
तमाम विरोधां और दबावों के बावजूद
जाति के जंगल का यह निरीह जीव
अपनी मुक्ति के लिये अड़ा है,
अपनी अस्मिता और अस्तित्व के लिये लड़ा है
और आज तमाम हौसलों के साथ
हाथों में खंजर लिये वह
दमन की दहलीज पर खड़ा है।[29]
जयप्रकाश कर्दम का कविता संकलन ‘गूंगा नहीं था मैं’ तीन क्षणिकाओं से समाप्त होता है, जिनमें पहली है, ‘जिंदगी’, दूसरी है ‘भूख’, तीसरी है ‘सभ्यता’ और चौथी ‘आग’ है। इन चारों से ही दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र बनता है। जीवन है, तो ‘भूख’ है, भूख है तो संघर्ष है, जिसमें कमाकर खाना दलितों की ‘सभ्यता’ है और यही ‘सभ्यता’ दलित की आग है, जो उसे ऊर्जावान बनाती है।
ईश कुमार गंगानिया का कविता–संघर्ष
वर्ष 2000 में जिन दलित कवियों के कविता-संकलनों ने नये जीवन मूल्यों के साथ दस्तक दी, उनमें ईश कुमार गंगानिया का कविता संकलन ‘हार नहीं मानूंगा’ विशेष उल्लेखनीय है। गंगानिया अपने संघर्ष को जारी रखते हुए कहते हैं–
चाहे कितने ही बोए जायें बीज
डालने को आपसी फूट
कुचल दूंगा इन्हें
अंकुरित होने से पहले
कितनी ही दुर्गम हो जायें राहें
अपना संघर्ष-संकल्प नहीं त्यागूंगा।
मैं हार नहीं मानूंगा।[30]
भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय की व्यवस्थाएं आकर्षित करती हैं, लेकिन भारतीय समाज में दलित वर्गों और शोषितों के प्रति वही दासता-असमानता और अन्याय की व्यवस्था आज भी जीवित है। कवि इसके लिये संविधान को नहीं, द्विज शोषक वर्ग को दोषी मानता है। ‘कब तक चलेगा’ कविता में वह कहता है–
भारतीय संविधान मना चुका है
अपनी स्वर्ण जयंती भी
लेकिन आज भी
न्याय की आंख पर
पट्टी बंधी है
तभी तो इक्कीसवीं सदी में भी
द्विज ही बने हैं इसकी आंखें…[31]
कवि पूछता है–
आखिर न्याय को
अंधा बनाने का ढोंग
कब तक चलेगा?[32]
कवि उन दलित-हितैषियों को भी शोषकों में शामिल करता है, जो दलित की गरीबी और भूख के नाम से देश-विदेश की सरकारों से धन लेकर अपना पेट भर रहे हैं। ऐसी स्वयं सेवी-संस्थाओं को कवि ‘चक्रवात’ कविता में उन चालाक शिकारियों की संज्ञा देता है, जो दलितों के कंधों पर बंदूक रखकर शिकार करते हैं। यथा–
यह न युद्ध का
न संधि का, बल्कि
अपने कंधों से
शिकारियों की
बंदूकें हटाने का समय है।
दलित को आती है जरूर कुछ
देशी-विदशी भीख सी आर्थिक मदद,
यहां दिखने वाले चेहरे तो दलितों के
लेकिन
पाने वाले हाथ
किसी और के होते हैं।[33]
गंगानिया भारत की आजादी को पूंजीवादी तानाशाही का गुलाम मानते हैं, जिसने राज्य की न्याय और प्रशासन-संस्थाओं को दमनकारी बना दिया है। यदि देश में लाखों गरीबों के सिर पर छत नहीं है, अचानक झुग्गी-झोपड़ियां जलकर राख हो जाती हैं और नरसंहार होते हैं, तो इस सबके पीछे उन्हें पूंजीवाद का हाथ ही दिखायी देता है। इसी पूंजीवाद के विरोध में जनाक्रोश को व्यक्त करती उनकी कविता ‘क्यों न फड़फड़ाएं’ की ये पंक्तियां द्रष्टव्य हैं–
झूठे हैं वे लोग
जो कहते हैं
भारत आजाद है।
भारत गुलाम है आज भी
ब्राह्मणशाही और पूंजीवाद की तानाशाही का
यही तानाशाही
भारतीयों के झोपड़े जलवाती है
नरसंहार कराती है
बूथ कैप्चरिंग करा
सत्ता हथियाती है।
इसकी विलासिता
जन्म देती है पांच सितारा संस्कृति को,
जबकि दाने-दाने को मोहताज
जनता को झेलने पड़ते हैं
मौसम की मार
कर्जों का भार
ब्राह्मणशाही पूंजीवाद की
तानाशाही के हाथों
तिल-तिल हलाल होती
भारतीय अस्मिता पर
क्यूं न फड़फड़ायें मेरी बाहें?[34]
दलित कवि बंदूक की आग से बचते हैं। वे लोकतांत्रिक तरीके से क्रान्ति करने में विश्वास करते हैं। उनका संघर्ष अहिंसक है। वे व्यवस्था-परिवर्तन के लिये रक्तपात का रास्ता नहीं अपनाते, वरन् संवैधानिक संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं। इसके लिये जरूरी है मनुष्य को मनुष्यता का बोध कराना और भारत के सभी नागरिकों को उसके दायरे में प्रतिष्ठित करना। दलित कविता का 1900 से 2000 तक सौ वर्षों का जीवन इसी संघर्ष का जीवन है।
(समाप्त)
संदर्भ :
[1] गूंगा नहीं था मैं (कविता संग्रह)- जयप्रकाश कर्दम, अतिश प्रकाशन, हरिनगर, दिल्ली, संस्करण- प्रथम, 1997, पृष्ठ 36
[2] वही, पृष्ठ 36-37
[3] वही, पृष्ठ 24-25
[4] डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर : राइटिंग्स एंड स्पीचेज, वॉल्यूम 5,पृष्ठ 20-23
[5] गूंगा नहीं था मैं, उपर्युक्त, पृष्ठ 25
[6] वही, पृष्ठ 55
[7] वही, पृष्ठ 57
[8] वही, पृष्ठ 58
[9] वही, पृष्ठ 59-60
[10] वही, पृष्ठ 45-46
[11] वही, पृष्ठ 46-47
[12] वही, पृष्ठ 47
[13] वही, पृष्ठ 48
[14] वही
[15] वही, पृष्ठ 40
[16] वही
[17] वही
[18] संसद से सड़क (कविता संग्रह)- धूमिल, राजकमल प्रकाशन, दरियागंज, नयी दिल्ली, छठा संस्करण, 1998, पृष्ठ 37
[19] गूंगा नहीं था मैं, उपर्युक्त, पृष्ठ 52
[20] वही
[21] वही, पृष्ठ 52-53
[22] वही, पृष्ठ 53
[23] वही
[24] गूंगा नहीं था मैं, उपर्युक्त, पृष्ठ 54
[25] वही, पृष्ठ 15
[26] वही, पृष्ठ 41
[27] वही, पृष्ठ 42
[28] वही, पृष्ठ 43-44
[29] वही, पृष्ठ 35
[30] हार नहीं मानूँगा (कविता संग्रह)- ईश कुमार गंगानिया, अतिश प्रकाशन, हरिनगर, दिल्ली, प्रथम संस्करण- 2000, पृष्ठ 59
[31] वही, पृष्ठ 63-64
[32] वही, पृष्ठ 64
[33] वही, 74-75
[34] वही, 89-90
(संपादन : नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in