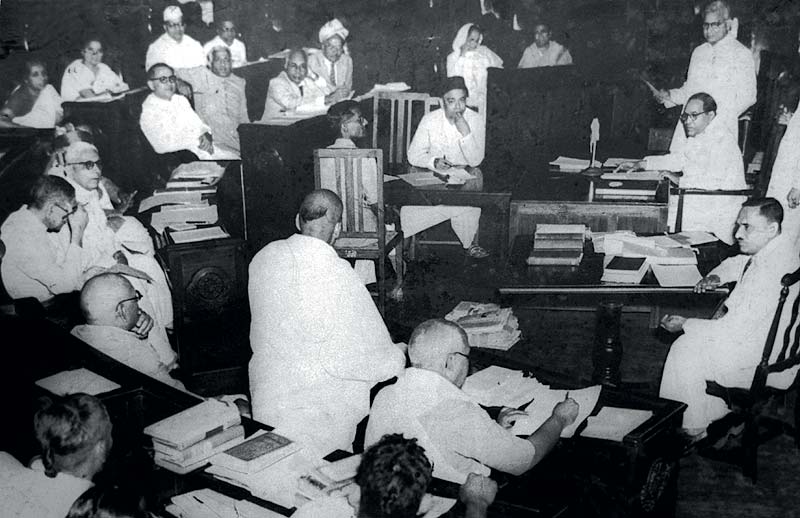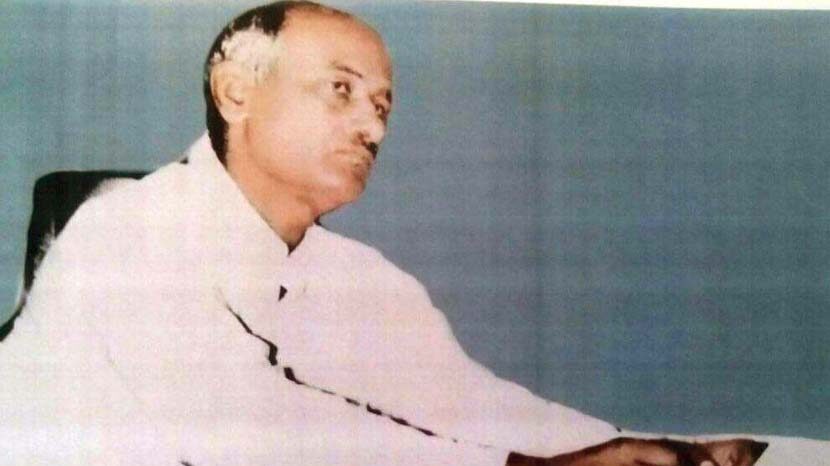महाराष्ट्र की प्रसिद्ध दलित लेखिका व सामाजिक कार्यकर्ता बेबी कांबले (1929 – 21 अप्रैल, 2012) उन महिला आंदोलनकारियों में रहीं, जिन्होंने डॉ. आंबेडकर के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। उनकी आत्मकथा ‘जिना आमुचा’ शीर्षक से 1986 में प्रकाशित हुई। मराठी से इसका अंग्रेज़ी अनुवाद ‘दी प्रिजंस वी ब्रोक’ शीर्षक से माया पंडित ने किया है तथा इसका प्रकाशन ओरिएंट ब्लैक स्वान ने किया है।
इस पूरी किताब को आत्मकथा कहने की बजाय महार समुदाय की जीवनी कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि यह बेबी कांबले के निजी जीवन के बारे में कम, बल्कि समूचे महार समुदाय के जीवन की कहानी अधिक कहती है। किताब के अंत में किताब की अनुवादक माया पंडित द्वारा बेबी कांबले का लिया गया एक साक्षात्कार भी प्रकाशित है। यह साक्षात्कार बेबी कांबले के व्यक्तिगत जीवन यात्रा की एक झलक देता है। इसमें बेबी कहती हैं– “इस किताब में मैंने अपने समुदाय के अनुभव को लिखा है। मेरे समुदाय की पीड़ा ही मेरी पीड़ा बन गई।”
इस किताब के कुछ अनूदित (इन अंशों का भावानुवाद इस आलेख की लेखिका ने स्वयं किया है) अंश यहां उद्धृत हैं–
“मेरे पिता का नाम पंढरीनाथ था। मेरे पिता एक ठेकेदार थे। लेकिन वह इतने उदार थे कि लोग उन्हें कर्ण कहते थे। उन्हें धन का कोई लोभ नहीं था। वह लोगों को खुश देखना चाहते थे …
“ठेकेदार बनने की भी उनकी एक मजेदार कहानी है। 1918 में फल्टन में एक नहर बनाने की योजना बनी। लेकिन काम शुरू करने से पहले कंटीली झाड़ियों का मैदान साफ़ करना था । मेरे पिता को ठेका मिला और उन्होंने उस काम को संतोषजनक तरीके से पूरा किया …
“उन दिनों औरतों को घर में बंद रखने का रिवाज़ था। एक परिवार जितना ज़्यादा अपने घर की औरतों को क़ैद करके रखता, उसका ‘सम्मान’ उतना ही ज़्यादा होता। मेरे पिता भी आई (मां) को पिंजरे में चिड़िया की तरह घर में बंद करके रखते थे… वह जो भी पैसे कमाते, उसे गंवा देते। इसलिए मां अक्सर उनसे झगड़ा करती कि ‘तुम्हारे इतना कमाने का क्या फायदा कि गांव में हमारे पास अपनी एक झोपड़ी तक नहीं है।… हमारे बच्चे क्या करेंगे?’ तब पिता उन्हें ‘शिक्षित’ करने का प्रयास करते। कहते– पैसे इकट्ठा करने से ख़ुशी नहीं मिलती। देखो, मैं कितना मेधावी हूं। बच्चे मां-बाप से सीखते हैं। तुम उनकी चिंता मत करो।
“मेरी मां इतनी घुटन में रहती और शोषित महसूस करती। संभवतः इसी वजह से वह बहुत असंवेदनशील और दूसरों के प्रति क्रूर-सी हो गई थी कि उनके किसी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। …

“वीरगांव के महारवाड़ा (बेबी कांबले अपने नाना-नानी के घर रहती थीं) में हमारे समुदाय (महार) के 15-16 घर थे। तीन-चार घर छोड़ बाकी घर गरीबों में भी गरीब थे। (वे सभी हिंदू धर्म को मानने वाले थे) …
“नौ साल की उम्र के बच्चे सींक की तरह दुबले-पतले थे। जब लड़कियों की माहवारी शुरू होती, मांएं अपनी गठरी से कोई गंदा चिथड़ा निकालतीं और किसी तरह उनके शरीर में लगा देतीं तथा उन्हें ढंक देतीं। कपड़े पहनने का उनका यही ढंग था। उनके कमर पर कोई चिथड़ा बांध दिया जाता और उसका एक सिरा पैरों के बीच से निकाल कर पीछे कमर पर बंधे उसी चिथड़े के सहारे खोंस दिया जाता… इस अवसर पर मरी देवी [मरी देवी कोई स्थानीय देवी थी] को ब्लाउज का कपड़ा चढ़ाया जाता। आई ने भी बड़ी मुश्किल से इसके लिए कपड़ा संभाल कर रखा था। उसे ब्लाउज की तरह सी दिया जाता। बड़ी होती लड़कियों की यही यूनिफ़ॉर्म होती। लड़कों के लिए भी उनके नंगेपन को ढंकने के लिए एक चिथड़ा होता था। इन चिथड़ों में जुंएं और लीखें (लार्वा) भरी होतीं, जिससे वे सारे दिन खुजली करते रहते। …
“हरेक घर में एक चबूतरे पर मिट्टी या पत्थर का बना पूजा स्थल होता था। इन चबूतरों के आकार से घर की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी। …
“आषाढ़ का महीना महारों का अपना महीना होता था। इस महीने घरों की लिपाई-पुताई होती, धार्मिक स्नान और अनुष्ठान होते। साल के 11 महीने महारों के लिए अभिशाप होते तो आषाढ़ का महीना महारों के लिए पवित्र महीना होता था। एक महीने के कर्मकांड से महारों के शोषित आत्मा को शुद्ध किया जाता। ढेर सारी पूजा-अर्चना के जरिए प्रार्थना की जाती कि भगवान उनके कष्टों को हर लेंगे। …
“आषाढ़ के महीने के मंगलवार, शुक्रवार, पूर्णिमा और अमावस्या को महार औरतों और ख़ास तौर पर बेचारी बहुओं के लिए बहुत ख़ास होते। इस दिन सास के द्वारा बनाई गई पूरनपोली उन्हें खाने को मिलती। इसी समय औरतों पर देवी आती। ढोल पर थापों के प्रहार तीखे होते जाते तब ‘देवी’ और भी विक्षिप्त होती जाती। बच्चे ‘देवी’ के इर्द-गिर्द तमाशा देखते और नाचने लगते। गांव के बड़े-बूढ़े सब देवी से प्रार्थना करते कि क्षमा कर दो देवी, उस औरत को छोड़ दो। इस तरह औरतों पर ‘देवी’ आती और गांव वाले चढ़ावा चढ़ाते तब कहीं जाकर ‘देवी’ क्षमा करती। सामूहिक भोज के साथ आषाढ़ का महीना पूरा होता। …
“इस तरह पूरा समुदाय भयंकर अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ा रहता। सवर्णों ने हम निम्न जातियों को कभी भी ज्ञान हासिल नहीं करने दिया। पीढ़ी-दर-पीढ़ी हमारा समुदाय अंधविश्वासों में डूबा रहा। फिर भी हम तुम्हारे हिंदू धर्म को मानते रहे और आस्थापूर्वक तुम्हारी सेवा करते रहे। …
“हमने कभी तुम्हारे ख़िलाफ़ विद्रोह नहीं किया … जब तुम पूजा करते थे, हमने कभी अपनी पूजा नहीं की … तुम गाय को पवित्र मानते हो, हमने कभी उसका अपमान नहीं किया … हमने हमेशा हिंदू धर्म के आदेशों का पालन किया … परंपराओं का पालन किया … हमने कभी भी उसका उल्लंघन नहीं किया … हम तुम्हारे घर में रहते, लेकिन एक बूंद पानी नहीं पीया … हमने कभी भी तुम्हारे रास्ते को नहीं काटा … हमने तय किया कि हम तुम्हारी सभ्यता और संस्कृति की सेवा करेंगे और करते रहे … लेकिन तुम हमेशा हमारे लिए क्रूर और अन्यायी बने रहे … हम भूसी की रोटी खाते रहे और कल्पना करते रहे कि हम पकवान खा रहे हैं … हमने अपनी झोपड़ियों को ही महल समझा … गरीबी को समृद्धि समझा … हम सपना देखते रहे और बादलों के आसरे झूला झूलते रहे कि हमारे स्याह सपनों में उम्मीद की कोई किरण तो कभी-न-कभी आएगी ही …
“महारवाड़ा में बच्चे अपनी देखभाल स्वयं करते, जब उनकी मांएं काम पर चली जातीं तो उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं होता था। कोई भी देखने वाला नहीं होता था कि वे बच्चे जिंदा हैं कि मर गए। अगर किसी ने एक बच्चे को पत्थर मार दिया और खून बहने लगता तो उस जगह पर तवे की कालिख लगा दी जाती और बच्चा फिर से खेलने दौड़ जाता।… बच्चे घर में जाकर भाखरी (रोटी) तलाशते और नाकाम रहते। मेरी आजी (नानी) अतिरिक्त बासी रोटी रखती और ज़रूरतमंद को देती। भूखे बच्चे बासी रोटी नमक-प्याज़ के साथ खाते। …
“औरतें जंगल से लकड़ी इकट्ठा करतीं और गांव में बेचने जातीं। वे उस सड़क से नहीं जा सकती थीं, जिसके ऊपर सवर्ण चलते थे … अगर सामने से कोई आता दिख जाता तो महार लोगों को सड़क से नीचे कंटीली झाड़ियों में उतरना पड़ता … सर झुकाकर कहना पड़ता ‘पांय लागूं सरकार’। ऐसा दिन भर में कई-कई बार कहना होता … अगर कोई नई ब्याहता या कोई और ऐसा नहीं करती तो उसके ऊपर क़यामत टूट पड़ती। वह मालिक सीधे चावड़ी में पहुंच जाता और गालियां देने लगता। उस औरत के घर के लोग बार-बार दया की भीख मांगते। …
“तुम महारों की हिम्मत बहुत बढ़ गई है … अपनी औकात भूल गए हो … मुफ्त की रोटी खाते हो … अगली बार ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा … इस तरह वे धमकाते। … सवर्ण मालिक तो चला जाता पर सभी उस बहू के ऊपर टूट पड़ते।
“महार औरतें जब गांव में जातीं तो अक्सर हम बच्चे भी उनके साथ जाते। औरतें जो फटी-चिथड़ी साड़ी पहनतीं, उसमें बार्डर या तो होता नहीं था या फिर होता तो उसे ऐसे पहनतीं कि बॉर्डर नहीं दिखाई देना चाहिए। यदि बार्डर वाली साड़ी हो तो वे उसे प्लेट की तह में ढंककर कर रखतीं। केवल सवर्ण औरतें ही चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी पहन सकती थीं। अपने आपको बचते-बचाती वे अलग-अलग जातियों के मोहल्ले में लकड़ी बेचते हुए ब्राह्मणों के मोहल्ले में लकड़ी लेकर पहुंचतीं और दूर से ही आवाज़ लगातीं। ब्राह्मण औरतें तरह-तरह से मोलभाव करतीं। वे उन्हें तरह-तरह के अपशब्द बोलतीं। हम बच्चों को डांटती कि हम उनकी चीज़ों को अपवित्र कर देते हैं। …
“कितना घृणित है यह हिंदू धर्म! मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम समृद्धि और धन का मज़ा नहीं उठाते तुम महारों का खून चूस कर मज़ा लेते हो! महार औरतों के खून और पसीने से जलावन की लकड़ियां भींगी रहतीं।… खेतों में उपजने वाला मक्का महारों के पसीने में डूबा होता, जिससे उनका शुद्ध पकवान बनता।… जिन महलों में तुम रहते हो उनके गारों में महारों का खून और पसीना मिला रहता है… तब तुम क्या अशुद्ध नहीं होते? … ये सारे अपमान तुम्हारे धर्म ने हमें दिया है … लेकिन अब हम यह समझ गए हैं कि तुम्हारा धर्म कितना निरर्थक है। हमें जानवरों से इंसान बनाया है संविधान के निर्माता डॉ. आंबेडकर ने। …
“हमारी औरतें सारी जिंदगी धरती माता की सेवा में लगा देतीं। लेकिन जब वे स्वयं मां बनती हैं तो उन्हें क्या मिलता है? अपने पेट को बांध कर वे असहाय-सा जीवन बितातीं।… अमूमन सभी बेटियां पहली जचगी के लिए अपने मायके जाती थीं। हालांकि ससुराल और मायके में गरीबी में कोई अंतर नहीं होता था। कम उम्र में ब्याह दी गईं बेटियां आमतौर पर शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर होती थीं। प्रसव पीड़ा उठने के साथ ही प्रसूता को कई बार गर्म पानी से नहलाया जाता। समूचा मोहल्ला प्रसव के समय इर्द-गिर्द जमा हो जाता। हर महिला अपने हाथ प्रसूता के शरीर में घुसा देती, जिसके कारण तरह-तरह के संक्रमण और सूजन हो जाता। महिलाएं कहीं से ज्वार मांग कर लातीं और उसे पका कर मां को दिया जाता। नवजात बच्चे को भी कई संक्रमित हाथों से गुजरना पड़ता। इस तरह मां और नवजात दोनों ही बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजरते। उनके लिए न तो खाना होता और ना ही पैसा। केवल अंतहीन दुःख और कष्ट! … हर 10 में से एक माँ और बच्चे को प्रसव के दौरान अपनी जान खो देनी पड़ती …
“दुनिया ने हमें गुलाम बनाया। तो हमारी भी सत्ता हासिल करने और गुलाम बनाने की इच्छाएं जाग जाती थीं। तो हमने अपनी बहुओं को गुलाम के रूप में देखा। आठ, नौ, दस साल की बच्चियां बहुएं बन कर आतीं। … शादी उनके लिए एक आपदा बनकर आती।… ससुराल आने के बाद मुर्गे की बांग के साथ उसके काम शुरू हो जाते। छोटी बच्ची को ढेर सारी रोटियां बनाने को दी जाती।… उसे रात में सोने नहीं दिया जाता … उनके नन्हें हाथों में छाले पड़ जाते और बाद में वे घट्ठे बन जाते … बेचारी बच्ची को घर में हर किसी की गालियां ही मिलतीं … मारपीट का सिलसिला अनवरत चलता रहता … पति भी आये दिन मार-पीट करता… इस तरह भय से कांपती बहू हर किसी का आसान शिकार होती थी …
“उन दिनों प्रत्येक सौ औरतों में एक की नाक काट दी जाती … घर में कष्ट सहती बहू कभी रात के अंधेरे में अपने घर भाग जाती तो मायके के लोग उसे वापस ससुराल पंहुचा देते और ससुराल में अक्सर पति उसे सज़ा देता और उसकी नाक काट लेता …
“हमारी हरेक पीढ़ी अपने बच्चों को शोषितों की गुलामी के लिए छोड़ देती। लेकिन बाबासाहब आंबेडकर के दिए तीन मूल्य – चरित्र, सत्य और नैतिकता – अन्याय से लड़ने और हमारी बेड़ियां तोड़ने के लिए तीन हथियार के रूप में हमेशा हमारे साथ रहे …
“आंबेडकर ने कहा था कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। ईश्वर से उनका पीछा छुड़ाओ। अपने बच्चों को स्कूल भेजो। जब तुम्हारे बच्चे शिक्षित होंगे, उनकी स्थिति सुधरेगी। हम इन्सान हैं। हमें भी इंसान की तरह जीने का हक है। जब पढ़ेंगे तभी हमारे बच्चे इसके प्रति जागरूक होंगे। …
“उन्होंने कहा कि हमारी बहनों में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है, उसे दूर करो। गांव भर की गंदगी मत साफ़ करो। जिन्होंने गंदगी की है, वे ही उसे साफ़ करें। मेरे प्यारे गरीब भाइयों और बहनों, मरे हुए जानवरों का मांस मत खाओ। यह दासता इतनी आसानी से नहीं छूटने वाली। इसके लिए हमें क्रांति करनी होगी। …
“बहुत छोटी उम्र में ही मैंने यह तय कर लिया था कि बाबासाहब द्वारा दिखाई गई रोशनी ही मेरे जीवन की पथ प्रदर्शक बनेगी। बाबासाहब के सिद्धांतों का मेरे जीवन पर गहन असर था। …
“मैंने धूप-अगरबत्ती से बाबासाहब की पूजा कभी नहीं की, लेकिन मैं उनके सिद्धांतों पर पक्का विश्वास करती थी। मेरा परिवार उनके बताये रास्ते पर चलता रहा, इसलिए हमें हमेशा संतुष्टि का भाव रहा। …
“मैं आंबेडकर आंदोलन की ही एक उपज हूं। मैं आठ साल की उम्र में इसके संपर्क में आ गई थी। …
“मेरे पिता पंढरीनाथ काकडे और अन्य कार्यकर्ता, जो पढ़े-लिखे थे, वे ‘डेली केसरी’ और ‘डेली सकाल’ जैसे अख़बार चावड़ी (गांव की चौपाल) में लेकर आते और उन्हें ज़ोर-ज़ोर से पढ़ते। इसके अलावा हम बाबासाहब द्वारा प्रकाशित अख़बार ‘बहिष्कृत भारत’ भी सुनते। इसमें बाबा साहब के भाषण प्रकशित होते। …
“मेरा नन्हा दिमाग ज्ञान के इस समुद्र से कुछ कतरे ग्रहण कर लेता। …
“बाबा के शब्द उसी समय से मेरे लिए कानून बन गए। सामाजिक काम जिंदा रहने का एक विकल्प बन गया। मेरे ह्रदय में एक नई ज्वाला जलने लगी। समूचे देश में एक नई बयार बहने लगी थी। श़फ़क़ के साथ एक नया सूर्य उदित हो रहा था। …”
सामान्य तौर पर आत्मकथाओं में मूलतः लेखक का निजी आख्यान ही होता है। ऐसा तभी होता है जब लेखक का ‘आत्म’ समाज से एकदम अलग हो। लेकिन जिस समुदाय की पीड़ा इतनी सघन और व्यापक हो, उसमें से व्यक्ति की निजी पीड़ा को अलगाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में तो उस व्यक्ति का जीवनवृत्त भी उसके समुदाय का जीवनवृत्त ही बन जाता है। इसे और आगे बढ़ाएं तो इस समुदाय की व्यापक मुक्ति में ही व्यक्ति की निजी मुक्ति भी निहित होती है।
बेबी कांबले की आत्मकथा की उपरोक्त झलकियों से हमें पता चलता है कि महाराष्ट्र में दलितों की ख़ासतौर से महार समुदाय की जीवनदशा कितनी दयनीय थी। वह विकट गरीबी, भुखमरी, अंधविश्वास, अमानवीयता जैसे न जाने कितनी बेड़ियों से जकड़ी हुई थी।
हम ऊपरी तौर पर दलितों के जीवन से कितनी भी सहानुभूति रख लें, लेकिन एक समुदाय के रूप में उनके जीवन ने जितनी वंचना झेली थी, उतने कष्ट में भींगे शब्द शायद हमें खोजने से भी न मिले। बेबी के आत्मकथन के एक-एक शब्द से उनके समुदाय की पीड़ा का अहसास पाठक को होता है।
भारत में महिलाओं की आत्मकथाएं मुख्यतः सवर्ण महिलाओं की ही मिलती है। महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत संभवतः रमाबाई रानाडे (1910) से होती है। सर्वाधिक चर्चित आत्मकथा लक्ष्मीबाई तिलक की थी, जो 1930 में प्रकाशित हुई थी। इन किताबों की चर्चा करते हुए किताब के अंत में आत्मकथाओं की विशद चर्चा करते हुए लेखक गोपाल गुरू कहते हैं कि दलित आत्मकथाओं की परंपरा बहुत बाद में शुरू हुई। दलित महिलाओं का लेखन तो एकदम हाल की परिघटना है।
दलित महिलाओं के साक्ष्य दलित पितृसत्ता और सामाजिक पितृसत्ता से राजनीतिक रूप से भीतर से मुठभेड़ करते हैं। इन अर्थों में बेबी कांबले की यह पुस्तक एक आईने की तरह है।
हम जानते हैं कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से हिंदू धर्म में दलितों की कितनी दयनीय दशा है, उसमें से भी दलित औरतों की स्थिति और भी कष्टप्रद है। बेबी इस तथ्य को कतई ढांकने का प्रयास नहीं करतीं। महार औरतों का ज़िक्र करते हुए वह नन्हीं-नन्हीं बच्चियों की स्थिति का जिस तरह से ज़िक्र करती हैं, उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रतिरोध करने वाली औरतों का नाक काट लिया जाना तो कल्पना से परे है।
किताब के अंत में माया पंडित द्वारा बेबी कांबले का लिया गया विस्तृत राजनीतिक साक्षात्कार में एक प्रश्न के जवाब में वह कहती हैं कि डॉ. आंबेडकर के आंदोलन में औरतों ने बड़ी भूमिका निभाई। उनका मानना है कि 1956 में डॉ. आंबेडकर के परिनिर्वाण के बाद दलित आंदोलन में भटकाव आया। हर दलित नेता अपने आपको उत्तर आंबेडकर समझने के चक्कर में अवसरवादी हो गया। अपने कथन की पुष्टि के लिए वह दलित पैंथर के नेता रामदास आठवले का उदाहरण देती हैं। आगे वह उन शिक्षित दलितों की भी आलोचना करती हैं, जो उच्च सरकारी पद हासिल करने के बाद गरीब दलितों की ओर देखते तक नहीं।
बेबी कांबले का मानना है कि 1956 में जब डॉ. आंबेडकर ने बौद्ध धम्म अपनाया तो समस्त महार समुदाय भी उनके साथ बौद्ध हो गया, लेकिन शेष दलित समुदाय पीछे छूट गए। उनके अनुसार बौद्ध धम्म का हर ओर प्रचार और अन्य दलित समुदायों को इसमे शामिल करना ही समस्या का समाधान है।
बेबी इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हैं कि डॉ. आंबेडकर के बाद से दलित आंदोलन में जो जुझने का माद्दा था, वह ख़त्म हो गया है। आज दलित नेता पैसों के पीछे भाग रहे हैं। अभी दलित संगठित नहीं रह गए हैं। वे बंटे हुए हैं। अब उनमें संघर्ष की कोई बात नहीं होती।
अपने व्यक्तिगत जीवन की बात करते हुए बेबी कहती हैं कि उनका जीवन उनके समुदाय की दूसरी औरतों से अलग नहीं था। “उन दिनों पुरुष औरतों की जिंदगी पर नियंत्रण रखते थे, और मैं कोई अपवाद नहीं थी।… मुझे अपने पूरी जिंदगी हिंसा का सामना करना पड़ा।…” साक्षात्कार में अपने पति के बारे में ज़िक्र करते हुए वह बताती हैं कि उनके पति उनके ऊपर शक करते थे। कई बार वे मारते-पीटते भी थे। लेकिन एक बड़े उद्देश्य के लिए वह पति के दुर्व्यवहार को बर्दाश्त कर लेतीं। इस तरह उनकी आत्मकथा के जरिए दलित आंदोलन और जीवन में पितृसत्ता का दंश उभर कर सामने आता है, जिसके बारे में पुरुषों द्वारा लिखित आत्मकथाओं में कम ही ज़िक्र मिलता है और अस्मिता के आंदोलन में जिसे बहुधा नज़रंदाज़ किया गया है।
अंत में वह कहती हैं– “मेरे लिए मेरे समुदाय के कष्ट हमेशा मेरे अपने कष्ट से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। मेरी पहचान मेरे अपने लोगों से ही है। इसलिए ‘जिना अमुचा’ मेरे समूचे समुदाय की जीवनी है।”
इस तरह बेबी कांबले की यह किताब केवल एक दलित समुदाय और उनकी औरतों की जीवनकथा ही नहीं है, बल्कि यह किताब हम सभी को एक हद तक यह रास्ता दिखाती है कि हम खुद अपनी जिंदगी की बेड़ियां कैसे तोड़ें।
(संपादन : राजन/नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in