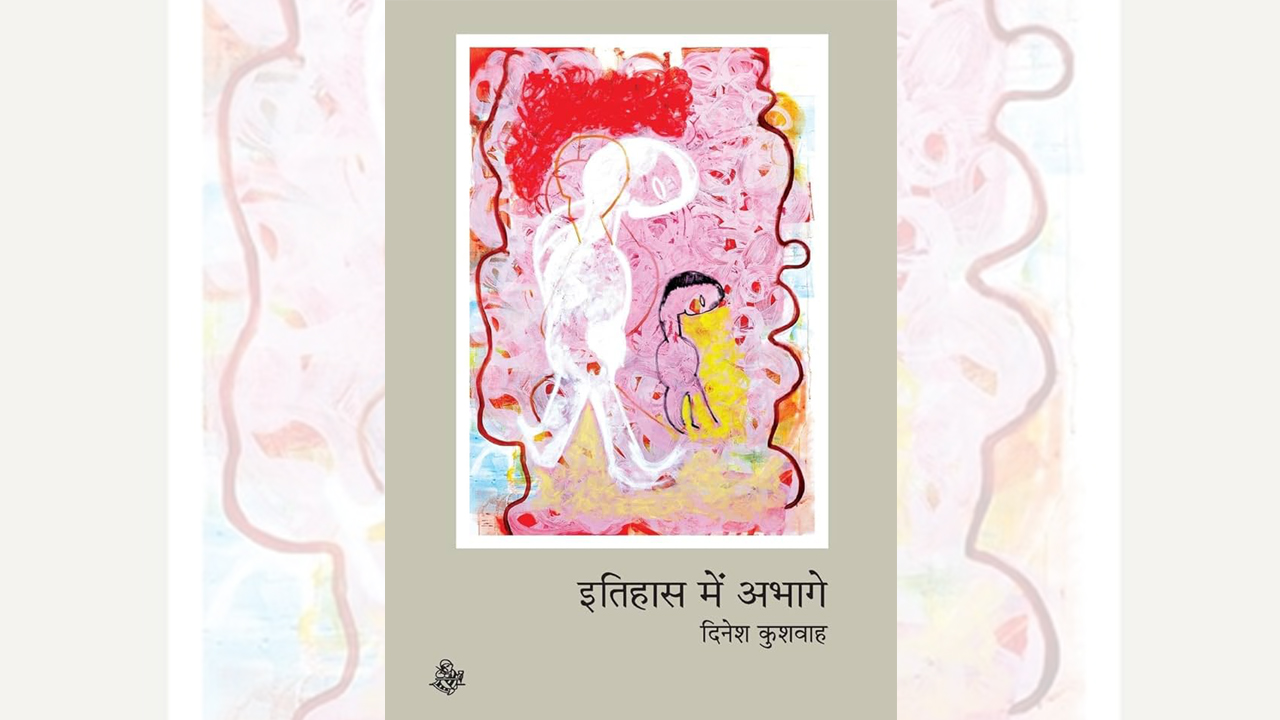आदिवासी पुरखा साहित्य की अपनी लंबी और समृद्ध परंपरा रही है। लेकिन एक आंदोलन के रूप में पिछले कुछ वर्षों में जैसे-जैसे आदिवासी विमर्श सामने आता जा रहा है, वैसे-वैसे आदिवासी समुदायों से आने वाले साहित्यकार साहित्य की दिकू विधाओं में भी कलम चलाने लगे हैं या चलाने को मजबूर हुए हैं। इससे एक आशंका भी जन्म लेती है कि विमर्श के शोरगुल में आदिवासी समाज-संस्कृति की मौलिकता कहीं दबकर न रह जाए।
आदिवासी साहित्यकार जिस आधुनिक विधा में ज्यादा लिख रहे हैं, वह है कविता। और सच कहें तो आदिवासी कविता ने पाठकहीन होती हिंदी कविता को एक नया जीवन देने का काम किया है। रामदयाल मुंडा, महादेव टोप्पो, वाहरू सोनवणे, हरीराम मीणा, ग्रेस कुजूर, निर्मला पुतुल, वंदना टेटे के साथ-साथ नई पीढ़ी में अनुज लुगुन और जसिंता केरकेट्टा की कविताएं चर्चा में हैं। इसी क्रम में सावित्री बड़ाईक के रूप में एक और नाम इस साहित्यिक धरा पर अंकुरा रहा है। उनकी कविताओं में मध्य भारत के आदिवासियों के वर्तमान जीवन-संघर्षों से लेकर उनकी सांस्कृतिक धरोहरों की गूंज सुनाई देती है। तथाकथित शाश्वतता के प्रति कोई दुराग्रह वे नहीं पालतीं अपितु आदिवासियत को बचाए रखने के लिए बदलते समय के साथ दो-दो हाथ करने के साथ ही गैरआदिवासियों के सहयोग का आह्वान भी करती हैं।
सावित्री बड़ाईक की कविताएं जब-तब छपती रही हैं, लेकिन वर्ष 2023 में अनुज्ञा प्रकाशन से आया ‘दिसुम का सिंगार’ उनका पहला काव्य संग्रह है। इस संग्रह की कविताओं में आप आदिवासियों के जीवन दर्शन, उनकी प्रतिरोध चेतना और श्रम के सौंदर्य में उनकी आस्था के अनुरूप ही अपनी विभिन्न कविताओं में शृंगार का आदिवासी मानक प्रस्तुत करती हैं। उनकी कविताएं दिखाती हैं कि आदिवासी सोने-चांदी जैसी बहुमूल्य कही जानेवाली धातुओं से बने आभूषणों से संपन्न कृत्रिम अलंकरणों में विश्वास नहीं करते। वे तो श्रम से पैदा खेती-किसानी से धरती के सौंदर्य में अभिवृद्धि करने में यकीन रखते हैं। इसी क्रम में पराए बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कल-कारखानों से कुरूप होती जा रही धरती की चिंता सावित्री बड़ाईक की कविताओं में झलकती है। वे गोदना जैसे परंपरागत आदिवासी बनाव-शृंगार को आदिवासी संघर्ष के इतिहास और संस्कृति की विषय वस्तु की व्यंजना के माध्यम के रूप में चिह्नित करती हैं।
कविताओं में आदिवासियों समेत बहुसंख्यक श्रम शक्ति को संसाधनविहीन बनाकर विषमता का पिरामिड खड़ा कर उसके शीर्ष पर विराजमान मुट्ठी भर लोगों के छल-छद्म, शोषण और अन्याय को रेखांकित किया गया है। इन प्रतिगामी ताकतों से अलग-अलग संघर्ष करते हुए सफल होना कठिन है, इसलिए धरती को और उसी के साथ जुड़े अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने-अपने स्तर पर आंदोलनरत तमाम छोटे-बड़े समूहों-संगठनों के बीच तालमेल की जरूरत पर बल दिया गया है, आदिवासियों को अपने सहधर्मी इन आंदोलनकारियों से सहिया जोड़ने के लिए कहा गया है। इस संदर्भ में आदिवासी अखड़ा की संवादधर्मिता के जनतांत्रिक पहलू को भी कविता में रेखांकित किया गया है।
सावित्री बड़ाईक अपनी कविताओं के जरिए तथाकथित सभ्य लोगों को भी चेताती है कि विकास के नाम पर उनके जल-जंगल-जमीन पर हमले करना बंद करके उनके वैकल्पिक जीवन दर्शन और स्वायत्त जीवन-शैली का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यदि आदिवासी नहीं बचेगा, तो यह धरती, यह प्रकृति भी आधुनिक मनुष्य के लोभ-लालच से बच नहीं पाएगी। इन कविताओं में बाज़ार और पूंजी की संयुक्त ताकत के सामने आदिवासी पहाड़ की तरह खड़े हुए नज़र आते हैं।
भाषा की लिपि और शास्त्रीय ज्ञान से वंचित रहने के कारण आदिवासियों को सभ्य समाज पिछड़ा बताता रहा है, लेकिन कवयित्री अपने आदिवासी पुरखों के लौहकर्म के ज्ञान, शिल्प कौशलों और उनकी हस्त-कलाओं के विभिन्न रूपों पर कविताएं लिखकर स्थापित कर देती हैं कि सभ्यता-संस्कृति के आर्य मानकों से इतर आदिवासी आयाम भी रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि इतिहास में आदिवासियों की पुरखा ज्ञान परंपरा और उनकी कलाओं को उनका वाजिब स्थान दिलवाया जाए। आदिवासी समाज उपयोगमूलकता और सौंदर्यमूलकता के आधार पर कलाओं को शिल्पकला और ललितकला, इस तरह की श्रेणियों और स्तरीकरण में विभाजित नहीं करता। आदिवासी कलाओं पर लिखी गई कविताओं में आदिवासी कला दृष्टि के इस विशिष्ट पहलू को साफ़ देखा जा सकता है।
आदिवासी के साथ-साथ एक स्त्री होने के कारण सावित्री बड़ाईक की कविताओं में आदिवासी स्त्री जीवन की विभिन्न छवियां भी स्वत: ही आ गई हैं। यह आदिवासी स्त्री घर की चार-दीवारी तक सीमित सामंती उच्च जातियों की स्त्री की जैसे अपनी आज़ादी के लिए अंदर ही अंदर घुटती-बिलखती स्त्री नहीं है, बल्कि खेतों-जंगलों में श्रम करती और हाट-बाज़ार करती स्त्री है। खेती-किसानी और जंगल पर होते हमलों के कारण छिनते आजीविका के स्रोतों के कारण आदिवासी स्त्रियों को मजदूरी की तलाश में आज शहरों के चौराहों पर भी देखा जा सकता है। काम की तलाश में शहर जाने को मजबूर ऐसी आदिवासी स्त्रियों की कर्मठता और स्वाभिमान को इन कविताओं में उल्लेखित किया गया है। नगरों-महानगरों में चंद निवालों के बल पर आदिवासी घरेलू कामगारों से जो बेगार करवाई जाती है, उनका जो शोषण होता है, उसके खिलाफ ये कविताएं पाठकों को झकझोरने का काम करती हैं। आदिवासी स्त्री की जिजीविषा और संघर्षशीलता के इस प्रसंग में अपनी मां की ममता और स्नेह को याद करते हुए कवयित्री लिखती हैं कि आदिवासी मांओं के कठोर श्रम करने वाले हाथ और धरती को नापते उनके पैर उसकी स्मृति में अमिट रूप से अंकित हैं। अपनी श्रमशील मां की शंख नदी-सी चौड़ी मुस्कान और उनके दुलार का वितान आज भी कवयित्री बेटी को आश्वस्ति से भर देने वाला है।
कवयित्री दिखाती हैं कि ये आदिवासिने घर-गृहस्थी का तमाम काम करते हुए, पीठ पर अपने छोटे-छोटे बच्चों को लादे हुए भी भविष्य के लिए जल-जंगल-जमीन के प्रश्नों पर नारे लगा रही हैं, मोर्चाबंदी कर रही हैं– “सूखी लकड़ी का गट्ठर / सिर पर उठाती हैं / पर / जल, जंगल, जमीन के प्रश्न पर / भविष्य को / छऊवा को / पीठ पर बेतराकर / समूह में निकलती हैं / उनके हाथ उठे हुए हैं / अपने प्रश्नों के साथ”[1]। स्पष्ट है कि इन आदिवासी स्त्रियों की यह लड़ाई अपने अस्तित्व की लड़ाई है। यह कोई एनजीओ प्रायोजित दिखावटी आंदोलन नहीं है, मुख्यधारा के नेताओं द्वारा पैसों के बल पर इकट्ठा भीड़ नहीं है।

यह भी ध्यातव्य है कि सवर्ण स्त्रियों की जैसे आदिवासियों में स्त्रियों के ऊपर पुंसवादी नैतिकता और मर्यादा की तलवार नहीं लटकी होती है, उन्हें घर की चार-दीवारी में बंद रहने का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है। यही कारण है कि अपने आदिवासी अस्तित्व पर छाये हर प्रकार के संकट के खिलाफ समय-समय पर आदिवासी स्त्रियां संघर्ष करती आई हैं।
समय के साथ जैसे-जैसे सभ्यता का विकास होता गया है, वैसे-वैसे आदिवासी समुदाय भी आखेट और वन्य उपजों के संग्रह के अतिरिक्त खेती-किसानी भी करने लगे। मध्य भारत के आदिवासी भी इस संदर्भ में कोई अपवाद नहीं रहे हैं, लेकिन आदिवासी समुदायों द्वारा जो खेती-किसानी की जाती है, वह मुनाफाधर्मी व्यावसायिक खेती के अंतर्गत नहीं आती। आदिवासी समुदायों के लिए किसानी अस्तित्व रक्षा से जुड़ा मसला होता है और मध्य भारत के आदिवासियों का अस्तित्व काफी हद तक धान की आदिम किसानी के साथ जुड़ा हुआ है। सावित्री बड़ाईक ने धान के ऊपर इसी शीर्षक से एक कविता लिखी हैं, जिसमें उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता के साथ आदिवासी ढंग की किसानी के वैशिष्ट्य को रेखांकित किया है।
वे प्रकृति के साथ तालमेल बैठाते हुए खेती के विभिन्न चरणों का उल्लेख करती हैं। स्पष्ट है कि आदिवासी प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते हुए कृषि कर्म संपन्न करते हैं। आदिवासी स्वयं को प्रकृति का स्वामी नहीं मानते। वे प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के अहंकार से वंचित होते हैं। उनका पूरा जीवन प्रकृति पर निर्भर होता है और प्रकृति के प्रति एक प्रकार की कृतज्ञता उनकी संपूर्ण सभ्यता-संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। कर्ता होने का अहंकार वे नहीं पालते।
आदिवासी समाज वैयक्तिक संपत्ति और इस संपत्ति के पुंसवादी वैध वारिसों वाली वसीयत में विश्वास नहीं करता है। कवयित्री का कहना है कि आदिवासी निजी वसीयत में नहीं, अपितु सामूहिकता की विरासत में यकीन रखते हैं। वे स्वयं को प्रकृति का संरक्षक, ट्रस्टी मानते हैं और चाहते हैं कि भावी पीढ़ियों के लिए, समस्त जीव-जंतुओं के लिए यह विरासत सुरक्षित रहे। वह दिखाती हैं कि वे प्रकृति की, बीजों की विविधता को बचाए रखना चाहते हैं, वे विविधता भरी इस प्रकृति को ही अपनी विरासत के रूप में अगली पीढ़ियों को सौंप जाना चाहते हैं– “छोड़ जाते हैं विरासत में / पेड़, पहाड़, जंगल की पगडंडियां / अकृत्रिम देशज बीजों को / ये बैंक बैलेंस नहीं / छोड़ जाते हैं”[2]।
‘दिसुम का सिंगार’ शीर्षक जिस कविता पर इनके पहले काव्य संकलन का शीर्षक आधारित है, वह कविता यही दिखाती है कि इस प्रकार की सहजीवी खेती आदिवासी खेती-किसानी को कम लागत वाली टिकाऊ अर्थव्यवस्था में बदल देती है। आदिवासी अपनी खेती-किसानी के लिए देशी-विदेशी कंपनियों के बीजों और खाद आदि पर निर्भर नहीं रहते। वे अपने धान आदि के बीजों को स्वयं विकसित करते हैं, उन्हें संरक्षित करते हैं। इस प्रकार महंगे रासायनिक उर्वरकों और कंपनियों के बीजों की गुलामी से वे आज भी बचे हुए हैं और बचे हुए हैं ऋण व्यवस्था पर टिकी बाज़ारोन्मुख खेती से। स्वायत्त कृषि व्यवस्था के दर्शन पर टिकी हुई विशुद्ध खेती से पैदा उत्पादों की तरफ ही आज का कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री बल दे रहा है। खेती और वृक्षारोपण के बीच भी एक संतुलन हमें वहां दिखाई देता है। खेत तैयार करने के लिए जंगलों का समूल विनाश नहीं किया जाता। पहली बात तो मुनाफे की भूख मिटाने के लिए खेती नहीं की जाती, अपितु अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए खेती-किसानी की जाती है। दूसरी बात, आदिवासी के द्वारा जो खेती-किसानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, वह बाजारोन्मुख निगमीय कृषि के जैसे मिट्टी आदि प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन और तदजन्य पर्यावरणीय असंतुलन की वजह नहीं बनती। यह खेती आदिवासी की स्वायत्तता और स्वाभिमान के साथ-साथ पौष्टिक आहार और प्रकृति की रक्षा का देशज ज्ञान-विज्ञान है और इसीलिए ‘दिसुम का सिंगार’ कविता में कवयित्री खेती के निगमीकरण का विरोध करते हुए देशज जैविक खेती की आदिवासी परंपरा पर बल देती हैं– “वे खेती के निगमीकरण से / खेती की नई तकनीक से / कर रहे हैं हमला / खानपान, फसलों की विविधता पर / हमारी पारंपरिक खेती पर …. दया के लाभार्थी झोले से नहीं / देशज धान से / बढ़ेगा हमारा स्वभिमान / देशज खेती से दूर होगा / भूख और खाद्य संकट / देशज खेती ही समाधान है / जलवायु संकट का”[3]।
अस्तु, दिकू सभ्यता कथित उत्पादन लागत और भौतिक उपयोगिता जैसे विवादित पैमानों पर आदिवासियों की हर उपलब्धि को नकारती आई है, उनके कला-कौशल को बेहूदा और पिछड़ा बताती आई है, लेकिन कवयित्री सावित्री बड़ाईक पराये प्रतिमानों पर आदिवासी धरोहरों को हेय मानने के विरुद्ध हैं। वे आदिवासी कला-कौशल को आदिवासी संस्कृति के साथ नाभि-नाल रूप से जुड़ा मानती हैं। अपनी ‘छोड़ब नहीं हुनर’ शीर्षक कविता में कवयित्री ने मशीनी सभ्यता के कलाहीन उत्पादों को अमरबेल की तरह बताया है, जो आदिवासी शिल्प कौशलों पर कुठाराघात कर रहे हैं। आज बाज़ार में उपलब्ध सस्ते निष्प्राण उत्पादों के सामने कलात्मक शिल्प कौशलों से जीवंत नज़र आने पर भी आदिवासी शिल्प का कोई लेनदार नहीं बचा है।
वैसे कवयित्री दिखाती हैं कि कल-कारखानों से उत्पादित प्लास्टिक, स्टील और नायलॉन के उत्पादों ने अपनी जमीन से जुड़ी आदिवासी कलाओं और शिल्पों को विस्थापित भले ही कर दिया हो, लेकिन आज भी आदिवासी अपनी कारीगरी और शिल्प को बचाने के लिए संघर्षरत हैं।
यह भी पढ़ें – आदिवासी स्त्री लेखन : अतीत से वर्तमान तक
वास्तव में मुनाफाखोर मशीनी सभ्यता के लिए आज चाहे आदिवासी शिल्पों का वैसा महत्व नहीं रह गया हो, लेकिन ये शिल्प कौशल अपने परिवेश की सहज उपज रहे हैं और भौतिक उपयोगिता के साथ-साथ इनका अपना एक कलात्मक सौंदर्य भी रहा करता है। इसीलिए कवयित्री कहती हैं– “पुरखा शिल्पकारों ने लिखी है / माटी, बांस, लकड़ियां / सूत, लोहे, पाषाण पर / सभ्यता के विकास की कविताए”[4]। आदिवासी समाज ने प्राकृतिक संसाधनों और अपने आस-पास के जीव-जंतुओं से सीखकर अपने ज्ञान-कौशल से सभ्यता के विकास में अपना योगदान दिया है। आदिवासी शिल्प-कौशल और अड़ौस-पड़ोस की कृषि सभ्यता के बीच परस्पर मैत्री संबंध हुआ करते थे। कारण कि दोनों सभ्यताएं एक-दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति किया करती थीं। लेकिन कवयित्री दिखाती हैं कि मशीनी उत्पादों ने दोनों सभ्यताओं के बीच चले आ रहे संवाद में अलगाव ला दिया है। आज आदिवासी शिल्प उत्पादों – तकली, करघे, चाक, छेनी, कातुछुरी, हथौड़ी, संडासी, कुटासी – का कोई खरीदार नहीं रह गया है। इस प्रकार औद्योगिक सभ्यता के कारण आदिवासी शिल्पकार अपने परंपरागत शिल्प कौशलों को छोड़कर अपने पहाड़ों-जंगलों से विस्थापित होने को मजबूर हैं।
रमणिका गुप्ता ने ‘आदिवासी स्वर और नयी शताब्दी’ शीर्षक पुस्तक के संपादकीय में लिखा है– “आदिवासियों की गति में नृत्य है, वाणी में गीत। जब वह चलता है तो थिरकता है और जब बोलता है तो गीत के स्वर फूटते हैं। वह अकेला नहीं, समूह में रहता है, समूह में सोचता है, समूह में जीता है।”[5] आदिवासियों के जीवन में यह गीत-संगीत इस प्रकार घुला-मिला रहता है कि यह एक तरह से उनके अस्तित्व का आधार ही होता है। आदिवासियों को आपस में जोड़ने वाला, उनमें सामूहिकता का विकास करने वाला भी यह होता है।
सावित्री बड़ाईक अपनी अनेक कविताओं में दिखाती हैं कि आदिवासी संस्कृति में जो गीतात्मकता-लयात्मकता होती है, वह उनके प्राकृतिक परिवेश की देन है। देशज धान की खेती से जुड़े श्रम को वे यों ही ‘दिसुम के सिंगार’ की संज्ञा नहीं दे देती हैं, अपितु वे अपनी इस कविता में व्यंजित करती हैं कि धान के खेतों और खलिहानों में पसीना बहाते आदिवासी अपने श्रम के बीच-बीच में अपने सामूहिक गीत-संगीत के द्वारा अपने दिसुम की वृद्धि करते रहते हैं। उनके श्रम और उमंग से भरे गीत, खेतों में झूमती देशज धान की बालियां, खान-पान और फसलों की विविधता जिस सौंदर्य की सृष्टि करती है, मशीनों से होने वाली निगमीय खेती में मुनाफे की अंधी भूख में यह सारा सौंदर्य सिरे से गायब मिलता है। खेती से पूंजी का निर्माण करने वाली निगमीय सभ्यता आदिवासियों की जमीन छीनकर, उनके जंगल छीनकर उन्हें संस्कृतिविहीन कर देना चाहती है और कवयित्री इस संस्कृतिविहीन बाज़ार केंद्रित खेती के संकट को अपनी कविता में चिह्नित करते हुए अपने आदिवासी समाज को चेताती हैं– “आओ बैल आधारित देशज खेती करें / पारंपरिक कला संस्कृति से जुड़ें / धरती का सिंगार करें”[6]।
गीत-संगीत और नृत्य आदिवासियों की रंग-बिरंगी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होते हैं। सावित्री बड़ाईक ने मध्य भारत के आदिवासियों में प्रचलित छऊ, पइका और झूमर जैसे विशिष्ट गीतों पर भी ‘यह धरती है छऊ, पइका, झूमर की’ शीर्षक से कविता लिखी है। आदिवासी जीवन और नृत्य-गान एक-दूसरे के पर्याय होते हैं। बिना नृत्य और गीत के आदिवासी समाज का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये कलाएं ही आदिवासियों को विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत रखने और संघर्ष करने की प्रेरणा देती हैं। बिरसा मुंडा के उलगुलान के पीछे नृत्य और गीत की भी बहुत बड़ी ताकत काम कर रही थी। उलगुलान और भूमकाल की याद को गीतों में जीवित रखकर आदिवासी स्वयं को प्रतिरोध की ऊर्जा से भरते रहते हैं। कवयित्री इन गीतों में निहित शक्ति का रहस्य समझने-समझाने और उसके प्रचार-प्रसार पर बल देती हैं– “तुम्हें बताना होगा डोम्बारी से डुम्बरपाट तक / क्यों गाते हैं क्रांतिगान / साझा करो गीत भूमकाल / साझा करो गीत उलगुलान / जंगल-जंगल गांव-गांव / पहाड़-पहाड़ गांव-गांव / फैला दो आदिवासी देस में / स्वायत्त अभिव्यक्ति का वितान”[7]। गीतों से ही आंदोलनरत आदिवासी अपने जल-जंगल-जमीन को बचाने के लिए संगठित प्रेरित होते हैं। आदिवासी गीत-संगीत की शक्ति से अनजान अंग्रेजों की तरह ही दिकू लोग अपने अस्तित्व के संकट में होने पर भी नाचते-गाते आदिवासियों पर चाहे हंसते हों लेकिन वे नहीं जानते कि आदिवासी समाज की ये कलाएं जीवन से जुड़ी होती हैं। भौतिक सुख-सुविधाओं से रहित संघर्षशील आदिवासी जीवन में आगे बढ़ने की उमंग-उल्लास इन्हीं से मिलती है।
मध्य भारत के आदिवासी समाज और संस्कृति में अखड़ा एक केंद्रीय संस्थान के रूप में होता है जहां आदिवासियों की पुरानी पीढ़ी अपने पुरखों द्वारा अर्जित हर प्रकार के ज्ञान-विज्ञान और कला-संस्कृति को नई पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। अखड़ा को आदिवासी समुदायों का विश्वविद्यालय भी कहा जा सकता है। सावित्री बड़ाईक ने इस पर भी ‘अखड़ा में जुटान’ शीर्षक से कविता लिखी है। अखड़ा में आदिवासी पारस्परिक सहयोग और साझेपन के सूत्र सीखते हैं। सामुदायिक उपयोग के छोटे बांध आदि बनाने के पाठ पढ़ते हैं। बड़े-बूढ़ों और मुंडा, मानकी, पाहन और मांझी जैसा परंपरागत आदिवासी नेतृत्व पुरखों की ज्ञान-परंपरा को जहां अखड़ा के माध्यम से नई पीढ़ी को सौंपता है, वहीं हर समस्या के समाधान के लिए अखड़ा में आदिवासी समाज को जुटाता है। अखड़ा में सब मिल-बैठकर जिस प्रकार लोकतांत्रिक ढंग से समस्या का समाधान निकालते हैं, जिस प्रकार पर्व आदि का आयोजन तय करते हैं, उससे एक जनतांत्रिक चेतना पैदा होती है। कवयित्री नवउदारवादी पूंजी केंद्रित सभ्यता से पैदा चुनौतियों पर विचार करने और शोषक सत्ताओं से दो-दो हाथ करने के लिए सभी आदिवासियों को और आदिवासी दर्शन में विश्वास रखने वाले गैर-आदिवासियों को भी संवाद के लिए अखड़ा में आमंत्रित करती है। कविता कहती है कि संवाद की यही परंपरा आदिवासी सभ्यता-संस्कृति से जुड़ी दूसरी संस्थाओं में भी दिखाई देती है।
‘हाट में आदिवासी’ शीर्षक कविता में कवयित्री पूंजीवाद द्वारा संचालित उपभोक्तावादी बाज़ार के जाल के समकक्ष आदिवासी हाट बाज़ार की वैकल्पिक दुनिया के वैशिष्ट्य को रेखांकित करती हैं। हाट बनाम आधुनिक बाज़ार के इस द्वंद्व के बहाने कवयित्री ने मनुष्य को उपभोक्ता में बदल देने के, सक्रिय कर्ता से निष्क्रिय उपभोक्ता में तब्दील कर देने के बाज़ार के षड्यंत्र को उजागर किया है– “हाट बाज़ार जाते / आदिवासी / बेचते हैं वनोपज / हाट को बाज़ार को / घर नहीं लाते / और न उनके घर / दूकान होते हैं / घर को सजाते नहीं बाज़ार से।”[8] आज विज्ञापनों के बल पर बाज़ार के सूत्रधारों ने घर और बाज़ार के अंतर को उपभोक्तावादी संस्कृति से पाट दिया है। बाज़ार में हर चीज उसके विक्रय मूल्य से तौली जाती है। इसलिए घर के अंदर बाज़ार की घुसपैठ से पारिवारिक-सामाजिक रिश्तों में भी पूंजीगत क्रय-विक्रय मूल्यों का आधिपत्य हो गया है, लेकिन आदिवासी समाज अपने कथित पिछड़ेपन और मुख्यधारा के बाज़ार से कटा होने के कारण आज भी बाज़ार द्वारा तय पूंजीगत मूल्यों से बचा हुआ है। कवयित्री कहती हैं कि आदिवासी समाज की अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं है कि बाज़ार होता न हो, लेकिन वहां बाज़ार और आदिवासी समाज का रिश्ता नितांत जरूरी चीजों तक ही सीमित रहता है।
बहरहाल, सावित्री बड़ाईक की कविताएं आदिवासी कलाओं और नृत्य-संगीत के प्रति कोई रोमानी दृष्टिकोण लेकर नहीं चलती हैं। कुछ दिकू साहित्यकारों के जैसे उनके लिए आदिवासियत अजायबघर में सजाने-दिखलाने की वस्तु नहीं है और न ही उनकी कविताओं में आदिवासी सिर्फ वर्ग संघर्ष की लड़ाई लड़ते और नक्सलियों-माओवादियों के रूप में सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाने को ही अभिशप्त हैं। यहां हमें जल-जंगल-जमीन की लड़ाई संस्कृति की लड़ाई के साथ, पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन के साथ जुड़ती नज़र आती है। कवयित्री बारंबार चेतावनी देती दिखाई देती हैं कि आदिवासियों के अस्तित्व के साथ ही इस धरती का अस्तित्व भी जुड़ा हुआ है। उनकी कविताएं हमें मुनाफाधर्मी भौतिकवादी दुनिया के एकाकीपन से ऊपर उठकर चराचर जगत के साथ सहिया जोड़ने की भावभूमि की ओर ले जाती हैं।
समीक्षित पुस्तक : दिसुम का सिंगार
कवयित्री : सावित्री बड़ाईक
प्रकाशन : अनुज्ञा प्रकाशन, नई दिल्ली
मूल्य : 350 रुपए (अजिल्द), 450 रुपए (सजिल्द)
[1] ‘दिसुम का सिंगार’ (सावित्री बड़ाईक) में संकलित कविता– ‘वे लोहा ले रही हैं’
[2] वही, ‘धान’
[3] वही, ‘दिसुम का सिंगार’
[4] वही, ‘छोड़ब नहीं हुनर’
[5] रमणिका गुप्ता (संपा.), आदिवासी स्वर और नयी शताब्दी, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 8
[6] वही, ‘दिसुम का सिंगार’
[7] वही, ‘आदिवासी स्त्रियां गाती हैं क्रांति गीत’
[8] वही ‘हाट में आदिवासी’
(संपादन : राजन/नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in