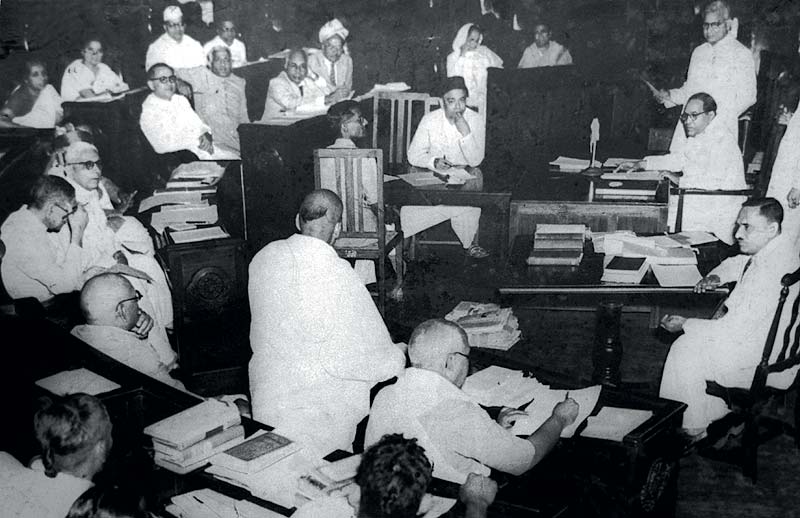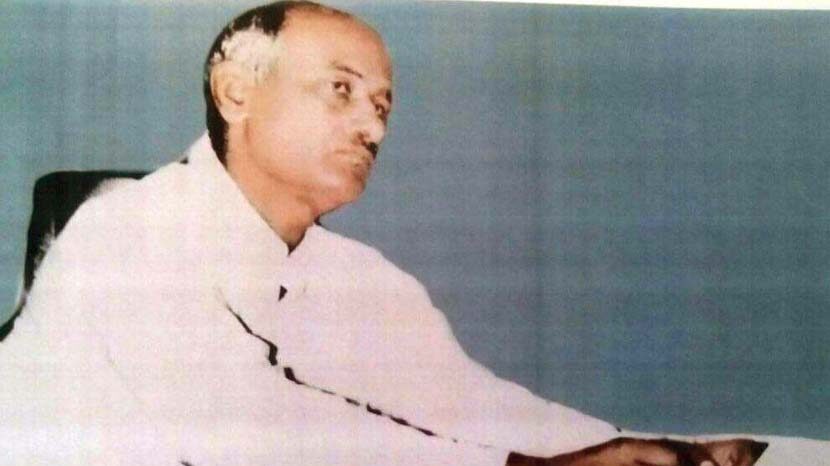वन्नियार, तमिलनाडू की एक ऐसी पिछड़ी जाति है जो लम्बे समय तक कृषि से जुड़ी हुई थी – भूस्वामी के रूप में नहीं, वरन बटाईदार और मजदूर के रूप में। उत्तरी तमिलनाडू में इस जाति की खासी आबादी है और कई संगठनों के जाल के जरिए इस जाति के सदस्य, एक सूत्र में बंधे हुए हैं। शहरीकरण और जमींदारों की विदाई के कारण, बटाईदारों को कुछ हद तक जमीनों पर मालिकाना हक मिला। इस जाति का एक तबका बुनकर भी है। हाल के वर्षों में, वन्नियार, अन्य व्यवसायों से भी जुड़ गए हैं। आरक्षण के कारण उन्हें सरकारी नौकरियां भी मिलीं हैं यद्यपि आज भी, विभिन्न कामधंधों में उनकी भागीदारी, आबादी में उनके हिस्से के अनुपात में नहीं है। उनमें से अधिकांश आज भी खेती ही कर रहे हैं और खेती से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। नेवेली लिग्नाइट बिजली कारखाने के आसपास के इलाके में उन्हें उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया। वन्नियार सुसंगठित हैं और द्रविड़ पार्टियों, कांग्रेस और सीमित संख्या में वामपंथी किसान सभाओं में राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। उनका राजनैतिक नेतृत्व, वन्नियारों, जो कि अति पिछड़ा वर्ग घोषित कर दिए गए हैं, को आरक्षण कोटे में निश्चित हिस्सा दिलवाने के लिए आंदोलनरत रहा है। इस जाति के राजनैतिक नेतृत्व का यह प्रयास भी रहा है कि उसे केन्द्र अथवा राज्य में सत्ता में सत्ताधारी राजैतिक दलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके।
एक अन्य जाति जिसकी हम चर्चा करेंगे वह मुकुल्लाथौर है। यह, दरअसल, कई समुदायों का एक समूह है, जिनकी बड़ी आबादी राज्य के दक्षिणी जिलों में रहती है। इसका एक तबका विमुक्त समुदाय भी है। इस समूह की जातियां, जिनमें अगामुदय्यार, कल्लार और मारवार शामिल हैं, कृषक समाज के हाशिए पर रहे हैं। पूर्व आधुनिक काल में वे मुख्यतः कानून-व्यवस्था बनाए रखने का और योद्धा के रूप में काम करते थे। वे किसी विशेष व्यवसाय से जुडे़ नहीं हैं, यद्यपि पूर्वी जिलों में उनमें से कुछ खेती करते हैं और प्रभावशाली ज़मींदार भी हैं। उनमें से कई औपनिवेशिक राज के अंतिम दौर में श्रीलंका और मलाया (आज के मलेशिया और सिंगापुर) के चाय और रबर बागानों में काम करने के लिए चले गए थे। कई ने औपनिवेशिक सरकार के अधिकारियों और मिशनरियों के प्रभाव में आकर अपने लड़ाकूपन का त्याग कर खेती शुरू कर दी और केरल से सटे राज्य के केन्द्रीय ज़िलों में बस गए। इन समुदायों का उभार सन 1925 में शुरू हुआ, जब उनके बीच से एक करिश्माई और शक्तिशाली स्थानीय नेता उभरा। उसे अब एक श्रद्धेय पूर्वज का दर्जा दे दिया गया है और इसी रूप में उसकी आराधना की जाती है। सन 1980 के दशक में शासक एआईएडीएमके ने उन्हें राजनीतिक समर्थन दिया और इससे भी उनकी ताकत में बढ़ोत्तरी हुई। स्थानीय परिस्थितियों, राजनीतिक संरक्षण और आरक्षण के चलते वे दक्षिणी जिलों में पुलिस और राजस्व महकमों के निचले दर्जों के पदों पर बड़ी संख्या में नियुक्त हो गए।

इसके साथ ही, मुकुल्लाथौरों का एक तबका वामपंथी आंदोलन में भी सक्रिय था, विशेषकर उन इलाकों में जहां वे खेती करते थे। इस जाति के कुछ सदस्य वाम नेतृत्व वाली ट्रेड यूनियनों में भी शामिल हो गए। द्रविड़ पार्टियों, फारवर्ड ब्लाक और कांग्रेस में भी इस जाति के सदस्यों की खासी मौजूदगी है।
एक तीसरा समुदाय जो काफी प्रभावशाली बन गया है वह है गोंडर, जिन्हें कोंगू वेलेला भी कहा जाता है। वे मूलतः किसान हैं। पश्चिमी तमिलनाडू के उन इलाकों में, जहां बहुत कम वर्षा होती है, अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने खेती करनी शुरू की और उनके कौशल और श्रम को औपनिवेशिक प्रशासकों ने भी सराहा। इस क्षेत्र में आर्थिक परिवर्तनों के चलते इस समुदाय के कुछ सदस्यों ने खेती छोड़ उद्यम स्थापित किए और आज उनमें से कई वस्त्र और उससे जुड़े उद्योगों से संबंधित इकाईयों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। वे होज़री इकाईयां भी चला रहे हैं और अपने उत्पादों का निर्यात भी कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश इकाईयां औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध तिरूप्पुर नगर में स्थित हैं। गोंदरों के जातिगत बंधुत्व ने उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजी जुटाने में उनकी मदद की। यद्यपि उनके बीच अब भी वर्गीय अंतर बरकरार हैं, तथापि कुल मिलाकर, यह जाति सफल और तेज़ी से ऊपर उठती हुई मानी जाती है। राजनीतिक दृष्टि से इस जाति का श्रेष्ठी वर्ग राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, यद्यपि बड़ी संख्या में इस जाति के सदस्य द्रविड़ और कम्युनिस्ट आंदोलन में भी शामिल थे। इस पूरे क्षेत्र में जाति-आधारित संगठनों की भरमार है और उनकी पहचान की राजनीति व ज्यादा से ज्यादा आरक्षण पाने की उनकी इच्छा ने उन्हें छोटे नगरों और ग्रामीण इलाकों के नेताओं का प्रियपात्र बना दिया है। इन जाति संगठनों को संबंधित जातियों का सम्पन्न तबका बिना प्रचार के आर्थिक सहयोग देता है।
चौथी जाति है नाडर, जो 19वीं सदी में लगभग अछूत माने जाते थे। आज वे तमिलनाडू के सबसे उन्नतिशील समुदायों में शामिल हैं। उनमें से कुछ सफल उद्यमी और शिक्षा शास्त्री हैं और उनके कामधंधे तमिलनाडू में ही नहीं वरन पूरे देश में फैले हुए हैं। यद्यपि नाडर ओबीसी का साथ देते आए हैं तथापि दलितों से उनकी कभी कोई प्रतिद्वंदिता नहीं रही। उनमें जाति से बाहर शादी करने पर उतने कड़े प्रतिबंध नहीं हैं, जितने कि अन्य जातियों में हैं। इस समुदाय का एक हिस्सा हिन्दुत्व की विचारधारा की ओर भी आकर्षित हो गया है और इसका एक कारण है मुसलमानों के साथ व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। यह विडंबनापूर्ण ही है क्योंकि आत्मसम्मान आंदोलन जब अपने चरम पर था, तब वे पेरियार के कट्टर समर्थकों में गिने जाते थे। जातिगत पदक्रम में उनके स्थान के बारे में संशय की स्थिति के चलते उन्हें अछूत प्रथा का ‘पालन‘ तो नहीं बनना पड़ा परंतु सामाजिक पदक्रम में अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वे वर्णधर्म का पालन करते रहे हैं। कुछ नाडर हिन्दुत्व आंदोलन से भी जुड़ गए हैं और इससे यह पता चलता है कि जातिगत पदक्रम किस तरह से धर्मनिरपेक्ष-धार्मिक ढांचे से जुड़ा हुआ है।
इन जातियों में से वन्नियार, मुकुल्लाथौर और गोंदर, दलितों पर हमलों में अग्रणी भूमिका निभाते आए हैं। इसके साथ-साथ, सत-शूद्र व वे तथाकथित अति-पिछड़ी जातियां, जो स्थानीय दृष्टि से वर्चस्वशाली हैं, भी मंदिरों में प्रवेश के मामले में दलितों को समान अधिकार देने की विरोधी रही हैं और ऐसी विवाहों के भी विरूद्ध रही हैं, जिनमें वर या वधु में से एक दलित हो।
दलितों पर हमले, दरअसल, एक प्रकार की सामाजिक असुरक्षा के भाव से उपजते हैं। जो दलित शिक्षा पा रहे हैं और उन्नति कर रहे हैं, वे जातिगत पदक्रम के नियमों की अवहेलना करते है और ऐसा करने वालों को उच्च व मध्यम जाति के लोग अपने लिए खतरा मानने लगते हैं। इस असुरक्षा के भाव का प्रकटीकरण हिंसा के रूप में होता है, जिसे अक्सर जाति संगठनों और राजनैतिक दलों का समर्थन हासिल होता है।
दलित नेता और राजनैतिक दल जो प्रश्न उठाते रहे हैं वह यह है कि जातिगत हितों, जो दलितों के प्रति बैरभाव के रूप में प्रकट होते हैं, के रहते हुए भी इस राज्य में एक शक्तिशाली जाति-विरोधी आंदोलन कैसे खड़ा हो गया और किस प्रकार इस आंदोलन का नेतृत्व सत्ता में आ सका। युवा दलित बुद्धिजीवी यह तर्क देते हैं कि इन जातियों के राजनैतिक और आर्थिक दबदबे और दलितों पर उनकी दादागिरी से यह जाहिर होता है कि द्रविड़ आंदोलन की सफलता सीमित थी। यह आंदोलन केवल ब्राह्मण-विरोधी राजनीति बनकर रह गया और जाति-विरोधी राजनीति का स्वरूप ग्रहण न कर सका। उनका यह भी कहना है कि यह आंदोलन और उसके सर्वेसर्वा पेरियार, जाति का विरोध करने में उतनी रूचि नहीं रखते थे जितनी कि वे ब्राह्मणों का विरोध करने में रखते थे।

इस प्रश्न का उत्तर आसान नहीं है। लगभग 50 साल से राज्य में गैर-ब्राह्मण सरकारों के शासन के बावजूद, दलितों के खिलाफ हिंसा जारी है और दलितों की सीमित सफलता के विरूद्ध शत्रुता का भाव आज भी बना हुआ है। इस मुद्दे का गंभीरता से अध्ययन किया जाना चाहिए और ऐसा करने के लिए, हमें बीते समय का अध्ययन तो करना ही होगा, हमें यह भी देखना होगा कि उस अतीत का इस्तेमाल आज के सरोकारों को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने और उनकी व्याख्या करने के लिए कैसे किया जा रहा है।
तमिलनाडू में जहां बड़ी संख्या में ऐसे दलित बुद्धिजीवी हैं जो अपने जाति-विरोधी संघर्ष की प्रेरणा पेरियार के विचारों से लेते हैं (वे मुख्यतः वे हैं जो द्विभाषी नहीं हैं और इसलिए उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर पढ़ा नहीं जाता), वहीं उतनी ही संख्या में ऐसे बुद्धिजीवी भी हैं जो अपने-अपने कारणों से व अलग-अलग तर्कों के आधार पर यह कहते हैं कि पेरियार दलितों के लिए अप्रासंगिक हैं।
जाति के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध
हम सबसे पहले यह ज़ोर देकर कहना चाहते हैं कि यह तर्क कि पेरियार जाति के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध नहीं थे, न तो इतिहास की कसौटी पर खरा उतरता है और ना ही अवधारणात्मक आधारों पर। यह कहना भी ठीक नहीं है कि पेरियार के सरोकार केवल गैर-ब्राह्मणों को ब्राह्मणों के बराबर दर्जा दिलवाने तक सीमित थे। अगर हम पेरियार के लंबे राजनीतिक जीवन का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि उन्होंने और उनके द्वारा स्थापित संगठनों व उनके आंदोलन के चिंतकों व सदस्यों ने लगातार जाति के विरोध में राजनीति की। यह अवश्य है कि अलग-अलग समय पर उनका ज़ोर अलग-अलग चीज़ों पर रहा और उनके तर्क भी बदलते रहे।
1925-1931 की अवधि में, पेरियार और उनके आत्मसम्मान आन्दोलन ने आमूल परिवर्तनवादी नास्तिकता का प्रचार किया और अछूत प्रथा के निवारण और दलितों को उनके नागरिक अधिकार दिलवाने व मंदिरों सहित सभी सार्वजनिक स्थलों में उनके प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों को हटवाने के लिए सघन प्रयास किये। उन्होंने राजनैतिक ब्राह्मणवाद-जो उनकी दृष्टि में कांग्रेस का राष्ट्रवाद था-का सैद्धांतिक आधारों पर ज़ोरदार विरोध किया। वे राजनैतिक ब्राह्मणवाद की जमकर निंदा करते थे और उसका मखौल बनाते थे। वे ब्राह्मणवादी हिन्दू धर्म के भी उतने ही कड़े आलोचक थे और हिन्दू धर्मग्रंथ, कर्मकांड और परंपराएं भी उनकी आलोचना से बच न सके। महिलाओं के मुद्दे पर भी उनके सुस्पष्ट विचार थे और वे महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के हामी थे। उनका यह मानना था कि महिलाओं को यौन संबंधों और विवाह के मामलों में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए और उन्हें समानता, न्याय और जनसाधारण की बेहतरी के लिए सार्वजनिक जीवन में हिस्सेदारी करने का बराबर अधिकार मिलना चाहिए।

सन 1932 से 1937 के बीच, विशेषकर 1935 तक, अपनी सोवियत संघ की यात्रा (1931-1932) के बाद पेरियार की जाति की समालोचना, उसके आर्थिक व भौतिक बुनियाद की समालोचना पर आधारित थी। आत्मसम्मान आंदोलन के पहले दशक के दौरान पेरियार ने गैर-ब्राह्मण शूद्रों और शत-शूद्र जातियों, दलितों, पढ़े-लिखे और शिक्षित पुरूषों और महिलाओं और गरीबों सभी को अपने आंदोलन का हिस्सा बनाया। दलित समूह, जातियों के संगठन व गैर-ब्राह्मण नागरिक समूह आत्मसम्मान आंदोलन से जुड़े हुए थे और पेरियार और उनके साथी इन सभी के मंचों से बोलते थे। दलितों के समानता और न्याय हासिल करने के अधिकार को पेरियार कितना महत्वपूर्ण मानते थे यह इससे साबित होता है कि आत्मसम्मान आंदोलन ने ‘‘कम्युनल अवार्ड’’ पर बाबासाहेब आंबेडकर के दृष्टिकोण का पूर्ण समर्थन किया और यह आंदोलन गांधी का उतना ही कड़ा आलोचक था, जितने कि आंबेडकर भविष्य में बने।
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तमिलनाडू या पुराने मद्रास में दलित प्रश्न पर विचार करने वाले पेरियार न तो पहले और न ही एकमात्र व्यक्ति थे। जैसा कि पंडित आईयोथी थास के जीवन और लेखन से स्पष्ट है, 19वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों या शायद उसके भी पहले से, इस इलाके में दलित संगठन, चर्च और समाचारपत्र दलितों के अधिकारों की बात करते आ रहे थे। युवा दलित अध्येताओं जैसे माथिवन्नन, स्टालिन राजंगम, रघुपति और बालासुब्रमण्यम द्वारा किए गए शोध से यह सामने आया है कि दलितों को एकसूत्र में बांधने के प्रयासों का इतिहास बहुत जटिल और पुराना है और यह उन क्षेत्रों तक सीमित नहीं था, जहां कांग्रेस, द्रविड़ आंदोलन या वाम आंदोलन का प्रभाव था। इसलिए, एक तरह से, पेरियार एक ऐसे समूह को संबोधित कर रहे थे, जिसका पहले से ही राजनीतिकरण हो चुका था। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने गणतंत्रवाद और महिलाओं की समानता से संबंधित कई चौका देने वाले और नए सिद्धांत प्रस्तुत किए, परंतु ब्राह्मणों और हिन्दू धर्म की उनकी आलोचना, दलित राजनैतिक क्षेत्रों के लिए नई नहीं थी। यह आलोचना सन 1890 के दशक से जारी थी।
कुल मिलाकर, जाति-विरोधी राजनीति के पहले दशक में जाति के उन्मूलन का आह्वान किया गया और इसका ज़रिया बना आत्मसम्मान पर आधारित बंधुत्व की राजनीति और ब्राह्मणवादी हिन्दू धर्म और मंदिरों में की जाने वाली आराधना की निंदा। यह राजनीति, तार्किकता और सामाजिक व लैंगिक समानता पर आधारित थी। आत्मसम्मान पर आधारित अपनी पहचान का निर्माण, जाति से मुक्त जीवन जीने का एक आवश्यक तत्व माना गया।
सन 1938 से 1947 के बीच जब आत्मसम्मान आंदोलन ने तमिलनाडू में शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी को थोपे जाने के विरूद्ध आंदोलन किया, तब भी इसमें राजनैतिक ब्राह्मणवाद की आलोचना निहित थी। पेरियार और उनके अनुयायियों का यह मानना था कि हिन्दी थोपने का प्रयास, दरअसल, राष्ट्रवादी ब्राम्हण-बनिया गठबंधन की राजनीति और संस्कृति को तमिलनाडू पर थोपने का प्रयास था। उनका यह मानना था कि इससे भारतीय राष्ट्रवाद संकीर्ण बनेगा और ऊँची जातियों के प्राधान्य को मज़बूती मिलेगी। इस दशक में जाति की आलोचना से राष्ट्रवाद की आलोचना भी जुड़ गई। भारत उन दिनों स्वतंत्रता के मुहाने पर खड़ा था और इस आलोचना को स्वर दिया द्रविड़ राष्ट्रवाद ने। यह इस आंदोलन के इतिहास का सबसे जटिल हिस्सा है, क्योंकि इसके कई परिणाम हुए। इसने द्रविड़ राष्ट्र के आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग को स्वर दिया और यह तर्क दिया कि द्रविड़ राष्ट्र, जातिमुक्त आदर्शलोक होगा। यद्यपि इस राजनीति में जाति की आलोचना निहित थी, तथापि उसमें पहले जितना सामाजिक पैनापन नहीं था।
सन 1948 से 1952 के बीच पेरियार का गुस्सा हिन्दू-हिन्दी-हिन्दुस्तान पर फूट पड़ा और वे वामपंथ के नज़दीक आए। परंतु 1952 के पहले आम चुनाव के बाद से लेकर 1967 तक उन्होंने व्यावहारिक राजनीति की। उन्हें लगा कि गैर-ब्राह्मण कांग्रेस नेता के. कामराज (जो 1954 से 1963 तक तमिलनाडू के मुख्यमंत्री थे) की सरकार, सामाजिक न्याय के उनके स्वप्न को पूरा कर सकेगी। इस स्वप्न में शामिल था आरक्षण, राजनैतिक पदों पर गैर-ब्राह्मणों की नियुक्तियां और आधुनिक औद्योगिक विकास। जाति की उनकी आलोचना ने अब के. कामराज की नीतियों के समर्थन का रूप ले लिया। पेरियार, सकारात्मक भेदभाव के हामी बन गए और आधुनिक, सामाजिक, व आर्थिक व्यवस्था के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध हो गए।
इस दौर में, विशेषकर 1950 के दशक के पूर्वाद्ध में पेरियार ने यह स्वीकार किया कि डा. आंबेडकर, उनके विचार और उनके संगठन तथा दलितों के हितों का बेहतर संरक्षण कर सकते हैं। जो लोग पेरियार को ठीक से नहीं समझ पाते, उन्हें ऐसा लग सकता है कि पेरियार ने स्वयं को शूद्रों के नेता के रूप में प्रस्तुत किया ना कि जाति-विरोधी राजनीतिज्ञ के रूप में।
इस जटिल राजनैतिक इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम पेरियार की विरासत का किस प्रकार आंकलन करें? द्रविड़ आंदोलन ने उनकी राजनीतिक विरासत के आधार पर सीमित सफलता हासिल की, विशेषकर आरक्षण व लोकलुभावन जनकल्याण योजनाओं के संदर्भ में। कामराज के समय जहां जनकल्याण कार्यक्रम, नीतियों का हिस्सा थे, वहीं एआईएडीएमके के दौर में इनने एक नया रूप ले लिया। इसके नतीजे में आज स्थिति यह बन गई है कि द्रविड़ आंदोलन के चिंतक और नेता, चाहे वे किसी भी राजनैतिक दल से जुड़ें हों, ‘दमित’ माने जाने लगे। दूसरी ओर, द्रविड़ राजनैतिक दलों ने जाति व्यवस्था के श्रेणीबद्ध पदक्रम, जातिगत शक्ति के भौतिक आधार और उसके सांस्कृतिक पक्ष, जिनमें विवाह शामिल हैं, को पीछे धकेल दिया और चुनावी राजनीति में लाभ पाने के लिए विशिष्ट जातियों को आकर्षित करने के प्रयास शुरू कर दिए।
अगर हम पेरियार की राजनैतिक यात्रा और तमिलनाडू की प्रमुख जातियों के जीवन और उनकी नियति में आए ऐतिहासिक परिवर्तनों को एकसाथ रखकर देखें तो हमें यह पता चलेगा कि पेरियार की भारतीय राज्य-विरोधी राजनीति, उनका ब्राम्हण विरोध और त्रुटिपूर्ण संघीय ढांचे के प्रति उनकी वितृष्णा ने एक ऐसी विचारधारा या योजना को जन्म नहीं दिया जो जाति के उन्मूलन में सहायक बन सकती थी, यद्यपि उसमें ऐसा करने के लिए आवश्यक विचारधारात्मक उपकरण मौजूद थे। पेरियार द्वारा 1944 में स्थापित ‘द्रविड़ कषगम’ ने कुछ मामलों में बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाई, जिनमें शामिल था जातिगत हिंसा के मामलों में दलितों का साथ देना और अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन व समर्थन। परंतु यह पार्टी एक ऐसा कार्यक्रम नहीं तैयार कर सकी जिससे उसकी विभिन्न गतिविधियों के समन्वय से कोई योजना बनाई जा सके। इस बीच, विकास और चुनावी राजनीति (जिनका संक्षिप्त विवरण हमने तमिलनाडू की चार सबसे वर्चस्वशाली पिछड़ी व अतिपिछड़ी जातियों के इतिहास की चर्चा करते हुए दिया है) ने पुराने और स्थानीय जातिगत पदक्रम को नया जीवन दिया, यद्यपि दलित इसे लगातार चुनौती देते रहे। इसका अंतिम परिणाम था दलितों के विरूद्ध घृणा, हिंसा और गुस्से का ज्वार।

अब हम कथित पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों पर वापिस आएं। इन जातियों के वे सदस्य, जो द्रविड़ ‘कषगम’ के साथ विचारधारा व कार्यक्रम के स्तर पर जुड़े थे, ने स्वतंत्रता के बाद के काल में सार्वजनिक और राजनैतिक मंचों से ब्राह्मणों की सत्ता और जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष तो किया, परंतु इसके साथ ही वे अपने रहवास के क्षेत्र, व्यवसाय और हिन्दू धर्म से अपने रिश्ते से परिभाषित विशिष्ट जातियों के सदस्य भी बने रहे। दलितों के साथ उनके रिश्ते इन दोनों कारकों से प्रभावित थे। कुछ मामलों में ये रिश्ते सकारात्मक थे और कम से कम सार्वजनिक रूप से बंधुत्व भाव पर आधारित थे तो अन्य मामलों में ये नकारात्मक भी थे, विशेषकर दर्जे, प्रधानता और सार्वजनिक संसाधनों पर अधिकार की प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में। उदाहरण के लिए अगर हम वन्नयारों की बात करें तो वे भारतीय राज्य के खिलाफ अपने अभियान या तमिल भाषा को बढ़ावा देने के अपने आंदोलन और सीमित वर्गीय संघर्षों में दलितों को अपना साथी मानते थे परंतु वे उनसे प्रतिद्वंदिता भी रखते थे। वे अपने लिए अधिक आरक्षण चाहते थे और इसके लिए अपने ‘पिछड़ेपन‘ का बखान भी करते थे। श्रेणीबद्ध असमानता के संदर्भ में उनकी यह मांग न्यायपूर्ण हो सकती थी परंतु दलितों के खिलाफ हिंसा करने के कारण उनके दावों की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है।
मुकुल्लाथौरों के मामले में स्थिति दूसरी थी। उन्हें सन् 1950 के दशक, बल्कि उसके पहले से ही, दलितों से चुनौती मिल रही थी और उन्होंने दलितों को हमेशा अपनी आवाज उठाने और स्वाधीन होने के उनके प्रयासों के लिए ‘सजा‘ देने का प्रयास किया। वे राजनीति में दलितों के अपने लिए अलग स्थान बनाने के प्रयासों के भी विरोधी थे। वे डा. आंबेडकर या अन्य स्थानीय दलित नेताओं (जैसे कि दलितों की श्रद्धा के पात्र इमेन्यूअल शेखरन, जिन्हें मुकुल्लाथौरों के एक समूह ने जान से मार डाला था) की मूर्तियां स्थापित करने के भी विरोधी थे।
गोंडरों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अलग राह चुनी। इस सिलसिले में डा. बालगोपाल की ‘‘प्रांतीय संपत्तिधारी वर्गों‘‘ की विवेचना उपयोगी है। उनका तर्क है कि आंध्रप्रदेश में ये वर्ग, जिनमें रेड्डी और नायडू शामिल थे, ने क्षेत्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय कांग्रेस के विरूद्ध अपना राजनैतिक रसूख और सत्ता कायम करने की कोशिश की। उनके लिए दलितों के विरूद्ध दंडात्मक हिंसा अपनी राजनैतिक शक्ति का प्रदर्शन करने का आवश्यक हिस्सा थी। यद्यपि गोंडर कांग्रेस के विरोधी नहीं हैं, परंतु वे एक ऐसे शक्तिशाली कृषक समुदाय हैं जिसने उद्योग-धंधों के जरिए संपत्ति अर्जित की और आगे बढ़े। वे अपने सामाजिक वर्चस्व को रेखांकित करने के लिए दलितों के खिलाफ हिंसा और उनका अपमान करते आए हैं।
संक्षेप में, तमिलनाडू के मामले में कुछ बातें एकदम साफ हैं। 20वीं सदी की शुरूआत से ही गैर-ब्राम्हणों और दलितों ने ब्राम्हणों की सत्ता को चुनौती देनी शुरू किया और विभिन्न उद्धेश्यों से एकसाथ मिलकर काम किया। परंतु उनकी एकता न तो वर्गीय एकता थी और ना ही जाति व्यवस्था के प्रति उनके एक से दृष्टिकोण से जन्मी थी। यह केवल ब्राह्मणों की सत्ता के खिलाफ क्रोध का प्रकटीकरण था और एक तरह से अवसरवादी राजनीति थी। इसमें कोइ संदेह नहीं कि इन वर्गों ने पेरियार, उनके आत्मसम्मान आंदोलन और उसके बाद द्रविड़ कषगम द्वारा वर्णधर्म की आलोचना को सुना और कुछ ने उसे आत्मसात भी किया। उन्होंने आस्था, विशेषकर हिन्दू धर्म, की आलोचना को भी सुना और समझा। दलितों ने इस आलोचना को अन्यों की तुलना में अधिक आत्मसात किया। जातिगत सत्ता के खिलाफ अनेक अभियान चले जो विशिष्ट मांगों पर केन्द्रित थे, विशेषकर 1920 के दशक से लेकर 1940 के दशक के अंत तक। यद्यपि विचारधारा के स्तर पर जाति का उन्मूलन, ब्राम्हणवादी हिंदुत्व के विरोध का केन्द्रीय तत्व था तथापि इस विरोध ने जाति के उन्मूलन के लिए किसी विशिष्ट कार्यक्रम का सृजन नहीं किया। किसी दौर में जोर अछूत प्रथा के उन्मूलन पर रहा तो अन्य दौरों में आर्थिक समानता और गैर-ब्र्र्राम्हणों के जातिगत गौरव की निंदा पर। एक दौर में महिलाओं की स्वाधीनता और आत्मसम्मान केन्द्र में था। सन् 1940 के दशक के बाद से जाति के उन्मूलन को अन्यायपूर्ण संघीय ढांचे और ब्राम्हण-बनिया आर्य राज्य को चुनौती देने से जोड़ दिया गया और जातिमुक्त द्रविड़नाडू की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। परंतु जब जाति विरोधी एजेंडा राष्ट्रवाद के विरोध की वृहद राजनीति का हिस्सा बन गया और पेरियार ने एकात्मक भारतीय राज्य के खिलाफ झंडा उठा लिया, तब द्रविड़ समुदाय, विशेषकर दलितों और अन्य जातियों के बीच की खाई, तनावों, विरोधाभासों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।
जाति का पहाड़
पेरियार अपने जीवन और कार्यों की उपादेयता के संबंध में बहुत आशावादी नहीं थे। अपनी मृत्यु के कुछ महीनों पहले आल इंडिया रेडियो को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उनका जीवन एक बाल के सहारे जाति के पहाड़ को पलटने के प्रयास से ज्यादा नहीं था। उन्होंने वह किया जो उन्हें उचित और न्यायपूर्ण लगा परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि न्याय प्राप्त हो गया। संघर्ष बहुत कठिन, लंबा और थकाने वाला था।
अंत में हम वामपंथियों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। वे वर्चस्वशाली, वर्गीय-जातिगत गठबंधन को उसकी सत्ता से बेदखल तो करना चाहते थे परंतु श्रेणीबद्ध असमानता से मुकाबला करने के लिए उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं था। वे उस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करना नहीं चाहते थे जो डा. आम्बेडकर के शब्दों में श्रम विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन थी। निश्चय ही विशिष्ट संदर्भों और संघर्षों में प्रेमपूर्ण बंधुत्व बना परंतु प्रश्न यह है कि क्या इसने नए बंधुत्ववादी सामाजिक मूल्यों को जन्म दिया, उस तरह की जिंदगी का निर्माण किया जिसकी कल्पना डा. आंबेडकर और पेरियार ने की थी। सन् 1940 के दशक और 1950 के दशक की शुरूआत में वामपंथियों ने द्रविड़ कषगम के कुछ घटकों के साथ मिलकर काम किया और जाति आधारित भेदभाव और हिंसा के विरूद्ध संघर्षों का समर्थन किया। उन्होंने खेतिहर मजदूरों के अपने संगठनों और ट्रेड यूनियनों, विशेषकर बागानों, चमड़ा उद्योग और साफ-सफाई से संबंधित श्रमिक संगठनों में दलितों को बड़ी संख्या में सदस्य बनाया। परंतु दलितों के स्वायत्त संगठन और ट्रेड यूनियनें भी थीं और बहुत कम मौकों पर दलित और वामपंथी संगठनों ने मिलकर काम किया। स्पष्टतः वामपंथी संगठन अधिक संगठित थे और उनके पास संसाधन भी अधिक थे। उन्हें दलित समूहों से यह सीखना था कि जाति का प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है और उसे वह महत्व देना था, जिसका वह हकदार था। यह दुःखद है कि ऐसा करने की बजाए संसदीय वामपंथियों ने एक या दूसरी द्रविड़ पार्टी के साथ अवसरवादी गठबंधन बनाकर विधानसभा में अपनी नाममात्र की उपस्थिति सुनिश्चित कर अपनी राजनीति की इतिश्री कर ली।
पिछले एक दशक में स्थितियों में कुछ परिवर्तन आए हैं। हालिया विधानसभा चुनाव में वामपंथी और दलित समूहों ने मिलकर काम किया और यह केवल एक रणनीतिक गठबंधन नहीं था। सीपीएम का अछूत प्रथा विरोधी मोर्चा और दलित राजनैतिक दल विदुथलाई सिरूथाईगल काची (वीसीके) भी मिलकर काम कर रहे हैं।
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +919968527911, ईमेल : info@forwardmagazine.in