ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलने की मंडल कमीशन की अनुशंसा को लागू हुए वर्षों बीत गए। इसके बाद भी ओबीसी वर्ग में शामिल जिन जातियों को आरक्षण की दरकार सबसे अधिक थी, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल सका। इस स्थिति ने केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय और पिछड़े वर्गों के लिए बने राष्ट्रीय आयोग (एनसीबीसी) को ओबीसी के उप वर्गीकरण के सवाल पर गंभीरतापूर्वक विचार करने पर विवश किया।
इसके तहत ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए एक पांच सदस्यीय आयोग का गठन 2 अक्टूबर 2017 को किया गया और इसकी कमान सेवानिवृत्त न्यायाधीश जी. रोहिणी को सौंपी गई। यह आयोग राजनीतिक रूप से इस बेहद संवेदनशील मुद्दे की पड़ताल कर रहा है।
नवंबर 2018 में इस आयोग द्वारा सरकार को रिपोर्ट सौंपी जानी है।
इस आयोग को जो जिम्मेदारी दी गई है, उसमें कई सवाल समाहित हैं। इसमें ओबीसी में शामिल जातियाें के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण का सवाल उल्लेखनीय है। लेकिन, यह कैसे हाे और इसके लिए उचित तंत्र, मानदंड एवं पैरामीटर क्या हाेने चाहिए? पहले यह तय हाे। इसके अलावा इस आयाेग काे उन जातियों की पहचान भी करनी है, जिन्हें उप वर्गीकरण में शामिल किया जाना है। वर्ष 2015 में पिछड़ा वर्ग आयाेग ने प्रस्ताव दिया था कि ओबीसी को निम्नलिखित तीन वर्गों मे विभाजित किया जाए :-
वर्ग 1- अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी ग्रुप ए) : ओबीसी में शामिल वे जातियां जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं। इनमें अादिवासी, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू जनजातियां भी शामिल हैं; जिनकी आजीविका का साधन उनके पारंपरिक पेशे हैं। वर्ग 2- अधिक पिछड़ा वर्ग (एमबीसी ग्रुप बी) : इसमें वे समूह शामिल हैं, जो अभी भी आजीविका के लिए अपने पारंपरिक साधनों पर निर्भर हैं।
वर्ग 3- पिछड़ा वर्ग (बीसी ग्रुप सी) : इसमें ओबीसी की संपन्न जातियां शामिल हैं।

उप वर्गीकरण के इस मुद्दे ने पहले और दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोगों का ध्यान भी अपनी अाेर खींचा था। यही वजह रही कि काका कालेलकर की अध्यक्षता वाले पहले पिछड़ा वर्ग आयोग (1955) ने 2,399 जातियों की एक सूची प्रस्तुत की और इनमें से 837 को ‘सबसे पिछड़ा’ के रूप में वर्गीकृत किया। एल.आर. नाईक (दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य) ने मध्यम पिछड़ा वर्ग और दमित पिछड़ा वर्ग के रूप में ओबीसी के वर्गीकरण का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने इन दो उप समूहों में क्रमशः 12 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के अनुपात में 27 प्रतिशत के कुल आरक्षण के आवंटन का सुझाव दिया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार (2004-2014) ने भी ओबीसी वर्ग में शामिल जातियों के बीच आरक्षण के असमान वितरण के सवाल को संज्ञान में लिया। इस असमान वितरण के कारण आरक्षण का लाभ ओबीसी वर्ग में शामिल उन जातियों को मिल जाता है, जो अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध हैं।
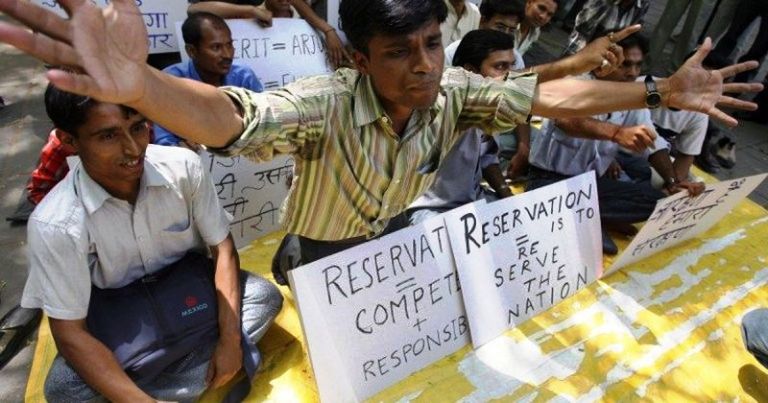
यही वजह रही कि कांग्रेस ने 2014 के अपने घोषणापत्र में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लोगों को सशक्त बनाने के लिए आरक्षण की लाभार्थी जातियों की पहचान हेतु एक विशेष आयोग के गठन का वादा किया था।
एनसीबीसी के अनुसार, 10 राज्य सरकारों ने (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु) ने अपने संस्थानों में ओबीसी को उप वर्गीकृत किया है। पिछले वर्ष 26 अक्टूबर 2017 को राजस्थान भी इस सूची में शामिल हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा है कि ओबीसी का उप वर्गीकरण किया जाना चाहिए, ताकि आरक्षण का समुचित और सही तरीके से पुनर्वितरण हो सके। इसके बावाजूद केंद्र और राज्यों के स्तर पर ओबीसी आरक्षण की स्थिति जस की तस है।
- जनवरी 2017 तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में ग्रुप-ए में 503 अधिकारियों में केवल 25 (4.97 प्रतिशत) अधिकारी ओबीसी के हैं।
- 2015 में 24 मंत्रालयों ने आंकड़े उपलब्ध कराए। इनमें से 12 मंत्रालयों, 10 विभागों और पांच संवैधानिक निकायों के ग्रुप-ए में ओबीसी अधिकारियों का प्रतिनिधित्व केवल 10.71 प्रतिशत था। वहीं, ग्रुप-बी के अधिकारियों में यह प्रतिनिधित्व 7.18 प्रतिशत है। शेष मंत्रालयों ने आंकड़े नहीं दिए।
इसलिए, उपलब्ध आंकड़ों से ओबीसी आरक्षण की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं मिलती है। उदाहरण के लिए, ग्रुप-ए, ग्रुप-बी और ग्रुप-सी की केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी के प्रतिनिधित्व के संबंध में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की तीन वार्षिक रिपोर्टें इस बाबत जानकारियों के लिए दी गईं। ये रिपोर्टें 01 जनवरी 2014, 01 जनवरी 2015 और 01 जनवरी 2016 को जारी की गईं। इनमें क्रमश: 71, 63 और 78 मंत्रालयों/विभागों के आंकड़े शामिल थे। इनके अनुसार, ग्रुप-ए, ग्रुप-बी और ग्रुप-सी की केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी की हिस्सेदारी क्रमश: 19.28 प्रतिशत, 18.24 प्रतिशत और 21.58 प्रतिशत बताई गई है।

वर्ष 2018 में लोकसभा में प्रश्नोत्तर-काल के दौरान सरकार की ओर से दिए गए एक जवाब में कहा गया कि 27 प्रतिशत का ओबीसी कोटा कई मंत्रालयों/विभागों में पूरा नहीं हुआ है। जैसा कि सारणी-1 में दिखाया गया है, जो अनिवार्य 27 प्रतिशत के खिलाफ औसत 4.56 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दर्शाता है। हालांकि, प्रदर्शित किए गए आंकड़े मंत्रालय/विभाग तालिका में तीनों आरक्षित श्रेणियों के लिए समान नहीं हैं और ये आंकड़े केवल उन मंत्रालयों से संबंधित हैं, जिनमें आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व निर्धारित हिस्सेदारी से बहुत कम है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरक्षण से ओबीसी (4.56 प्रतिशत) की तुलना में अनुसूचित जाति समूहों (12.37 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजाति समूहों (2.42 प्रतिशत) को अधिक लाभ मिला है। जबकि, इन तीनों समूहों के लिए क्रमश: 27 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
तालिका 1. केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व – 2016
| मंत्रालय / विभाग | एससी (15% अनिवार्य) | मंत्रालय / विभाग | एसटी (7.5% अनिवार्य) | मंत्रालय / विभाग | अोबीसी (27% अनिवार्य) |
|---|---|---|---|---|---|
| अंतरिक्ष | 11.66 | निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन | 1.96 | कृषि अनुसंधान और शिक्षा | 2.78 |
| कार्मिक और प्रशिक्षण | 12.25 | राष्ट्रपति सचिवालय | 2.04 | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | 3.12 |
| पेयजल और स्वच्छता | 12.36 | कैबिनेट सचिवालय | 2.28 | भूमि संसाधन | 5.33 |
| कैबिनेट सचिवालय | 12.70 | सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण | 2.85 | विज्ञान और प्रौद्योगिकी | 5.71 |
| आयुष | 12.87 | पंचायती राज | 2.99 | कोयला | 5.86 |
| औसत | 12.37 | 2.42 | 4.56 |
स्रोत : लोकसभा प्रश्नकाल, द हिंदू, 4 अप्रैल 2018, पृष्ठ-9
इसी प्रकार आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 35 में से 24 केंद्रीय मंत्रालयों, 37 केंद्रीय विभागों में से 25 और विभिन्न संवैधानिक निकायों में मंडल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद भी (8 सितंबर1993 से ) पिछले 24 साल में कर्मचारियों के तीन समूहों में से किसी एक को भी निर्धारित आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका है। (तालिका 2 देखें)। 01 जनवरी 2017 तक, 24 मंत्रालयों में ग्रुप-ए के अधिकारियों में से केवल 17 प्रतिशत ही ओबीसी हैं। वहीं, ग्रुप-बी (14 प्रतिशत), ग्रुप-सी (11 प्रतिशत) और ग्रुप-डी (10 प्रतिशत) ही आेबीसी हैं यानी इन ग्रुप्स में उनका प्रतिनिधित्व ग्रुप-ए से भी कम हैं।
24 मंत्रालयों के कर्मचारियों में, 25 विभाग (37 में से) और आठ संवैधानिक निकायाें (प्रधान मंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय और भारत के निर्वाचन आयोग सहित) को मिलाकर भी ओबीसी की हिस्सेदारी चार समूहों ग्रुप-ए, ग्रुप-बी, ग्रुप-सी और ग्रुप-डी में क्रमश: केवल 14 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 17 प्रतिशत और 18 प्रतिशत है।
हालांकि, अंतर को भरने के लिए समय-समय पर विशेष भर्तियां निकाली भी गईं। लेकिन, यह कहना अतिशयाेक्ति नहीं कि बैकलॉग रह जाने से सामाजिक न्याय का लक्ष्य हासिल नहीं हाे पाता है। यह स्थिति आज भी कायम है।
तालिका 2. 01 जनवरी 2017 को मंत्रालयों के समूहों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व :
| प्रकार | ओबीसी कर्मचारियों का प्रतिशत 24 मंत्रालयों में | 57 मंत्रालयों/विभागों/संवैधानिक निकायों में ओबीसी कर्मचारियों का प्रतिशत |
|---|---|---|
| ग्रुप-ए | 17% | 14% |
| ग्रुप-बी | 14% | 15% |
| ग्रुप-सी | 11% | 17% |
| ग्रुप-डी | 10% | 18% |
स्रोत : द हिंदू, 10 दिसंबर 2017, पृष्ठ-1
सार्वजनिक सेवाओं में ओबीसी के कम प्रतिनिधित्व पर विश्वास करने योग्य आंकड़ों की उपलब्धता के बावजूद, ओबीसी वर्ग के सामुदाय-वार लाभार्थियों के आंकड़ों की अनुपलब्धता और प्रस्तावित उप-वर्गीकरण अभ्यास के बिना ‘कोटा के भीतर कोटा’ की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक दुर्जेय कार्य है।
इस प्रकार, ओबीसी उप वर्गीकरण का कार्य नीचे प्रस्तुत कारकों के कारण वास्तव में कठिन है :
- समुदायों/वर्गों की बड़ी संख्या
ओबीसी की छतरी के तहत बड़ी संख्या में जातियों का अस्तित्व संघीय शासन के भारतीय संदर्भ में उनके वैज्ञानिक उप वर्गीकरण को अत्यधिक चुनौतीपूर्ण बनाता है, जिसमें ओबीसी जातियों की अलग-अलग केंद्रीय और राज्य स्तरीय सूचियां तैयार की जाती हैं; जो दशकों से अपरिवर्तित हैं। कालेलकर आयोग ने 1951 में 11.35 करोड़ की अनुमानित आबादी के साथ 2,399 जातियों की पहचान की, जो देश की आबादी का 32 प्रतिशत है। मंडल आयोग ने 3,743 जातियों को सूचीबद्ध किया, जो कुल भारतीय आबादी का 52 प्रतिशत माना गया। पीपुल्स ऑफ इंडिया सर्वे (1994) में 4,646 जातियों/समुदायों की पहचान की, जिसमें 1,046 ओबीसी जातियां भी शामिल थीं। एनसीबीसी के नवीनतम अभिलेखों के अनुसार, 31 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 2,514 ओबीसी जातियां/समूह हैं।
- विषमता और इसका प्रसार
एक और जटिल मुद्दा विषमता और बड़ी संख्या में ओबीसी जातियों के लोगों की स्थानीय उपस्थिति है। जाति के आंकड़ों के एकत्रीकरण की समस्याओं की दृष्टि से 2001 की जनगणना के संदर्भ में दिल्ली संगोष्ठी {आर्थिक विकास संस्थान (दिल्ली संस्थान की समाजशास्त्र इकाई) द्वारा जुलाई 1998 को आयोजित संगाेष्ठी} में सुझाव दिया गया था कि राज्य-स्तर से परे कोई समेकन/एकत्रीकरण न किया जाए। यह स्थानीय संस्थान के रूप में जाति की वास्तविकताओं को भी बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करेगा। क्योंकि, सभी जातियों का 86 प्रतिशत एकल राज्यों तक सीमित था।
- जाति संबंधित विश्वसनीय डाटा की कमी
एक विशेषज्ञ ने कहा कि किस जाति को आरक्षण में तरजीह दी जाए, इससे संबंधित विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ समुदायों को आरक्षण की अनुचित मांग करने के लिए प्रेरित करता है। ओबीसी एक विषम और आंतरिक तौर पर व्यापक रूप से विभेदित श्रेणी है, जिसकी स्थितियों और समुदायवार संख्यात्मक स्थिति का आधिकारिक तौर पर सर्वेक्षण नहीं किया गया है। जबकि, दलितों और जनजातियों का किया गया है। इसलिए, एनसीबीसी ओबीसी केंद्रित डाटा के लिए मंत्रालयों और सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना-2011 (एसईसीसी-2011) से जुड़े आंकड़ों के लिए अनुरोध कर रही है।
- आरक्षण की अधिकतम सीमा
देश की कुल आबादी में ओबीसी (52 प्रतिशत) के अनुमानित हिस्से को देखते हुए और सरकारी भर्ती में योग्यता और आरक्षण की चिंताओं के बीच संतुलन बनाने की जरूरत के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तय की है। इसलिए, प्रत्येक समूह के भीतर और ओबीसी के भीतर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का मुद्दा चुनौतीपूर्ण है और कोई भी समाधान, जो किसी एक समुदाय को लाभ पहुंचाता है; वास्तव में किसी दूसरे के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। इसलिए :
- वैज्ञानिक तरीके से ओबीसी में ऐसे वर्गों की पहचान करना, जिन्हें आरक्षण की आवश्यकता अधिक है। क्याेंकि, आरक्षण के कोटे में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि एक तंत्र, मानदंड के साथ-साथ पैरामीटर तय किए जाएं। साथ ही यह भी जरूरी है कि सामाजिक बहिष्कार की प्रक्रिया (भौतिक स्तर पर पिछड़ेपन से परे, संस्थाओं और प्रक्रियाओं को शामिल करने) को आगे बढ़ाया जाए; ताकि यह पता चल सके कि ओबीसी में शामिल विभिन्न जातियों के बीच आरक्षण की असमानता किस हद तक है।
- अंतर समूहों व अंतर समूहों के स्तरों पर सामाजिक न्याय का लाभ अधिक-से-अधिक हो। इसके लिए कुछ ओबीसी जातियों का समावेशन ओबीसी की अगड़ी जातियों के आंशिक/संपूर्ण बहिष्करण के जरिए किया जा सकता है।
- ओबीसी वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय का लाभ अधिक-से-अधिक मिल सके। इस क्रम में कोटा के भीतर कोटा का इस्तेमाल करते हुए परेटो दक्षता सिद्धांत के मुताबिक, संसाधनों पर आर्थिक आवंटन किया जाना काफी उपयोगी साबित होगा। बिना दो कैटेगरी को मिलने वाले लाभ में कमी किए यदि किसी एक कैटेगरी को मिलने वाले सामाजिक न्याय का लाभ दिला पाना असंभव हो, तो ओबीसी कोटे के तीन चिह्नित वर्गों में बंटवारे को परेटो दक्षता सिद्धांत के अनुरूप माना जा सकता है।
- चूंकि, 86 प्रतिशत ओबीसी अत्यधिक स्थानीयकृत हैं। इसलिए उन वर्गों ने, जिनकी उपस्थिति अखिल भारतीय स्तर पर है और जिन्होंने देश की संस्कृति और विरासत में योगदान दिया है और जिनकी एक अलग सांस्कृतिक पहचान (जैसे विश्वकर्मा- कारीगर -समुदाय) है। उन्हें एमबीसी (ग्रुप-बी) में मान्यता देने और समावेशित किए जाने की आवश्यकता है।
- एलआर नायक (सदस्य, मंडल आयोग) की प्रस्तावना के हिसाब से जो दमित पिछड़ा वर्गों को 15 प्रतिशत उप-कोटा आवंटित करने के लिए है, वह एमबीसी (ग्रुप-बी) को यह उप-कोटा आवंटित किया जा सकता है। शेष को ईबीसी (ग्रुप-ए) और पिछड़ा वर्ग (ग्रुप-सी) काे क्रमश: सात प्रतिशत और पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है।
वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना के संबंध में बीते 31 अगस्त 2018 को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त की बैठक में जनगणना के हिस्से के रूप में विस्तृत ओबीसी डाटा एकत्र करने का निर्णय लिया गया। हमारे पास एकमात्र व्यापक डाटा, जो कि ओबीसी से संबंधित हैं; आठ दशक पुराना है। यह 1931 की जनगणना से लिया गया हैं।
सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना 2011 में जाति जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए जाने को लेकर आलोचनाओं के मद्देनजर पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाने के संबंध में निर्णय लिया गया। फरवरी 2021 में होने वाली जनगणना के संबंध में कहा जा रहा है कि 2020 में 25 लाख जनगणनाकर्मी पूरे देश में ‘हेड काउंटिंग’ के जरिये आंकड़े एकत्रित करेंगे और तब अंतिम सूचनाएं सार्वजनिक की जाएंगी। यह उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें तीन साल का समय लगेगा। जाहिर तौर पर यह किसी भी तरीके से न तो रोहिणी आयोग की अनुशंसाआें (30 नवंबर 2018 तक रिपोर्ट आने की उम्मीद) के क्रियान्वयन में सहायक साबित होगा और न ही पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की कोई मदद करेगा, जिसे आरक्षण और आरक्षण के परे शिकायतों के निवारण के लिए सिविल कोर्ट जैसे अधिकारों के प्रावधान किए गए हैं।
अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं, उनसे तो यही लगता है कि यह सब 2019 में होने वाले चुनाव में ओबीसी के वोटों के लिए मीडिया के सहयोग से छद्म वादे किए जा रहे हैं। इसकी वजह यह कि जी. रोहिणी कमीशन ने अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपी है और न ही पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग (जिसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है) का गठन किया गया है।
हालांकि, रोहिणी अयोग की अवधि 30 नवंबर 2018 तक बढ़ा दी गई है। आयोग के मुताबिक, सर्वेक्षण, अध्ययन और दौरे आदि के माध्यम से ओबीसी संगठनों, संघ व राज्यों, शैक्षणिक संस्थानों और संबंधित व्यक्तियों से डाटा व सूचनाओं के संग्रह का कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन, क्रॉस-चेकिंग तथा रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसे और अधिक समय चाहिए। लेकिन, ऊपर वर्णित चुनौतियों को देखते हुए किसी को भी आश्चर्य हो सकता है कि कैसे यह आयोग न्यायसंगत पुनर्वितरण के उद्देश्य के लिए सौंपे गए जटिल कार्य को राष्ट्रव्यापी परामर्श और कई मुद्दों के विस्तृत अध्ययन के बगैर पूरा कर सकता है।
(अनुवाद : अभय कुमार, कॉपी संपादन : प्रेम/सिद्धार्थ/एफपी डेस्क)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। हमारी किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति, सामाज व राजनीति की व्यापक समस्याओं के सूक्ष्म पहलुओं को गहराई से उजागर करती हैं। पुस्तक-सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें







